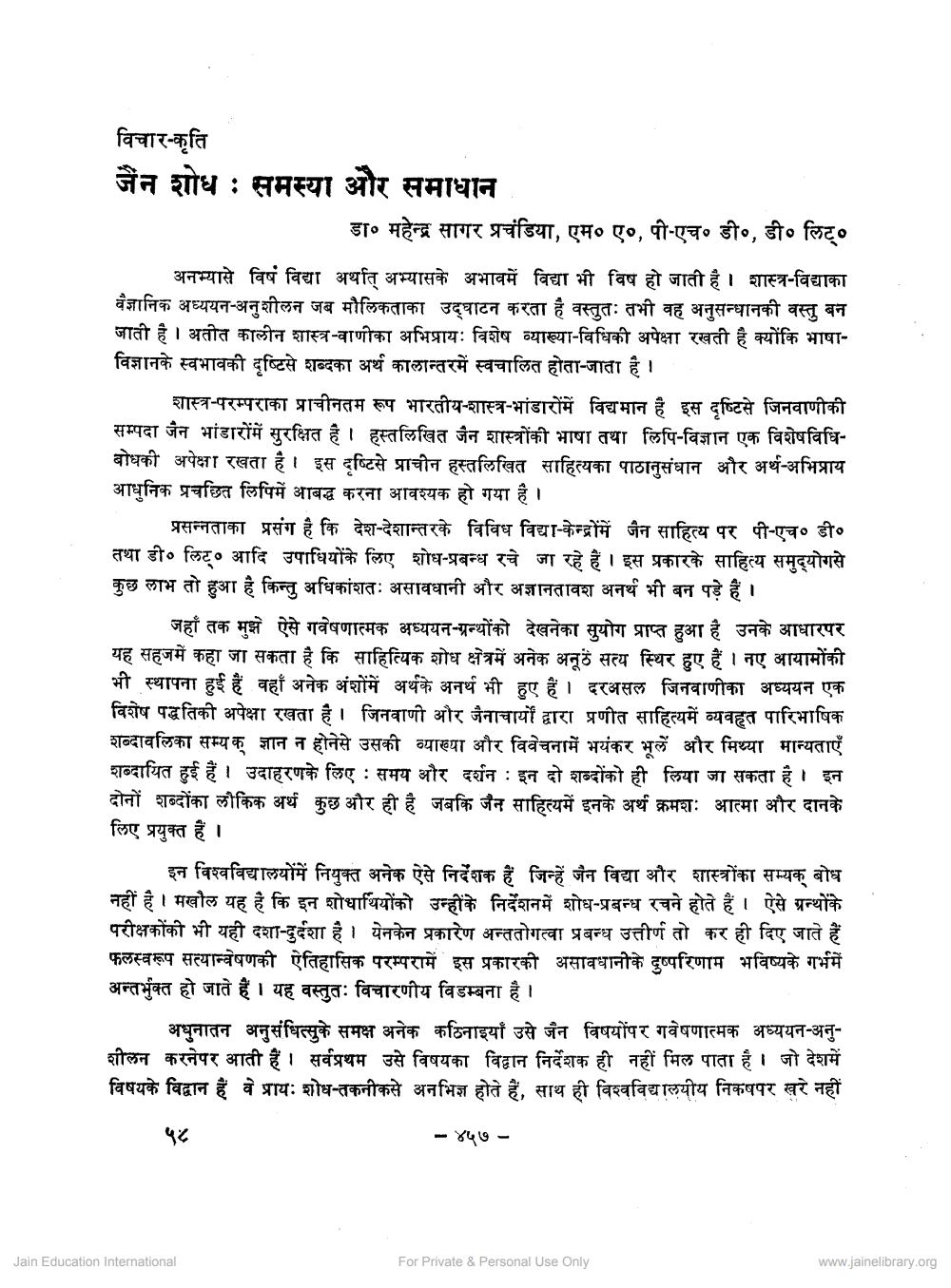Book Title: Jain shodh Samasya aur Samadhan Author(s): Mahendrasagar Prachandiya Publisher: Z_Kailashchandra_Shastri_Abhinandan_Granth_012048.pdf View full book textPage 1
________________ विचार-कृति जैन शोध : समस्या और समाधान डा. महेन्द्र सागर प्रचंडिया, एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट० अनभ्यासे विषं विद्या अर्थात अभ्यासके अभावमें विद्या भी विष हो जाती है। शास्त्र-विद्याका वैज्ञानिक अध्ययन-अनुशीलन जब मौलिकताका उदघाटन करता है वस्तुतः तभी वह अनुसन्धानकी वस्तु बन जाती है। अतीत कालीन शास्त्र-वाणीका अभिप्रायः विशेष व्याख्या-विधिकी अपेक्षा रखती है क्योंकि भाषाविज्ञानके स्वभावकी दृष्टिसे शब्दका अर्थ कालान्तरमें स्वचालित होता-जाता है । शास्त्र-परम्पराका प्राचीनतम रूप भारतीय-शास्त्र-भांडारोंमें विद्यमान है इस दृष्टिसे जिनवाणीकी सम्पदा जैन भांडारोंमें सुरक्षित है। हस्तलिखित जैन शास्त्रोंकी भाषा तथा लिपि-विज्ञान एक विशेषविधिबोधकी अपेक्षा रखता है। इस दष्टिसे प्राचीन हस्तलिखित साहित्यका पाठानुसंधान और अर्थ-अभिप्राय आधनिक प्रचछित लिपिमें आबद्ध करना आवश्यक हो गया है। प्रसन्नताका प्रसंग है कि देश-देशान्तरके विविध विद्या-केन्द्रोंमें जैन साहित्य पर पी-एच० डी० तथा डी० लिट् आदि उपाधियोंके लिए शोध-प्रबन्ध रचे जा रहे हैं । इस प्रकारके साहित्य समुद्योगसे कुछ लाभ तो हुआ है किन्तु अधिकांशतः असावधानी और अज्ञानतावश अनर्थ भी बन पड़े हैं । जहाँ तक मुझे ऐसे गवेषणात्मक अध्ययन-ग्रन्थोंको देखनेका सुयोग प्राप्त हुआ है उनके आधारपर यह सहजमें कहा जा सकता है कि साहित्यिक शोध क्षेत्रमें अनेक अनूठे सत्य स्थिर हुए हैं । नए आयामोंकी भी स्थापना हुई है वहाँ अनेक अंशोंमें अर्थके अनर्थ भी हुए हैं। दरअसल जिनवाणीका अध्ययन एक विशेष पद्धतिकी अपेक्षा रखता है। जिनवाणी और जैनाचार्यों द्वारा प्रणीत साहित्यमें व्यवहृत पारिभाषिक शब्दावलिका सम्यक ज्ञान न होनेसे उसकी व्याख्या और विवेचनामें भयंकर भूलें और मिथ्या मान्यताएँ शब्दायित हुई हैं। उदाहरणके लिए : समय और दर्शन : इन दो शब्दोंको ही लिया जा सकता है। इन दोनों शब्दोंका लौकिक अर्थ कुछ और ही है जबकि जैन साहित्यमें इनके अर्थ क्रमशः आत्मा और दानके लिए प्रयुक्त हैं। इन विश्वविद्यालयोंमें नियुक्त अनेक ऐसे निर्देशक हैं जिन्हें जैन विद्या और शास्त्रोंका सम्यक् बोध नहीं है । मखौल यह है कि इन शोधार्थियोंको उन्हींके निर्देशनमें शोध-प्रबन्ध रचने होते हैं। ऐसे ग्रन्थोंके परीक्षकोंकी भी यही दशा-दुर्दशा है। येनकेन प्रकारेण अन्ततोगत्वा प्रबन्ध उत्तीर्ण तो कर ही दिए जाते हैं फलस्वरूप सत्यान्वेषणकी ऐतिहासिक परम्परामें इस प्रकारकी असावधानीके दुष्परिणाम भविष्यके गर्भमें अन्तर्भुक्त हो जाते हैं । यह वस्तुतः विचारणीय विडम्बना है। अधुनातन अनुसंधित्सुके समक्ष अनेक कठिनाइयाँ उसे जैन विषयोंपर गवेषणात्मक अध्ययन-अनुशीलन करनेपर आती हैं। सर्वप्रथम उसे विषयका विद्वान निर्देशक ही नहीं मिल पाता है । जो देशमें विषयके विद्वान है वे प्रायः शोध-तकनीकसे अनभिज्ञ होते हैं, साथ ही विश्वविद्यालयीय निकषपर खरे नहीं ५८ Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2