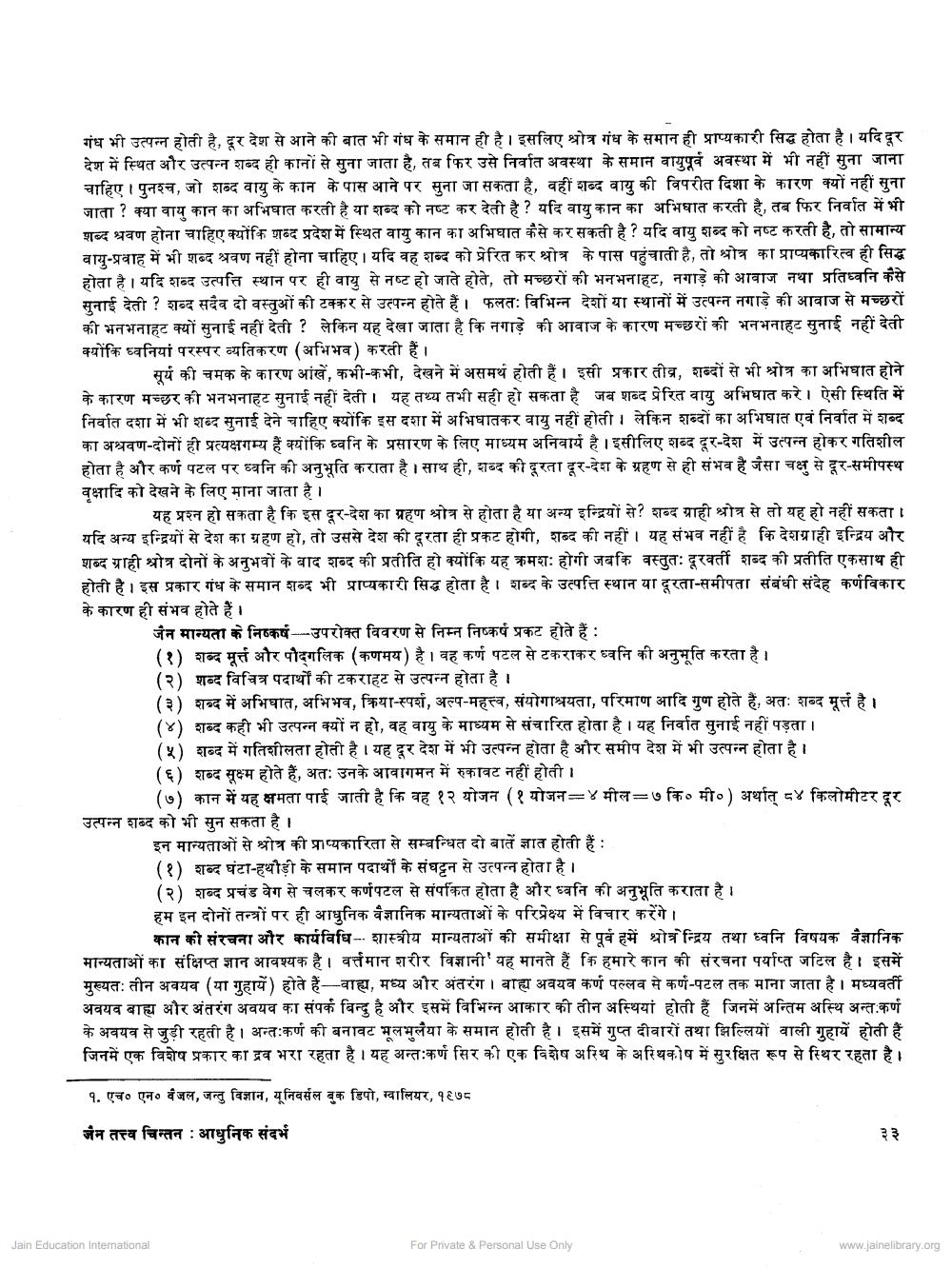Book Title: Jain Shastriya Parampara evam Adhunik Vaigyanik Author(s): Nandlal Jain Publisher: Z_Deshbhushanji_Maharaj_Abhinandan_Granth_012045.pdf View full book textPage 2
________________ गंध भी उत्पन्न होती है, दूर देश से आने की बात भी गंध के समान ही है। इसलिए श्रोत्र गंध के समान ही प्राप्यकारी सिद्ध होता है। यदि दूर देश में स्थित और उत्पन्न शब्द ही कानों से सुना जाता है, तब फिर उसे निर्वात अवस्था के समान वायुपूर्व अवस्था में भी नहीं सुना जाना चाहिए। पुनश्च, जो शब्द वायु के कान के पास आने पर सुना जा सकता है, वहीं शब्द वायु की विपरीत दिशा के कारण क्यों नहीं सुना जाता ? क्या वायु कान का अभिघात करती है या शब्द को नष्ट कर देती है ? यदि वायु कान का अभिघात करती है, तब फिर निर्वात में भी शब्द श्रवण होना चाहिए क्योंकि शब्द प्रदेश में स्थित वायु कान का अभिघात कैसे कर सकती है ? यदि वायु शब्द को नष्ट करती है, तो सामान्य वायु प्रवाह में भी शब्द श्रवण नहीं होना चाहिए। यदि वह शब्द को प्रेरित कर श्रोत्र के पास पहुंचाती है, तो श्रोत्र का प्राप्यकारित्व ही सिद्ध होता है । यदि शब्द उत्पत्ति स्थान पर ही वायु से नष्ट हो जाते होते, तो मच्छरों की भनभनाहट, नगाड़े की आवाज नथा प्रतिध्वनि कैसे सुनाई देती ? शब्द सदैव दो वस्तुओं की टक्कर से उत्पन्न होते हैं । फलतः विभिन्न देशों या स्थानों में उत्पन्न नगाड़े की आवाज से मच्छरों की भनभनाहट क्यों सुनाई नहीं देती ? लेकिन यह देखा जाता है कि नगाड़े की आवाज के कारण मच्छरों की भनभनाहट सुनाई नहीं देती क्योंकि ध्वनियां परस्पर व्यतिकरण ( अभिभव) करती हैं। सूर्य की चमक के कारण आंखें, कभी-कभी देखने में असमर्थ होती हैं । इसी प्रकार तीव्र, शब्दों से भी श्रोत्र का अभिघात होने · के कारण मच्छर की भनभनाहट सुनाई नहीं देती । यह तथ्य तभी सही हो सकता है जब शब्द प्रेरित वायु अभिघात करे। ऐसी स्थिति में निर्वात दशा में भी शब्द सुनाई देने चाहिए क्योंकि इस दशा में अभिघातकर वायु नहीं होती। लेकिन शब्दों का अभिघात एवं निर्वात में शब्द का अश्रवण- दोनों ही प्रत्यक्षगम्य हैं क्योंकि ध्वनि के प्रसारण के लिए माध्यम अनिवार्य है। इसीलिए शब्द दूर देश में उत्पन्न होकर गतिशील होता है और कर्ज पटल पर ध्वनि की अनुभूति कराता है। साथ ही शब्द की दूरता दूरदेश के ग्रहण से ही संभव है जैसा चक्षु से दूर समीपस्थ वृक्षादि को देखने के लिए माना जाता है। यह प्रश्न हो सकता है कि इस दूर देश का ग्रहण श्रोत्र से होता है या अन्य इन्द्रियों से ? शब्द ग्राही श्रोत्र से तो यह हो नहीं सकता । यदि अन्य इन्द्रियों से देश का ग्रहण हो, तो उससे देश की दूरता ही प्रकट होगी, शब्द की नहीं। यह संभव नहीं है कि देशग्राही इन्द्रिय और शब्द ग्राही धोज दोनों के अनुभवों के बाद शब्द की प्रतीति हो क्योंकि यह क्रमशः होगी जबकि वस्तुतः दूरवर्ती शब्द की प्रतीति एकसाथ ही होती है। इस प्रकार गंध के समान शब्द भी प्राप्यकारी सिद्ध होता है। शब्द के उत्पत्ति स्थान या दूरता-समीपता संबंधी संदेह कर्णविकार के कारण ही संभव होते हैं। जैन मान्यता के निष्कर्ष उपरोक्त विवरण से निम्न निष्कर्ष प्रकट होते हैं : (१) शब्द मूर्त्त और पौद्गलिक ( कणमय) है। वह कर्ण पटल से टकराकर ध्वनि की अनुभूति करता है । (२) शब्द विचित्र पदार्थों की टकराहट से उत्पन्न होता है । (३) शब्द में अभिषात, अभिभव किया-स्पर्श, अल्प- महत्व, संयोगाश्रयता, परिमाण आदि गुण होते हैं, अतः शब्द मूर्त है। (४) शब्द कही भी उत्पन्न क्यों न हो, वह वायु के माध्यम से संचारित होता है। यह निर्वात सुनाई नहीं पड़ता। (५) शब्द में गतिशीलता होती है। यह दूर देश में भी उत्पन्न होता है और समीप देश में भी उत्पन्न होता है । (६) शब्द सूक्ष्म होते हैं, अतः उनके आवागमन में रुकावट नहीं होती । (७) कान में यह क्षमता पाई जाती है कि वह १२ योजन (१ योजन = ४ मील = ७ कि० मी०) अर्थात् ६४ किलोमीटर दूर उत्पन्न शब्द को भी सुन सकता है। इन मान्यताओं से श्रोष की प्राप्यकारिता से सम्बन्धित दो बातें ज्ञात होती है (१) शब्द टाही के समान पदार्थों के संघट्टन से उत्पन्न होता है। (२) शब्द प्रचंड वेग से चलकर कर्णपटल से संपर्कत होता है और ध्वनि की अनुभूति कराता है । हम इन दोनों तन्त्रों पर ही आधुनिक वैज्ञानिक मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में विचार करेंगे। कान की संरचना और कार्यविधि - शास्त्रीय मान्यताओं की समीक्षा से पूर्व हमें श्रोत्रन्द्रिय तथा ध्वनि विषयक वैज्ञानिक मान्यताओं का संक्षिप्त ज्ञान आवश्यक है। वर्तमान शरीर विज्ञानी' यह मानते हैं कि हमारे कान की संरचना पर्याप्त जटिल है। इसमें मुख्यत: तीन अवयव ( या गुहायें) होते हैं—बाह्य, मध्य और अंतरंग । बाह्य अवयव कर्ण पल्लव से कर्ण-पटल तक माना जाता है। मध्यवर्ती अवयव बाह्य और अंतरंग अवयव का संपर्क बिन्दु है और इसमें विभिन्न आकार की तीन अस्थियां होती हैं जिनमें अन्तिम अस्थि अन्तः कर्ण के अवयव से जुड़ी रहती है। अन्तः कर्ण की बनावट मूलभुलैया के समान होती है। इसमें गुप्त दीवारों तथा झिल्लियों वाली गुहायें होती है जिनमें एक विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है। यह अन्त:कर्ण सिर की एक विशेष अस्थि के अस्थिकोष में सुरक्षित रूप से स्थिर रहता है। १. एच० एन० जल, जन्तु विज्ञान, यूनिवर्सल बुक डिपो, ग्वालियर, १६७८ जैन तत्त्व चिन्तन : आधुनिक संदर्भ Jain Education International For Private & Personal Use Only ३३ www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4