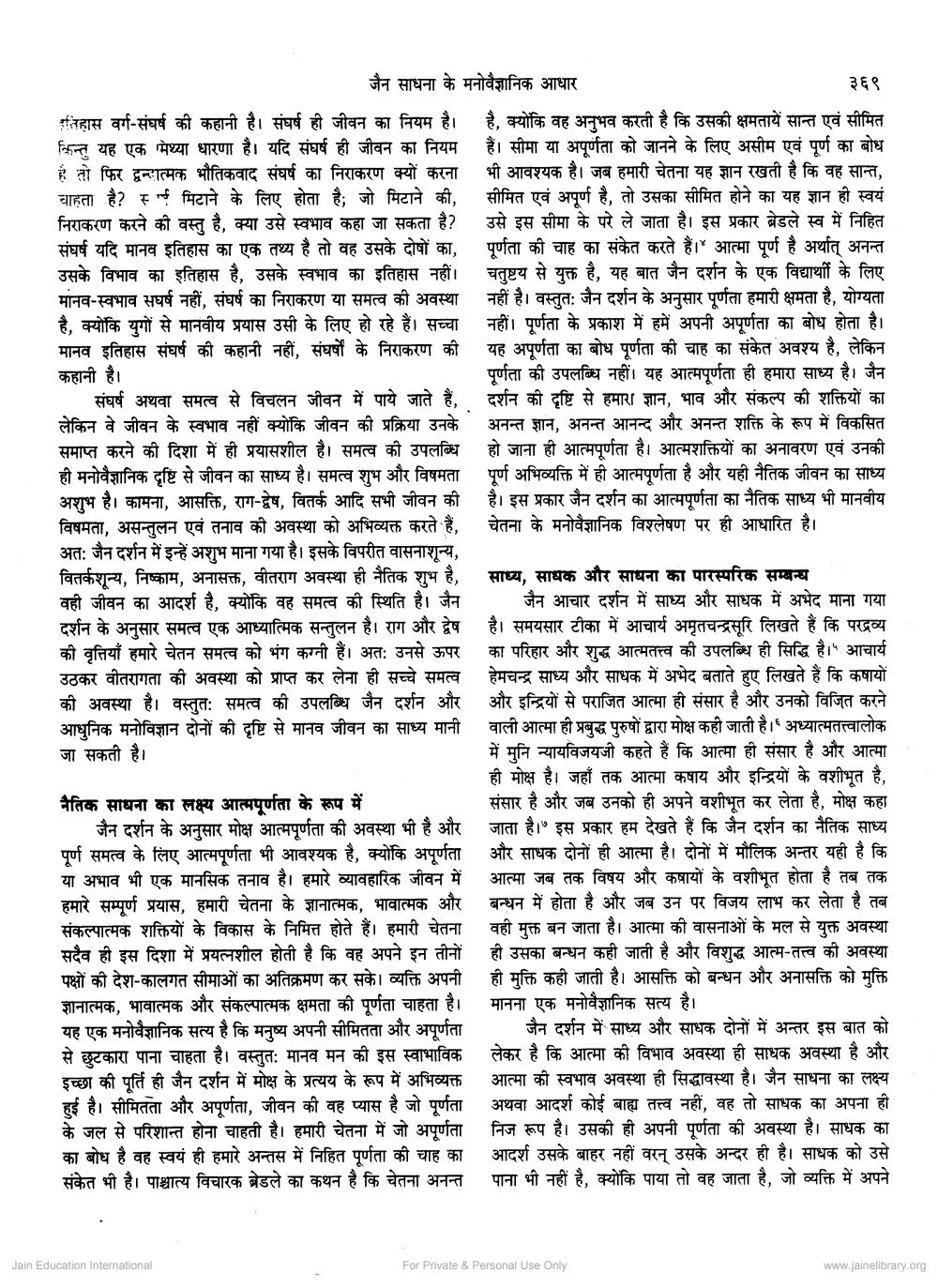Book Title: Jain Sadhna ke Manovaigyanik Adhar Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Z_Shwetambar_Sthanakvasi_Jain_Sabha_Hirak_Jayanti_Granth_012052.pdf View full book textPage 2
________________ जैन साधना के मनोवैज्ञानिक आधार ३६९ इतिहास वर्ग-संघर्ष की कहानी है। संघर्ष ही जीवन का नियम है। है, क्योंकि वह अनुभव करती है कि उसकी क्षमतायें सान्त एवं सीमित किन्तु यह एक मेथ्या धारणा है। यदि संघर्ष ही जीवन का नियम हैं। सीमा या अपूर्णता को जानने के लिए असीम एवं पूर्ण का बोध है तो फिर द्वन्दात्मक भौतिकवाद संघर्ष का निराकरण क्यों करना भी आवश्यक है। जब हमारी चेतना यह ज्ञान रखती है कि वह सान्त, चाहता है? सई मिटाने के लिए होता है; जो मिटाने की, सीमित एवं अपूर्ण है, तो उसका सीमित होने का यह ज्ञान ही स्वयं निराकरण करने की वस्तु है, क्या उसे स्वभाव कहा जा सकता है? उसे इस सीमा के परे ले जाता है। इस प्रकार बेडले स्व में निहित संघर्ष यदि मानव इतिहास का एक तथ्य है तो वह उसके दोषों का, पूर्णता की चाह का संकेत करते हैं।' आत्मा पूर्ण है अर्थात् अनन्त उसके विभाव का इतिहास है, उसके स्वभाव का इतिहास नहीं। चतुष्टय से युक्त है, यह बात जैन दर्शन के एक विद्यार्थी के लिए मानव-स्वभाव सघर्ष नहीं, संघर्ष का निराकरण या समत्व की अवस्था नहीं है। वस्तुत: जैन दर्शन के अनुसार पूर्णता हमारी क्षमता है, योग्यता है, क्योकि युगों से मानवीय प्रयास उसी के लिए हो रहे हैं। सच्चा नहीं। पूर्णता के प्रकाश में हमें अपनी अपूर्णता का बोध होता है। मानव इतिहास संघर्ष की कहानी नहीं, संघर्षों के निराकरण की यह अपूर्णता का बोध पूर्णता की चाह का संकेत अवश्य है, लेकिन कहानी है। पूर्णता की उपलब्धि नहीं। यह आत्मपूर्णता ही हमारा साध्य है। जैन संघर्ष अथवा समत्व से विचलन जीवन में पाये जाते हैं, दर्शन की दृष्टि से हमारा ज्ञान, भाव और संकल्प की शक्तियों का लेकिन वे जीवन के स्वभाव नहीं क्योंकि जीवन की प्रक्रिया उनके अनन्त ज्ञान, अनन्त आनन्द और अनन्त शक्ति के रूप में विकसित समाप्त करने की दिशा में ही प्रयासशील है। समत्व की उपलब्धि हो जाना ही आत्मपूर्णता है। आत्मशक्तियों का अनावरण एवं उनकी ही मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जीवन का साध्य है। समत्व शुभ और विषमता पूर्ण अभिव्यक्ति में ही आत्मपूर्णता है और यही नैतिक जीवन का साध्य अशुभ है। कामना, आसक्ति, राग-द्वेष, वितर्क आदि सभी जीवन की है। इस प्रकार जैन दर्शन का आत्मपूर्णता का नैतिक साध्य भी मानवीय विषमता, असन्तुलन एवं तनाव की अवस्था को अभिव्यक्त करते हैं, चेतना के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर ही आधारित है। अत: जैन दर्शन में इन्हें अशुभ माना गया है। इसके विपरीत वासनाशून्य, वितर्कशून्य, निष्काम, अनासक्त, वीतराग अवस्था ही नैतिक शुभ है, साध्य, साधक और साधना का पारस्परिक सम्बन्ध वही जीवन का आदर्श है, क्योंकि वह समत्व की स्थिति है। जैन जैन आचार दर्शन में साध्य और साधक में अभेद माना गया दर्शन के अनुसार समत्व एक आध्यात्मिक सन्तुलन है। राग और द्वेष है। समयसार टीका में आचार्य अमृतचन्द्रसूरि लिखते हैं कि परद्रव्य की वृत्तियाँ हमारे चेतन समत्व को भंग करती हैं। अत: उनसे ऊपर का परिहार और शुद्ध आत्मतत्त्व की उपलब्धि ही सिद्धि है।' आचार्य उठकर वीतरागता की अवस्था को प्राप्त कर लेना ही सच्चे समत्व हेमचन्द्र साध्य और साधक में अभेद बताते हुए लिखते हैं कि कषायों की अवस्था है। वस्तुत: समत्व की उपलब्धि जैन दर्शन और और इन्द्रियों से पराजित आत्मा ही संसार है और उनको विजित करने आधुनिक मनोविज्ञान दोनों की दृष्टि से मानव जीवन का साध्य मानी वाली आत्मा ही प्रबुद्ध पुरुषों द्वारा मोक्ष कही जाती है। अध्यात्मतत्त्वालोक जा सकती है। में मुनि न्यायविजयजी कहते हैं कि आत्मा ही संसार है और आत्मा ही मोक्ष है। जहाँ तक आत्मा कषाय और इन्द्रियों के वशीभूत है, नैतिक साधना का लक्ष्य आत्मपूर्णता के रूप में संसार है और जब उनको ही अपने वशीभूत कर लेता है, मोक्ष कहा जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष आत्मपूर्णता की अवस्था भी है और जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन दर्शन का नैतिक साध्य पूर्ण समत्व के लिए आत्मपूर्णता भी आवश्यक है, क्योंकि अपूर्णता और साधक दोनों ही आत्मा है। दोनों में मौलिक अन्तर यही है कि या अभाव भी एक मानसिक तनाव है। हमारे व्यावहारिक जीवन में आत्मा जब तक विषय और कषायों के वशीभूत होता है तब तक हमारे सम्पूर्ण प्रयास, हमारी चेतना के ज्ञानात्मक, भावात्मक और बन्धन में होता है और जब उन पर विजय लाभ कर लेता है तब संकल्पात्मक शक्तियों के विकास के निमित्त होते हैं। हमारी चेतना वही मुक्त बन जाता है। आत्मा की वासनाओं के मल से युक्त अवस्था सदैव ही इस दिशा में प्रयत्नशील होती है कि वह अपने इन तीनों ही उसका बन्धन कही जाती है और विशुद्ध आत्म-तत्त्व की अवस्था पक्षों की देश-कालगत सीमाओं का अतिक्रमण कर सके। व्यक्ति अपनी ही मुक्ति कही जाती है। आसक्ति को बन्धन और अनासक्ति को मुक्ति ज्ञानात्मक, भावात्मक और संकल्पात्मक क्षमता की पूर्णता चाहता है। मानना एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि मनुष्य अपनी सीमितता और अपूर्णता जैन दर्शन में साध्य और साधक दोनों में अन्तर इस बात को से छुटकारा पाना चाहता है। वस्तुत: मानव मन की इस स्वाभाविक लेकर है कि आत्मा की विभाव अवस्था ही साधक अवस्था है और इच्छा की पूर्ति ही जैन दर्शन में मोक्ष के प्रत्यय के रूप में अभिव्यक्त आत्मा की स्वभाव अवस्था ही सिद्धावस्था है। जैन साधना का लक्ष्य हुई है। सीमितता और अपूर्णता, जीवन की वह प्यास है जो पूर्णता अथवा आदर्श कोई बाह्य तत्त्व नहीं, वह तो साधक का अपना ही के जल से परिशान्त होना चाहती है। हमारी चेतना में जो अपूर्णता निज रूप है। उसकी ही अपनी पूर्णता की अवस्था है। साधक का का बोध है वह स्वयं ही हमारे अन्तस में निहित पूर्णता की चाह का आदर्श उसके बाहर नहीं वरन् उसके अन्दर ही है। साधक को उसे संकेत भी है। पाश्चात्य विचारक ब्रेडले का कथन है कि चेतना अनन्त पाना भी नहीं है, क्योंकि पाया तो वह जाता है, जो व्यक्ति में अपने Jain Education Intemational For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9