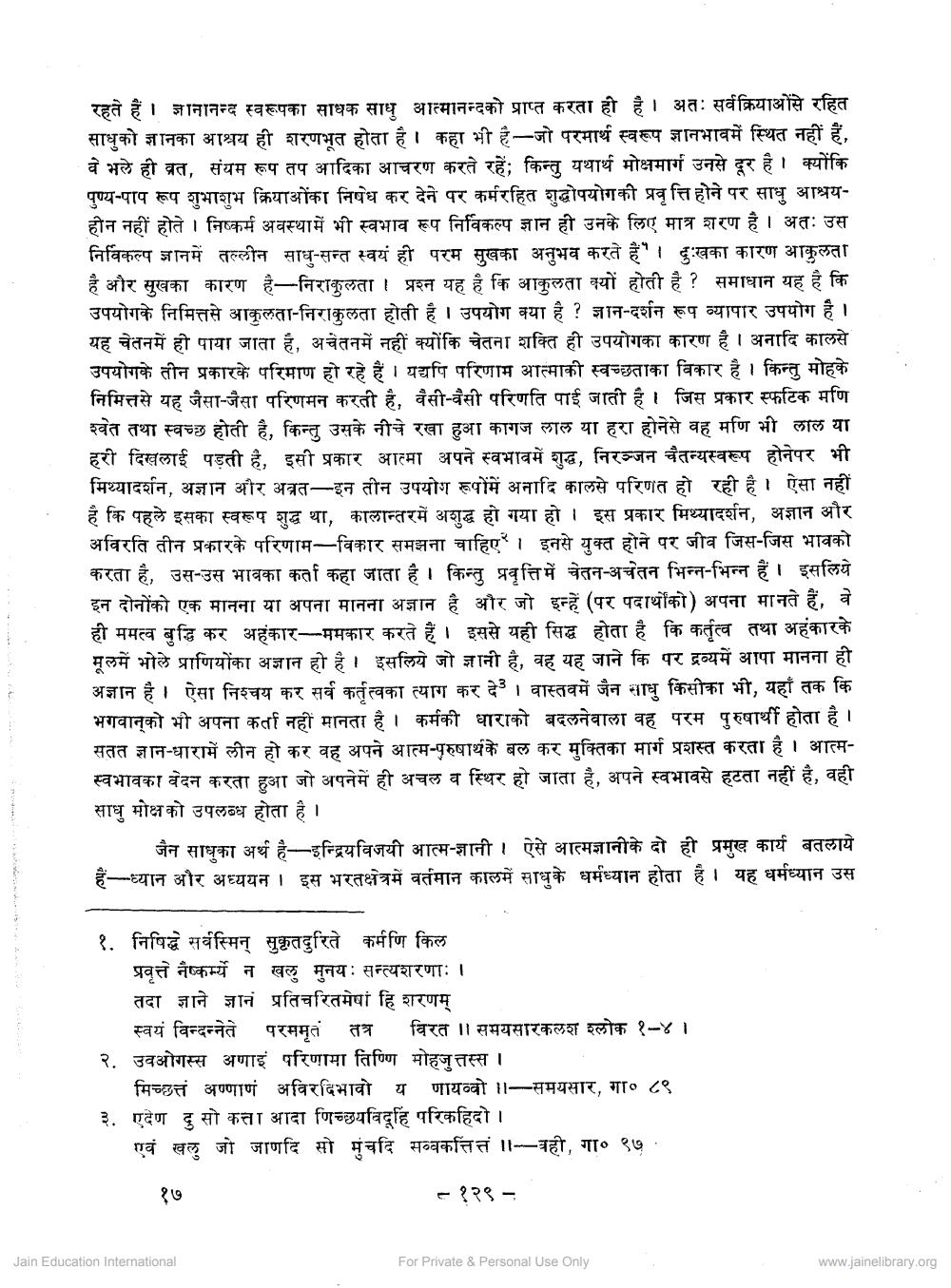Book Title: Jain Parampara me Sant aur Unki Sadhna Paddhati Author(s): Devendra Kumar Jain Publisher: Z_Kailashchandra_Shastri_Abhinandan_Granth_012048.pdf View full book textPage 7
________________ रहते हैं। ज्ञानानन्द स्वरूपका साधक साधु आत्मानन्दको प्राप्त करता ही है। अतः सर्वक्रियाओंसे रहित साधुको ज्ञानका आश्रय ही शरणभूत होता है। कहा भी है-जो परमार्थ स्वरूप ज्ञानभावमें स्थित नहीं हैं, वे भले ही व्रत, संयम रूप तप आदिका आचरण करते रहें। किन्तु यथार्थ मोक्षमार्ग उनसे दूर है। क्योंकि पुण्य-पाप रूप शुभाशुभ क्रियाओंका निषेध कर देने पर कर्मरहित शुद्धोपयोगकी प्रवृत्ति होने पर साधु आश्रयहीन नहीं होते । निष्कर्म अवस्था में भी स्वभाव रूप निर्विकल्प ज्ञान ही उनके लिए मात्र शरण है । अतः उस निर्विकल्प ज्ञानमें तल्लीन साध-सन्त स्वयं ही परम सुखका अनुभव करते हैं। दुःखका कारण आकुलता है और सुखका कारण है-निराकूलता। प्रश्न यह है कि आकूलता क्यों होती है ? समाधान यह है कि उपयोगके निमित्तसे आकुलता-निराकुलता होती है । उपयोग क्या है ? ज्ञान-दर्शन रूप व्यापार उपयोग है। यह चेतनमें हो पाया जाता है, अचेतनमें नहीं क्योंकि चेतना शक्ति ही उपयोगका कारण है । अनादि उपयोगके तीन प्रकारके परिमाण हो रहे हैं । यद्यपि परिणाम आत्माकी स्वच्छताका विकार है। किन्तु मोहके निमित्तसे यह जैसा-जैसा परिणमन करती है, वैसी-वैसी परिणति पाई जाती है। जिस प्रकार स्फटिक मणि श्वेत तथा स्वच्छ होती है, किन्तु उसके नीचे रखा हुआ कागज लाल या हरा होनेसे वह मणि भी लाल या हरी दिखलाई पड़ती है, इसी प्रकार आत्मा अपने स्वभावमें शुद्ध, निरञ्जन चैतन्यस्वरूप होनेपर भी मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अव्रत-इन तीन उपयोग रूपोंमें अनादि कालसे परिणत हो रही है। ऐसा नहीं है कि पहले इसका स्वरूप शुद्ध था, कालान्तरमें अशुद्ध हो गया हो। इस प्रकार मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति तीन प्रकारके परिणाम-विकार समझना चाहिए। इनसे युक्त होने पर जीव जिस-जिस भावको करता है, उस-उस भावका कर्ता कहा जाता है। किन्तु प्रवृत्ति में चेतन-अचेतन भिन्न-भिन्न हैं। इसलिये इन दोनोंको एक मानना या अपना मानना अज्ञान है और जो इन्हें (पर पदार्थोंको) अपना मानते हैं, वे ही ममत्व बुद्धि कर अहंकार--ममकार करते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि कर्तृत्व तथा अहंकारके मूलमें भोले प्राणियोंका अज्ञान हो है। इसलिये जो ज्ञानी है, वह यह जाने कि पर द्रव्यमें आपा मानना ही अज्ञान है। ऐसा निश्चय कर सर्व कर्तत्वका त्याग कर दे । वास्तवमें जैन साधु किसीका भी, यहाँ तक कि भगवान्को भी अपना कर्ता नहीं मानता है। कर्मकी धाराको बदलनेवाला वह परम पुरुषार्थी होता है । सतत ज्ञान-धारामें लीन हो कर वह अपने आत्म-पुरुषार्थ के बल कर मुक्तिका मार्ग प्रशस्त करता है । आत्मस्वभावका वेदन करता हआ जो अपने में ही अचल व स्थिर हो जाता है, अपने स्वभावसे हटता नहीं है, वही साधु मोक्षको उपलब्ध होता है । जैन साधुका अर्थ है-इन्द्रियविजयी आत्म-ज्ञानी। ऐसे आत्मज्ञानीके दो ही प्रमुख कार्य बतलाये हैं-ध्यान और अध्ययन । इस भरतक्षेत्रमें वर्तमान कालमें साधुके धर्मध्यान होता है। यह धर्मध्यान उस १. निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृतदुरिते कर्मणि किल प्रवृत्ते नैष्कर्म्यं न खलु मुनयः सन्त्यशरणाः । तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणम् स्वयं विन्दन्नेते परममतं तत्र विरत ।। समयसारकलश श्लोक १-४ । २. उवओगस्स अणाइं परिणामा तिण्णि मोहजत्तस्स । मिच्छत्तं अण्णाणं अविरदिभावो य णायव्वो ॥-समयसार, गा० ८९ ३. एदेण दु सो कत्ता आदा णिच्छयविहि परिकहिदो। एवं खलु जो जाणदि सो मुंचदि सब्बकत्तित्तं ।।-वही, गा० ९७ . - १२९ - Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12