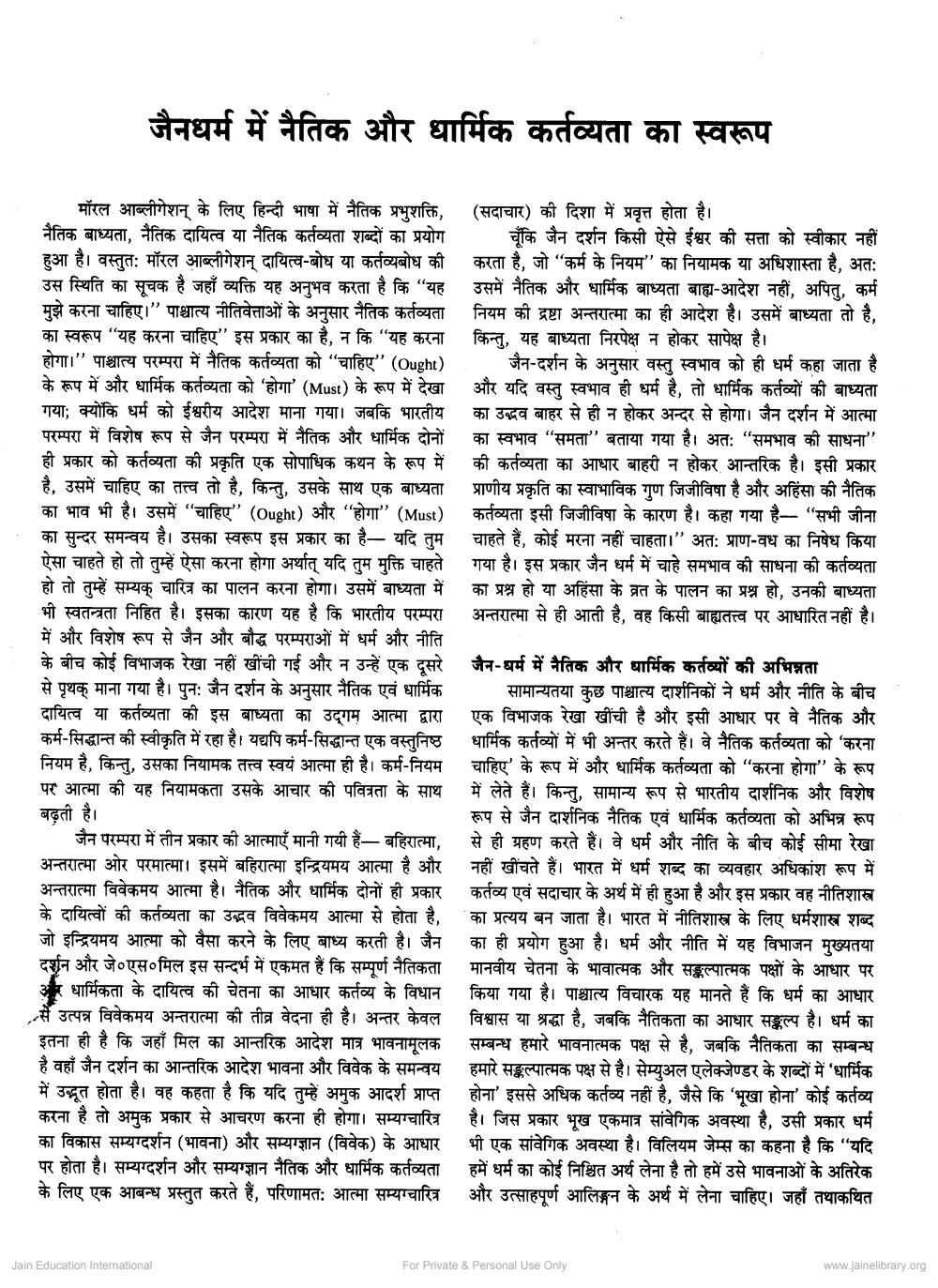Book Title: Jain Dharm me Naitik aur Dharmik Kartavyata ka Swarup Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Z_Shwetambar_Sthanakvasi_Jain_Sabha_Hirak_Jayanti_Granth_012052.pdf View full book textPage 1
________________ जैनधर्म में नैतिक और धार्मिक कर्तव्यता का स्वरूप मॉरल आब्लीगेशन के लिए हिन्दी भाषा में नैतिक प्रभुशक्ति, नैतिक बाध्यता, नैतिक दायित्व या नैतिक कर्तव्यता शब्दों का प्रयोग हुआ है। वस्तुतः मॉरल आब्लीगेशन दायित्व बोध या कर्तव्यबोध की उस स्थिति का सूचक है जहाँ व्यक्ति यह अनुभव करता है कि "यह मुझे करना चाहिए।” पाश्चात्य नीतिवेत्ताओं के अनुसार नैतिक कर्तव्यता का स्वरूप "यह करना चाहिए" इस प्रकार का है, न कि "यह करना होगा।" पाश्चात्य परम्परा में नैतिक कर्तव्यता को "चाहिए" (Ought) के रूप में और धार्मिक कर्तव्यता को 'होगा' (Must) के रूप में देखा गया; क्योंकि धर्म को ईश्वरीय आदेश माना गया जबकि भारतीय परम्परा में विशेष रूप से जैन परम्परा में नैतिक और धार्मिक दोनों ही प्रकार को कर्तव्यता की प्रकृति एक सोपाधिक कथन के रूप में है, उसमें चाहिए का तत्त्व तो है, किन्तु उसके साथ एक बाध्यता का भाव भी है। उसमें "चाहिए" (Ought) और "होगा" (Must) का सुन्दर समन्वय है। उसका स्वरूप इस प्रकार का है— यदि तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हें ऐसा करना होगा अर्थात् यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें सम्यक् चारित्र का पालन करना होगा। उसमें बाध्यता में भी स्वतन्त्रता निहित है। इसका कारण यह है कि भारतीय परम्परा में और विशेष रूप से जैन और बौद्ध परम्पराओं में धर्म और नीति के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं खींची गई और न उन्हें एक दूसरे से पृथक् माना गया है पुनः जैन दर्शन के अनुसार नैतिक एवं धार्मिक दायित्व या कर्तव्यता की इस बाध्यता का उद्गम आत्मा द्वारा कर्म सिद्धान्त की स्वीकृति में रहा है। यद्यपि कर्म सिद्धान्त एक वस्तुनिष्ठ नियम हैं, किन्तु उसका नियामक तत्त्व स्वयं आत्मा ही है। कर्म-नियम पर आत्मा की यह नियामकता उसके आचार की पवित्रता के साथ बढ़ती है। जैन परम्परा में तीन प्रकार की आत्माएँ मानी गयी हैं— बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । इसमें बहिरात्मा इन्द्रियमय आत्मा है और अन्तरात्मा विवेकमय आत्मा है। नैतिक और धार्मिक दोनों ही प्रकार के दायित्वों की कर्तव्यता का उद्भव विवेकमय आत्मा से होता है, जो इन्द्रियमय आत्मा को वैसा करने के लिए बाध्य करती है। जैन दर्शन और जे०एस० मिल इस सन्दर्भ में एकमत हैं कि सम्पूर्ण नैतिकता और धार्मिकता के दायित्व की चेतना का आधार कर्तव्य के विधान उत्पन्न विवेकमय अन्तरात्मा की तीव्र वेदना ही है। अन्तर केवल इतना ही है कि जहाँ मिल का आन्तरिक आदेश मात्र भावनामूलक है वहाँ जैन दर्शन का आन्तरिक आदेश भावना और विवेक के समन्वय में उद्भूत होता है वह कहता है कि यदि तुम्हें अमुक आदर्श प्राप्त करना है तो अमुक प्रकार से आचरण करना ही होगा । सम्यग्चारित्र का विकास सम्यग्दर्शन (भावना) और सम्यग्ज्ञान (विवेक) के आधार पर होता है। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान नैतिक और धार्मिक कर्तव्यता के लिए एक आबन्ध प्रस्तुत करते हैं, परिणामतः आत्मा सम्यग्चारित्र Jain Education International (सदाचार) की दिशा में प्रवृत्त होता है । चूँकि जैन दर्शन किसी ऐसे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, जो "कर्म के नियम" का नियामक या अधिशास्ता है, अतः उसमें नैतिक और धार्मिक बाध्यता बाह्य आदेश नहीं, अपितु, कर्म नियम की द्रष्टा अन्तरात्मा का ही आदेश है। उसमें बाध्यता तो है, किन्तु, यह बाध्यता निरपेक्ष न होकर सापेक्ष है। जैन दर्शन के अनुसार वस्तु स्वभाव को ही धर्म कहा जाता है और यदि वस्तु स्वभाव ही धर्म है, तो धार्मिक कर्तव्यों की बाध्यता का उद्भव बाहर से ही न होकर अन्दर से होगा। जैन दर्शन में आत्मा का स्वभाव "समता' बताया गया है। अतः "समभाव की साधना " की कर्तव्यता का आधार बाहरी न होकर आन्तरिक है। इसी प्रकार प्राणीय प्रकृति का स्वाभाविक गुण जिजीविषा है और अहिंसा की नैतिक कर्तव्यता इसी जिजीविषा के कारण है। कहा गया है- "सभी जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता।" अतः प्राण वध का निषेध किया गया है। इस प्रकार जैन धर्म में चाहे समभाव की साधना की कर्तव्यता का प्रश्न हो या अहिंसा के व्रत के पालन का प्रश्न हो, उनकी बाध्यता अन्तरात्मा से ही आती है, वह किसी बाह्यतत्त्व पर आधारित नहीं है। जैन धर्म में नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों की अभिन्नता सामान्यतया कुछ पाश्चात्य दार्शनिकों ने धर्म और नीति के बीच एक विभाजक रेखा खींची है और इसी आधार पर वे नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों में भी अन्तर करते हैं। वे नैतिक कर्तव्यता को 'करना चाहिए' के रूप में और धार्मिक कर्तव्यता को " करना होगा" के रूप में लेते हैं किन्तु सामान्य रूप से भारतीय दार्शनिक और विशेष रूप से जैन दार्शनिक नैतिक एवं धार्मिक कर्तव्यता को अभिन्न रूप से ही ग्रहण करते हैं। वे धर्म और नीति के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खींचते हैं। भारत में धर्म शब्द का व्यवहार अधिकांश रूप में कर्तव्य एवं सदाचार के अर्थ में ही हुआ है और इस प्रकार वह नीतिशास्त्र का प्रत्यय बन जाता है। भारत में नीतिशास्त्र के लिए धर्मशास्त्र शब्द का ही प्रयोग हुआ है धर्म और नीति में यह विभाजन मुख्यतया मानवीय चेतना के भावात्मक और सङ्कल्पात्मक पक्षों के आधार पर किया गया है। पाश्चात्य विचारक यह मानते हैं कि धर्म का आधार विश्वास या श्रद्धा है, जबकि नैतिकता का आधार सङ्कल्प है। धर्म का सम्बन्ध हमारे भावनात्मक पक्ष से है, जबकि नैतिकता का सम्बन्ध हमारे सङ्कल्पात्मक पक्ष से है। सेम्युअल एलेक्जेण्डर के शब्दों में 'धार्मिक होना' इससे अधिक कर्तव्य नहीं है, जैसे कि 'भूखा होना कोई कर्तव्य है। जिस प्रकार भूख एकमात्र सांवेगिक अवस्था है, उसी प्रकार धर्म भी एक सांवेगिक अवस्था है। विलियम जेम्स का कहना है कि "यदि हमें धर्म का कोई निश्चित अर्थ लेना है तो हमें उसे भावनाओं के अतिरेक और उत्साहपूर्ण आलिङ्गन के अर्थ में लेना चाहिए। जहाँ तथाकथित For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org.Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11