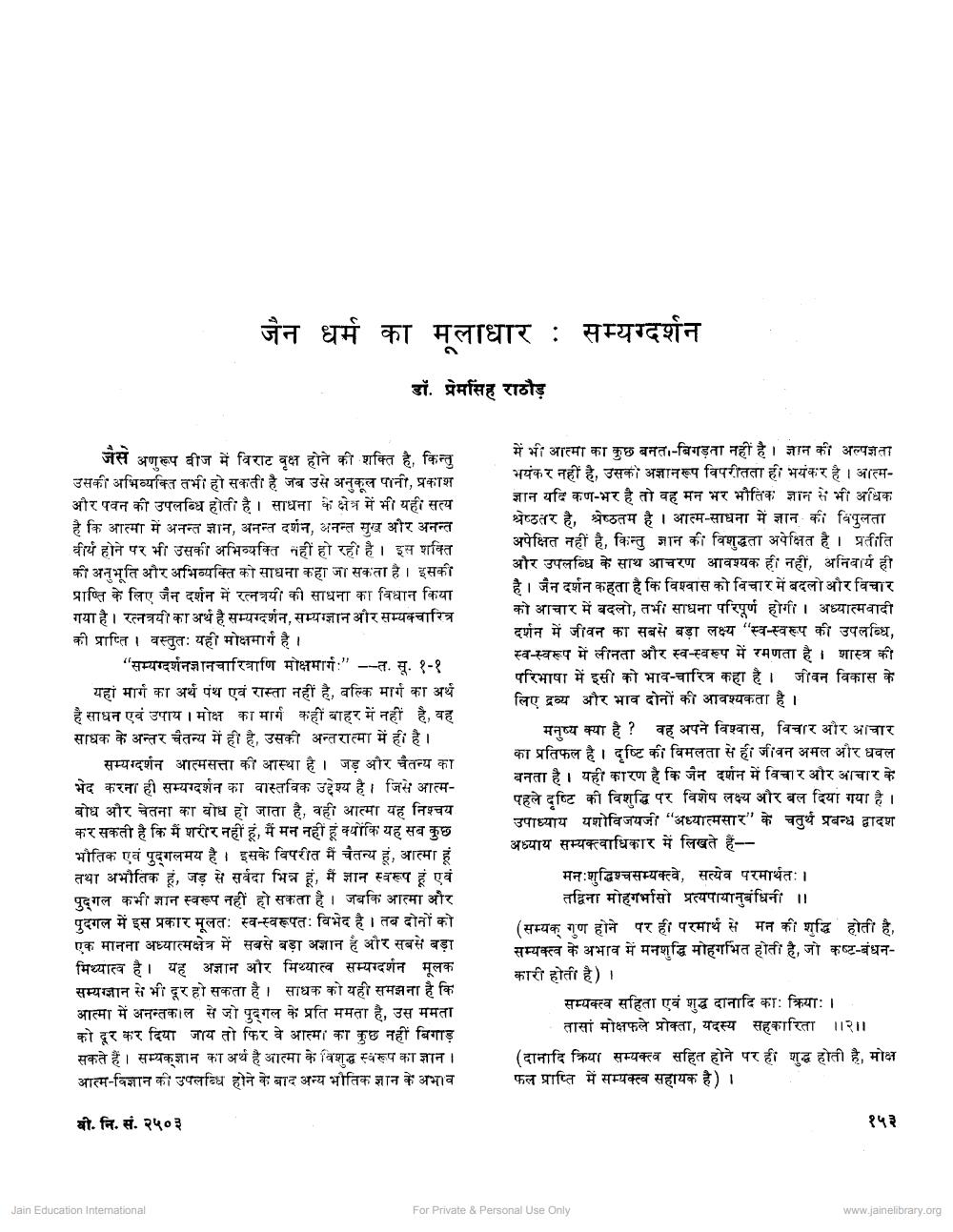Book Title: Jain Dharm ka Muladhar Samyagdarshan Author(s): Premsinh Rathod Publisher: Z_Rajendrasuri_Janma_Sardh_Shatabdi_Granth_012039.pdf View full book textPage 1
________________ जैन धर्म का मूलाधार : सम्यग्दर्शन डॉ. प्रेमसिंह राठौड़ जैसे अणुरूप बीज में विराट वृक्ष होने की शक्ति है, किन्तु उसकी अभिव्यक्ति तभी हो सकती है जब उसे अनुकूल पानी, प्रकाश और पवन की उपलब्धि होती है। साधना के क्षेत्र में भी यही सत्य है कि आत्मा में अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। इस शक्ति की अनुभूति और अभिव्यक्ति को साधना कहा जा सकता है। इसकी प्राप्ति के लिए जैन दर्शन में रत्नत्रयी की साधना का विधान किया गया है। रत्नत्रयी का अर्थ है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की प्राप्ति । वस्तुतः यही मोक्षमार्ग है। “सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः" --त. सू. १-१ यहा मार्ग का अर्थ पंथ एवं रास्ता नहीं है, बल्कि मार्ग का अर्थ है साधन एवं उपाय । मोक्ष का मार्ग कहीं बाहर में नहीं है, वह साधक के अन्तर चैतन्य में ही है, उसकी अन्तरात्मा में ही है। सम्यग्दर्शन आत्मसत्ता की आस्था है। जड़ और चैतन्य का भेद करना ही सम्यग्दर्शन का वास्तविक उद्देश्य है। जिसे आत्मबोध और चेतना का बोध हो जाता है, वही आत्मा यह निश्चय कर सकती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं क्योंकि यह सब कुछ भौतिक एवं पुद्गलमय है। इसके विपरीत मैं चैतन्य हूं, आत्मा हूं तथा अभौतिक हूं, जड़ से सर्वदा भिन्न हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं एवं पुद्गल कभी ज्ञान स्वरूप नहीं हो सकता है। जबकि आत्मा और पुदगल में इस प्रकार मूलत: स्व-स्वरूपतः विभेद है । तब दोनों को एक मानना अध्यात्मक्षेत्र में सबसे बड़ा अज्ञान है और सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। यह अज्ञान और मिथ्यात्व सम्यग्दर्शन मूलक सम्यग्ज्ञान से भी दूर हो सकता है। साधक को यही समझना है कि आत्मा में अनन्तकाल से जो पुद्गल के प्रति ममता है, उस ममता को दूर कर दिया जाय तो फिर वे आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। सम्यकज्ञान का अर्थ है आत्मा के विशुद्ध स्वरूप का ज्ञान । आत्म-विज्ञान की उपलब्धि होने के बाद अन्य भौतिक ज्ञान के अभाव में भी आत्मा का कुछ बनता-बिगड़ता नहीं है। ज्ञान की अल्पज्ञता भयंकर नहीं है, उसको अज्ञानरूप विपरीतता ही भयंकर है । आत्मज्ञान यदि कण-भर है तो वह मन भर भौतिक ज्ञान से भी अधिक श्रेष्ठतर है, श्रेष्ठतम है । आत्म-साधना में ज्ञान की विपुलता अपेक्षित नहीं है, किन्तु ज्ञान की विशुद्धता अपेक्षित है। प्रतीति और उपलब्धि के साथ आचरण आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य ही है। जैन दर्शन कहता है कि विश्वास को विचार में बदलो और विचार को आचार में बदलो, तभी साधना परिपूर्ण होगी। अध्यात्मवादी दर्शन में जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य "स्व-स्वरूप की उपलब्धि, स्व-स्वरूप में लीनता और स्व-स्वरूप में रमणता है। शास्त्र की परिभाषा में इसी को भाव-चारित्र कहा है। जीवन विकास के लिए द्रव्य और भाव दोनों की आवश्यकता है। मनुष्य क्या है ? वह अपने विश्वास, विचार और आचार का प्रतिफल है। दृष्टि की विमलता से ही जीवन अमल और धवल बनता है। यही कारण है कि जैन दर्शन में विचार और आचार के पहले दृष्टि की विशुद्धि पर विशेष लक्ष्य और बल दिया गया है। उपाध्याय यशोविजयजी "अध्यात्मसार" के चतुर्थ प्रबन्ध द्वादश अध्याय सम्यक्त्वाधिकार में लिखते हैं मनःशुद्धिश्चसम्यक्त्वे, सत्येव परमार्थतः । तद्विना मोहगर्भासो प्रत्यपायानुबंधिनी ।। (सम्यक् गुण होने पर ही परमार्थ से मन की शुद्धि होती है, सम्यक्त्व के अभाव में मनशुद्धि मोहगर्भित होती है, जो कष्ट-बंधनकारी होती है)। सम्यक्त्व सहिता एवं शुद्ध दानादि का: क्रियाः । तासां मोक्षफले प्रोक्ता, यदस्य सहकारिता ।।२।। (दानादि क्रिया सम्यक्त्व सहित होने पर ही शुद्ध होती है, मोक्ष फल प्राप्ति में सम्यक्त्व सहायक है) । बी. नि. सं. २५०३ १५३ Jain Education Intemational For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6