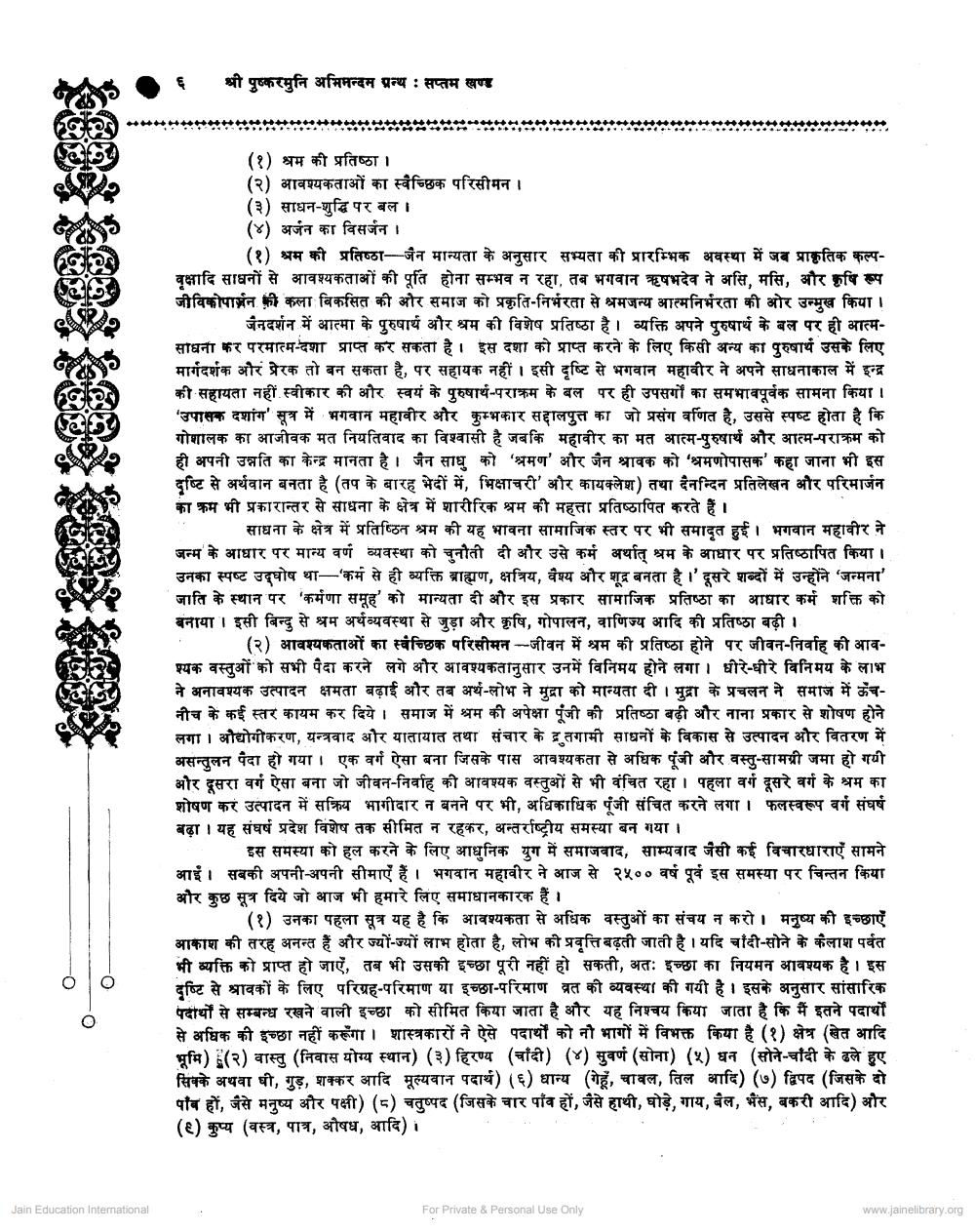Book Title: Jain Darshan me Samtavadi Samaj Rachna ke Arthik Tattva Author(s): Narendra Bhanavat Publisher: Z_Pushkarmuni_Abhinandan_Granth_012012.pdf View full book textPage 2
________________ ६ श्री पुष्करमुनि अभिमन्दम पन्थ : सप्तम खण्ड अपने पुरुषा प्राप्त करने के और स्वयंसहायक नहीं। (१) श्रम की प्रतिष्ठा। (२) आवश्यकताओं का स्वैच्छिक परिसीमन । (३) साधन-शुद्धि पर बल । (४) अर्जन का विसर्जन । (१) श्रम की प्रतिष्ठा-जैन मान्यता के अनुसार सभ्यता की प्रारम्भिक अवस्था में जब प्राकृतिक कल्पवृक्षादि साधनों से आवश्यकताओं की पूर्ति होना सम्भव न रहा, तब भगवान ऋषभदेव ने असि, मसि, और कृषि रूप जीविकोपार्जन की कला विकसित की और समाज को प्रकृति-निर्भरता से श्रमजन्य आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख किया। जैनदर्शन में आत्मा के पुरुषार्थ और श्रम की विशेष प्रतिष्ठा है। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बल पर ही आत्मसाधना कर परमात्म-दशा प्राप्त कर सकता है। इस दशा को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य का पुरुषार्थ उसके लिए मार्गदर्शक और प्रेरक तो बन सकता है, पर सहायक नहीं। इसी दृष्टि से भगवान महावीर ने अपने साधनाकाल में इन्द्र की सहायता नहीं स्वीकार की और स्वयं के पुरुषार्थ-पराक्रम के बल पर ही उपसर्गों का समभावपूर्वक सामना किया। 'उपासक दशांग' सूत्र में भगवान महावीर और कुम्भकार सद्दालपुत्त का जो प्रसंग वर्णित है, उससे स्पष्ट होता है कि गोशालक का आजीवक मत नियतिवाद का विश्वासी है जबकि महावीर का मत आत्म-पुरुषार्थ और आत्म-पराक्रम को ही अपनी उन्नति का केन्द्र मानता है। जैन साधु को 'श्रमण' और जैन श्रावक को 'श्रमणोपासक' कहा जाना भी इस दृष्टि से अर्थवान बनता है (तप के बारह भेदों में, भिक्षाचरी' और कायक्लेश) तथा दैनन्दिन प्रतिलेखन और परिमार्जन का क्रम भी प्रकारान्तर से साधना के क्षेत्र में शारीरिक श्रम की महत्ता प्रतिष्ठापित करते हैं । - साधना के क्षेत्र में प्रतिष्ठित श्रम की यह भावना सामाजिक स्तर पर भी समादृत हुई। भगवान महावीर ने जन्म के आधार पर मान्य वर्ण व्यवस्था को चुनौती दी और उसे कर्म अर्थात् श्रम के आधार पर प्रतिष्ठापित किया। उनका स्पष्ट उद्घोष था—'कर्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनता है। दूसरे शब्दों में उन्होंने 'जन्मना' जाति के स्थान पर 'कर्मणा समूह' को मान्यता दी और इस प्रकार सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार कर्म शक्ति को बनाया । इसी बिन्दु से श्रम अर्थव्यवस्था से जुड़ा और कृषि, गोपालन, वाणिज्य आदि की प्रतिष्ठा बढ़ी। (२) आवश्यकताओं का स्वैच्छिक परिसीमन-जीवन में श्रम की प्रतिष्ठा होने पर जीवन-निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं को सभी पैदा करने लगे और आवश्यकतानुसार उनमें विनिमय होने लगा। धीरे-धीरे विनिमय के लाभ ने अनावश्यक उत्पादन क्षमता बढ़ाई और तब अर्थ-लोभ ने मुद्रा को मान्यता दी । मुद्रा के प्रचलन ने समाज में ऊँचनीच के कई स्तर कायम कर दिये। समाज में श्रम की अपेक्षा पूंजी की प्रतिष्ठा बढ़ी और नाना प्रकार से शोषण होने लगा। औद्योगीकरण, यन्त्रवाद और यातायात तथा संचार के द्रुतगामी साधनों के विकास से उत्पादन और वितरण में असन्तुलन पैदा हो गया। एक वर्ग ऐसा बना जिसके पास आवश्यकता से अधिक पूंजी और वस्तु-सामग्री जमा हो गयी और दूसरा वर्ग ऐसा बना जो जीवन-निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं से भी वंचित रहा। पहला वर्ग दूसरे वर्ग के श्रम का शोषण कर उत्पादन में सक्रिय भागीदार न बनने पर भी, अधिकाधिक पूंजी संचित करने लगा। फलस्वरूप वर्ग संघर्ष बढ़ा । यह संघर्ष प्रदेश विशेष तक सीमित न रहकर, अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन गया। इस समस्या को हल करने के लिए आधुनिक युग में समाजवाद, साम्यवाद जैसी कई विचारधाराएँ सामने आई। सबकी अपनी-अपनी सीमाएँ हैं। भगवान महावीर ने आज से २५०० वर्ष पूर्व इस समस्या पर चिन्तन किया और कुछ सूत्र दिये जो आज भी हमारे लिए समाधानकारक हैं। (१) उनका पहला सूत्र यह है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय न करो। मनुष्य की इच्छाएँ आकाश की तरह अनन्त हैं और ज्यों-ज्यों लाभ होता है, लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है । यदि चाँदी-सोने के कैलाश पर्वत भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाएँ, तब भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, अतः इच्छा का नियमन आवश्यक है। इस दृष्टि से श्रावकों के लिए परिग्रह-परिमाण या इच्छा-परिमाण व्रत की व्यवस्था की गयी है। इसके अनुसार सांसारिक पदार्थों से सम्बन्ध रखने वाली इच्छा को सीमित किया जाता है और यह निश्चय किया जाता है कि मैं इतने पदार्थों से अधिक की इच्छा नहीं करूँगा। शास्त्रकारों ने ऐसे पदार्थों को नौ भागों में विभक्त किया है (१) क्षेत्र (खेत आदि भूमि) (२) वास्तु (निवास योग्य स्थान) (३) हिरण्य (चाँदी) (४) सुवर्ण (सोना) (५) धन (सोने-चांदी के ढले हुए सिक्के अथवा घी, गुड़, शक्कर आदि मूल्यवान पदार्थ) (६) धान्य (गेहूँ, चावल, तिल आदि) (७) द्विपद (जिसके दो पाँव हों, जैसे मनुष्य और पक्षी) (८) चतुष्पद (जिसके चार पाँव हों, जैसे हाथी, घोड़े, गाय, बैल, भैस, बकरी आदि) और (९) कुप्य (वस्त्र, पात्र, औषध, आदि)। 00 Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5