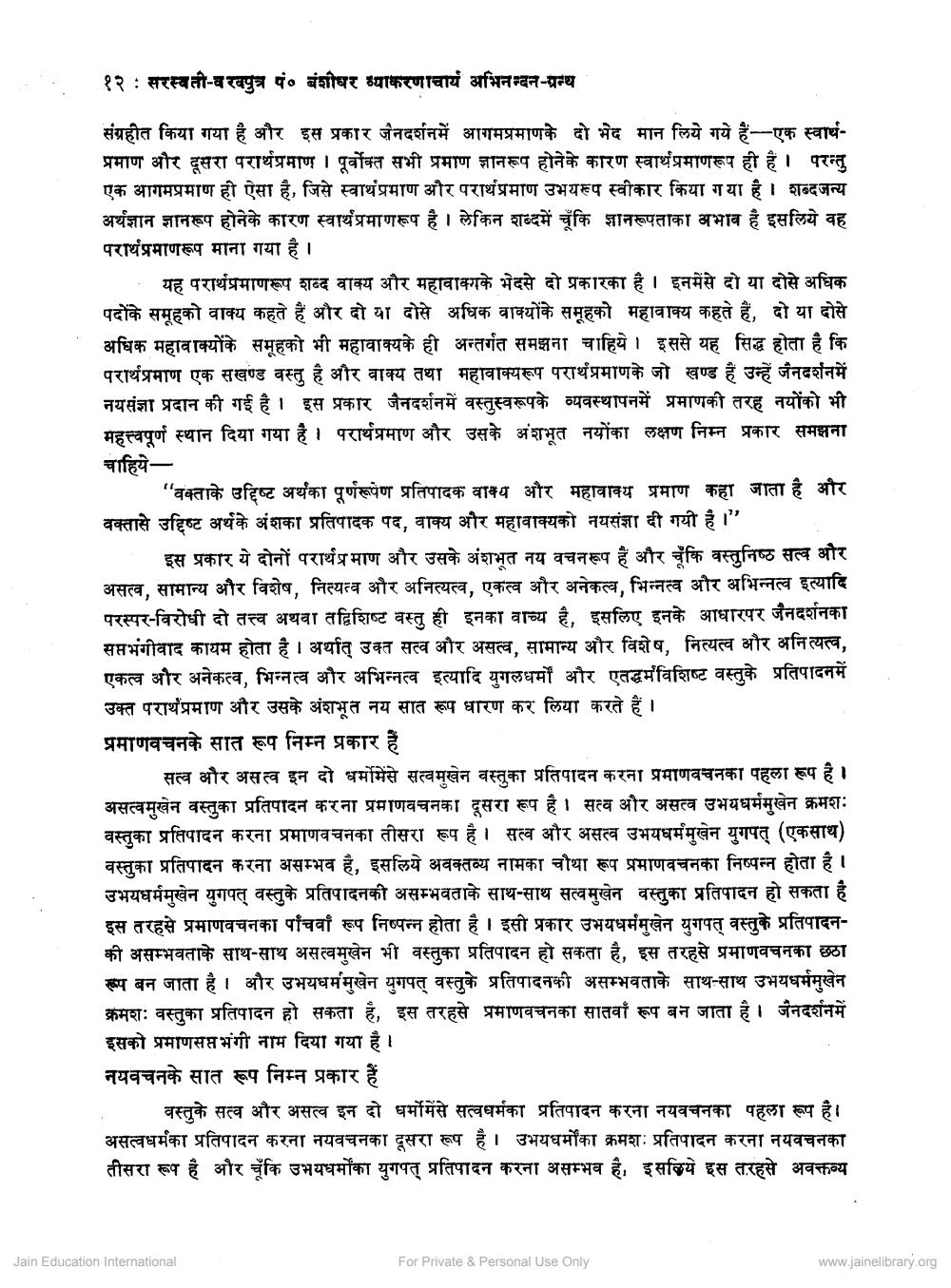Book Title: Jain Darshan me Praman aur Nay Author(s): Bansidhar Pandit Publisher: Z_Bansidhar_Pandit_Abhinandan_Granth_012047.pdf View full book textPage 4
________________ १२ : सरस्वती-वरवपुत्र पं० बंशीधर व्याकरणाचार्य अभिनन्दन-ग्रन्थ संग्रहीत किया गया है और इस प्रकार जैनदर्शनमें आगमप्रमाणके दो भेद मान लिये गये हैं-एक स्वार्थप्रमाण और दूसरा परार्थप्रमाण । पूर्वोक्त सभी प्रमाण ज्ञानरूप होने के कारण स्वार्थप्रमाणरूप ही है। परन्तु एक आगमप्रमाण ही ऐसा है, जिसे स्वार्थप्रमाण और परार्थप्रमाण उभयरूप स्वीकार किया गया है। शब्दजन्य अर्थज्ञान ज्ञानरूप होनेके कारण स्वार्थप्रमाणरूप है । लेकिन शब्दमें चूँकि ज्ञानरूपताका अभाव है इसलिये वह परार्थप्रमाणरूप माना गया है। यह परार्थप्रमाणरूप शब्द वाक्य और महावाक्यके भेदसे दो प्रकारका है। इनमें से दो या दोसे अधिक पदोंके समूहको वाक्य कहते हैं और दो या दोसे अधिक वाक्योंके समूहको महावाक्य कहते हैं, दो या दोसे अधिक महावाक्योंके समूहको भी महावाक्यके ही अन्तर्गत समझना चाहिये। इससे यह सिद्ध होता है कि परार्थप्रमाण एक सखण्ड वस्तु है और वाक्य तथा महावाक्यरूप परार्थप्रमाणके जो खण्ड हैं उन्हें जैनदर्शनमें नयसंज्ञा प्रदान की गई है। इस प्रकार जैनदर्शनमें वस्तुस्वरूपके व्यवस्थापनमें प्रमाणकी तरह नयोंको भी महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है । परार्थप्रमाण और उसके अंशभूत नयोंका लक्षण निम्न प्रकार समझना चाहिये "वक्ताके उद्दिष्ट अर्थका पूर्णरूपेण प्रतिपादक वाक्य और महावाक्य प्रमाण कहा जाता है और वक्तासे उद्दिष्ट अर्थके अंशका प्रतिपादक पद, वाक्य और महावाक्यको नयसंज्ञा दी गयी है।" इस प्रकार ये दोनों परार्थप्रमाण और उसके अंशभूत नय वचनरूप हैं और चूँकि वस्तुनिष्ठ सत्व और असत्व, सामान्य और विशेष, नित्यत्व और अनित्यत्व, एकत्व और अनेकत्व, भिन्नत्व और अभिन्नत्व परस्पर-विरोधी दो तत्त्व अथवा तद्विशिष्ट वस्तु ही इनका वाच्य है, इसलिए इनके आधारपर जैनदर्शनका सप्तभंगीवाद कायम होता है। अर्थात उक्त सत्व और असत्व, सामान्य और विशेष. नित्यत्व और अनित्यत्व, एकत्व और अनेकत्व, भिन्नत्व और अभिन्नत्व इत्यादि युगलधर्मों और एतद्धर्मविशिष्ट वस्तुके प्रतिपादनमें उक्त परार्थप्रमाण और उसके अंशभूत नय सात रूप धारण कर लिया करते हैं। प्रमाणवचनके सात रूप निम्न प्रकार हैं सत्व और असत्व इन दो धर्मोमेंसे सत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाणवचनका पहला रूप है। असत्वमखेन वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाणवचनका दूसरा रूप है। सत्व और असत्व उभयधर्ममुखेन क्रमशः वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाणवचनका तीसरा रूप है। सत्व और असत्व उभयधर्ममुखेन युगपत् (एकसाथ) वस्तुका प्रतिपादन करना असम्भव है, इसलिये अवक्तव्य नामका चौथा रूप प्रमाणवचनका निष्पन्न होता है । उभयधर्ममुखेन युगपत् वस्तुके प्रतिपादनकी असम्भवताके साथ-साथ सत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाणवचनका पाँचवाँ रूप निष्पन्न होता है । इसी प्रकार उभयधर्ममुखेन युगपत् वस्तुके प्रतिपादनकी असम्भवताके साथ-साथ असत्वमुखेन भी वस्तुका प्रतिपादन हो सकता है, इस तरहसे प्रमाणवचनका छठा रूप बन जाता है। और उभयधर्ममुखेन युगपत् वस्तुके प्रतिपादनकी असम्भवताके साथ-साथ उभयधर्ममुखेन क्रमशः वस्तुका प्रतिपादन हो सकता है, इस तरहसे प्रमाणवचनका सातवाँ रूप बन जाता है। जैनदर्शनमें इसको प्रमाणसप्तभंगी नाम दिया गया है। नयवचनके सात रूप निम्न प्रकार हैं वस्तुके सत्व और असत्व इन दो धर्मोमेंसे सत्वधर्मका प्रतिपादन करना नयवचनका पहला रूप है। असत्वधर्मका प्रतिपादन करना नयवचनका दूसरा रूप है। उभयधर्मोका क्रमशः प्रतिपादन करना नयवचनका तीसरा रूप है और चूंकि उभयधर्मोंका युगपत् प्रतिपादन करना असम्भव है, इसलिये इस तरहसे अवक्तव्य Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5