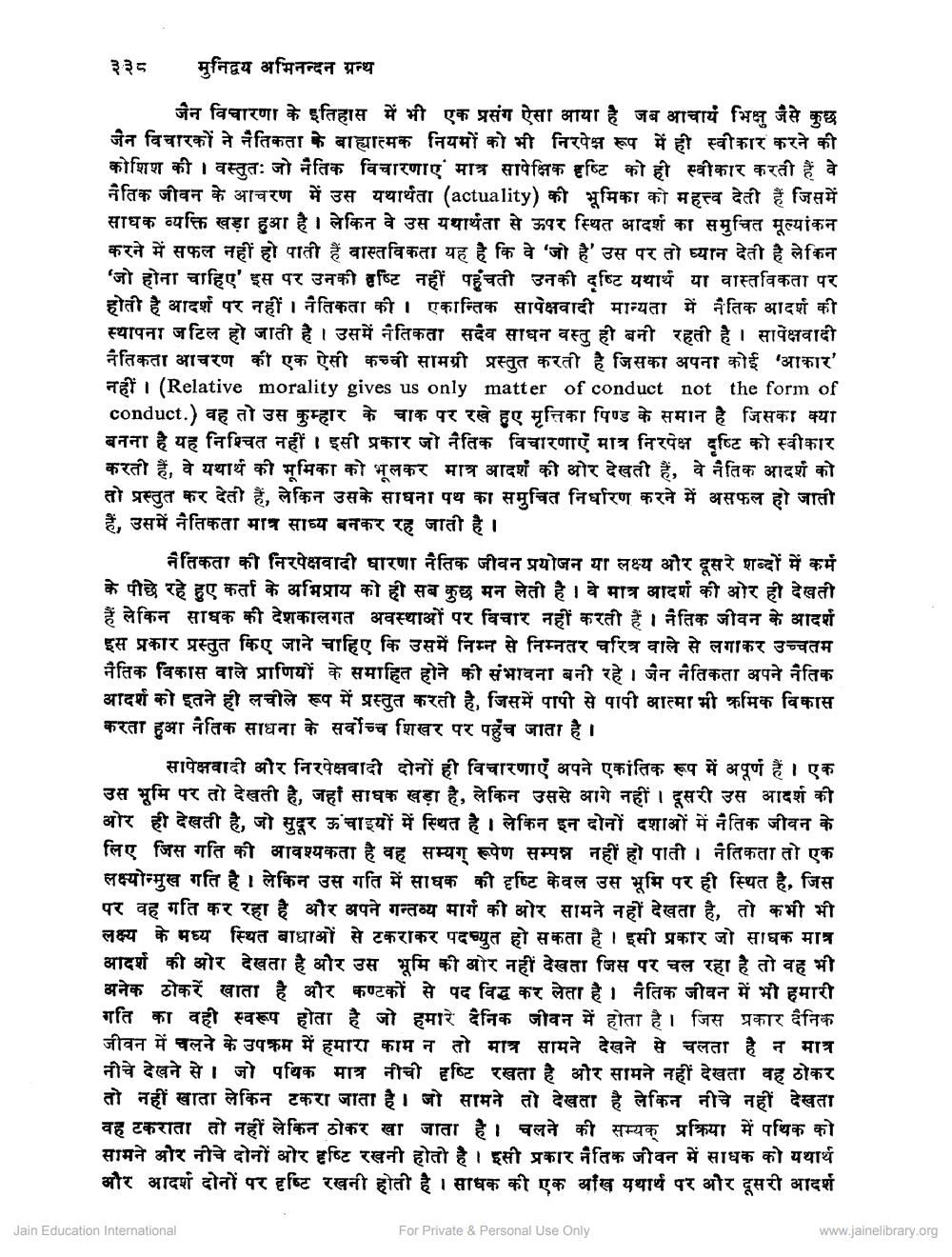Book Title: Jain Darshan me Naitikta ki Sapkeshata aur Nirpekshata Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Z_Munidway_Abhinandan_Granth_012006.pdf View full book textPage 7
________________ ३३८ मुनिद्वय अभिनन्दन ग्रन्थ जैन विचारणा के इतिहास में भी एक प्रसंग ऐसा आया है जब आचार्य भिक्षु जैसे कुछ जैन विचारकों ने नैतिकता के बाह्यात्मक नियमों को भी निरपेक्ष रूप में ही स्वीकार करने की कोशिश की। वस्तुतः जो नैतिक विचारणाएं मात्र सापेक्षिक दृष्टि को ही स्वीकार करती हैं वे नैतिक जीवन के आचरण में उस यथार्थता (actuality) की भूमिका को महत्त्व देती हैं जिसमें साधक व्यक्ति खड़ा हुआ है। लेकिन वे उस यथार्थता से ऊपर स्थित आदर्श का समुचित मूल्यांकन करने में सफल नहीं हो पाती हैं वास्तविकता यह है कि वे 'जो है' उस पर तो ध्यान देती है लेकिन 'जो होना चाहिए' इस पर उनकी दृष्टि नहीं पहुंचती उनकी दृष्टि यथार्थ या वास्तविकता पर होती है आदर्श पर नहीं । नैतिकता की । एकान्तिक सापेक्षवादी मान्यता में नैतिक आदर्श की स्थापना जटिल हो जाती है। उसमें नैतिकता सदैव साधन वस्तु ही बनी रहती है। सापेक्षवादी नैतिकता आचरण की एक ऐसी कच्ची सामग्री प्रस्तुत करती है जिसका अपना कोई 'आकार' नहीं। (Relative morality gives us only matter of conduct not the form of conduct.) वह तो उस कुम्हार के चाक पर रखे हुए मृत्तिका पिण्ड के समान है जिसका क्या बनना है यह निश्चित नहीं। इसी प्रकार जो नैतिक विचारणाएँ मात्र निरपेक्ष दृष्टि को स्वीकार करती हैं, वे यथार्थ की भूमिका को भूलकर मात्र आदर्श की ओर देखती हैं, वे नैतिक आदर्श को तो प्रस्तुत कर देती हैं, लेकिन उसके साधना पथ का समुचित निर्धारण करने में असफल हो जाती हैं, उसमें नैतिकता मात्र साध्य बनकर रह जाती है। नैतिकता की निरपेक्षवादी धारणा नैतिक जीवन प्रयोजन या लक्ष्य और दूसरे शब्दों में कर्म के पीछे रहे हुए कर्ता के अभिप्राय को ही सब कुछ मन लेती है। वे मात्र आदर्श की ओर ही देखती हैं लेकिन साधक की देशकालगत अवस्थाओं पर विचार नहीं करती हैं। नैतिक जीवन के आदर्श इस प्रकार प्रस्तुत किए जाने चाहिए कि उसमें निम्न से निम्नतर चरित्र वाले से लगाकर उच्चतम नैतिक विकास वाले प्राणियों के समाहित होने की संभावना बनी रहे। जैन नैतिकता अपने नैतिक आदर्श को इतने ही लचीले रूप में प्रस्तुत करती है, जिसमें पापी से पापी आत्मा भी क्रमिक विकास करता हआ नतिक साधना के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है। सापेक्षवादी और निरपेक्षवादी दोनों ही विचारणाएं अपने एकांतिक रूप में अपूर्ण हैं । एक उस भूमि पर तो देखती है, जहां साधक खड़ा है, लेकिन उससे आगे नहीं। दूसरी उस आदर्श की ओर ही देखती है, जो सुदूर ऊंचाइयों में स्थित है। लेकिन इन दोनों दशाओं में नैतिक जीवन के लिए जिस गति की आवश्यकता है वह सम्यग रूपेण सम्पन्न नहीं हो पाती। नैतिकता तो एक लक्ष्योन्मुख गति है। लेकिन उस गति में साधक की दृष्टि केवल उस भूमि पर ही स्थित है, जिस पर वह गति कर रहा है और अपने गन्तव्य मार्ग की ओर सामने नहीं देखता है, तो कभी भी लक्ष्य के मध्य स्थित बाधाओं से टकराकर पदच्युत हो सकता है । इसी प्रकार जो साधक मात्र आदर्श की ओर देखता है और उस भूमि की ओर नहीं देखता जिस पर चल रहा है तो वह भी अनेक ठोकरें खाता है और कण्टकों से पद विद्ध कर लेता है। नैतिक जीवन में भी हमारी गति का वही स्वरूप होता है जो हमारे दैनिक जीवन में होता है। जिस प्रकार दैनिक जीवन में चलने के उपक्रम में हमारा काम न तो मात्र सामने देखने से चलता है न मात्र नीचे देखने से। जो पथिक मात्र नीची दृष्टि रखता है और सामने नहीं देखता वह ठोकर तो नहीं खाता लेकिन टकरा जाता है। जो सामने तो देखता है लेकिन नीचे नहीं देखता वह टकराता तो नहीं लेकिन ठोकर खा जाता है। चलने की सम्यक प्रक्रिया में पथिक को सामने और नीचे दोनों ओर दृष्टि रखनी होतो है। इसी प्रकार नैतिक जीवन में साधक को यथार्थ और आदर्श दोनों पर दृष्टि रखनी होती है। साधक की एक आँख यथार्थ पर और दूसरी आदर्श Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 5 6 7 8 9