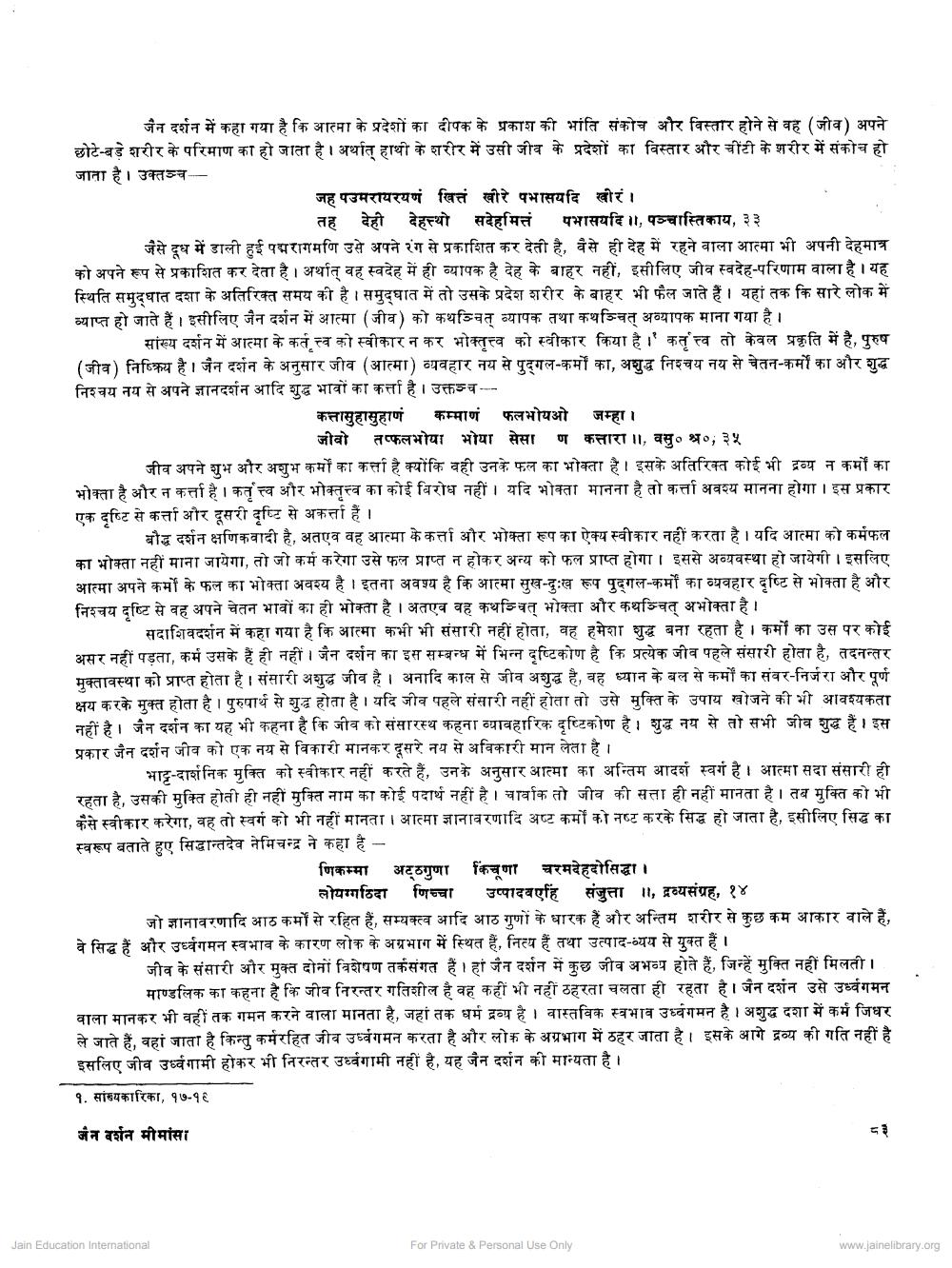Book Title: Jain Darshan me Jiv Dravya Author(s): Shreyans Jain Publisher: Z_Deshbhushanji_Maharaj_Abhinandan_Granth_012045.pdf View full book textPage 3
________________ जैन दर्शन में कहा गया है कि आत्मा के प्रदेशों का दीपक के प्रकाश की भांति संकोच और विस्तार होने से वह (जीव ) अपने छोटे-बड़े शरीर के परिमाण का हो जाता है। अर्थात् हाथी के शरीर में उसी जीव के प्रदेशों का विस्तार और चींटी के शरीर में संकोच हो जाता है। उक्तञ्च जह पउमरायरयणं खित्तं खीरे पभासयदि खोरं । तह देही देहवो सदेहमित्तं पभासयदि ॥ पञ्चास्तिकाय, ३३ जैसे दूध में डाली हुई पद्मरागमणि उसे अपने रंग से प्रकाशित कर देती है, वैसे ही देह में रहने वाला आत्मा भी अपनी देहमात्र को अपने रूप से प्रकाशित कर देता है। अर्थात् वह स्वदेह में ही व्यापक है देह के बाहर नहीं, इसीलिए जीव स्वदेह-परिणाम वाला है। यह स्थिति समुद्घात दशा के अतिरिक्त समय की है। समुद्घात में तो उसके प्रदेश शरीर के बाहर भी फैल जाते हैं। यहां तक कि सारे लोक में व्याप्त हो जाते हैं । इसीलिए जैन दर्शन में आत्मा (जीव ) को कथञ्चित् व्यापक तथा कथञ्चित् अव्यापक माना गया है। सांख्य दर्शन में आत्मा के कर्त त्त्व को स्वीकार न कर भोक्तृत्त्व को स्वीकार किया है।' कर्तृत्त्व तो केवल प्रकृति में है, पुरुष (जीव) निष्क्रिय है। जैन दर्शन के अनुसार जीव (आत्मा) व्यवहार नय से पुद्गल कर्मों का अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों का और शुद्ध निश्चय नय से अपने ज्ञानदर्शन आदि शुद्ध भावों का कर्त्ता है। उक्तञ्च -- जम्हा । ताहाहाणं कम्माणं फलभोयओ जीवो तप्फलभोया भोया सेसा ण कत्तारा ॥ वसु० श्र०, ३५ जीव अपने शुभ और अशुभ कर्मों का कर्त्ता है क्योंकि वही उनके फल का भोक्ता है। इसके अतिरिक्त कोई भी द्रव्य न कर्मों का भोक्ता है और न कर्त्ता है । कर्तृ त्त्व और भोक्तृत्त्व का कोई विरोध नहीं । यदि भोक्ता मानना है तो कर्त्ता अवश्य मानना होगा। इस प्रकार एक दृष्टि से कर्त्ता और दूसरी दृष्टि से अकर्त्ता हैं । बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है, अतएव वह आत्मा के कर्त्ता और भोक्ता रूप का ऐक्य स्वीकार नहीं करता है। यदि आत्मा को कर्मफल का भोक्ता नहीं माना जायेगा, तो जो कर्म करेगा उसे फल प्राप्त न होकर अन्य को फल प्राप्त होगा। इससे अव्यवस्था हो जायेगी । इसलिए आत्मा अपने कर्मों के फल का भोक्ता अवश्य है। इतना अवश्य है कि आत्मा सुख-दुःख रूप पुद्गल - कर्मों का व्यवहार दृष्टि से भोक्ता है और निश्चय दृष्टि से वह अपने वेतन भावों का ही भोक्ता है। अतएव यह कचित् भोक्ता और कथञ्चित् अभोक्ता है। सदाशिवदर्शन में कहा गया है कि आत्मा कभी भी संसारी नहीं होता, वह हमेशा शुद्ध बना रहता है। कर्मों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता, कर्म उसके हैं ही नहीं। जैन दर्शन का इस सम्बन्ध में भिन्न दृष्टिकोण है कि प्रत्येक जीव पहले संसारी होता है, तदनन्तर मुक्तावस्था को प्राप्त होता है । संसारी अशुद्ध जीव है। अनादि काल से जीव अशुद्ध है, वह ध्यान के बल से कर्मों का संवर-निर्जरा और पूर्ण क्षय करके मुक्त होता है। पुस्वार्थ से युद्ध होता है। यदि जीव पहले संसारी नहीं होता तो उसे मुक्ति के उपाय खोजने की भी आवश्यकता नहीं है। जैन दर्शन का यह भी कहना है कि जीव को संसारस्थ कहना व्यावहारिक दृष्टिकोण है। शुद्ध नय से तो सभी जीव शुद्ध हैं। इस प्रकार जैन दर्शन जीव को एक नय से विकारी मानकर दूसरे नय से अविकारी मान लेता है । भाट्ट दार्शनिक मुक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं, उनके अनुसार आत्मा का अन्तिम आदर्श स्वर्ग है। आत्मा सदा संसारी ही रहता है, उसकी मुक्ति होती ही नहीं मुक्ति नाम का कोई पदार्थ नहीं है। चार्वाक तो जीव की सत्ता ही नहीं मानता है। तब मुक्ति को भी कैसे स्वीकार करेगा, वह तो स्वर्ग को भी नहीं मानता। आत्मा ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मों को नष्ट करके सिद्ध हो जाता है, इसीलिए सिद्ध का स्वरूप बताते हुए सिद्धान्तदेव नेमिचन्द्र ने कहा है णिकम्मा अगुणा लोयग्गठिदा णिच्चा शिचूणा चरमनेोसिद्धा उप्पादव एहि संजुत्ता ॥ द्रव्यसंग्रह, १४ जो ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से रहित हैं, सम्यक्त्व आदि आठ गुणों के धारक हैं और अन्तिम शरीर से कुछ कम आकार वाले हैं, वे सिद्ध हैं और उर्ध्वगमन स्वभाव के कारण लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, नित्य हैं तथा उत्पाद व्यय से युक्त हैं । जीव के संसारी और मुक्त दोनों विशेषण तर्कसंगत है। हां जैन दर्शन में कुछ जीव अभव्य होते हैं, जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती। मण्डलिक का कहना है कि जीव निरन्तर गतिशील है वह कहीं भी नहीं ठहरता चलता ही रहता है। जैन दर्शन उसे उर्ध्वगमन वाला मानकर भी वहीं तक गमन करने वाला मानता है, जहां तक धर्म द्रव्य है । वास्तविक स्वभाव उर्ध्वगमन है । अशुद्ध दशा में कर्म जिधर ले जाते हैं, वहां जाता है किन्तु कर्मरहित जीव उर्ध्वगमन करता है और लोक के अग्रभाग में ठहर जाता है। इसके आगे द्रव्य की गति नहीं है। इसलिए जीव उर्ध्वगामी होकर भी निरन्तर उर्ध्वगामी नहीं है, यह जैन दर्शन की मान्यता है । १. सांख्यकारिका, १७-१६ जैन दर्शन मीमांसा Jain Education International For Private & Personal Use Only ८३ www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4