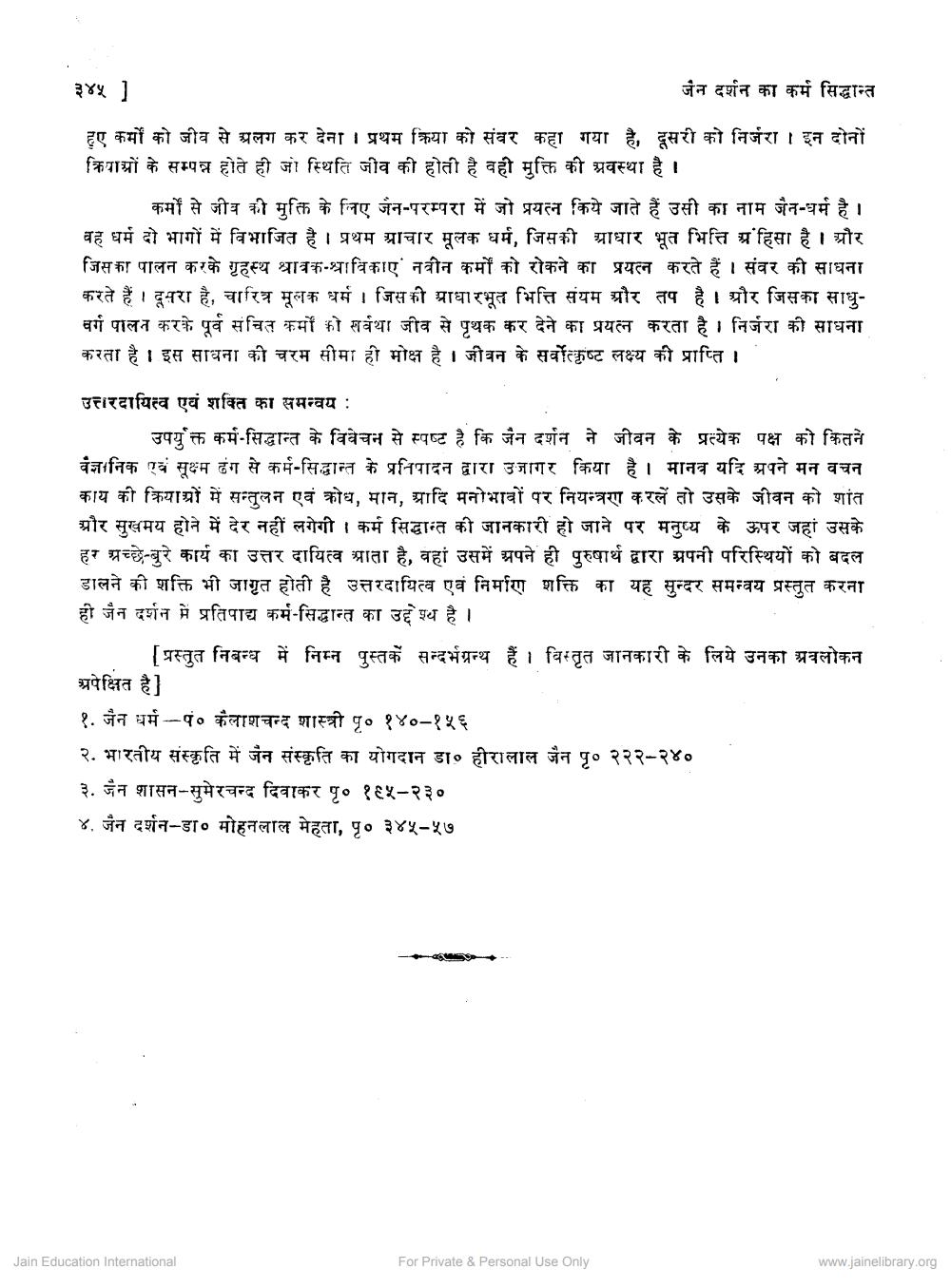Book Title: Jain Darshan ka Karmsiddhant Jivan ka Manovaigyanik Vishleshan Author(s): Prem Suman Jain Publisher: Z_Jinvijay_Muni_Abhinandan_Granth_012033.pdf View full book textPage 7
________________ 345 ] जैन दर्शन का कर्म सिद्धान्त हुए कर्मों को जीव से अलग कर देना / प्रथम क्रिया को संवर कहा गया है, दूसरी को निर्जरा / इन दोनों क्रियाओं के सम्पन्न होते ही जो स्थिति जीव की होती है वही मुक्ति की अवस्था है। कर्मों से जीव की मुक्ति के लिए जैन-परम्परा में जो प्रयत्न किये जाते हैं उसी का नाम जैन-धर्म है। वह धर्म दो भागों में विभाजित है। प्रथम प्राचार मूलक धर्म, जिसकी आधार भूत भित्ति अंहिसा है / और जिसका पालन करके गृहस्थ श्रावक-श्राविकाए नवीन कर्मों को रोकने का प्रयत्न करते हैं / संवर की साधना करते हैं / दूसरा है, चारित्र मूलक धर्म / जिसकी आधारभूत भित्ति संयम और तप है। और जिसका साधुवर्ग पालन करके पूर्व संचित कर्मों को सर्वथा जीव से पृथक कर देने का प्रयत्न करता है। निर्जरा की साधना करता है। इस साधना की चरम सीमा ही मोक्ष है / जीवन के सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य की प्राप्ति / उत्तरदायित्व एवं शक्ति का समन्वय : उपर्युक्त कर्म-सिद्धान्त के विवेचन से स्पष्ट है कि जैन दर्शन ने जीवन के प्रत्येक पक्ष को कितने वैज्ञानिक एवं सूक्ष्म ढंग से कर्म-सिद्धान्त के प्रतिपादन द्वारा उजागर किया है। मानव यदि अपने मन वचन और सुखमय होने में देर नहीं लगेगी। कर्म सिद्धान्त की जानकारी हो जाने पर मनुष्य के ऊपर जहां उसके हर अच्छे-बुरे कार्य का उत्तर दायित्व आता है, वहां उसमें अपने ही पुरुषार्थ द्वारा अपनी परिस्थियों को बदल डालने की शक्ति भी जागृत होती है उत्तरदायित्व एवं निर्माण शक्ति का यह सुन्दर समन्वय प्रस्तुत करना ही जैन दर्शन में प्रतिपाद्य कर्म-सिद्धान्त का उद्देश्य है। [प्रस्तुत निबन्ध में निम्न पुस्तकें सन्दर्भग्रन्थ हैं। विस्तृत जानकारी के लिये उनका अवलोकन अपेक्षित है] 1. जैन धर्म-पं० कैलाशचन्द शास्त्री पृ० 140-156 2. भारतीय संस्कृति में जैन संस्कृति का योगदान डा० हीरालाल जैन पृ० 222-240 3. जैन शासन-सुमेरचन्द दिवाकर पृ० 165-230 4. जैन दर्शन-डा० मोहनलाल मेहता, पृ० 345-57 - -- +-- Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 5 6 7