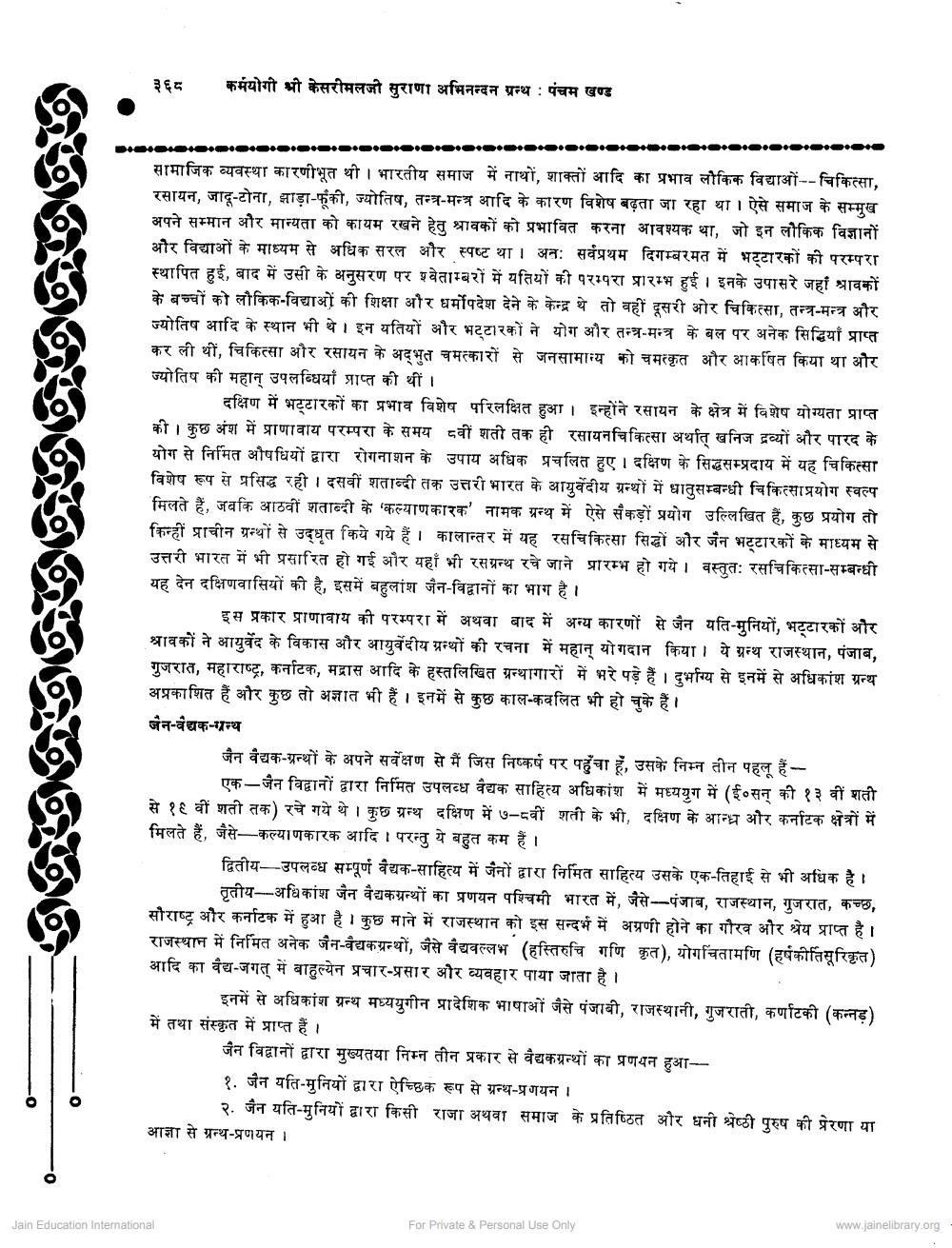Book Title: Jain Ayurved Parampara aur Sahitya Author(s): Rajendraprasad Bhatnagar Publisher: Z_Kesarimalji_Surana_Abhinandan_Granth_012044.pdf View full book textPage 6
________________ ३६८ कर्मयोगी श्री केसरीमलजी सुराणा अभिनन्दन ग्रन्थ : पंचम खण्ड 100. ........................................... सामाजिक व्यवस्था कारणीभूत थी। भारतीय समाज में नाथों, शाक्तों आदि का प्रभाव लौकिक विद्याओं--चिकित्सा, रसायन, जादू-टोना, झाड़ा-फूंकी, ज्योतिष, तन्त्र-मन्त्र आदि के कारण विशेष बढ़ता जा रहा था। ऐसे समाज के सम्मुख अपने सम्मान और मान्यता को कायम रखने हेतु श्रावकों को प्रभावित करना आवश्यक था, जो इन लौकिक विज्ञानों और विद्याओं के माध्यम से अधिक सरल और स्पष्ट था। अत: सर्वप्रथम दिगम्बरमत में भट्टारकों की परम्परा स्थापित हुई, बाद में उसी के अनुसरण पर श्वेताम्बरों में यतियों की परम्परा प्रारम्भ हुई। इनके उपासरे जहाँ श्रावकों के बच्चों को लौकिक-विद्याओं की शिक्षा और धर्मोपदेश देने के केन्द्र थे तो वहीं दूसरी ओर चिकित्सा, तन्त्र-मन्त्र और ज्योतिष आदि के स्थान भी थे। इन यतियों और भट्टारकों ने योग और तन्त्र-मन्त्र के बल पर अनेक सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थीं, चिकित्सा और रसायन के अद्भुत चमत्कारों से जनसामान्य को चमत्कृत और आकर्षित किया था और ज्योतिष की महान् उपलब्धियाँ प्राप्त की थीं। दक्षिण में भट्टारकों का प्रभाव विशेष परिलक्षित हुआ। इन्होंने रसायन के क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त की। कुछ अंश में प्राणावाय परम्परा के समय ८वीं शती तक ही रसायनचिकित्सा अर्थात् खनिज द्रव्यों और पारद के योग से निर्मित औषधियों द्वारा रोगनाशन के उपाय अधिक प्रचलित हुए। दक्षिण के सिद्धसम्प्रदाय में यह चिकित्सा विशेष रूप से प्रसिद्ध रही । दसवीं शताब्दी तक उत्तरी भारत के आयुर्वेदीय ग्रन्थों में धातुसम्बन्धी चिकित्साप्रयोग स्वल्प मिलते हैं, जबकि आठवीं शताब्दी के 'कल्याणकारक' नामक ग्रन्थ में ऐसे सैकड़ों प्रयोग उल्लिखित हैं, कुछ प्रयोग तो किन्हीं प्राचीन ग्रन्थों से उद्धृत किये गये हैं। कालान्तर में यह रसचिकित्सा सिद्धों और जैन भट्टारकों के माध्यम से उत्तरी भारत में भी प्रसारित हो गई और यहाँ भी रसग्रन्थ रचे जाने प्रारम्भ हो गये। वस्तुत: रसचिकित्सा-सम्बन्धी यह देन दक्षिणवासियों की है, इसमें बहुलांश जैन-विद्वानों का भाग है। इस प्रकार प्राणावाय की परम्परा में अथवा बाद में अन्य कारणों से जैन यति-मुनियों, भट्टारकों और श्रावकों ने आयुर्वेद के विकास और आयुर्वेदीय ग्रन्थों की रचना में महान् योगदान किया। ये ग्रन्थ राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मद्रास आदि के हस्तलिखित ग्रन्थागारों में भरे पड़े हैं। दुर्भाग्य से इनमें से अधिकांश ग्रन्थ अप्रकाशित हैं और कुछ तो अज्ञात भी हैं। इनमें से कुछ काल-कवलित भी हो चुके हैं। जैन-वैद्यक-ग्रन्थ जैन वैद्यक-ग्रन्थों के अपने सर्वेक्षण से मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, उसके निम्न तीन पहलू हैं एक-जैन विद्वानों द्वारा निर्मित उपलब्ध वैद्यक साहित्य अधिकांश में मध्ययुग में (ई०सन् की १३ वीं शती से १६ वीं शती तक) रचे गये थे। कुछ ग्रन्थ दक्षिण में ७-८वीं शती के भी, दक्षिण के आन्ध्र और कर्नाटक क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे-कल्याणकारक आदि । परन्तु ये बहुत कम हैं। द्वितीय-उपलब्ध सम्पूर्ण वैद्यक-साहित्य में जैनों द्वारा निर्मित साहित्य उसके एक-तिहाई से भी अधिक है। तृतीय----अधिकांश जैन वैद्यकग्रन्थों का प्रणयन पश्चिमी भारत में, जैसे--पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र और कर्नाटक में हुआ है। कुछ माने में राजस्थान को इस सन्दर्भ में अग्रणी होने का गौरव और श्रेय प्राप्त है। राजस्थान में निर्मित अनेक जैन-वैद्यकग्रन्थों, जैसे वैद्यवल्लभ (हस्तिरुचि गणि कृत), योगचितामणि (हर्षकीतिसूरिकृत) आदि का वैद्य-जगत् में बाहुल्येन प्रचार-प्रसार और व्यवहार पाया जाता है। इनमें से अधिकांश ग्रन्थ मध्ययुगीन प्रादेशिक भाषाओं जैसे पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, कर्णाटकी (कन्नड़) में तथा संस्कृत में प्राप्त हैं। जैन विद्वानों द्वारा मुख्यतया निम्न तीन प्रकार से वैद्यकग्रन्थों का प्रणयन हुआ-- १. जैन यति-मुनियों द्वारा ऐच्छिक रूप से ग्रन्थ-प्रणयन । २. जैन यति-मुनियों द्वारा किसी राजा अथवा समाज के प्रतिष्ठित और धनी श्रेष्ठी पुरुष की प्रेरणा या आज्ञा से ग्रन्थ-प्रणयन । For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org Jain Education InternationalPage Navigation
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11