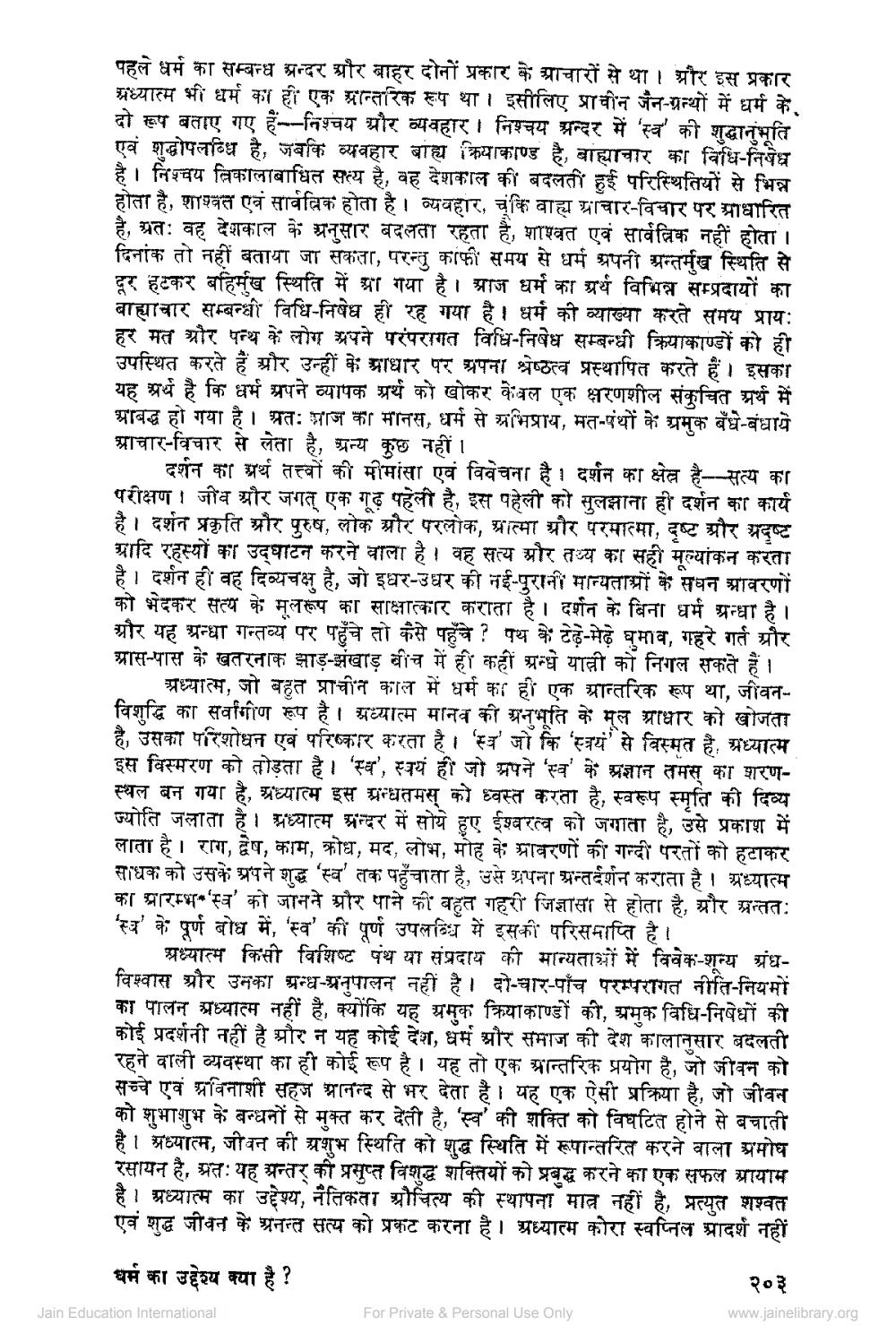Book Title: Dharm Ka Uddesh Kya Hai Author(s): Amarmuni Publisher: Z_Panna_Sammikkhaye_Dhammam_Part_01_003408_HR.pdf View full book textPage 9
________________ पहले धर्म का सम्बन्ध अन्दर और बाहर दोनों प्रकार के प्राचारों से था। और इस प्रकार अध्यात्म भी धर्म का ही एक प्रान्तरिक रूप था। इसीलिए प्राचीन जैन-ग्रन्थों में धर्म के. दो रूप बताए गए हैं---निश्चय और व्यवहार । निश्चय अन्दर में 'स्व' की शुद्धानुभूति एवं शुद्धोपलब्धि है, जबकि व्यवहार बाह्य क्रियाकाण्ड है, बाह्याचार का विधि-निषेध है। निश्चय त्रिकालाबाधित सत्य है, वह देशकाल की बदलती हई परिस्थितियों से भिन्न होता है, शाश्वत एवं सार्वत्रिक होता है। व्यवहार, चूंकि बाह्य प्राचार-विचार पर आधारित है, अतः वह देशकाल के अनुसार बदलता रहता है, शाश्वत एवं सार्वत्रिक नहीं होता। दिनांक तो नहीं बताया जा सकता, परन्तु काफी समय से धर्म अपनी अन्तर्मुख स्थिति से दूर हटकर बहिर्मुख स्थिति में आ गया है। आज धर्म का अर्थ विभिन्न सम्प्रदायों का बाह्याचार सम्बन्धी विधि-निषेध ही रह गया है। धर्म की व्याख्या करते समय प्रायः हर मत और पन्थ के लोग अपने परंपरागत विधि-निषेध सम्बन्धी क्रियाकाण्डों को ही उपस्थित करते है और उन्हीं के आधार पर अपना श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करते हैं। इसका यह अर्थ है कि धर्म अपने व्यापक अर्थ को खोकर केवल एक क्षरणशील संकुचित अर्थ में आबद्ध हो गया है। अतः माज का मानस, धर्म से अभिप्राय, मत-पंथों के अमुक बँधे-बंधाये आचार-विचार से लेता है, अन्य कुछ नहीं।। दर्शन का अर्थ तत्त्वों की मीमांसा एवं विवेचना है । दर्शन का क्षेत्र है-सत्य का परीक्षण। जीव और जगत् एक गूढ़ पहेली है, इस पहेली को सुलझाना ही दर्शन का कार्य है। दर्शन प्रकृति और पुरुष, लोक और परलोक, प्रात्मा और परमात्मा, दृष्ट और अदृष्ट प्रादि रहस्यों का उद्घाटन करने वाला है। वह सत्य और तथ्य का सही मूल्यांकन करता है। दर्शन ही वह दिव्यचक्षु है, जो इधर-उधर की नई-पुरानी मान्यताओं के सघन आवरणों को भेदकर सत्य के मूलरूप का साक्षात्कार कराता है। दर्शन के बिना धर्म अन्धा है। और यह अन्धा गन्तव्य पर पहुँचे तो कैसे पहुँचे? पथ के टेढ़े-मेढ़े घुमाव, गहरे गर्त और आस-पास के खतरनाक झाड़-झंखाड़ बीच में ही कहीं अन्धे यात्री को निगल सकते हैं। अध्यात्म, जो बहुत प्राचीन काल में धर्म का ही एक अान्तरिक रूप था, जीवनविशुद्धि का सर्वागीण रूप है। अध्यात्म मानव की अनुभूति के मूल आधार को खोजता है, उसका परिशोधन एवं परिष्कार करता है। 'स्व' जो कि 'स्त्रयं' से विस्मत है, अध्यात्म इस विस्मरण को तोड़ता है। 'स्व', स्वयं ही जो अपने 'स्व' के प्रज्ञान तमस् का शरणस्थल बन गया है, अध्यात्म इस अन्धतमस् को ध्वस्त करता है, स्वरूप स्मृति की दिव्य ज्योति जलाता है। अध्यात्म अन्दर में सोये हुए ईश्वरत्व को जगाता है, उसे प्रकाश में लाता है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के प्रावरणों की गन्दी परतों को हटाकर साधक को उसके अपने शुद्ध 'स्व' तक पहुँचाता है, उसे अपना अन्तर्दर्शन कराता है। अध्यात्म का प्रारम्भ 'स्व' को जानने और पाने की बहुत गहरी जिज्ञासा से होता है, और अन्ततः 'स्व' के पूर्ण बोध में, 'स्व' की पूर्ण उपलब्धि में इसकी परिसमाप्ति है। अध्यात्म किसी विशिष्ट पंथ या संप्रदाय की मान्यताओं में विवेक-शून्य अंधविश्वास और उनका अन्ध-अनुपालन नहीं है। दो-चार-पाँच परम्परागत नीति-नियमों का पालन अध्यात्म नहीं है, क्योंकि यह अमक क्रियाकाण्डों की, अमक विधि-निषेधों की कोई प्रदर्शनी नहीं है और न यह कोई देश, धर्म और समाज की देश कालानुसार बदलती रहने वाली व्यवस्था का ही कोई रूप है। यह तो एक अान्तरिक प्रयोग है, जो जीवन को सच्चे एवं अविनाशी सहज मानन्द से भर देता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जो जीवन को शुभाशुभ के बन्धनों से मुक्त कर देती है, 'स्व' की शक्ति को विघटित होने से बचाती है। अध्यात्म, जीवन की अशुभ स्थिति को शुद्ध स्थिति में रूपान्तरित करने वाला अमोघ रसायन है, अतः यह अन्तर् की प्रसुप्त विशुद्ध शक्तियों को प्रबुद्ध करने का एक सफल आयाम है। अध्यात्म का उद्देश्य, नैतिकता औचित्य की स्थापना मात्र नहीं है, प्रत्युत शश्वत एवं शुद्ध जीवन के अनन्त सत्य को प्रकट करना है। अध्यात्म कोरा स्वप्निल प्रादर्श नहीं धर्म का उद्देश्य क्या है ? २०३ Jain Education Intemational For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 7 8 9 10