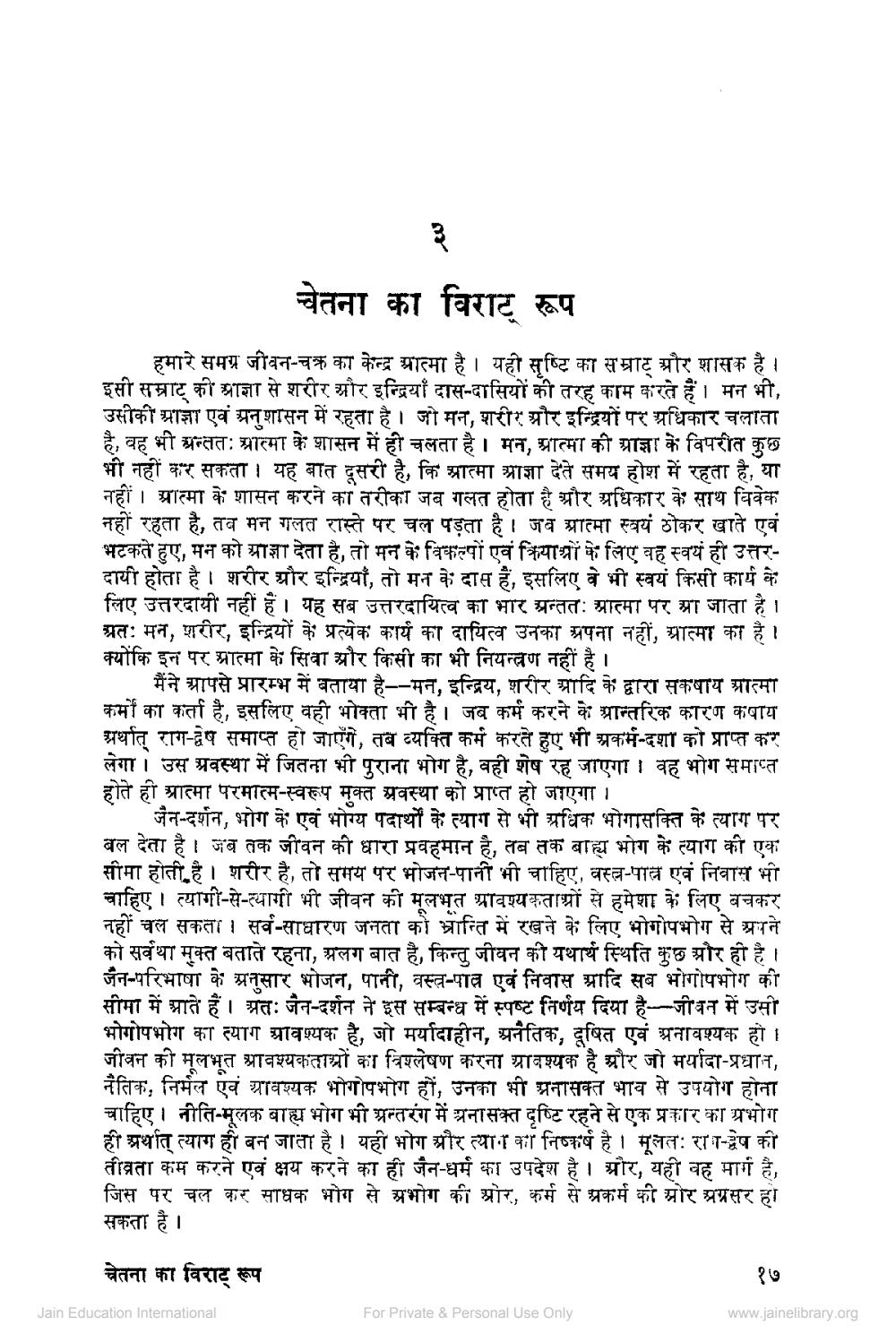Book Title: Chetna Ka Virat Swarup Author(s): Amarmuni Publisher: Z_Panna_Sammikkhaye_Dhammam_Part_01_003408_HR.pdf View full book textPage 1
________________ चेतना का विराट रूप हमारे समग्र जीवन-चक्र का केन्द्र प्रात्मा है। यही सष्टि का सम्राट और शासक है। इसी सम्राट की आज्ञा से शरीर और इन्द्रियाँ दास-दासियों की तरह काम करते हैं। मन भी, उसीकी आज्ञा एवं अनुशासन में रहता है। जो मन, शरीर और इन्द्रियों पर अधिकार चलाता है, वह भी अन्तत: आत्मा के शासन में ही चलता है। मन, आत्मा की आज्ञा के विपरीत कुछ भी नहीं कर सकता। यह बात दूसरी है, कि आत्मा आज्ञा देते समय होश में रहता है, या नहीं। प्रात्मा के शासन करने का तरीका जब गलत होता है और अधिकार के साथ विवेक नहीं रहता है, तब मन गलत रास्ते पर चल पड़ता है। जब आत्मा स्वयं ठोकर खाते एवं भटकते हुए, मन को प्राज्ञा देता है, तो मन के विकल्पों एवं क्रियाओं के लिए वह स्वयं ही उत्तरदायी होता है। शरीर और इन्द्रियाँ, तो मन के दास है, इसलिए वे भी स्वयं किसी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। यह सब उत्तरदायित्व का भार अन्ततः आत्मा पर आ जाता है । अतः मन, शरीर, इन्द्रियों के प्रत्येक कार्य का दायित्व' उनका अपना नहीं, प्रात्मा का है। क्योंकि इन पर आत्मा के सिवा और किसी का भी नियन्त्रण नहीं है। ___मैंने आपसे प्रारम्भ में बताया है--मन, इन्द्रिय, शरीर आदि के द्वारा सकषाय आत्मा कर्मों का कर्ता है, इसलिए वही भोक्ता भी है। जब कर्म करने के आन्तरिक कारण कषाय अर्थात राग-द्वेष समाप्त हो जाएंगे, तब व्यक्ति कर्म करते हए भी अकर्म-दशा को प्राप्त कर लेगा। उस अवस्था में जितना भी पुराना भोग है, वही शेष रह जाएगा। वह भोग समाप्त होते ही प्रात्मा परमात्म-स्वरूप मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। जैन-दर्शन, भोग के एवं भोग्य पदार्थों के त्याग से भी अधिक भोगासक्ति के त्याग पर बल देता है। जब तक जीवन की धारा प्रवहमान है, तब तक बाह्य भोग के त्याग की एक सीमा होती है। शरीर है, तो समय पर भोजन-पानी भी चाहिए, वस्त्र-पात्र एवं निवास भी चाहिए। त्यागी-से-त्यागी भी जीवन की मूलभत आवश्यकताओं से हमेशा के लिए बचकर नहीं चल सकता। सर्व-साधारण जनता को भ्रान्ति में रखने के लिए भोगोपभोग से अपने को सर्वथा मुक्त बताते रहना, अलग बात है, किन्तु जीवन की यथार्थ स्थिति कुछ और ही है। जैन-परिभाषा के अनुसार भोजन, पानी, वस्त्र-पान एवं निवास आदि सब भोगोपभोग की सीमा में आते हैं। अतः जैन-दर्शन ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्णय दिया है-जीवन में उसी भोगोपभोग का त्याग आवश्यक है, जो मर्यादाहीन, अनैतिक, दूषित एवं अनावश्यक हो । जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का विश्लेषण करना आवश्यक है और जो मर्यादा-प्रधान, नैतिक, निर्मल एवं आवश्यक भोगोपभोग हों, उनका भी अनासक्त भाव से उपयोग होना चाहिए। नीति-मूलक बाह्य भोग भी अन्तरंग में अनासक्त दृष्टि रहने से एक प्रकार का प्रभोग ही अर्थात् त्याग ही बन जाता है। यही भोग और त्याग का निष्कर्ष है। मूलतः राग-द्वेष की तीव्रता कम करने एवं क्षय करने का ही जैन-धर्म का उपदेश है। और, यही वह मार्ग है, जिस पर चल कर साधक भोग से अभोग की ओर, कर्म से अकर्म की ओर अग्रसर हो सकता है। चेतना का विराट रूप Jain Education Intemational For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10