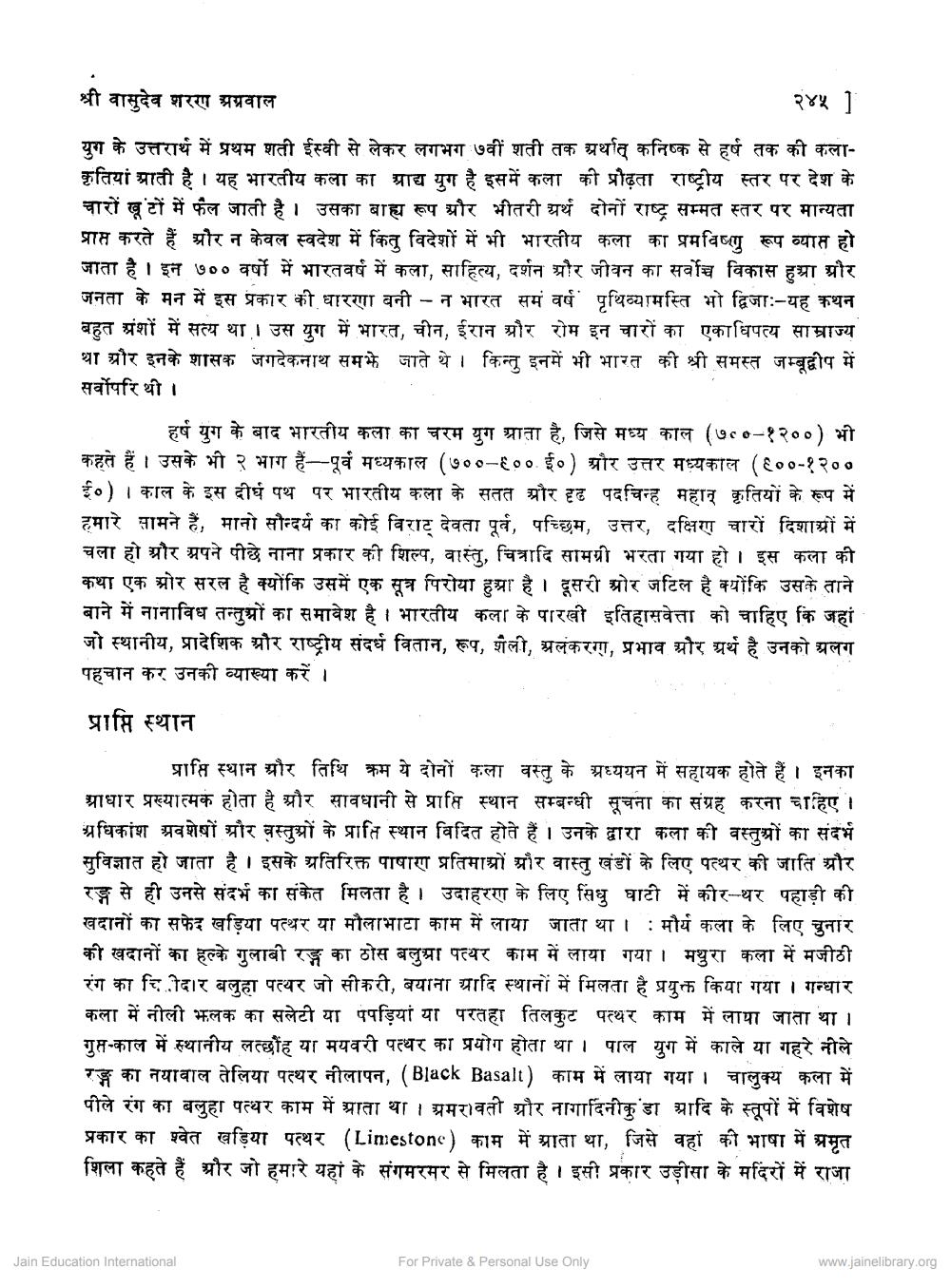Book Title: Bharatiya Kala ke Mukhya Tattva Author(s): Vasudev S Agarwal Publisher: Z_Jinvijay_Muni_Abhinandan_Granth_012033.pdf View full book textPage 3
________________ श्री वासुदेव शरण अग्रवाल २४५ ] युग के उत्तरार्थ में प्रथम शती ईस्वी से लेकर लगभग ७वीं शती तक अर्थात् कनिष्क से हर्ष तक की कलाकृतियां आती है । यह भारतीय कला का प्राद्य युग है इसमें कला की प्रौढ़ता राष्ट्रीय स्तर पर देश के चारों खूटों में फैल जाती है । उसका बाह्य रूप और भीतरी अर्थ दोनों राष्ट्र सम्मत स्तर पर मान्यता प्राप्त करते हैं और न केवल स्वदेश में किंतु विदेशों में भी भारतीय कला का प्रमविष्णु रूप व्याप्त हो जाता है । इन ७०० वर्षो में भारतवर्ष में कला, साहित्य, दर्शन और जीवन का सर्वोच्च विकास हुआ और जनता के मन में इस प्रकार की धारणा बनी - न भारत समं वर्ष पृथिव्यामस्ति भो द्विजाः- यह कथन बहुत अंशों में सत्य था । उस युग में भारत, चीन, ईरान और रोम इन चारों का एकाधिपत्य साम्राज्य था और इनके शासक जगदेकनाथ समझे जाते थे । किन्तु इनमें भी भारत की श्री समस्त जम्बूद्वीप में सर्वोपरि थी । हर्ष युग के बाद भारतीय कला का चरम युग प्राता है, जिसे मध्य काल ( ७०० - १२०० ) भी कहते हैं । उसके भी २ भाग हैं- पूर्व मध्यकाल ( ७००-६०० ई० ) और उत्तर मध्यकाल ( १००-१२०० ई० ) । काल के इस दीर्घ पथ पर भारतीय कला के सतत और दृढ पदचिन्ह महान कृतियों के रूप में हमारे सामने हैं, मानो सौन्दर्य का कोई विराट् देवता पूर्व पच्छिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में चला हो और अपने पीछे नाना प्रकार की शिल्प, वास्तु, चित्रादि सामग्री भरता गया हो। इस कला की कथा एक ओर सरल है क्योंकि उसमें एक सूत्र पिरोया हुआ है । दूसरी ओर जटिल है क्योंकि उसके ताने बाने में नानाविध तन्तुनों का समावेश है। भारतीय कला के पारखी इतिहासवेत्ता को चाहिए कि जहां जो स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय संदर्भ वितान, रूप, शैली, अलंकरण, प्रभाव और अर्थ है उनको अलग पहचान कर उनकी व्याख्या करें । प्राप्ति स्थान प्राप्ति स्थान और तिथि क्रम ये दोनों कला वस्तु के अध्ययन में सहायक होते हैं । इनका श्राधार प्रख्यात्मक होता है और सावधानी से प्राप्ति स्थान सम्बन्धी सूचना का संग्रह करना चाहिए । अधिकांश अवशेषों और वस्तुओं के प्राति स्थान विदित होते हैं । उनके द्वारा कला की वस्तुओं का संदर्भ सुविज्ञात हो जाता है । इसके अतिरिक्त पाषाण प्रतिमानों और वास्तु खंडों के लिए पत्थर की जाति और रङ्ग से ही उनसे संदर्भ का संकेत मिलता है । उदाहरण के लिए सिंधु घाटी में कीर-थर पहाड़ी की खदानों का सफेद खड़िया पत्थर या मौलाभाटा काम में लाया जाता था । : मौर्य कला के लिए चुनार की खदानों का हल्के गुलाबी रङ्ग का ठोस बलुआ पत्थर काम में लाया गया। मथुरा कला में मजीठी रंग काचिदार बलुहा पत्थर जो सीकरी, बयाना यादि स्थानों में मिलता है प्रयुक्त किया गया । गन्धार कला में नीली झलक का सलेटी या पपड़ियां या परतहा तिलकुट पत्थर काम में लाया जाता था । गुप्त-काल में स्थानीय लछौंह या मयवरी पत्थर का प्रयोग होता था । पाल युग में काले या गहरे नीले रङ्ग का नयावाल तेलिया पत्थर नीलापन, ( Black Basalt) काम में लाया गया । चालुक्य कला में पीले रंग का बलुहा पत्थर काम में आता था । अमरावती और नागादिनीकुडा आदि के स्तूपों में विशेष प्रकार का श्वेत खड़िया पत्थर (Limestone ) काम में आता था, जिसे वहां की भाषा में अमृत शिला कहते हैं और जो हमारे यहां के संगमरमर से मिलता है। इसी प्रकार उड़ीसा के मदिरों में राजा Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17