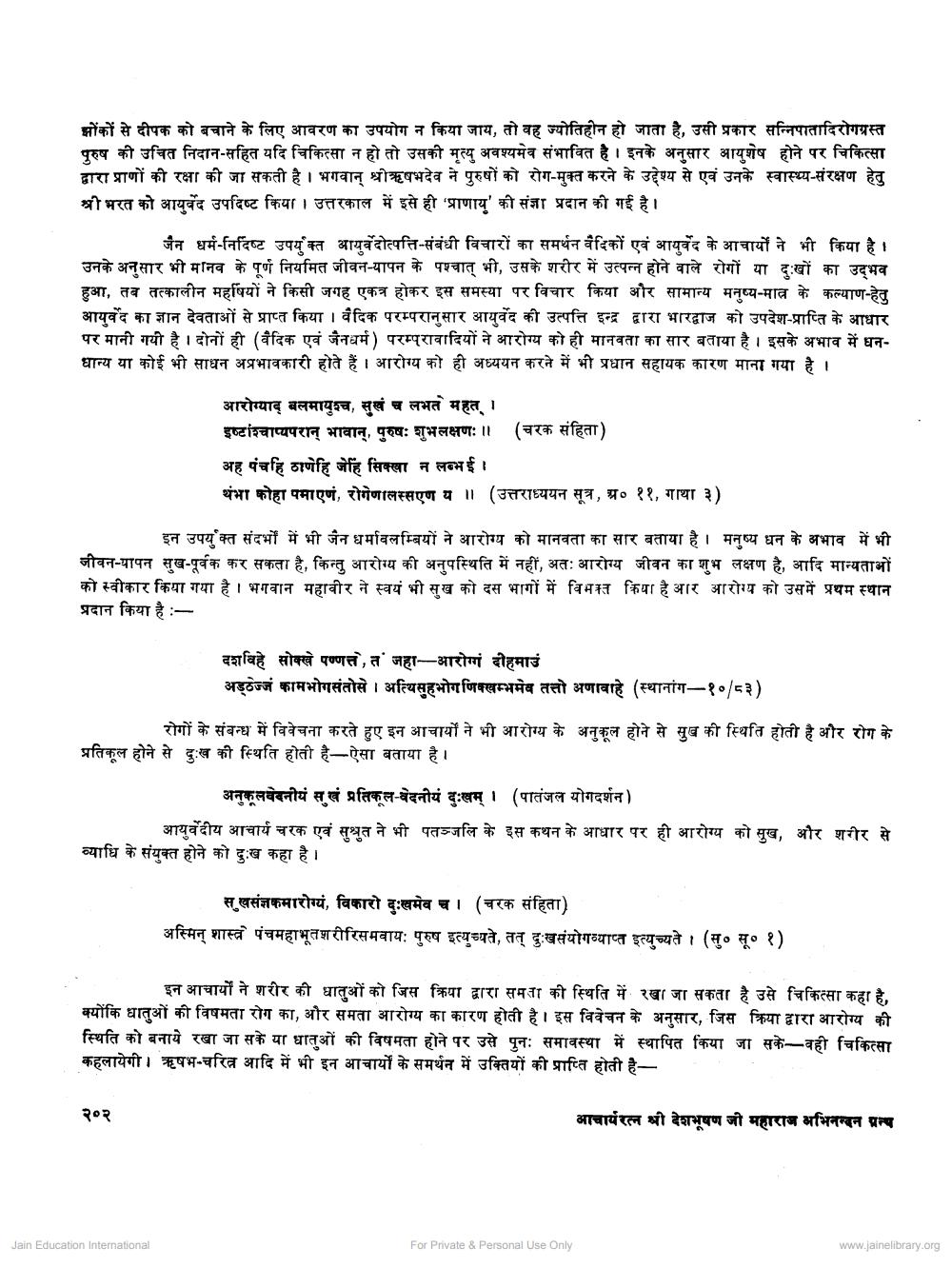Book Title: Ayurved aur Jain Dharm Ek Vivechanatmaka Adhyayan Author(s): Pramod Malviya, Shobha Mowar, Yagnadutta Shukl, Purnachandra Jain Publisher: Z_Deshbhushanji_Maharaj_Abhinandan_Granth_012045.pdf View full book textPage 2
________________ झोंकों से दीपक को बचाने के लिए आवरण का उपयोग न किया जाय, तो वह ज्योतिहीन हो जाता है, उसी प्रकार सन्निपातादिरोगग्रस्त पुरुष की उचित निदान-सहित यदि चिकित्सा न हो तो उसकी मृत्यु अवश्यमेव संभावित है । इनके अनुसार आयुशेष होने पर चिकित्सा द्वारा प्राणों की रक्षा की जा सकती है । भगवान् श्रीऋषभदेव ने पुरुषों को रोग-मुक्त करने के उद्देश्य से एवं उनके स्वास्थ्य-संरक्षण हेतु श्री भरत को आयुर्वेद उपदिष्ट किया। उत्तरकाल में इसे ही 'प्राणायु' की संज्ञा प्रदान की गई है। जैन धर्म-निर्दिष्ट उपर्युक्त आयुर्वेदोत्पत्ति-संबंधी विचारों का समर्थन वैदिकों एवं आयुर्वेद के आचार्यों ने भी किया है। उनके अनुसार भी मानव के पूर्ण नियमित जीवन-यापन के पश्चात् भी, उसके शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगों या दुःखों का उद्भव हुआ, तब तत्कालीन महर्षियों ने किसी जगह एकत्र होकर इस समस्या पर विचार किया और सामान्य मनुष्य-मात्र के कल्याण-हेतु आयर्वेद का ज्ञान देवताओं से प्राप्त किया । वैदिक परम्परानुसार आयुर्वेद की उत्पत्ति इन्द्र द्वारा भारद्वाज को उपदेश-प्राप्ति के आधार पर मानी गयी है । दोनों ही (वैदिक एवं जैनधर्म) परम्परावादियों ने आरोग्य को ही मानवता का सार बताया है। इसके अभाव में धनधान्य या कोई भी साधन अप्रभावकारी होते हैं। आरोग्य को ही अध्ययन करने में भी प्रधान सहायक कारण माना गया है । आरोग्याद् बलमायुश्च, सुखं च लभते महत् । इष्टांश्चाप्यपरान् भावान्, पुरुषः शुभलक्षणः ॥ (चरक संहिता) अह पंचहि ठाणेहि जेहि सिक्खा न लन्भई। थंभा कोहा पमाएणं, रोगेणालस्सएण य ॥ (उत्तराध्ययन सूत्र, अ० ११, गाथा ३) इन उपर्युक्त संदर्भो में भी जैन धर्मावलम्बियों ने आरोग्य को मानवता का सार बताया है। मनुष्य धन के अभाव में भी जीवन-यापन सुख-पूर्वक कर सकता है, किन्तु आरोग्य की अनुपस्थिति में नहीं, अत: आरोग्य जीवन का शुभ लक्षण है, आदि मान्यताओं को स्वीकार किया गया है। भगवान महावीर ने स्वयं भी सुख को दस भागों में विभक्त किया है आर आरोग्य को उसमें प्रथम स्थान प्रदान किया है : दशविहे सोक्खे पण्णत्ते, तजहा-आरोग्गं दोहमाउं अड्ठेज्जं कामभोगसंतोसे । अत्थिसुहभोगणिक्खम्भमेव तत्तो अणावाहे (स्थानांग-१०/८३) रोगों के संबन्ध में विवेचना करते हुए इन आचार्यों ने भी आरोग्य के अनुकूल होने से सुख की स्थिति होती है और रोग के प्रतिकूल होने से दुःख की स्थिति होती है-ऐसा बताया है। अनुकूलवेदनीयं सुखं प्रतिकूल-वेदनीयं दुःखम् । (पातंजल योगदर्शन) आयुर्वेदीय आचार्य चरक एवं सुश्रुत ने भी पतञ्जलि के इस कथन के आधार पर ही आरोग्य को सुख, और शरीर से व्याधि के संयुक्त होने को दुःख कहा है। सु खसंज्ञकमारोग्यं, विकारो दुःखमेव च । (चरक संहिता) अस्मिन् शास्त्र पंचमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुष इत्युच्यते, तत् दुःखसंयोगव्याप्त इत्युच्यते । (सु० सू० १) इन आचार्यों ने शरीर की धातुओं को जिस क्रिया द्वारा समता की स्थिति में रखा जा सकता है उसे चिकित्सा कहा है, क्योंकि धातुओं की विषमता रोग का, और समता आरोग्य का कारण होती है। इस विवेचन के अनुसार, जिस क्रिया द्वारा आरोग्य की स्थिति को बनाये रखा जा सके या धातुओं की विषमता होने पर उसे पुनः समावस्था में स्थापित किया जा सके-बही चिकित्सा कहलायेगी। ऋषभ-चरित्र आदि में भी इन आचार्यों के समर्थन में उक्तियों की प्राप्ति होती है २०२ आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन अन्य Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4