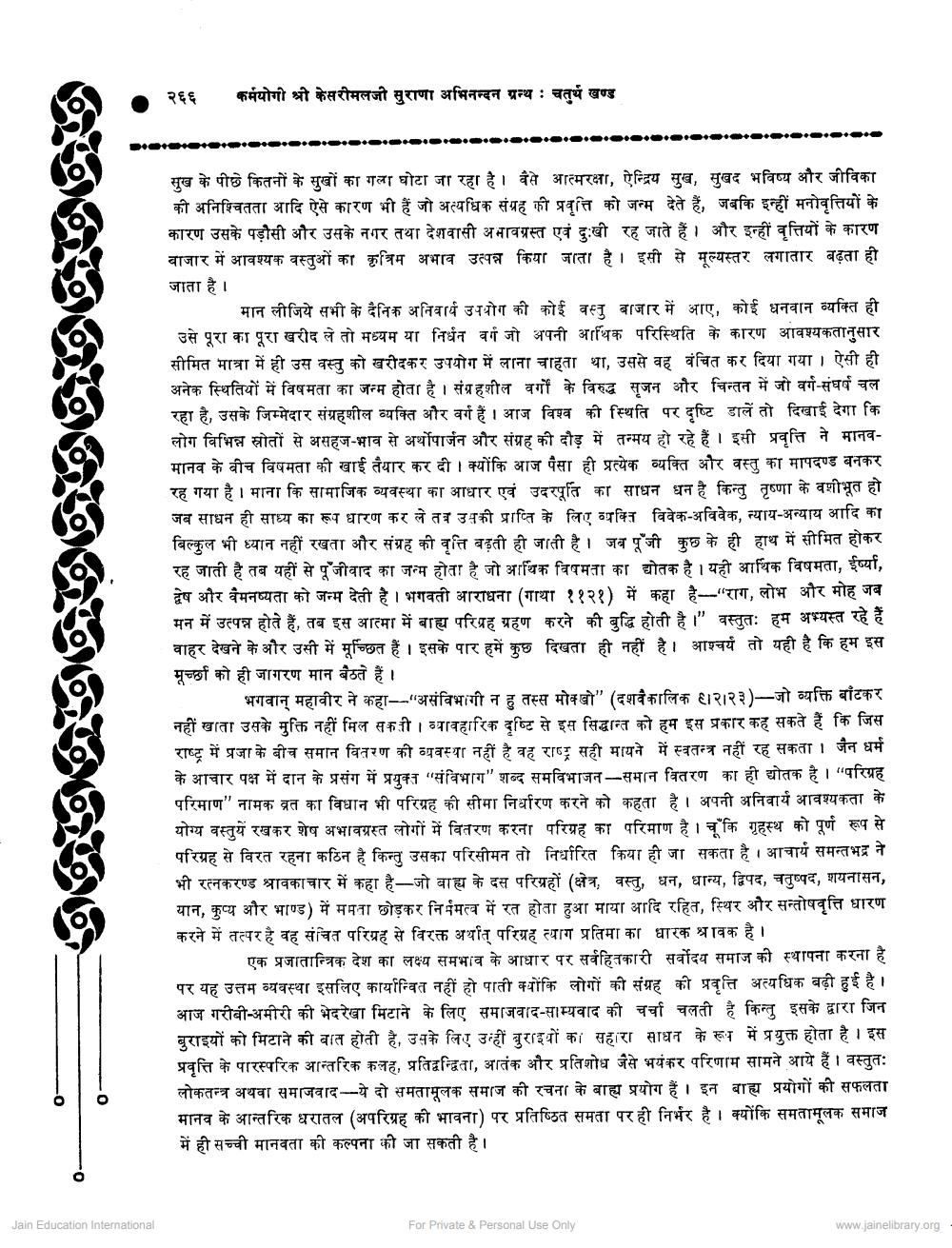Book Title: Aparigrahavad Arthik Samta ka Adhar Author(s): Fulchandra Jain Shatri Publisher: Z_Kesarimalji_Surana_Abhinandan_Granth_012044.pdf View full book textPage 2
________________ Jain Education International २६६ कर्मयोगी श्री केसरीमलजी सुराणा अभिनन्दन ग्रन्थ : चतुर्थ खण्ड सुख के पीछे कितनों के सुखों का गला घोटा जा रहा है। वैसे आत्मरक्षा, ऐन्द्रिय सुख, को अनिश्चितता आदि ऐसे कारण भी हैं जो अत्यधिक संग्रह की प्रवृत्ति को जन्म देते हैं, कारण उसके पड़ोसी और उसके नगर तथा देशवासी अनावग्रस्त एवं दुःखी रह जाते हैं बाजार में आवश्यक वस्तुओं का कृत्रिम अभाव उत्पन्न किया जाता है। इसी से जाता है। सुखद भविष्य और जीविका जबकि इन्हीं मनोवृत्तियों के और इन्हीं वृत्तियों के कारण मूल्यस्तर लगातार बढ़ता ही मान लीजिये सभी के दैनिक अनिवार्य उपयोग की कोई वस्तु बाजार में आए. कोई धनवान व्यक्ति ही उसे पूरा का पूरा खरीद ले तो मध्यम या निर्धन वर्ग जो अपनी आर्थिक परिस्थिति के कारण आवश्यकतानुसार सीमित मात्रा में ही उस वस्तु को खरीदकर उपयोग में लाना चाहता था, उससे वह वंचित कर दिया गया। ऐसी ही अनेक स्थितियों में विषमता का जन्म होता है संग्रहीत वर्गों के विरुद्ध सूजन और चिन्तन में जो वर्ग संपर्व चल रहा है, उसके जिम्मेदार संग्रहसील व्यक्ति और वर्ग हैं। आज विश्व की स्थिति पर दृष्टि डालें तो दिखाई देगा कि लोग विभिन्न स्रोतों से असहज भाव से अर्थोपार्जन और संग्रह की दौड़ में तन्मय हो रहे हैं। इसी प्रवृत्ति मे मानवमानव के बीच विषमता की खाई तैयार कर दी। क्योंकि आज पैसा ही प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु का मापदण्ड बनकर रह गया है। माना कि सामाजिक व्यवस्था का आधार एवं उदरपूर्ति का साधन धन है किन्तु तृष्णा के वशीभूत हो जब साधन ही साध्य का रूप धारण कर ले तत्र उसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति विवेक अविवेक, न्याय-अन्याय आदि का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता और संग्रह की वृत्ति बढ़ती ही जाती है। जब पूँजी कुछ के ही हाथ में सीमित होकर रह जाती है तब यहीं से पूँजीवाद का जन्म होता है जो आर्थिक विषमता का द्योतक है। यही आर्थिक विषमता, ईर्ष्या द्वेष और वैमनष्यता को जन्म देती है । भगवती आराधना (गाथा ११२१ ) में कहा है- "राग, लोभ और मोह जब मन में उत्पन्न होते हैं, तब इस आत्मा में बाह्य परिग्रह ग्रहण करने की बुद्धि होती है ।" वस्तुतः हम अभ्यस्त रहे हैं। बाहर देखने के और उसी में मूच्छित हैं। इसके पार हमें कुछ दिखता ही नहीं है। आश्चर्य तो यही है कि हम इस मूर्च्छा को ही जागरण मान बैठते हैं। भगवान् महावीर ने कहा--"असंविभागी न हु तस्स मोक्खो" ( दशवैकालिक है।२।२३ ) - जो व्यक्ति बाँटकर नहीं खाता उसके मुक्ति नहीं मिल सकती । व्यावहारिक दृष्टि से इस सिद्धान्त को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जिस राष्ट्र में प्रजा के बीच समान वितरण की व्यवस्था नहीं है वह राष्ट्र सही मायने में स्वतन्त्र नहीं रह सकता । जैन धर्म के आचार पक्ष में दान के प्रसंग में प्रयुक्त "संविभाग" शब्द समविभाजन - समान वितरण का ही द्योतक है । " परिग्रह परिमाण" नामक व्रत का विधान भी परिग्रह की सीमा निर्धारण करने को कहता है । अपनी अनिवार्य आवश्यकता के योग्य वस्तुयें रखकर शेष अभावग्रस्त लोगों में वितरण करना परिग्रह का परिमाण है। चूँकि गृहस्थ को पूर्ण रूप से परिग्रह से विरत रहना कठिन है किन्तु उसका परिसीमन तो निर्धारित किया ही जा सकता है आचार्य समन्तभद्र ने भी रत्नकरण्ड श्रावकाचार में कहा है- जो बाह्य के दस परिग्रहों (क्षेत्र, वस्तु, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, शयनासन, यान, कुप्य और भाण्ड) में ममता छोड़कर निर्ममत्व में रत होता हुआ माया आदि रहित, स्थिर और सन्तोषवृत्ति धारण करने में तत्पर है वह संचित परिग्रह से विरक्त अर्थात् परिवह स्वाग प्रतिमा का 1 धारक धावक है। एक प्रजातान्त्रिक देश का लक्ष्य समभाव के आधार पर सर्वहितकारी सर्वोदय समाज की स्थापना करना है। पर यह उत्तम व्यवस्था इसलिए कार्यान्वित नहीं हो पाती क्योंकि लोगों की संग्रह की प्रवृत्ति अत्यधिक बढ़ी हुई है । आज गरीबी अमीरी की भेदरेखा मिटाने के लिए समाजवाद साम्यवाद की चर्चा चलती है किन्तु इसके द्वारा जिन बुराइयों को मिटाने की बात होती है, उसके लिए उन्हीं बुराइयों का सहारा साधन के रूप में प्रयुक्त होता है । इस प्रवृत्ति के पारस्परिक आन्तरिक कलह आतंक और प्रतिशोध जैसे भयंकर परिणाम सामने आये है। वस्तुतः लोकतन्त्र अथवा समाजवाद -- ये दो समतामूलक समाज की रचना के बाह्य प्रयोग हैं। इन मानव के आन्तरिक धरातल (अपरिग्रह की भावना) पर प्रतिष्ठित समता पर ही निर्भर है। में ही सच्ची मानवता की कल्पना की जा सकती है। बाह्य प्रयोगों की सफलता क्योंकि समतामूलक समाज For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org.Page Navigation
1 2 3 4