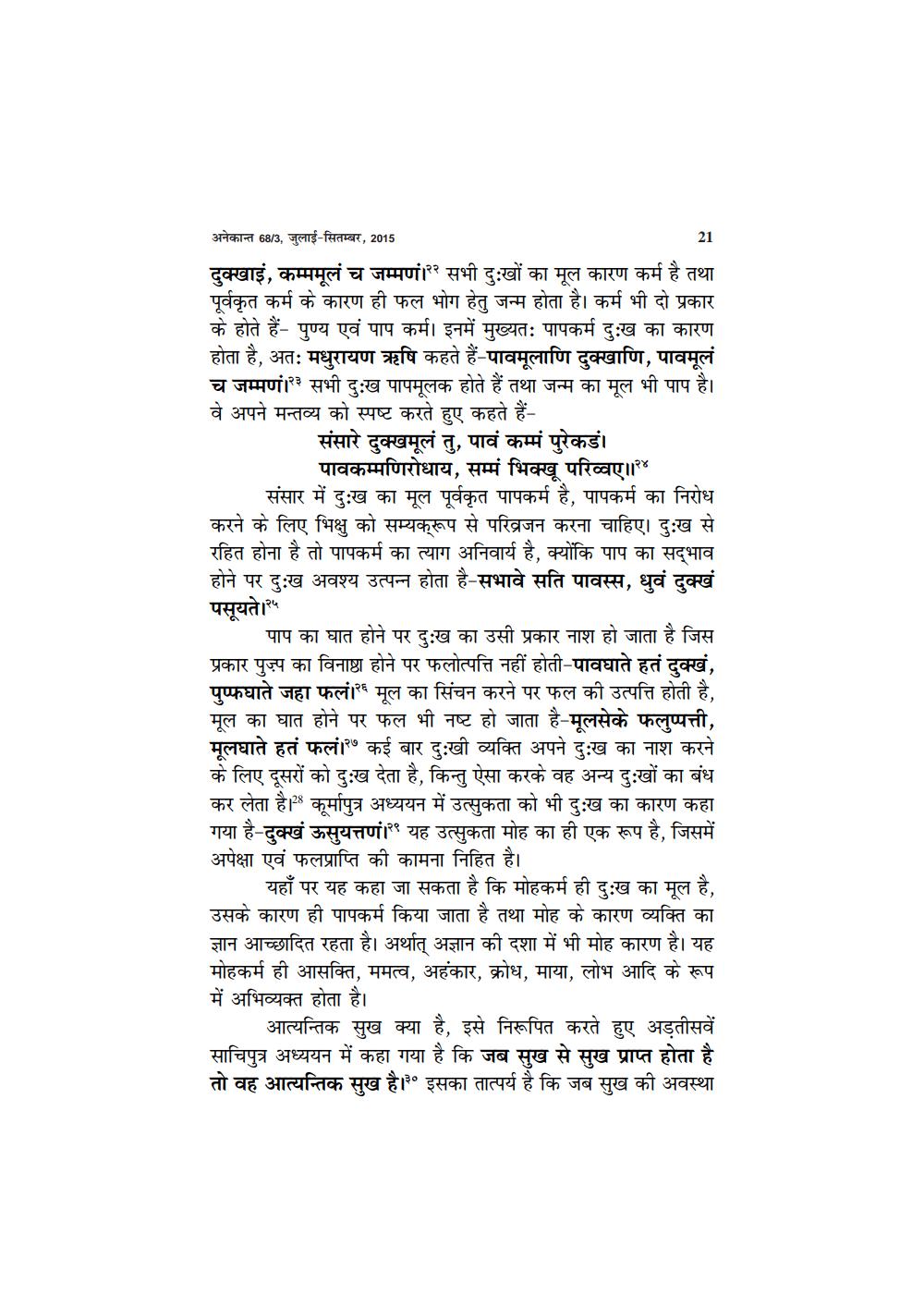________________
अनेकान्त 68/3, जुलाई-सितम्बर, 2015 दुक्खाई, कम्ममूलं च जम्मण।२२ सभी दु:खों का मूल कारण कर्म है तथा पूर्वकृत कर्म के कारण ही फल भोग हेतु जन्म होता है। कर्म भी दो प्रकार के होते हैं- पुण्य एवं पाप कर्म। इनमें मुख्यतः पापकर्म दुःख का कारण होता है, अतः मधुरायण ऋषि कहते हैं-पावमूलाणि दुक्खाणि, पावमूलं च जम्मण।२३ सभी दुःख पापमूलक होते हैं तथा जन्म का मूल भी पाप है। वे अपने मन्तव्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं
संसारे दुक्खमूलं तु, पावं कम्मं पुरेकडं।
पावकम्मणिरोधाय, सम्मं भिक्खू परिव्वए॥४ संसार में दु:ख का मूल पूर्वकृत पापकर्म है, पापकर्म का निरोध करने के लिए भिक्षु को सम्यक्रूप से परिव्रजन करना चाहिए। दु:ख से रहित होना है तो पापकर्म का त्याग अनिवार्य है, क्योंकि पाप का सद्भाव होने पर दु:ख अवश्य उत्पन्न होता है-सभावे सति पावस्स, धुवं दक्खं पसूयते।५
पाप का घात होने पर दु:ख का उसी प्रकार नाश हो जाता है जिस प्रकार पूज्प का विनाष्ठा होने पर फलोत्पत्ति नहीं होती-पावघाते हतं दक्खं, पुष्फघाते जहा फल।२६ मूल का सिंचन करने पर फल की उत्पत्ति होती है, मूल का घात होने पर फल भी नष्ट हो जाता है-मूलसेके फलुप्पत्ती, मूलघाते हतं फल।७ कई बार दुःखी व्यक्ति अपने दुःख का नाश करने के लिए दूसरों को दु:ख देता है, किन्तु ऐसा करके वह अन्य दु:खों का बंध कर लेता है। कूर्मापुत्र अध्ययन में उत्सुकता को भी दुःख का कारण कहा गया है-दुक्खं ऊसुयत्तणं। यह उत्सुकता मोह का ही एक रूप है, जिसमें अपेक्षा एवं फलप्राप्ति की कामना निहित है।
यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि मोहकर्म ही दुःख का मूल है, उसके कारण ही पापकर्म किया जाता है तथा मोह के कारण व्यक्ति का ज्ञान आच्छादित रहता है। अर्थात् अज्ञान की दशा में भी मोह कारण है। यह मोहकर्म ही आसक्ति, ममत्व, अहंकार, क्रोध, माया, लोभ आदि के रूप में अभिव्यक्त होता है।
आत्यन्तिक सुख क्या है, इसे निरूपित करते हुए अड़तीसवें साचिपुत्र अध्ययन में कहा गया है कि जब सुख से सुख प्राप्त होता है तो वह आत्यन्तिक सुख है। इसका तात्पर्य है कि जब सुख की अवस्था