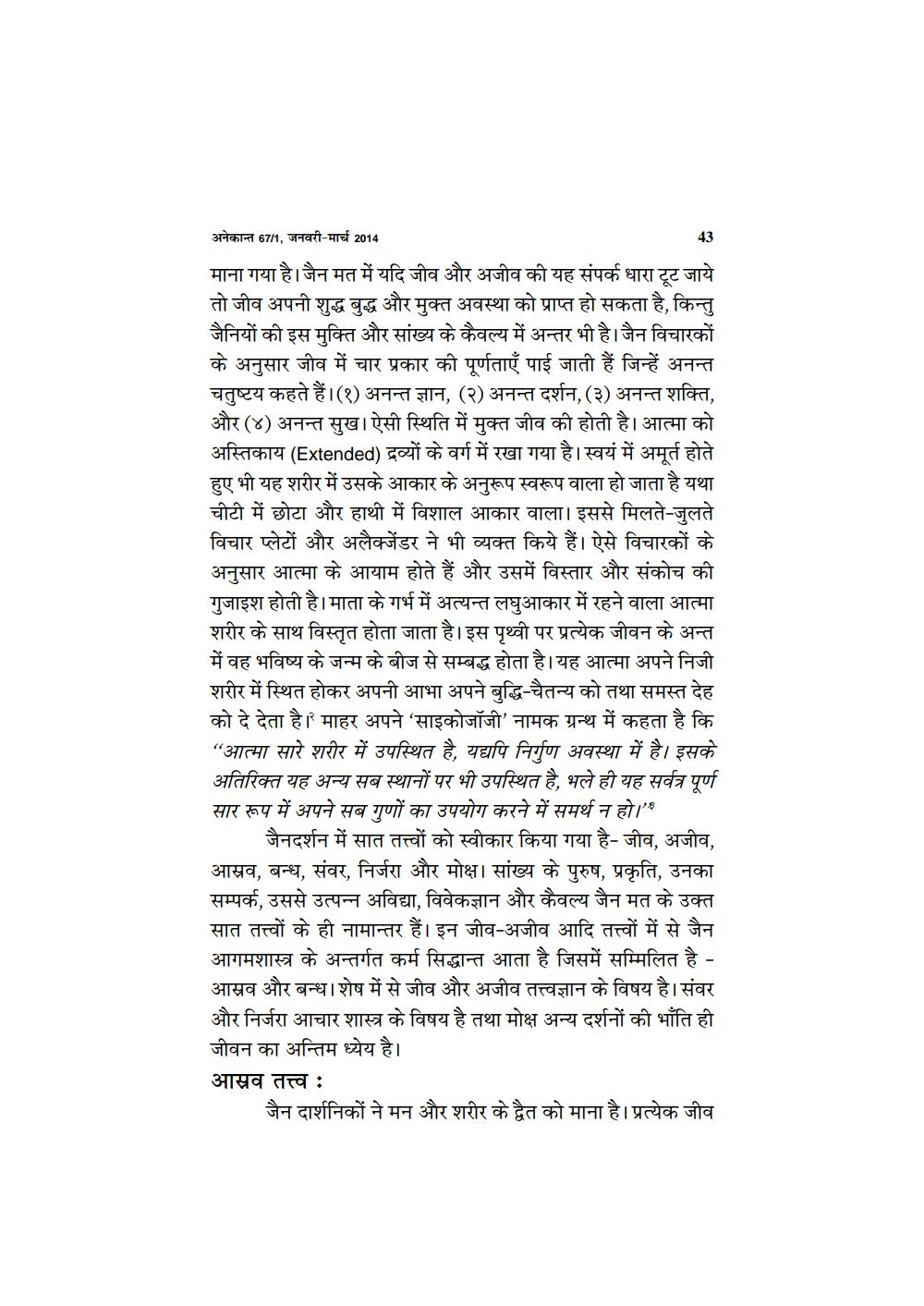________________
अनेकान्त 67/1, जनवरी-मार्च 2014 माना गया है। जैन मत में यदि जीव और अजीव की यह संपर्क धारा टूट जाये तो जीव अपनी शुद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त हो सकता है, किन्तु जैनियों की इस मुक्ति और सांख्य के कैवल्य में अन्तर भी है। जैन विचारकों के अनुसार जीव में चार प्रकार की पूर्णताएँ पाई जाती हैं जिन्हें अनन्त चतुष्टय कहते हैं। (१) अनन्त ज्ञान, (२) अनन्त दर्शन, (३) अनन्त शक्ति,
और (४) अनन्त सुख। ऐसी स्थिति में मुक्त जीव की होती है। आत्मा को अस्तिकाय (Extended) द्रव्यों के वर्ग में रखा गया है। स्वयं में अमूर्त होते हुए भी यह शरीर में उसके आकार के अनुरूप स्वरूप वाला हो जाता है यथा चीटी में छोटा और हाथी में विशाल आकार वाला। इससे मिलते-जुलते विचार प्लेटों और अलैक्जेंडर ने भी व्यक्त किये हैं। ऐसे विचारकों के अनुसार आत्मा के आयाम होते हैं और उसमें विस्तार और संकोच की गुजाइश होती है। माता के गर्भ में अत्यन्त लघुआकार में रहने वाला आत्मा शरीर के साथ विस्तृत होता जाता है। इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीवन के अन्त में वह भविष्य के जन्म के बीज से सम्बद्ध होता है। यह आत्मा अपने निजी शरीर में स्थित होकर अपनी आभा अपने बुद्धि-चैतन्य को तथा समस्त देह को दे देता है। माहर अपने ‘साइकोजॉजी' नामक ग्रन्थ में कहता है कि “आत्मा सारे शरीर में उपस्थित है, यद्यपि निर्गुण अवस्था में है। इसके अतिरिक्त यह अन्य सब स्थानों पर भी उपस्थित है, भले ही यह सर्वत्र पूर्ण सार रूप में अपने सब गुणों का उपयोग करने में समर्थ न हो।
जैनदर्शन में सात तत्त्वों को स्वीकार किया गया है- जीव. अजीव. आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। सांख्य के पुरुष, प्रकृति, उनका सम्पर्क, उससे उत्पन्न अविद्या, विवेकज्ञान और कैवल्य जैन मत के उक्त सात तत्त्वों के ही नामान्तर हैं। इन जीव-अजीव आदि तत्त्वों में से जैन आगमशास्त्र के अन्तर्गत कर्म सिद्धान्त आता है जिसमें सम्मिलित है - आस्रव और बन्ध। शेष में से जीव और अजीव तत्त्वज्ञान के विषय है। संवर और निर्जरा आचार शास्त्र के विषय है तथा मोक्ष अन्य दर्शनों की भाँति ही जीवन का अन्तिम ध्येय है। आस्रव तत्त्व :
जैन दार्शनिकों ने मन और शरीर के द्वैत को माना है। प्रत्येक जीव