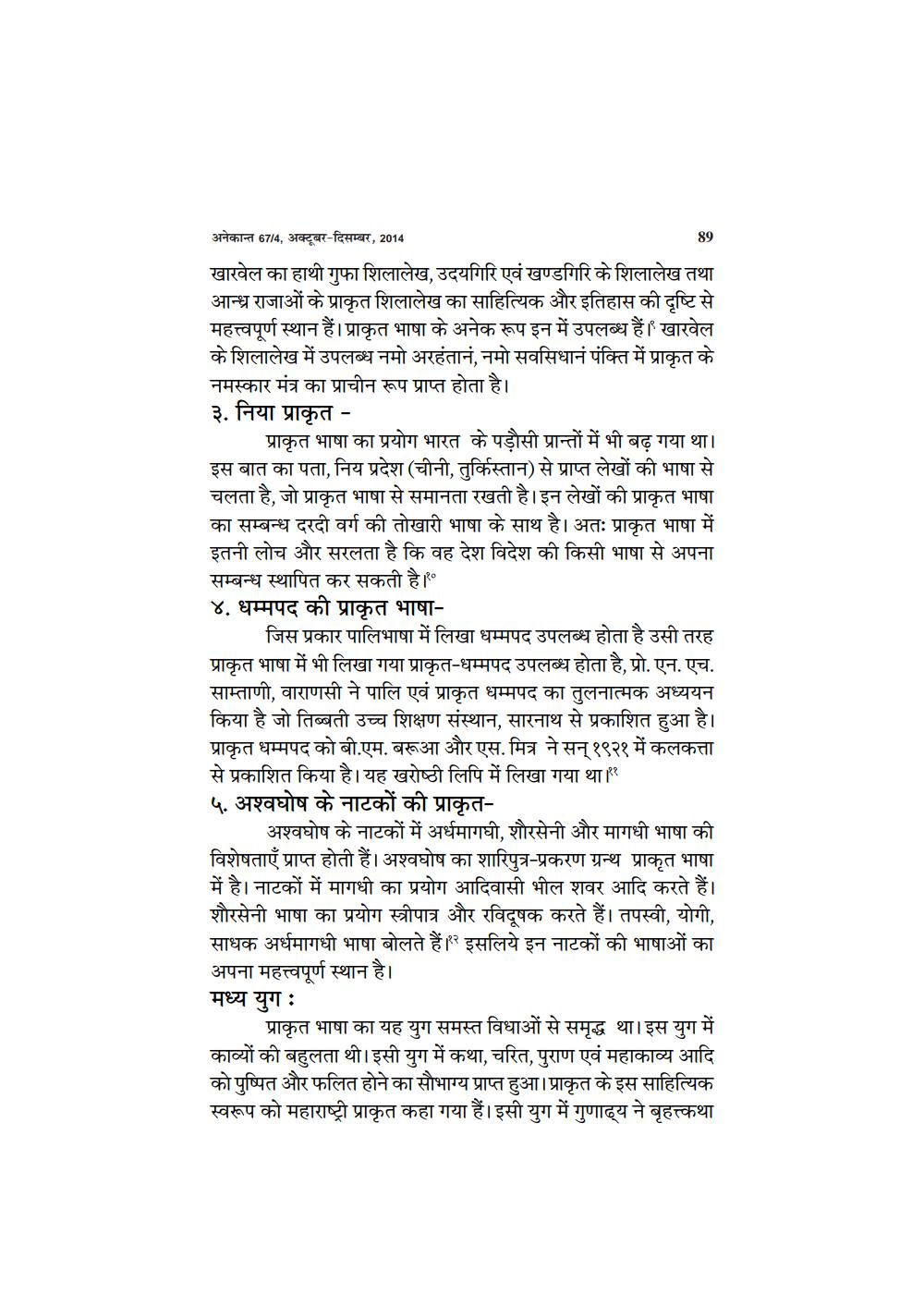________________
अनेकान्त 67/4, अक्टूबर-दिसम्बर, 2014 खारवेल का हाथी गुफा शिलालेख, उदयगिरि एवं खण्डगिरि के शिलालेख तथा आन्ध्र राजाओं के प्राकृत शिलालेख का साहित्यिक और इतिहास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। प्राकृत भाषा के अनेक रूप इन में उपलब्ध हैं। खारवेल के शिलालेख में उपलब्ध नमो अरहंतानं, नमो सवसिधानं पंक्ति में प्राकृत के नमस्कार मंत्र का प्राचीन रूप प्राप्त होता है। ३. निया प्राकृत -
प्राकृत भाषा का प्रयोग भारत के पड़ौसी प्रान्तों में भी बढ़ गया था। इस बात का पता, निय प्रदेश (चीनी, तुर्किस्तान) से प्राप्त लेखों की भाषा से चलता है, जो प्राकृत भाषा से समानता रखती है। इन लेखों की प्राकृत भाषा का सम्बन्ध दरदी वर्ग की तोखारी भाषा के साथ है। अतः प्राकत भाषा में इतनी लोच और सरलता है कि वह देश विदेश की किसी भाषा से अपना सम्बन्ध स्थापित कर सकती है। ४. धम्मपद की प्राकृत भाषा
__ जिस प्रकार पालिभाषा में लिखा धम्मपद उपलब्ध होता है उसी तरह प्राकृत भाषा में भी लिखा गया प्राकृत-धम्मपद उपलब्ध होता है, प्रो. एन. एच. साम्ताणी. वाराणसी ने पालि एवं प्राकृत धम्मपद का तुलनात्मक अध्ययन किया है जो तिब्बती उच्च शिक्षण संस्थान, सारनाथ से प्रकाशित हुआ है। प्राकृत धम्मपद को बी.एम.बरूआ और एस.मित्र ने सन् १९२१ में कलकत्ता से प्रकाशित किया है। यह खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था।११ ५. अश्वघोष के नाटकों की प्राकृत
अश्वघोष के नाटकों में अर्धमागधी, शौरसेनी और मागधी भाषा की विशेषताएँ प्राप्त होती हैं। अश्वघोष का शारिपुत्र-प्रकरण ग्रन्थ प्राकृत भाषा में है। नाटकों में मागधी का प्रयोग आदिवासी भील शवर आदि करते हैं। शौरसेनी भाषा का प्रयोग स्त्रीपात्र और रविदूषक करते हैं। तपस्वी, योगी, साधक अर्धमागधी भाषा बोलते हैं। इसलिये इन नाटकों की भाषाओं का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। मध्य युग ः
प्राकृत भाषा का यह युग समस्त विधाओं से समृद्ध था। इस युग में काव्यों की बहुलता थी। इसी युग में कथा, चरित, पुराण एवं महाकाव्य आदि को पुष्पित और फलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्राकृत के इस साहित्यिक स्वरूप को महाराष्ट्री प्राकृत कहा गया हैं। इसी युग में गुणाढ्य ने बृहत्कथा