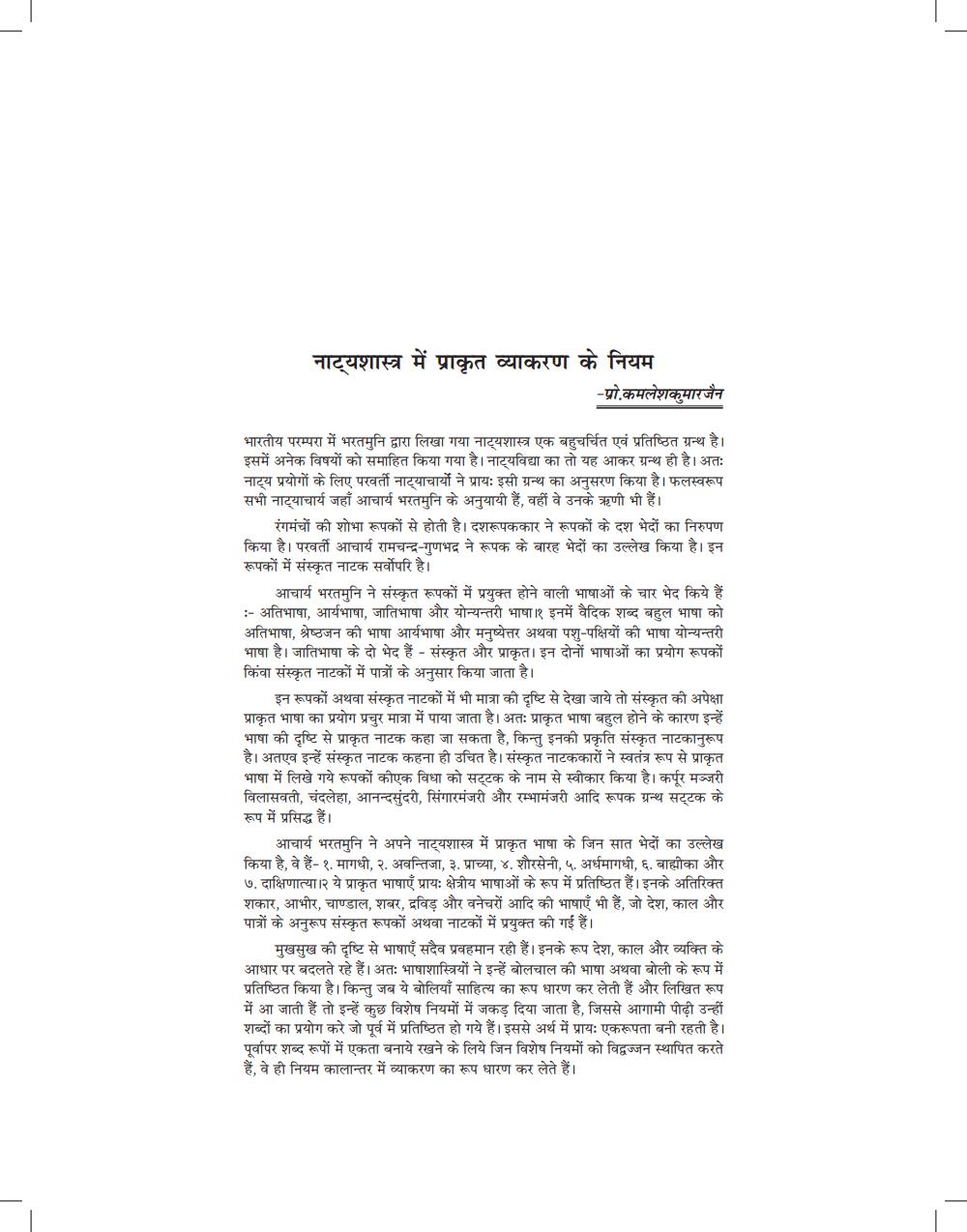________________
नाट्यशास्त्र में प्राकृत व्याकरण के नियम
- प्रो. कमलेशकुमार जैन
भारतीय परम्परा में भरतमुनि द्वारा लिखा गया नाट्यशास्त्र एक बहुचर्चित एवं प्रतिष्ठित ग्रन्थ है। इसमें अनेक विषयों को समाहित किया गया है। नाट्यविद्या का तो यह आकर ग्रन्थ ही है। अतः नाट्य प्रयोगों के लिए परवर्ती नाट्याचार्यों ने प्रायः इसी ग्रन्थ का अनुसरण किया है। फलस्वरूप सभी नाट्याचार्य जहाँ आचार्य भरतमुनि के अनुयायी हैं, वहीं वे उनके ऋणी भी हैं।
रंगमंचों की शोभा रूपकों से होती है। दशरूपककार ने रूपकों के दश भेदों का निरुपण किया है। परवर्ती आचार्य रामचन्द्र गुणभद्र ने रूपक के बारह भेदों का उल्लेख किया है। इन रूपकों में संस्कृत नाटक सर्वोपरि है।
आचार्य भरतमुनि ने संस्कृत रूपकों में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के चार भेद किये हैं। :- अतिभाषा, आर्यभाषा, जातिभाषा और योन्यन्तरी भाषा । १ इनमें वैदिक शब्द बहुल भाषा को अति भाषा श्रेष्ठजन की भाषा आर्यभाषा और मनुष्येत्तर अथवा पशु-पक्षियों की भाषा योन्यन्तरी भाषा है। जातिभाषा के दो भेद हैं- संस्कृत और प्राकृत। इन दोनों भाषाओं का प्रयोग रूपकों किंवा संस्कृत नाटकों में पात्रों के अनुसार किया जाता है।
इन रूपकों अथवा संस्कृत नाटकों में भी मात्रा की दृष्टि से देखा जाये तो संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत भाषा का प्रयोग प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अतः प्राकृत भाषा बहुल होने के कारण इन्हें भाषा की दृष्टि से प्राकृत नाटक कहा जा सकता है, किन्तु इनकी प्रकृति संस्कृत नाटकानुरूप है। अतएव इन्हें संस्कृत नाटक कहना ही उचित है। संस्कृत नाटककारों ने स्वतंत्र रूप से प्राकृत भाषा में लिखे गये रूपकों कीएक विधा को सट्टक के नाम से स्वीकार किया है। कर्पूर मञ्जरी विलासवती, चंदलेहा, आनन्दसुंदरी, सिंगारमंजरी और रम्भामंजरी आदि रूपक ग्रन्थ सट्टक के रूप में प्रसिद्ध हैं।
आचार्य भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में प्राकृत भाषा के जिन सात भेदों का उल्लेख किया है, वे हैं - १. मागधी, २. अवन्तिजा, ३. प्राच्या, ४. शौरसेनी, ५. अर्धमागधी, ६. बाह्मीका और ७. दाक्षिणात्या । २ ये प्राकृत भाषाएँ प्रायः क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनके अतिरिक्त शकार, आभीर, चाण्डाल, शबर, द्रविड़ और वनेचरों आदि की भाषाएँ भी हैं, जो देश, काल और पात्रों के अनुरूप संस्कृत रूपकों अथवा नाटकों में प्रयुक्त की गई हैं।
मुखसुख की दृष्टि से भाषाएँ सदैव प्रवहमान रही हैं। इनके रूप देश, काल और व्यक्ति के आधार पर बदलते रहे हैं। अतः भाषाशास्त्रियों ने इन्हें बोलचाल की भाषा अथवा बोली के रूप में प्रतिष्ठित किया है। किन्तु जब ये बोलियाँ साहित्य का रूप धारण कर लेती हैं और लिखित रूप में आ जाती हैं तो इन्हें कुछ विशेष नियमों में जकड़ दिया जाता है, जिससे आगामी पीढ़ी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करे जो पूर्व में प्रतिष्ठित हो गये हैं। इससे अर्थ में प्रायः एकरूपता बनी रहती है। पूर्वापर शब्द रूपों में एकता बनाये रखने के लिये जिन विशेष नियमों को विद्वज्जन स्थापित करते हैं, वे ही नियम कालान्तर में व्याकरण का रूप धारण कर लेते हैं।