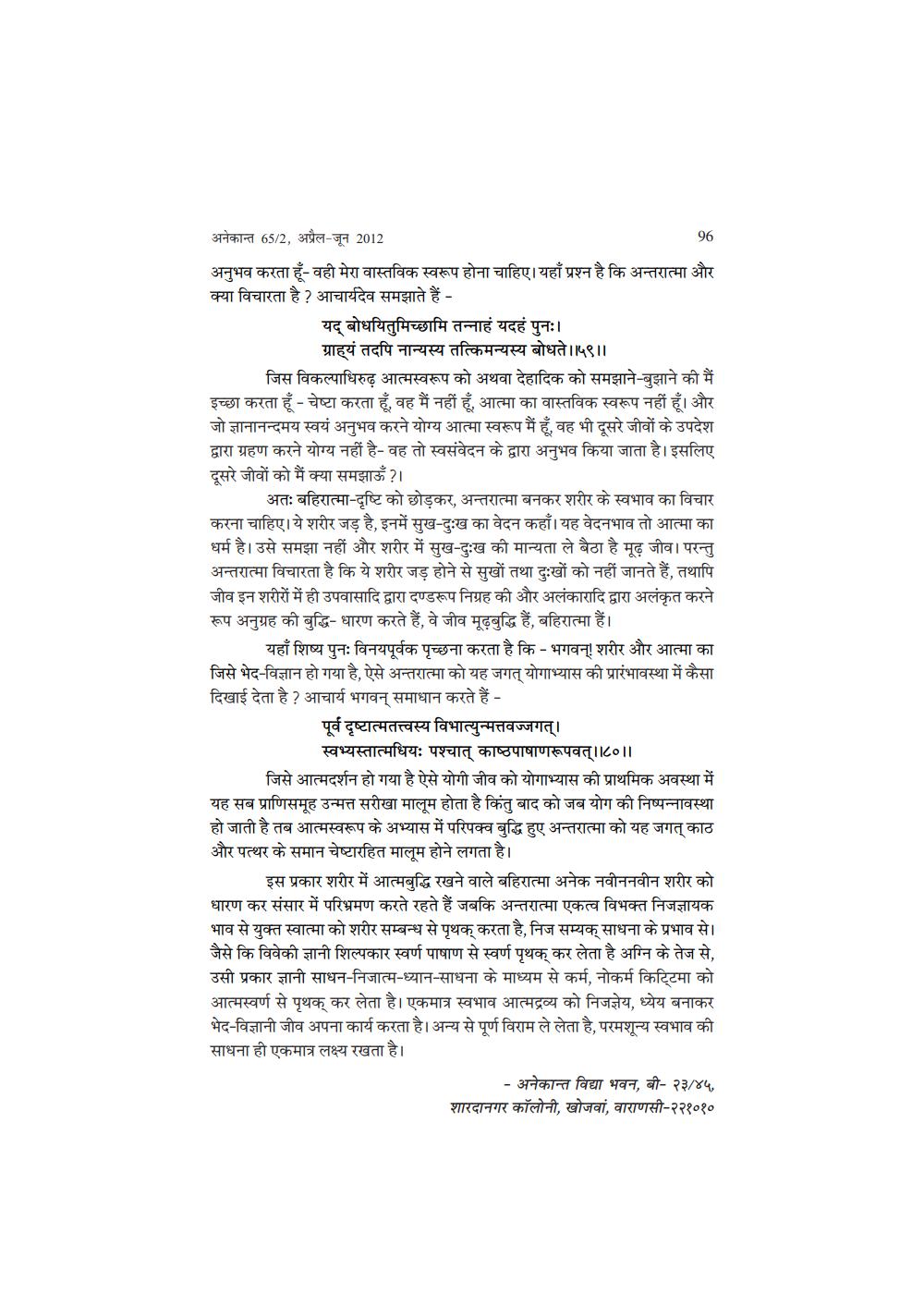________________
अनेकान्त 65/2, अप्रैल-जून 2012 अनुभव करता हूँ-वही मेरा वास्तविक स्वरूप होना चाहिए। यहाँ प्रश्न है कि अन्तरात्मा और क्या विचारता है? आचार्यदेव समझाते हैं -
यद् बोधयितुमिच्छामि तन्नाहं यदहं पुनः।
ग्राह्यं तदपि नान्यस्य तत्किमन्यस्य बोधते।।५९।। जिस विकल्पाधिरुढ़ आत्मस्वरूप को अथवा देहादिक को समझाने-बुझाने की मैं इच्छा करता हूँ - चेष्टा करता हूँ, वह मैं नहीं हूँ, आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं हूँ। और जो ज्ञानानन्दमय स्वयं अनुभव करने योग्य आत्मा स्वरूप मैं हूँ, वह भी दूसरे जीवों के उपदेश द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है- वह तो स्वसंवेदन के द्वारा अनुभव किया जाता है। इसलिए दूसरे जीवों को मैं क्या समझाऊँ ?।
अतः बहिरात्मा-दृष्टि को छोड़कर, अन्तरात्मा बनकर शरीर के स्वभाव का विचार करना चाहिए। ये शरीर जड़ है, इनमें सुख-दुःख का वेदन कहाँ। यह वेदनभाव तो आत्मा का धर्म है। उसे समझा नहीं और शरीर में सुख-दुःख की मान्यता ले बैठा है मूढ़ जीव। परन्तु अन्तरात्मा विचारता है कि ये शरीर जड़ होने से सुखों तथा दुःखों को नहीं जानते हैं, तथापि जीव इन शरीरों में ही उपवासादि द्वारा दण्डरूप निग्रह की और अलंकारादि द्वारा अलंकृत करने रूप अनुग्रह की बुद्धि- धारण करते हैं, वे जीव मूढ़बुद्धि हैं, बहिरात्मा हैं।
यहाँ शिष्य पुनः विनयपूर्वक पृच्छना करता है कि - भगवन्! शरीर और आत्मा का जिसे भेद-विज्ञान हो गया है, ऐसे अन्तरात्मा को यह जगत् योगाभ्यास की प्रारंभावस्था में कैसा दिखाई देता है ? आचार्य भगवन् समाधान करते हैं -
पूर्व दृष्टात्मतत्त्वस्य विभात्युन्मत्तवज्जगत्।
स्वभ्यस्तात्मधियः पश्चात् काष्ठपाषाणरूपवत्।।८।। जिसे आत्मदर्शन हो गया है ऐसे योगी जीव को योगाभ्यास की प्राथमिक अवस्था में यह सब प्राणिसमूह उन्मत्त सरीखा मालूम होता है किंतु बाद को जब योग की निष्पन्नावस्था हो जाती है तब आत्मस्वरूप के अभ्यास में परिपक्व बुद्धि हुए अन्तरात्मा को यह जगत् काठ और पत्थर के समान चेष्टारहित मालूम होने लगता है।
इस प्रकार शरीर में आत्मबुद्धि रखने वाले बहिरात्मा अनेक नवीननवीन शरीर को धारण कर संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं जबकि अन्तरात्मा एकत्व विभक्त निजज्ञायक भाव से युक्त स्वात्मा को शरीर सम्बन्ध से पृथक् करता है, निज सम्यक् साधना के प्रभाव से। जैसे कि विवेकी ज्ञानी शिल्पकार स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण पृथक् कर लेता है अग्नि के तेज से, उसी प्रकार ज्ञानी साधन-निजात्म-ध्यान-साधना के माध्यम से कर्म, नोकर्म किट्टिमा को आत्मस्वर्ण से पृथक् कर लेता है। एकमात्र स्वभाव आत्मद्रव्य को निजज्ञेय, ध्येय बनाकर भेद-विज्ञानी जीव अपना कार्य करता है। अन्य से पूर्ण विराम ले लेता है, परमशून्य स्वभाव की साधना ही एकमात्र लक्ष्य रखता है।
- अनेकान्त विद्या भवन, बी-२३/४५, शारदानगर कॉलोनी, खोजवां, वाराणसी-२२१०१०