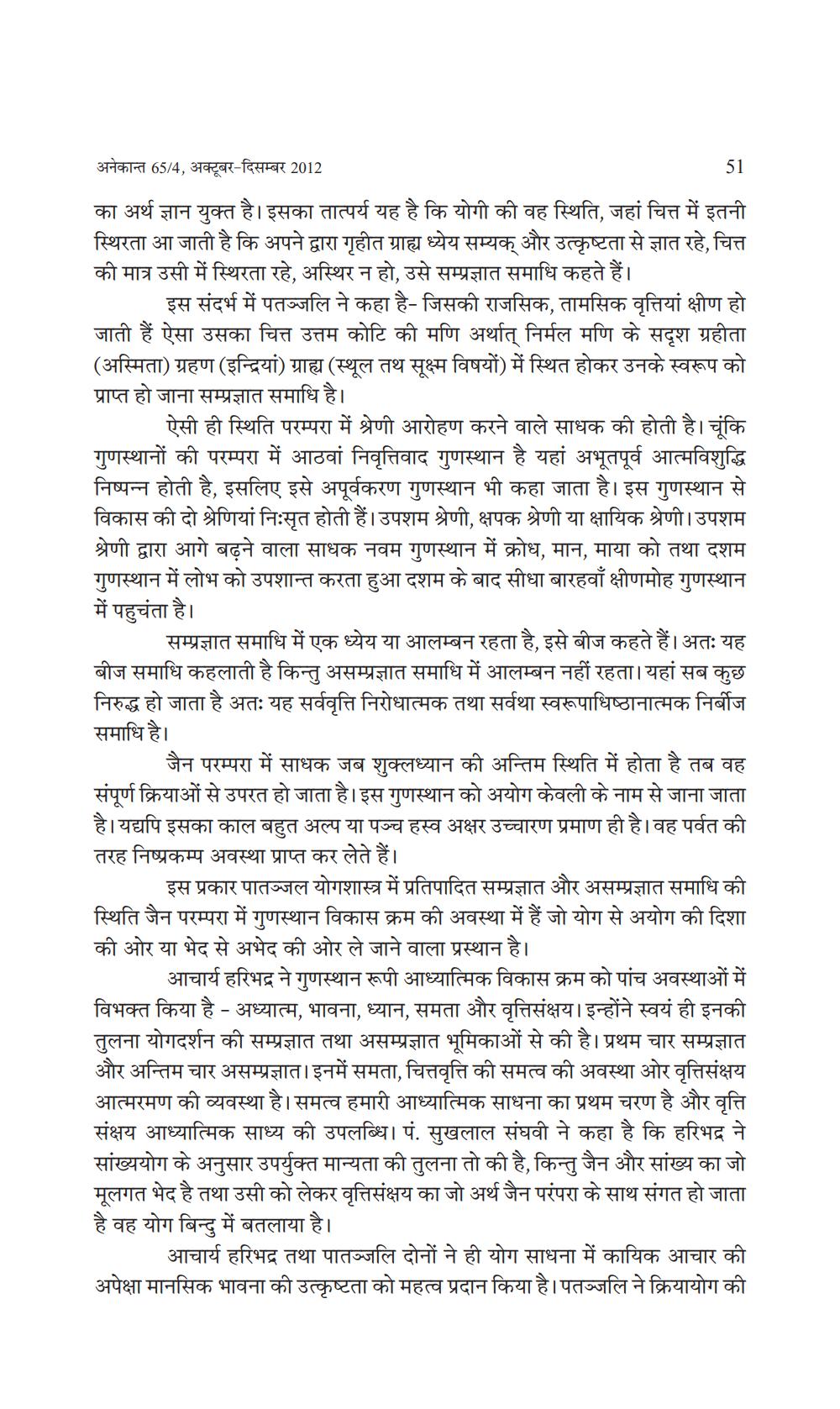________________
अनेकान्त 65/4, अक्टूबर-दिसम्बर 2012 का अर्थ ज्ञान युक्त है। इसका तात्पर्य यह है कि योगी की वह स्थिति, जहां चित्त में इतनी स्थिरता आ जाती है कि अपने द्वारा गृहीत ग्राह्य ध्येय सम्यक् और उत्कृष्टता से ज्ञात रहे, चित्त की मात्र उसी में स्थिरता रहे, अस्थिर न हो, उसे सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं।
इस संदर्भ में पतञ्जलि ने कहा है- जिसकी राजसिक, तामसिक वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं ऐसा उसका चित्त उत्तम कोटि की मणि अर्थात् निर्मल मणि के सदृश ग्रहीता (अस्मिता) ग्रहण (इन्द्रियां) ग्राह्य (स्थूल तथ सूक्ष्म विषयों) में स्थित होकर उनके स्वरूप को प्राप्त हो जाना सम्प्रज्ञात समाधि है।
ऐसी ही स्थिति परम्परा में श्रेणी आरोहण करने वाले साधक की होती है। चूंकि गुणस्थानों की परम्परा में आठवां निवृत्तिवाद गुणस्थान है यहां अभूतपूर्व आत्मविशुद्धि निष्पन्न होती है, इसलिए इसे अपूर्वकरण गुणस्थान भी कहा जाता है। इस गुणस्थान से विकास की दो श्रेणियां निःसृत होती हैं। उपशम श्रेणी, क्षपक श्रेणी या क्षायिक श्रेणी। उपशम श्रेणी द्वारा आगे बढ़ने वाला साधक नवम गुणस्थान में क्रोध, मान, माया को तथा दशम गुणस्थान में लोभ को उपशान्त करता हुआ दशम के बाद सीधा बारहवाँ क्षीणमोह गुणस्थान में पहुचंता है।
सम्प्रज्ञात समाधि में एक ध्येय या आलम्बन रहता है, इसे बीज कहते हैं। अतः यह बीज समाधि कहलाती है किन्तु असम्प्रज्ञात समाधि में आलम्बन नहीं रहता। यहां सब कुछ निरुद्ध हो जाता है अतः यह सर्ववृत्ति निरोधात्मक तथा सर्वथा स्वरूपाधिष्ठानात्मक निर्बीज समाधि है।
जैन परम्परा में साधक जब शुक्लध्यान की अन्तिम स्थिति में होता है तब वह संपूर्ण क्रियाओं से उपरत हो जाता है। इस गुणस्थान को अयोग केवली के नाम से जाना जाता है। यद्यपि इसका काल बहुत अल्प या पञ्च हस्व अक्षर उच्चारण प्रमाण ही है। वह पर्वत की तरह निष्प्रकम्प अवस्था प्राप्त कर लेते हैं।
इस प्रकार पातञ्जल योगशास्त्र में प्रतिपादित सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात समाधि की स्थिति जैन परम्परा में गुणस्थान विकास क्रम की अवस्था में हैं जो योग से अयोग की दिशा की ओर या भेद से अभेद की ओर ले जाने वाला प्रस्थान है।
आचार्य हरिभद्र ने गुणस्थान रूपी आध्यात्मिक विकास क्रम को पांच अवस्थाओं में विभक्त किया है - अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता और वृत्तिसंक्षय। इन्होंने स्वयं ही इनकी तुलना योगदर्शन की सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात भूमिकाओं से की है। प्रथम चार सम्प्रज्ञात और अन्तिम चार असम्प्रज्ञात। इनमें समता, चित्तवृत्ति की समत्व की अवस्था ओर वृत्तिसंक्षय आत्मरमण की व्यवस्था है। समत्व हमारी आध्यात्मिक साधना का प्रथम चरण है और वृत्ति संक्षय आध्यात्मिक साध्य की उपलब्धि। पं. सुखलाल संघवी ने कहा है कि हरिभद्र ने सांख्ययोग के अनुसार उपर्युक्त मान्यता की तुलना तो की है, किन्तु जैन और सांख्य का जो मूलगत भेद है तथा उसी को लेकर वृत्तिसंक्षय का जो अर्थ जैन परंपरा के साथ संगत हो जाता है वह योग बिन्दु में बतलाया है।
आचार्य हरिभद्र तथा पातञ्जलि दोनों ने ही योग साधना में कायिक आचार की अपेक्षा मानसिक भावना की उत्कृष्टता को महत्व प्रदान किया है। पतञ्जलि ने क्रियायोग की