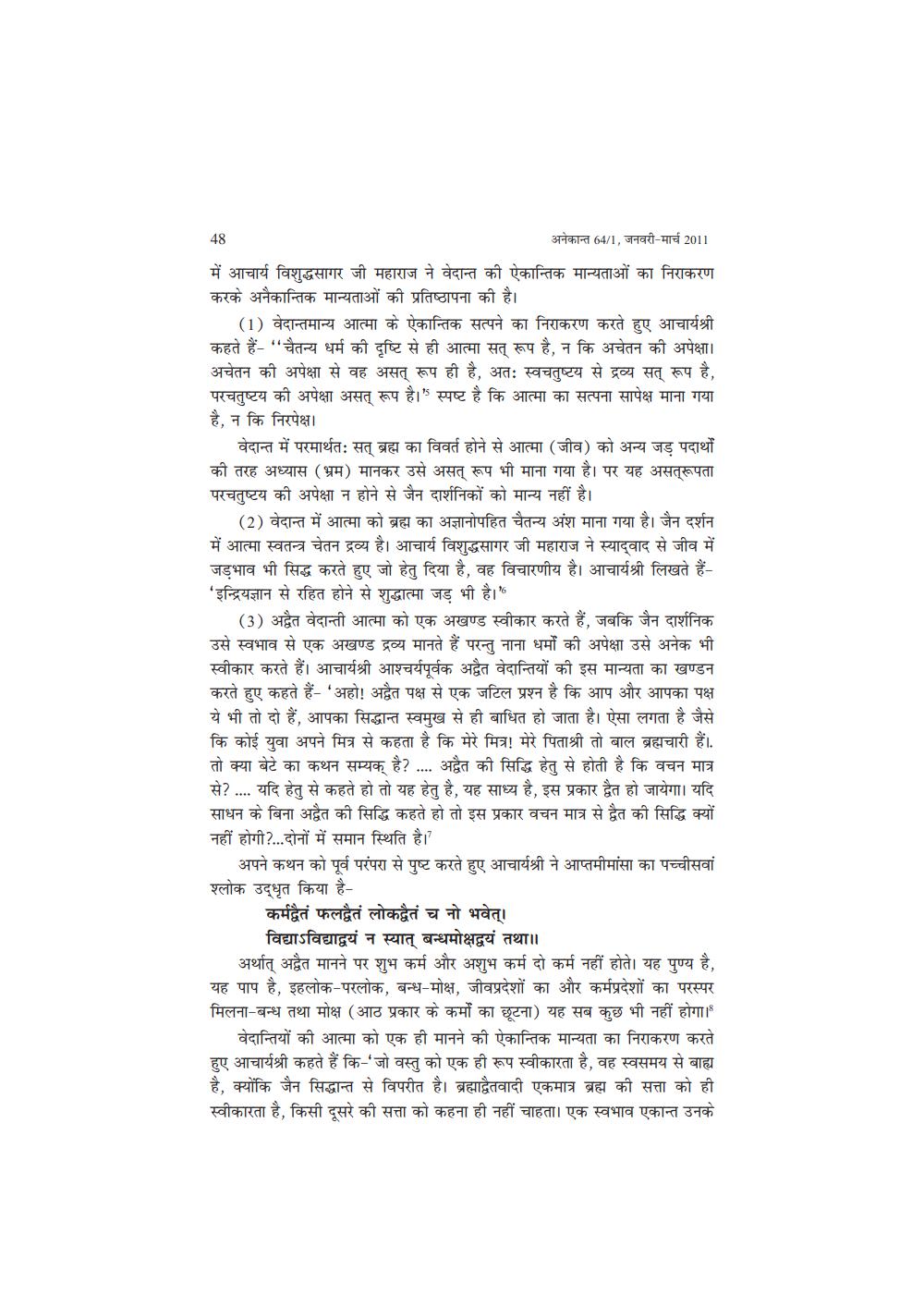________________
अनेकान्त 64/1, जनवरी-मार्च 2011
में आचार्य विशुद्धसागर जी महाराज ने वेदान्त की ऐकान्तिक मान्यताओं का निराकरण करके अनैकान्तिक मान्यताओं की प्रतिष्ठापना की है।
(1) वेदान्तमान्य आत्मा के ऐकान्तिक सत्पने का निराकरण करते हुए आचार्यश्री कहते हैं- "चैतन्य धर्म की दृष्टि से ही आत्मा सत् रूप है, न कि अचेतन की अपेक्षा। अचेतन की अपेक्षा से वह असत् रूप ही है, अतः स्वचतुष्टय से द्रव्य सत् रूप है, परचतुष्टय की अपेक्षा असत् रूप है। स्पष्ट है कि आत्मा का सत्पना सापेक्ष माना गया है, न कि निरपेक्ष।
वेदान्त में परमार्थतः सत् ब्रह्म का विवर्त होने से आत्मा (जीव) को अन्य जड़ पदार्थों की तरह अध्यास (भ्रम) मानकर उसे असत् रूप भी माना गया है। पर यह असत्रूपता परचतुष्टय की अपेक्षा न होने से जैन दार्शनिकों को मान्य नहीं है।
(2) वेदान्त में आत्मा को ब्रह्म का अज्ञानोपहित चैतन्य अंश माना गया है। जैन दर्शन में आत्मा स्वतन्त्र चेतन द्रव्य है। आचार्य विशुद्धसागर जी महाराज ने स्याद्वाद से जीव में जड़भाव भी सिद्ध करते हुए जो हेतु दिया है, वह विचारणीय है। आचार्यश्री लिखते हैं'इन्द्रियज्ञान से रहित होने से शुद्धात्मा जड़ भी है।"
(3) अद्वैत वेदान्ती आत्मा को एक अखण्ड स्वीकार करते हैं, जबकि जैन दार्शनिक उसे स्वभाव से एक अखण्ड द्रव्य मानते हैं परन्तु नाना धर्मों की अपेक्षा उसे अनेक भी स्वीकार करते हैं। आचार्यश्री आश्चर्यपूर्वक अद्वैत वेदान्तियों की इस मान्यता का खण्डन करते हुए कहते हैं- 'अहो! अद्वैत पक्ष से एक जटिल प्रश्न है कि आप और आपका पक्ष ये भी तो दो हैं, आपका सिद्धान्त स्वमुख से ही बाधित हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई युवा अपने मित्र से कहता है कि मेरे मित्र! मेरे पिताश्री तो बाल ब्रह्मचारी हैं।. तो क्या बेटे का कथन सम्यक् है? .... अद्वैत की सिद्धि हेतु से होती है कि वचन मात्र से? .... यदि हेतु से कहते हो तो यह हेतु है, यह साध्य है, इस प्रकार द्वैत हो जायेगा। यदि साधन के बिना अद्वैत की सिद्धि कहते हो तो इस प्रकार वचन मात्र से द्वैत की सिद्धि क्यों नहीं होगी?...दोनों में समान स्थिति है।'
अपने कथन को पूर्व परंपरा से पुष्ट करते हुए आचार्यश्री ने आप्तमीमांसा का पच्चीसवां श्लोक उद्धृत किया है
कर्मद्वैतं फलद्वैतं लोकद्वैतं च नो भवेत्। विद्याऽविद्याद्वयं न स्यात् बन्धमोक्षद्वयं तथा॥ अर्थात् अद्वैत मानने पर शुभ कर्म और अशुभ कर्म दो कर्म नहीं होते। यह पुण्य है, यह पाप है, इहलोक-परलोक, बन्ध-मोक्ष, जीवप्रदेशों का और कर्मप्रदेशों का परस्पर मिलना-बन्ध तथा मोक्ष (आठ प्रकार के कर्मों का छूटना) यह सब कुछ भी नहीं होगा।
वेदान्तियों की आत्मा को एक ही मानने की ऐकान्तिक मान्यता का निराकरण करते हुए आचार्यश्री कहते हैं कि-'जो वस्तु को एक ही रूप स्वीकारता है, वह स्वसमय से बाह्य है, क्योंकि जैन सिद्धान्त से विपरीत है। ब्रह्माद्वैतवादी एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को ही स्वीकारता है, किसी दूसरे की सत्ता को कहना ही नहीं चाहता। एक स्वभाव एकान्त उनके