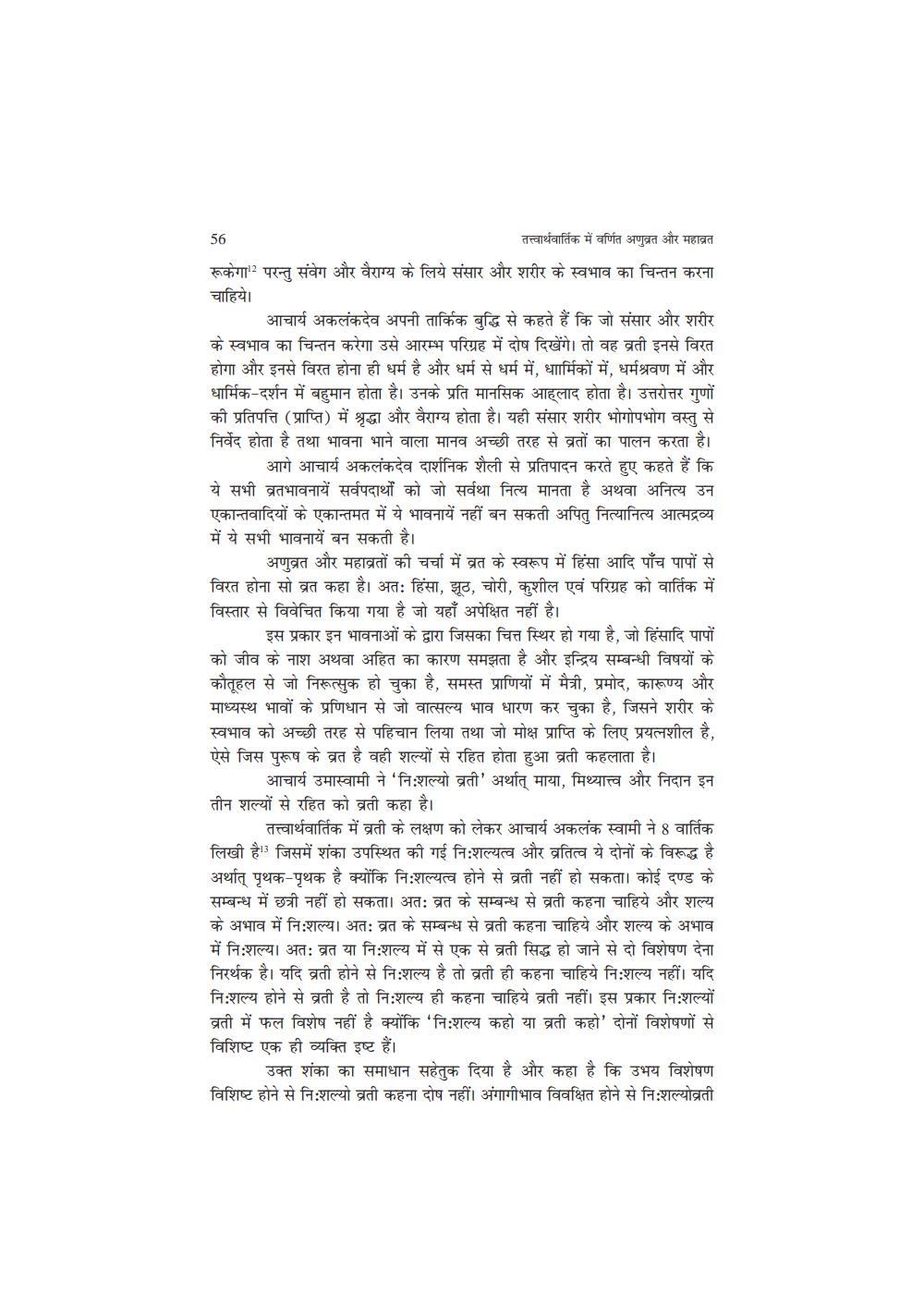________________
तत्त्वार्थवार्तिक में वर्णित अणुव्रत और महाव्रत रूकेगा परन्तु संवेग और वैराग्य के लिये संसार और शरीर के स्वभाव का चिन्तन करना चाहिये।
आचार्य अकलंकदेव अपनी तार्किक बुद्धि से कहते हैं कि जो संसार और शरीर के स्वभाव का चिन्तन करेगा उसे आरम्भ परिग्रह में दोष दिखेंगे। तो वह व्रती इनसे विरत होगा और इनसे विरत होना ही धर्म है और धर्म से धर्म में, धार्मिकों में, धर्मश्रवण में और धार्मिक-दर्शन में बहुमान होता है। उनके प्रति मानसिक आह्लाद होता है। उत्तरोत्तर गुणों की प्रतिपत्ति (प्राप्ति) में श्रद्धा और वैराग्य होता है। यही संसार शरीर भोगोपभोग वस्तु से निर्वेद होता है तथा भावना भाने वाला मानव अच्छी तरह से व्रतों का पालन करता है।
__ आगे आचार्य अकलंकदेव दार्शनिक शैली से प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि ये सभी व्रतभावनायें सर्वपदार्थों को जो सर्वथा नित्य मानता है अथवा अनित्य उन एकान्तवादियों के एकान्तमत में ये भावनायें नहीं बन सकती अपितु नित्यानित्य आत्मद्रव्य में ये सभी भावनायें बन सकती है।
अणुव्रत और महाव्रतों की चर्चा में व्रत के स्वरूप में हिंसा आदि पाँच पापों से विरत होना सो व्रत कहा है। अतः हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील एवं परिग्रह को वार्तिक में विस्तार से विवेचित किया गया है जो यहाँ अपेक्षित नहीं है।
इस प्रकार इन भावनाओं के द्वारा जिसका चित्त स्थिर हो गया है, जो हिंसादि पापों को जीव के नाश अथवा अहित का कारण समझता है और इन्द्रिय सम्बन्धी विषयों के कौतूहल से जो निरूत्सुक हो चुका है, समस्त प्राणियों में मैत्री, प्रमोद, कारूण्य और माध्यस्थ भावों के प्रणिधान से जो वात्सल्य भाव धारण कर चुका है, जिसने शरीर के स्वभाव को अच्छी तरह से पहिचान लिया तथा जो मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, ऐसे जिस पुरूष के व्रत है वही शल्यों से रहित होता हुआ व्रती कहलाता है।
आचार्य उमास्वामी ने 'निःशल्यो व्रती' अर्थात् माया, मिथ्यात्त्व और निदान इन तीन शल्यों से रहित को व्रती कहा है।
तत्त्वार्थवार्तिक में व्रती के लक्षण को लेकर आचार्य अकलंक स्वामी ने 8 वार्तिक लिखी है। जिसमें शंका उपस्थित की गई निःशल्यत्व और व्रतित्व ये दोनों के विरूद्ध है अर्थात् पृथक-पृथक है क्योंकि निःशल्यत्व होने से व्रती नहीं हो सकता। कोई दण्ड के सम्बन्ध में छत्री नहीं हो सकता। अतः व्रत के सम्बन्ध से व्रती कहना चाहिये और शल्य के अभाव में नि:शल्य। अत: व्रत के सम्बन्ध से व्रती कहना चाहिये और शल्य के अभाव में नि:शल्य। अतः व्रत या निःशल्य में से एक से व्रती सिद्ध हो जाने से दो विशेषण देना निरर्थक है। यदि व्रती होने से निःशल्य है तो व्रती ही कहना चाहिये निःशल्य नहीं। यदि निःशल्य होने से व्रती है तो नि:शल्य ही कहना चाहिये व्रती नहीं। इस प्रकार निःशल्यों व्रती में फल विशेष नहीं है क्योंकि 'नि:शल्य कहो या व्रती कहो' दोनों विशेषणों से विशिष्ट एक ही व्यक्ति इष्ट हैं।
उक्त शंका का समाधान सहेतुक दिया है और कहा है कि उभय विशेषण विशिष्ट होने से निःशल्यो व्रती कहना दोष नहीं। अंगागीभाव विवक्षित होने से निःशल्योव्रती