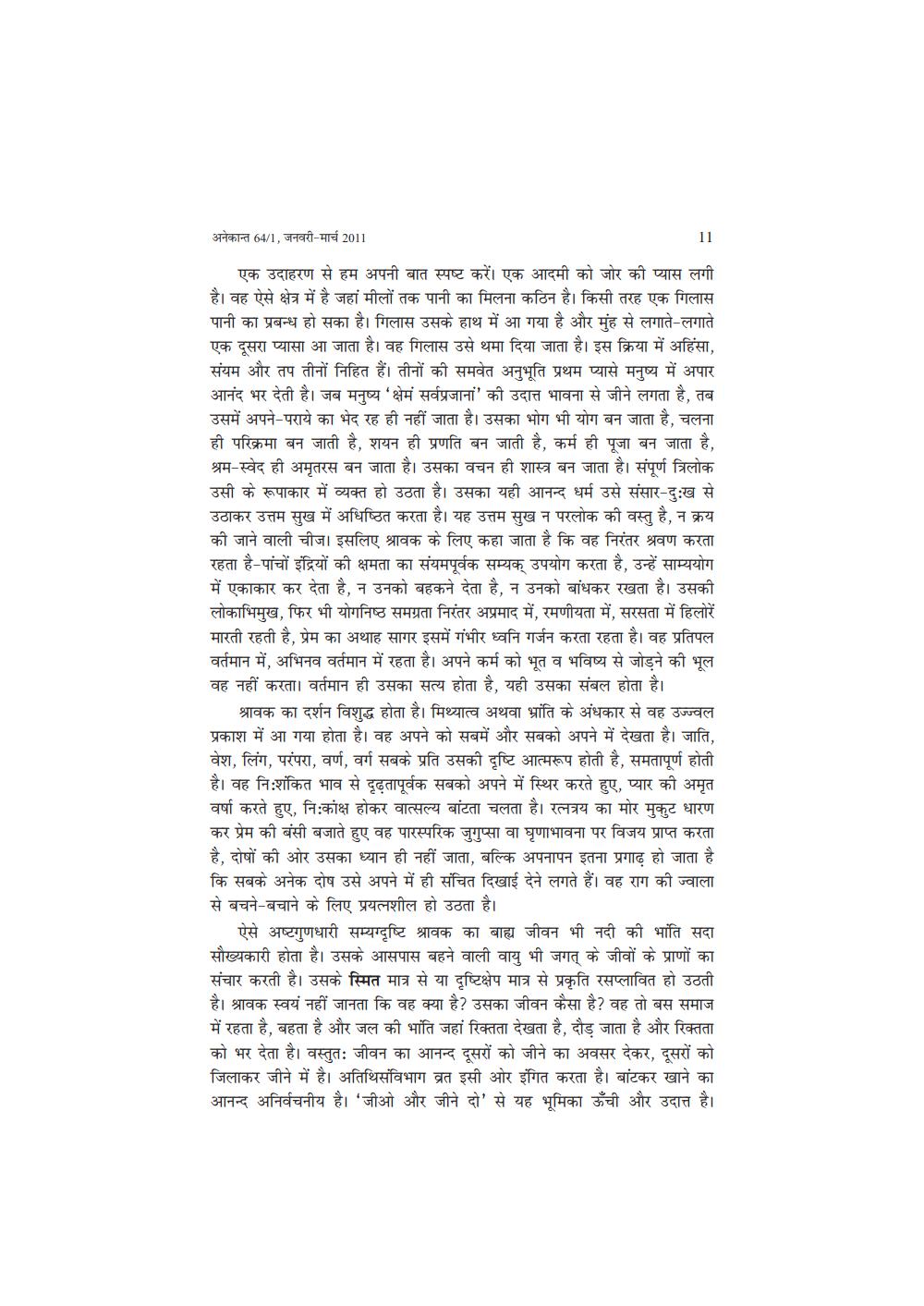________________
अनेकान्त 64/1, जनवरी-मार्च 2011
11
___ एक उदाहरण से हम अपनी बात स्पष्ट करें। एक आदमी को जोर की प्यास लगी है। वह ऐसे क्षेत्र में है जहां मीलों तक पानी का मिलना कठिन है। किसी तरह एक गिलास पानी का प्रबन्ध हो सका है। गिलास उसके हाथ में आ गया है और मुंह से लगाते-लगाते एक दूसरा प्यासा आ जाता है। वह गिलास उसे थमा दिया जाता है। इस क्रिया में अहिंसा, संयम और तप तीनों निहित हैं। तीनों की समवेत अनुभूति प्रथम प्यासे मनुष्य में अपार आनंद भर देती है। जब मनुष्य 'क्षेमं सर्वप्रजानां' की उदात्त भावना से जीने लगता है, तब उसमें अपने-पराये का भेद रह ही नहीं जाता है। उसका भोग भी योग बन जाता है, चलना ही परिक्रमा बन जाती है, शयन ही प्रणति बन जाती है, कर्म ही पूजा बन जाता है, श्रम-स्वेद ही अमृतरस बन जाता है। उसका वचन ही शास्त्र बन जाता है। संपूर्ण त्रिलोक उसी के रूपाकार में व्यक्त हो उठता है। उसका यही आनन्द धर्म उसे संसार-दु:ख से उठाकर उत्तम सुख में अधिष्ठित करता है। यह उत्तम सुख न परलोक की वस्तु है, न क्रय की जाने वाली चीज। इसलिए श्रावक के लिए कहा जाता है कि वह निरंतर श्रवण करता रहता है-पांचों इंद्रियों की क्षमता का संयमपूर्वक सम्यक् उपयोग करता है, उन्हें साम्ययोग में एकाकार कर देता है, न उनको बहकने देता है, न उनको बांधकर रखता है। उसकी लोकाभिमुख, फिर भी योगनिष्ठ समग्रता निरंतर अप्रमाद में, रमणीयता में, सरसता में हिलोरें मारती रहती है, प्रेम का अथाह सागर इसमें गंभीर ध्वनि गर्जन करता रहता है। वह प्रतिपल वर्तमान में, अभिनव वर्तमान में रहता है। अपने कर्म को भूत व भविष्य से जोड़ने की भूल वह नहीं करता। वर्तमान ही उसका सत्य होता है, यही उसका संबल होता है।
श्रावक का दर्शन विशुद्ध होता है। मिथ्यात्व अथवा भ्रांति के अंधकार से वह उज्ज्वल प्रकाश में आ गया होता है। वह अपने को सबमें और सबको अपने में देखता है। जाति, वेश, लिंग, परंपरा, वर्ण, वर्ग सबके प्रति उसकी दृष्टि आत्मरूप होती है, समतापूर्ण होती है। वह नि:शंकित भाव से दृढ़तापूर्वक सबको अपने में स्थिर करते हुए, प्यार की अमृत वर्षा करते हुए, नि:कांक्ष होकर वात्सल्य बांटता चलता है। रत्नत्रय का मोर मुकुट धारण कर प्रेम की बंसी बजाते हुए वह पारस्परिक जुगुप्सा वा घृणाभावना पर विजय प्राप्त करता है, दोषों की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता, बल्कि अपनापन इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि सबके अनेक दोष उसे अपने में ही संचित दिखाई देने लगते हैं। वह राग की ज्वाला से बचने-बचाने के लिए प्रयत्नशील हो उठता है।
ऐसे अष्टगुणधारी सम्यग्दृष्टि श्रावक का बाह्य जीवन भी नदी की भांति सदा सौख्यकारी होता है। उसके आसपास बहने वाली वायु भी जगत् के जीवों के प्राणों का संचार करती है। उसके स्मित मात्र से या दृष्टिक्षेप मात्र से प्रकृति रसप्लावित हो उठती है। श्रावक स्वयं नहीं जानता कि वह क्या है? उसका जीवन कैसा है? वह तो बस समाज में रहता है, बहता है और जल की भांति जहां रिक्तता देखता है, दौड़ जाता है और रिक्तता को भर देता है। वस्तुतः जीवन का आनन्द दूसरों को जीने का अवसर देकर, दूसरों को जिलाकर जीने में है। अतिथिसंविभाग व्रत इसी ओर इंगित करता है। बांटकर खाने का आनन्द अनिर्वचनीय है। 'जीओ और जीने दो' से यह भूमिका ऊँची और उदात्त है।