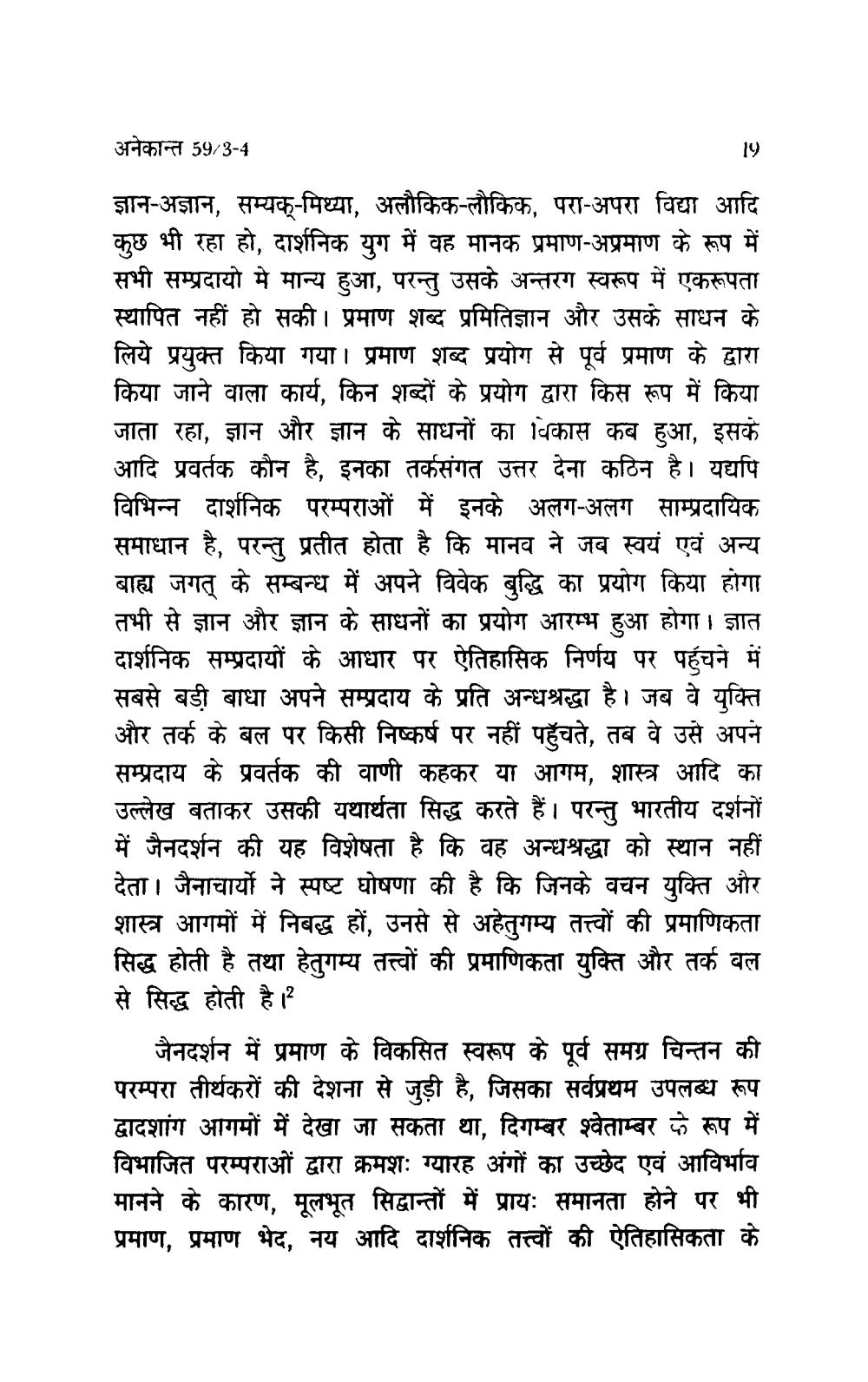________________
अनेकान्त 59/3-4
ज्ञान-अज्ञान, सम्यक्-मिथ्या, अलौकिक-लौकिक, परा-अपरा विद्या आदि कुछ भी रहा हो, दार्शनिक युग में वह मानक प्रमाण-अप्रमाण के रूप में सभी सम्प्रदायो मे मान्य हुआ, परन्तु उसके अन्तरग स्वरूप में एकरूपता स्थापित नहीं हो सकी। प्रमाण शब्द प्रमितिज्ञान और उसके साधन के लिये प्रयुक्त किया गया। प्रमाण शब्द प्रयोग से पूर्व प्रमाण के द्वारा किया जाने वाला कार्य, किन शब्दों के प्रयोग द्वारा किस रूप में किया जाता रहा, ज्ञान और ज्ञान के साधनों का विकास कब हुआ, इसके आदि प्रवर्तक कौन है, इनका तर्कसंगत उत्तर देना कठिन है। यद्यपि विभिन्न दार्शनिक परम्पराओं में इनके अलग-अलग साम्प्रदायिक समाधान है, परन्तु प्रतीत होता है कि मानव ने जब स्वयं एवं अन्य बाह्य जगत् के सम्बन्ध में अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग किया होगा तभी से ज्ञान और ज्ञान के साधनों का प्रयोग आरम्भ हुआ होगा। ज्ञात दार्शनिक सम्प्रदायों के आधार पर ऐतिहासिक निर्णय पर पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा अपने सम्प्रदाय के प्रति अन्धश्रद्धा है। जब वे युक्ति
और तर्क के बल पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, तब वे उसे अपने सम्प्रदाय के प्रवर्तक की वाणी कहकर या आगम, शास्त्र आदि का उल्लेख बताकर उसकी यथार्थता सिद्ध करते हैं। परन्तु भारतीय दर्शनों में जैनदर्शन की यह विशेषता है कि वह अन्धश्रद्धा को स्थान नहीं देता। जैनाचार्यों ने स्पष्ट घोषणा की है कि जिनके वचन युक्ति और शास्त्र आगमों में निबद्ध हों, उनसे से अहेतुगम्य तत्त्वों की प्रमाणिकता सिद्ध होती है तथा हेतुगम्य तत्त्वों की प्रमाणिकता युक्ति और तर्क बल से सिद्ध होती है।
जैनदर्शन में प्रमाण के विकसित स्वरूप के पूर्व समग्र चिन्तन की परम्परा तीर्थकरों की देशना से जुड़ी है, जिसका सर्वप्रथम उपलब्ध रूप द्वादशांग आगमों में देखा जा सकता था, दिगम्बर श्वेताम्बर के रूप में विभाजित परम्पराओं द्वारा क्रमशः ग्यारह अंगों का उच्छेद एवं आविर्भाव मानने के कारण, मूलभूत सिद्धान्तों में प्रायः समानता होने पर भी प्रमाण, प्रमाण भेद, नय आदि दार्शनिक तत्त्वों की ऐतिहासिकता के