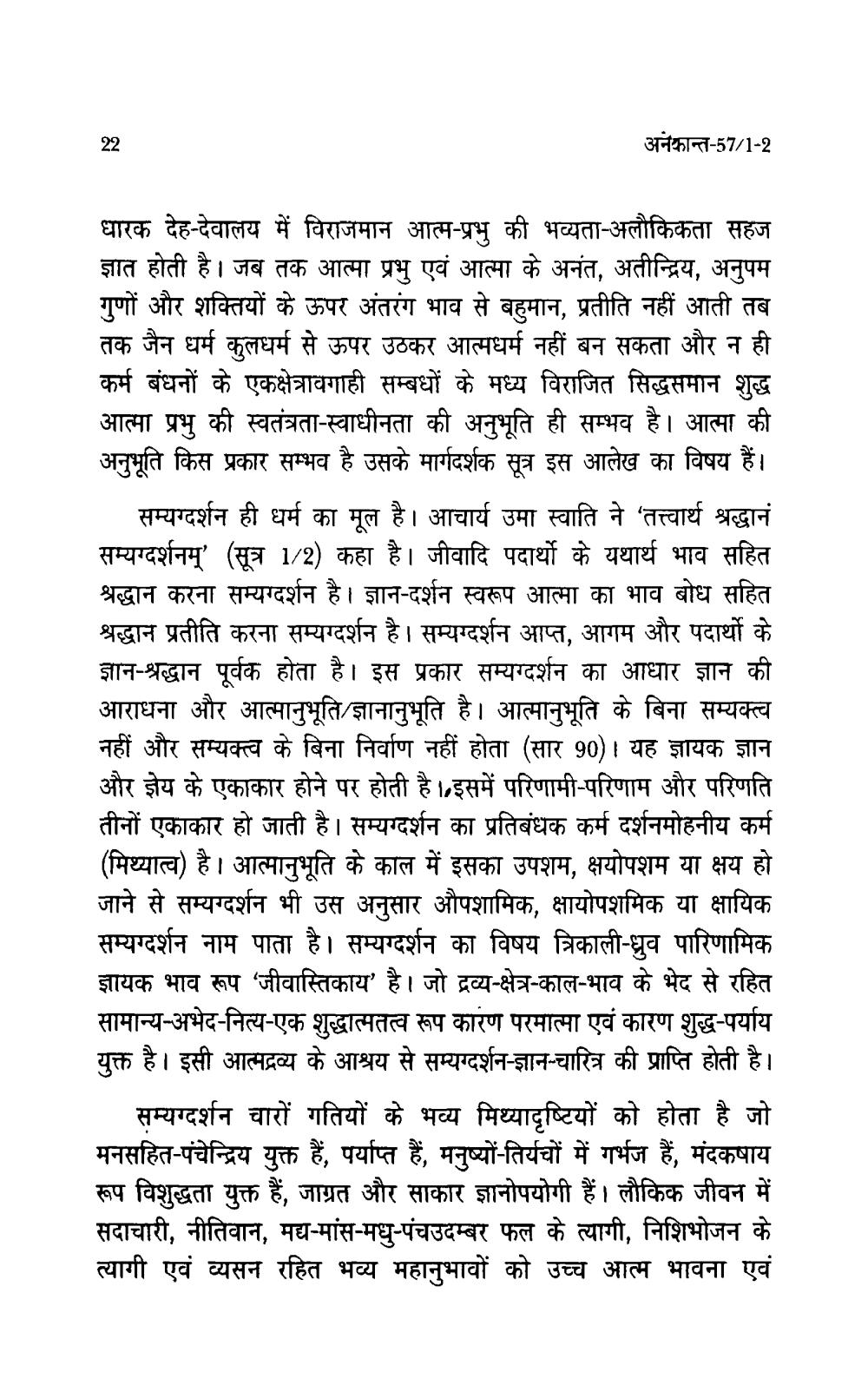________________
अनेकान्त-57/1-2
धारक देह-देवालय में विराजमान आत्म-प्रभु की भव्यता-अलौकिकता सहज ज्ञात होती है। जब तक आत्मा प्रभु एवं आत्मा के अनंत, अतीन्द्रिय, अनुपम गुणों और शक्तियों के ऊपर अंतरंग भाव से बहुमान, प्रतीति नहीं आती तब तक जैन धर्म कुलधर्म से ऊपर उठकर आत्मधर्म नहीं बन सकता और न ही कर्म बंधनों के एकक्षेत्रावगाही सम्बधों के मध्य विराजित सिद्धसमान शुद्ध आत्मा प्रभु की स्वतंत्रता-स्वाधीनता की अनुभूति ही सम्भव है। आत्मा की अनुभूति किस प्रकार सम्भव है उसके मार्गदर्शक सूत्र इस आलेख का विषय हैं।
सम्यग्दर्शन ही धर्म का मूल है। आचार्य उमा स्वाति ने 'तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्' (सूत्र 1/2) कहा है। जीवादि पदार्थो के यथार्थ भाव सहित श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। ज्ञान-दर्शन स्वरूप आत्मा का भाव बोध सहित श्रद्धान प्रतीति करना सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शन आप्त, आगम और पदार्थो के ज्ञान-श्रद्धान पूर्वक होता है। इस प्रकार सम्यग्दर्शन का आधार ज्ञान की आराधना और आत्मानुभूति/ज्ञानानुभूति है। आत्मानुभूति के बिना सम्यक्त्व नहीं और सम्यक्त्व के बिना निर्वाण नहीं होता (सार 90)। यह ज्ञायक ज्ञान
और ज्ञेय के एकाकार होने पर होती है। इसमें परिणामी परिणाम और परिणति तीनों एकाकार हो जाती है। सम्यग्दर्शन का प्रतिबंधक कर्म दर्शनमोहनीय कर्म (मिथ्यात्व) है। आत्मानुभूति के काल में इसका उपशम, क्षयोपशम या क्षय हो जाने से सम्यग्दर्शन भी उस अनुसार औपशामिक, क्षायोपशमिक या क्षायिक सम्यग्दर्शन नाम पाता है। सम्यग्दर्शन का विषय त्रिकाली-ध्रुव पारिणामिक ज्ञायक भाव रूप 'जीवास्तिकाय' है। जो द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव के भेद से रहित सामान्य-अभेद-नित्य-एक शुद्धात्मतत्व रूप कारण परमात्मा एवं कारण शुद्ध-पर्याय युक्त है। इसी आत्मद्रव्य के आश्रय से सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की प्राप्ति होती है।
सम्यग्दर्शन चारों गतियों के भव्य मिथ्यादृष्टियों को होता है जो मनसहित-पंचेन्द्रिय युक्त हैं, पर्याप्त हैं, मनुष्यों-तिर्यचों में गर्भज हैं, मंदकषाय रूप विशुद्धता युक्त हैं, जाग्रत और साकार ज्ञानोपयोगी हैं। लौकिक जीवन में सदाचारी, नीतिवान, मद्य-मांस-मधु-पंचउदम्बर फल के त्यागी, निशिभोजन के त्यागी एवं व्यसन रहित भव्य महानुभावों को उच्च आत्म भावना एवं