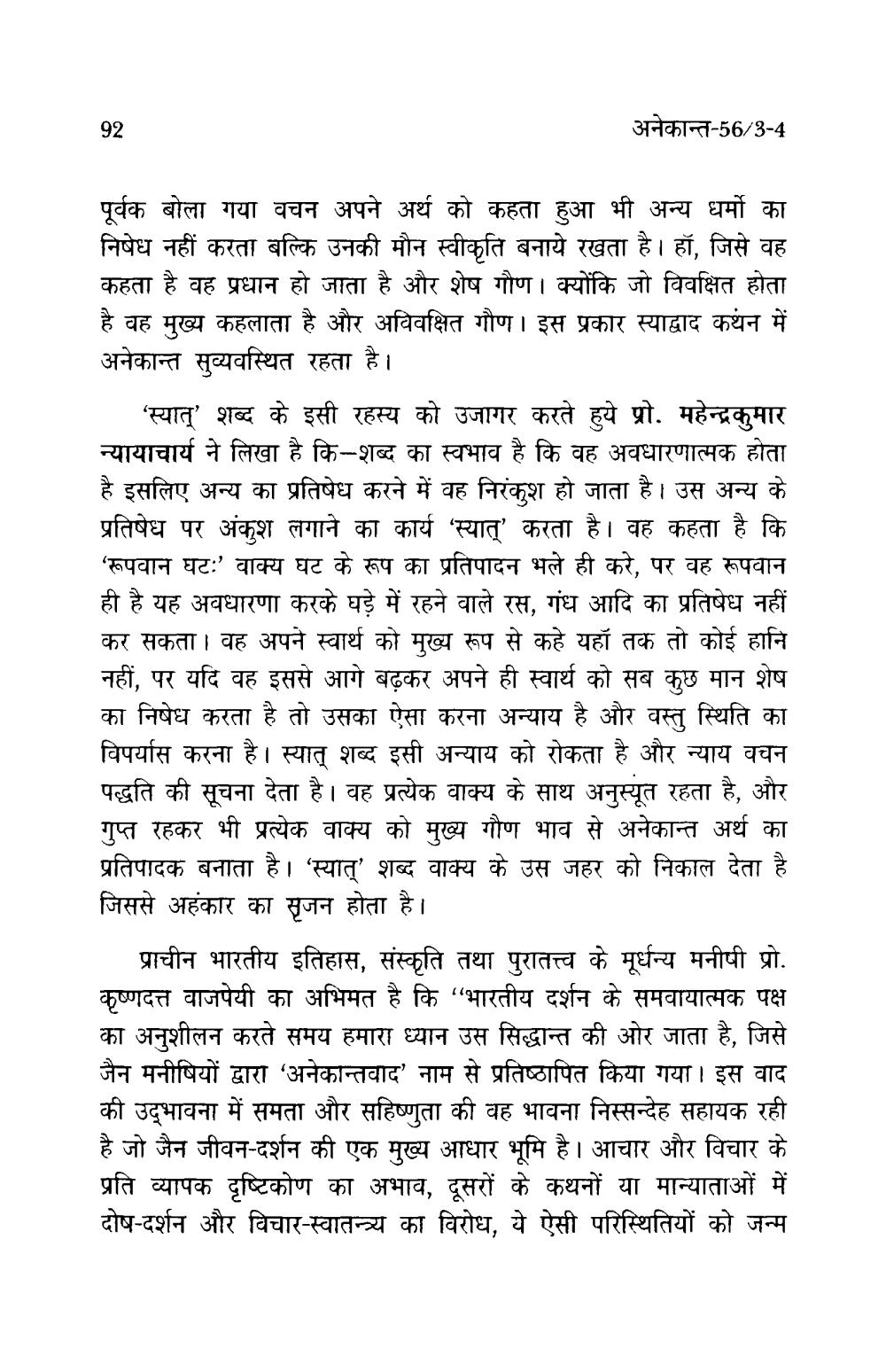________________
92
अनेकान्त-56/3-4
पूर्वक बोला गया वचन अपने अर्थ को कहता हुआ भी अन्य धर्मो का निषेध नहीं करता बल्कि उनकी मौन स्वीकृति बनाये रखता है। हॉ, जिसे वह कहता है वह प्रधान हो जाता है और शेष गौण। क्योंकि जो विवक्षित होता है वह मुख्य कहलाता है और अविवक्षित गौण। इस प्रकार स्याद्वाद कथन में अनेकान्त सुव्यवस्थित रहता है।
'स्यात' शब्द के इसी रहस्य को उजागर करते हुये प्रो. महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य ने लिखा है कि-शब्द का स्वभाव है कि वह अवधारणात्मक होता है इसलिए अन्य का प्रतिषेध करने में वह निरंकुश हो जाता है। उस अन्य के प्रतिषेध पर अंकुश लगाने का कार्य 'स्यात्' करता है। वह कहता है कि 'रूपवान घटः' वाक्य घट के रूप का प्रतिपादन भले ही करे, पर वह रूपवान ही है यह अवधारणा करके घड़े में रहने वाले रस, गंध आदि का प्रतिषेध नहीं कर सकता। वह अपने स्वार्थ को मुख्य रूप से कहे यहाँ तक तो कोई हानि नहीं, पर यदि वह इससे आगे बढ़कर अपने ही स्वार्थ को सब कुछ मान शेष का निषेध करता है तो उसका ऐसा करना अन्याय है और वस्तु स्थिति का विपर्यास करना है। स्यात् शब्द इसी अन्याय को रोकता है और न्याय वचन पद्धति की सूचना देता है। वह प्रत्येक वाक्य के साथ अनुस्यूत रहता है, और गुप्त रहकर भी प्रत्येक वाक्य को मुख्य गौण भाव से अनेकान्त अर्थ का प्रतिपादक बनाता है। 'स्यात्' शब्द वाक्य के उस जहर को निकाल देता है जिससे अहंकार का सृजन होता है।
प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्त्व के मूर्धन्य मनीषी प्रो. कृष्णदत्त वाजपेयी का अभिमत है कि "भारतीय दर्शन के समवायात्मक पक्ष का अनुशीलन करते समय हमारा ध्यान उस सिद्धान्त की ओर जाता है, जिसे जैन मनीषियों द्वारा ‘अनेकान्तवाद' नाम से प्रतिष्ठापित किया गया। इस वाद की उद्भावना में समता और सहिष्णुता की वह भावना निस्सन्देह सहायक रही है जो जैन जीवन-दर्शन की एक मुख्य आधार भूमि है। आचार और विचार के प्रति व्यापक दृष्टिकोण का अभाव, दूसरों के कथनों या मान्याताओं में दोष-दर्शन और विचार-स्वातन्त्र्य का विरोध, ये ऐसी परिस्थितियों को जन्म