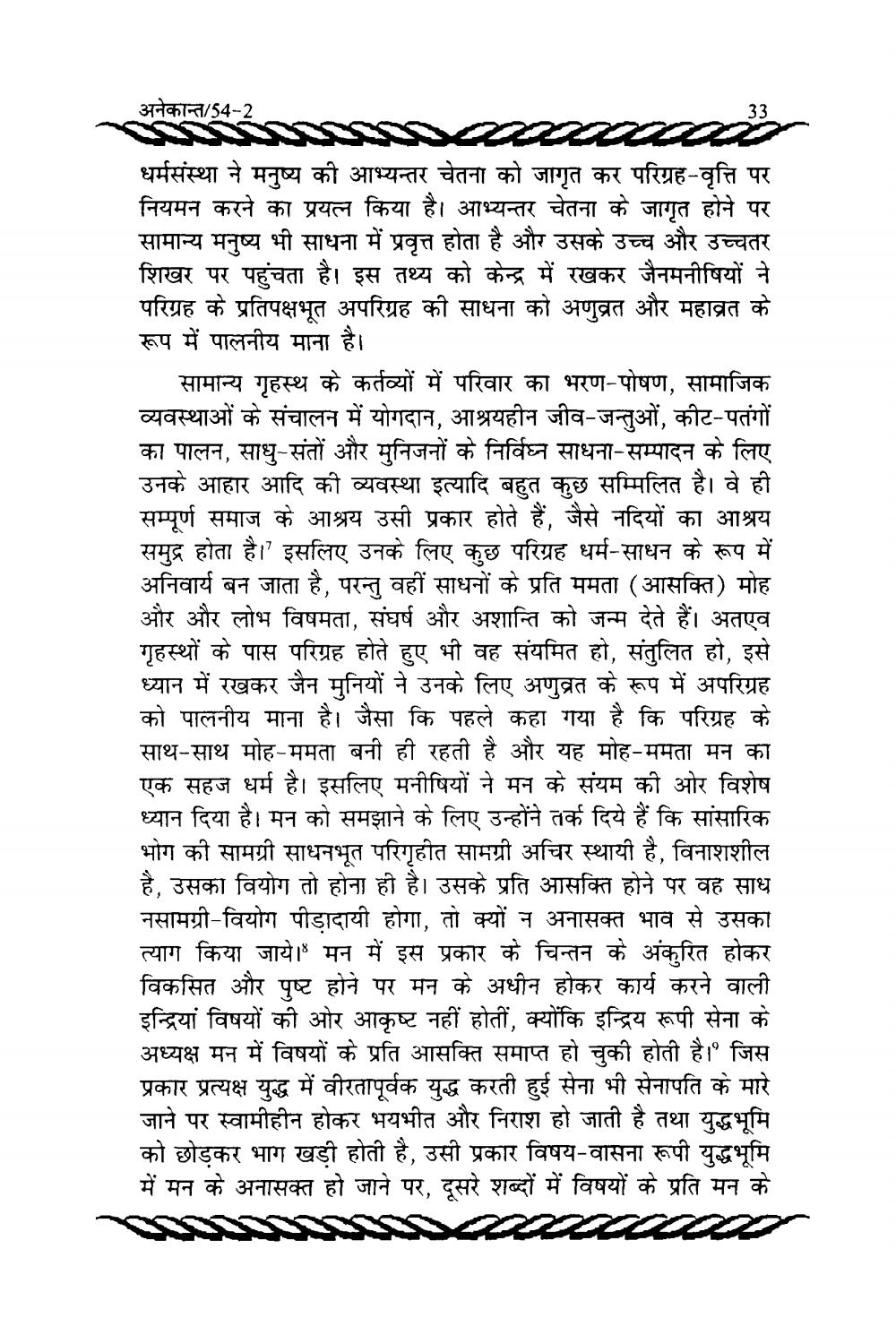________________
अनेकान्त/54-2
धर्मसंस्था ने मनुष्य की आभ्यन्तर चेतना को जागृत कर परिग्रह-वृत्ति पर नियमन करने का प्रयत्न किया है। आभ्यन्तर चेतना के जागृत होने पर सामान्य मनुष्य भी साधना में प्रवृत्त होता है और उसके उच्च और उच्चतर शिखर पर पहुंचता है। इस तथ्य को केन्द्र में रखकर जैनमनीषियों ने परिग्रह के प्रतिपक्षभूत अपरिग्रह की साधना को अणुव्रत और महाव्रत के रूप में पालनीय माना है।
सामान्य गृहस्थ के कर्तव्यों में परिवार का भरण-पोषण, सामाजिक व्यवस्थाओं के संचालन में योगदान, आश्रयहीन जीव-जन्तुओं, कीट-पतंगों का पालन, साधु-संतों और मुनिजनों के निर्विघ्न साधना-सम्पादन के लिए उनके आहार आदि की व्यवस्था इत्यादि बहुत कुछ सम्मिलित है। वे ही सम्पूर्ण समाज के आश्रय उसी प्रकार होते हैं, जैसे नदियों का आश्रय समुद्र होता है। इसलिए उनके लिए कुछ परिग्रह धर्म-साधन के रूप में अनिवार्य बन जाता है, परन्तु वहीं साधनों के प्रति ममता (आसक्ति) मोह और और लोभ विषमता, संघर्ष और अशान्ति को जन्म देते हैं। अतएव गृहस्थों के पास परिग्रह होते हुए भी वह संयमित हो, संतुलित हो, इसे ध्यान में रखकर जैन मुनियों ने उनके लिए अणुव्रत के रूप में अपरिग्रह को पालनीय माना है। जैसा कि पहले कहा गया है कि परिग्रह के साथ-साथ मोह-ममता बनी ही रहती है और यह मोह-ममता मन का एक सहज धर्म है। इसलिए मनीषियों ने मन के संयम की ओर विशेष ध्यान दिया है। मन को समझाने के लिए उन्होंने तर्क दिये हैं कि सांसारिक भोग की सामग्री साधनभूत परिगृहीत सामग्री अचिर स्थायी है, विनाशशील है, उसका वियोग तो होना ही है। उसके प्रति आसक्ति होने पर वह साध नसामग्री-वियोग पीडादायी होगा, तो क्यों न अनासक्त भाव से उसका त्याग किया जाये। मन में इस प्रकार के चिन्तन के अंकुरित होकर विकसित और पुष्ट होने पर मन के अधीन होकर कार्य करने वाली इन्द्रियां विषयों की ओर आकृष्ट नहीं होती, क्योंकि इन्द्रिय रूपी सेना के अध्यक्ष मन में विषयों के प्रति आसक्ति समाप्त हो चुकी होती है। जिस प्रकार प्रत्यक्ष युद्ध में वीरतापूर्वक युद्ध करती हुई सेना भी सेनापति के मारे जाने पर स्वामीहीन होकर भयभीत और निराश हो जाती है तथा युद्धभूमि को छोड़कर भाग खड़ी होती है, उसी प्रकार विषय-वासना रूपी युद्धभूमि में मन के अनासक्त हो जाने पर, दूसरे शब्दों में विषयों के प्रति मन के