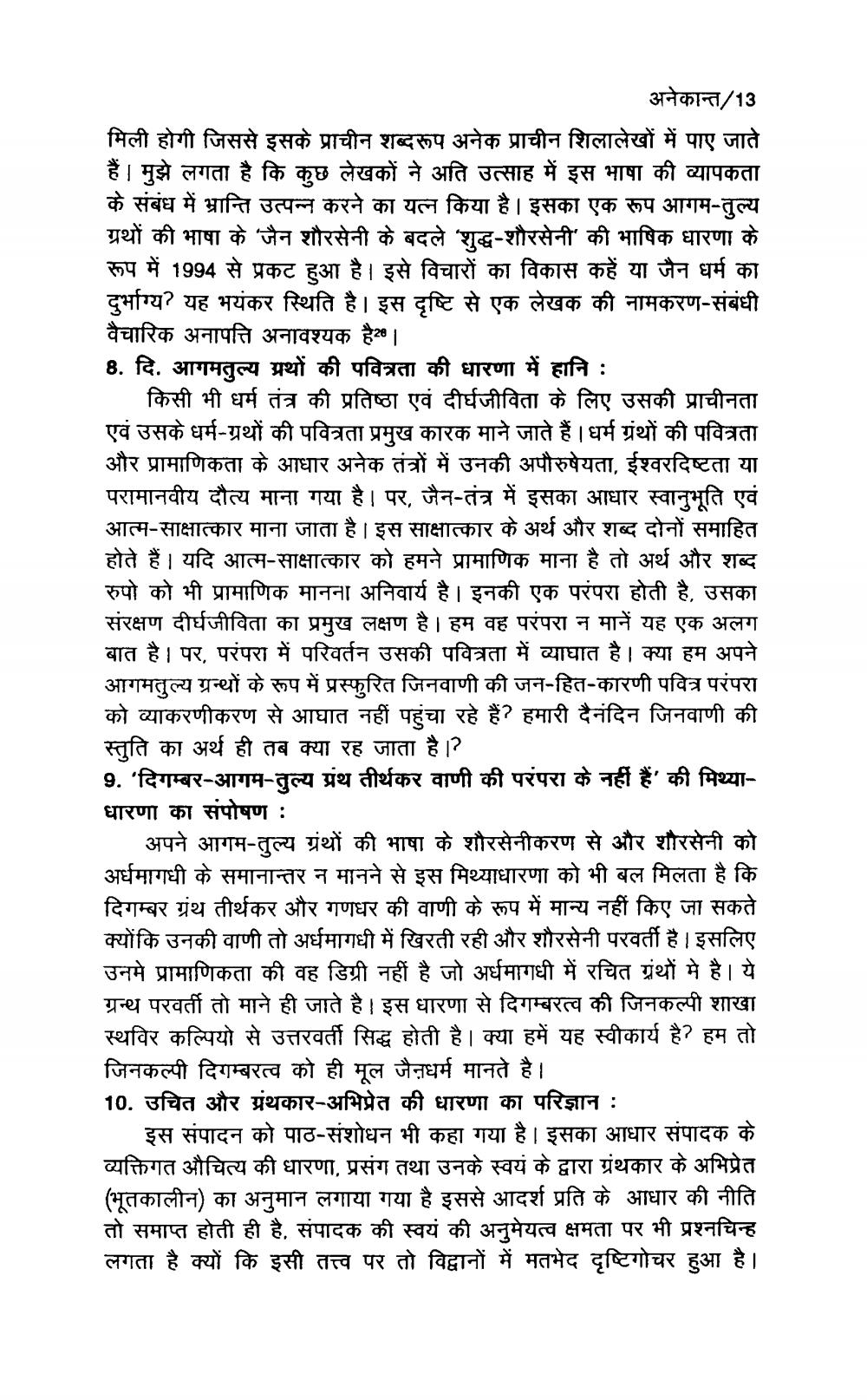________________
अनेकान्त/13 मिली होगी जिससे इसके प्राचीन शब्दरूप अनेक प्राचीन शिलालेखों में पाए जाते हैं। मुझे लगता है कि कुछ लेखकों ने अति उत्साह में इस भाषा की व्यापकता के संबंध में भ्रान्ति उत्पन्न करने का यत्न किया है। इसका एक रूप आगम-तुल्य ग्रथों की भाषा के 'जैन शौरसेनी के बदले 'शुद्ध-शौरसेनी' की भाषिक धारणा के रूप में 1994 से प्रकट हुआ है। इसे विचारों का विकास कहें या जैन धर्म का दुर्भाग्य? यह भयंकर स्थिति है। इस दृष्टि से एक लेखक की नामकरण-संबंधी वैचारिक अनापत्ति अनावश्यक है | 8. दि. आगमतुल्य प्रथों की पवित्रता की धारणा में हानि :
किसी भी धर्म तंत्र की प्रतिष्ठा एवं दीर्घजीविता के लिए उसकी प्राचीनता एवं उसके धर्म-ग्रथों की पवित्रता प्रमुख कारक माने जाते हैं। धर्म ग्रंथों की पवित्रता और प्रामाणिकता के आधार अनेक तंत्रों में उनकी अपौरुषेयता, ईश्वरदिष्टता या परामानवीय दौत्य माना गया है। पर, जैन-तंत्र में इसका आधार स्वानुभूति एवं आत्म-साक्षात्कार माना जाता है। इस साक्षात्कार के अर्थ और शब्द दोनों समाहित होते हैं। यदि आत्म-साक्षात्कार को हमने प्रामाणिक माना है तो अर्थ और शब्द रुपो को भी प्रामाणिक मानना अनिवार्य है। इनकी एक परंपरा होती है, उसका संरक्षण दीर्घजीविता का प्रमुख लक्षण है। हम वह परंपरा न मानें यह एक अलग बात है। पर, परंपरा में परिवर्तन उसकी पवित्रता में व्याघात है। क्या हम अपने आगमतुल्य ग्रन्थों के रूप में प्रस्फुरित जिनवाणी की जन-हित-कारणी पवित्र परंपरा को व्याकरणीकरण से आघात नहीं पहुंचा रहे हैं? हमारी दैनंदिन जिनवाणी की स्तुति का अर्थ ही तब क्या रह जाता है? 9. "दिगम्बर-आगम-तुल्य ग्रंथ तीर्थकर वाणी की परंपरा के नहीं हैं' की मिथ्याधारणा का संपोषण : __ अपने आगम-तुल्य ग्रंथों की भाषा के शौरसेनीकरण से और शौरसेनी को अर्धमागधी के समानान्तर न मानने से इस मिथ्याधारणा को भी बल मिलता है कि दिगम्बर ग्रंथ तीर्थकर और गणधर की वाणी के रूप में मान्य नहीं किए जा सकते क्योंकि उनकी वाणी तो अर्धमागधी में खिरती रही और शौरसेनी परवर्ती है। इसलिए उनमे प्रामाणिकता की वह डिग्री नहीं है जो अर्धमागधी में रचित ग्रंथों में है। ये ग्रन्थ परवर्ती तो माने ही जाते है। इस धारणा से दिगम्बरत्व की जिनकल्पी शाखा स्थविर कल्पियो से उत्तरवर्ती सिद्ध होती है। क्या हमें यह स्वीकार्य है? हम तो जिनकल्पी दिगम्बरत्व को ही मूल जैनधर्म मानते है। 10. उचित और ग्रंथकार-अभिप्रेत की धारणा का परिज्ञान :
इस संपादन को पाठ-संशोधन भी कहा गया है। इसका आधार संपादक के व्यक्तिगत औचित्य की धारणा, प्रसंग तथा उनके स्वयं के द्वारा ग्रंथकार के अभिप्रेत (भूतकालीन) का अनुमान लगाया गया है इससे आदर्श प्रति के आधार की नीति तो समाप्त होती ही है, संपादक की स्वयं की अनुमेयत्व क्षमता पर भी प्रश्नचिन्ह लगता है क्यों कि इसी तत्त्व पर तो विद्वानों में मतभेद दृष्टिगोचर हुआ है।