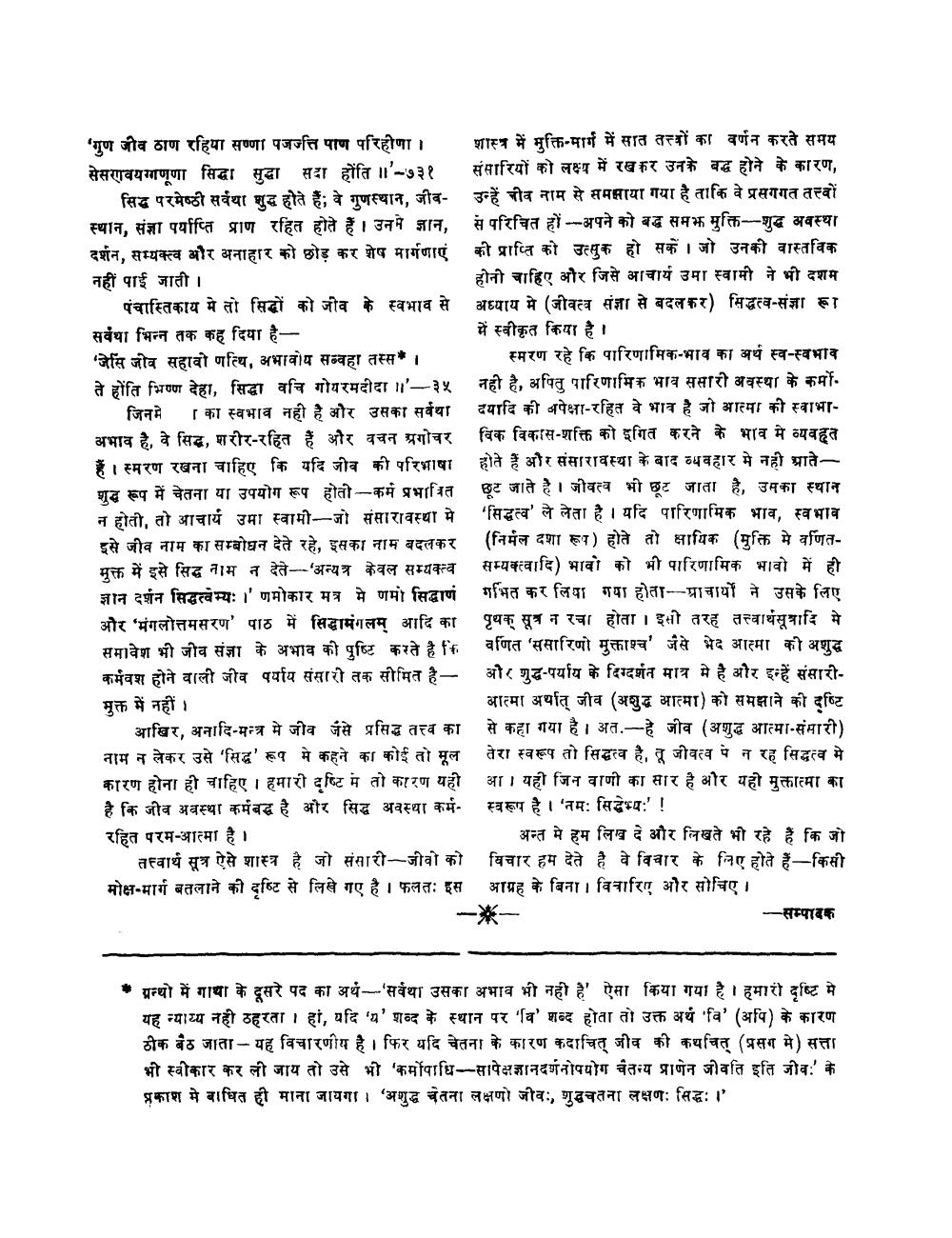________________
'गुण जीव ठाण रहिया सण्णा पजत्ति पाण परिहीणा। शास्त्र में मुक्ति-मार्ग में सात तत्त्वों का वर्णन करते समय सेसणवयग्गणूणा सिद्धा सुद्धा सदा होंति ॥'-७३१ संसारियों को लक्ष्य में रखकर उनके बद्ध होने के कारण,
सिद्ध परमेष्ठी सर्वथा शुद्ध होते हैं; वे गुणस्थान, जीव- उन्हें जीव नाम से समझाया गया है ताकि वे प्रसगगत तत्त्वों स्थान, संज्ञा पर्याप्ति प्राण रहित होते हैं। उनमें ज्ञान, से परिचित हों-अपने को बद्ध समझ मुक्ति-शुद्ध अवस्था दर्शन, सम्यक्त्व और अनाहार को छोड़ कर शेष मार्गणाएं की प्राप्ति को उत्सुक हो सके । जो उनकी वास्तविक नहीं पाई जाती।
होनी चाहिए और जिसे आचार्य उमा स्वामी ने भी दशम पंचास्तिकाय मे तो सिद्धों को जीव के स्वभाव से अध्याय मे (जीवत्व संज्ञा से बदलकर) सिद्धत्व-संज्ञा रूा सर्वथा भिन्न तक कह दिया है
में स्वीकृत किया है। 'जेसि जीव सहावो णत्थि, अभावोय सब्वहा तस्स*। स्मरण रहे कि पारिणामिक-भाव का अर्थ स्व-स्वभाव ते होंति भिण्ण देहा, सिद्धा वचि गोयरमदीदा ॥'-३५ नही है, अपितु पारिणामिक भाव ससारी अवस्था के कर्मो.
जिनमे ।का स्वभाव नहीं है और उसका सर्वथा दयादि की अपेक्षा-रहित वे भाव है जो आत्मा की स्वाभाअभाव है, वे सिद्ध, शरीर-रहित हैं और वचन अगोचर विक विकास-शक्ति को इगित करने के भाव में व्यवहत हैं। स्मरण रखना चाहिए कि यदि जीव की परिभाषा होते हैं और संसारावस्था के बाद व्यवहार मे नही पातेशुद्ध रूप में चेतना या उपयोग रूप होती-कर्म प्रभावित छूट जाते है । जीवत्व भी छूट जाता है, उसका स्थान न होती, तो आचार्य उमा स्वामी-जो संसारावस्था मे सिद्धत्व' ले लेता है । यदि पारिणामिक भाव, स्वभाव इसे जीव नाम का सम्बोधन देते रहे, इसका नाम बदलकर (निर्मल दशा रूप) होते तो क्षायिक (मुक्ति मे वणितमुक्त में इसे सिद्ध नाम न देते-- 'अन्यत्र केवल सम्यक्त्व सम्यक्त्वादि) भावो को भी पारिणामिक भावो में ही ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः।' णमोकार मत्र मे णमो सिद्धाणं गर्भित कर लिया गया होता-प्राचार्यों ने उसके लिए और 'मंगलोत्तमसरण' पाठ में सिद्धामंगलम् आदि का पृथक् सूत्र न रचा होता। इसी तरह तत्त्वार्थसूत्रादि मे समावेश भी जीव संज्ञा के अभाव की पुष्टि करते है कि वणित 'ससारिणो मुक्ताश्च' जैसे भेद आत्मा की अशुद्ध कर्मवश होने वाली जीव पर्याय संसारी तक सीमित है- और शुद्ध-पर्याय के दिग्दर्शन मात्र में है और इन्हें संसारीमुक्त में नहीं।
आत्मा अर्थात् जीव (अशुद्ध आत्मा) को समझाने की दृष्टि आखिर, अनादि-मन्त्र मे जीव जैसे प्रसिद्ध तत्त्व का से कहा गया है। अत. हे जीव (अशुद्ध आत्मा-संसारी) नाम न लेकर उसे 'सिद्ध' रूप मे कहने का कोई तो मूल तेरा स्वरूप तो सिद्धत्व है, तू जीवत्व पे न रह सिद्धत्व मे कारण होना ही चाहिए। हमारी दृष्टि में तो कारण यही आ। यही जिन वाणी का सार है और यही मुक्तात्मा का है कि जीव अवस्था कर्मबद्ध है और सिद्ध अवस्था कर्म- स्वरूप है । 'नम: सिद्धेभ्यः' ! रहित परम-आत्मा है।
अन्त मे हम लिख दे और लिखते भी रहे हैं कि जो तत्त्वार्थ सूत्र ऐसे शास्त्र है जो संसारी-जीवो को विचार हम देते है वे विचार के लिए होते हैं-किसी मोक्ष-मार्ग बतलाने की दृष्टि से लिखे गए है । फलतः इस आग्रह के बिना। विद्यारिए और सोचिए।
-सम्पादक
* ग्रन्थो में गाथा के दूसरे पद का अर्थ--'सर्वथा उसका अभाव भी नहीं है' ऐसा किया गया है। हमारी दृष्टि मे
यह न्याय्य नही ठहरता । हां, यदि 'य' शब्द के स्थान पर 'वि' शब्द होता तो उक्त अर्थ 'वि' (अपि) के कारण ठीक बैठ जाता-यह विचारणीय है। फिर यदि चेतना के कारण कदाचित् जीव की कथचित् (प्रसग मे) सत्ता भी स्वीकार कर ली जाय तो उसे भी 'कर्मोपाधि-सापेक्षज्ञानदर्शनोपयोग चैतन्य प्राणेन जीवति इति जीवः' के प्रकाश मे बाधित ही माना जायगा। 'अशुद्ध चेतना लक्षणो जीवः, शुद्धचतना लक्षण: सिद्धः ।'