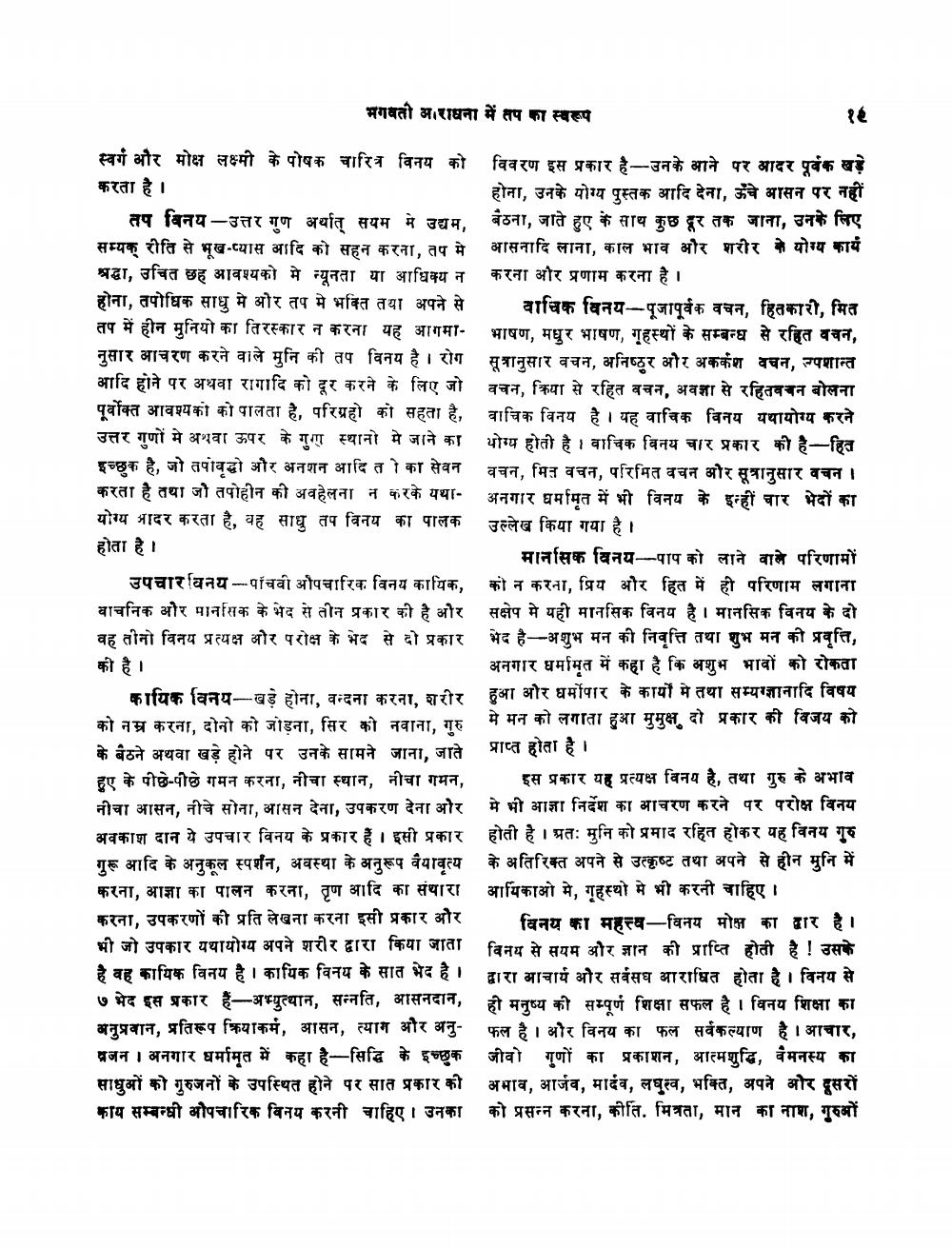________________
भगवती आराधना में तप का स्वरूप
स्वर्ग और मोक्ष लक्ष्मी के पोषक चारित्र विनय को विवरण इस प्रकार है-उनके आने पर आदर पूर्वक खड़े करता है।
होना, उनके योग्य पुस्तक आदि देना, ऊँचे आसन पर नहीं तप विनय-उत्तर गुण अर्थात् सयम मे उद्यम, बैठना, जाते हुए के साथ कुछ दूर तक जाना, उनके लिए सम्यक् रीति से भूख-प्यास आदि को सहन करना, तप मे आसनादि लाना, काल भाव और शरीर के योग्य कार्य श्रद्धा, उचित छह आवश्यको मे न्यूनता या आधिक्य न करना और प्रणाम करना है। होना, तपोधिक साधु मे और तप मे भक्ति तया अपने से वाचिक विनय-पूजापूर्वक वचन, हितकारी, मित तप में हीन मुनियो का तिरस्कार न करना यह आगमा- भाषण, मधुर भाषण, गृहस्थों के सम्बन्ध से रहित वचन, नुसार आचरण करने वाले मुनि की तप विनय है । रोग सूत्रानुसार वचन, अनिष्ठर और अकर्कश वचन, उपशान्त आदि होने पर अथवा रागादि को दूर करने के लिए जो वचन, किया से रहित वचन, अवज्ञा से रहितवचन बोलना पूर्वोक्त आवश्यको को पालता है, परिग्रहो को सहता है, वाचिक विनय है। यह वाचिक विनय यथायोग्य करने उत्तर गुणों मे अथवा ऊपर के गुण स्थानो मे जाने का योग्य होती है । वाचिक विनय चार प्रकार की है-हित इच्छुक है, जो तपोवृद्धो और अनशन आदि तो का सेवन वचन, मित वचन, परिमित वचन और सूत्रानुसार वचन । करता है तथा जो तपोहीन की अवहेलना न करके यथा
अनगार धर्मामृत में भी विनय के इन्हीं चार भेदों का योग्य आदर करता है, वह साधु तप विनय का पालक उल्लेख किया गया है। होता है।
मानसिक विनय-पाप को लाने वाले परिणामों उपचारविनय--पाँचवी औपचारिक विनय कायिक, को न करना, प्रिय और हित में ही परिणाम लगाना वाचनिक और मानसिक के भेद से तीन प्रकार की है और सक्षेप मे यही मानसिक विनय है। मानसिक विनय के दो वह तीनो विनय प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार भेद है-अशुभ मन की निवृत्ति तथा शुभ मन की प्रवृत्ति, की है।
अनगार धर्मामत में कहा है कि अशुभ भावों को रोकता कायिक विनय-खड़े होना, वन्दना करना, शरीर हुआ और धर्मापार के काया मे तथा सम्यग्ज्ञानादि विषय को नम्र करना, दोनो को जोड़ना, सिर को नवाना, गरु मे मन को लगाता हुआ मुमुक्ष दो प्रकार की विजय को के बैठने अथवा खड़े होने पर उनके सामने जाना, जाते प्राप्त होता है। हुए के पीछे-पीछे गमन करना, नीचा स्थान, नीचा गमन, इस प्रकार यह प्रत्यक्ष विनय है, तथा गुरु के अभाव नीचा आसन, नीचे सोना, आसन देना, उपकरण देना और में भी आज्ञा निर्देश का आचरण करने पर परोक्ष विनय अवकाश दान ये उपचार विनय के प्रकार हैं। इसी प्रकार होती है । अत: मुनि को प्रमाद रहित होकर यह विनय गुरु गुरू आदि के अनुकूल स्पर्शन, अवस्था के अनुरूप वैयावृत्य के अतिरिक्त अपने से उत्कृष्ट तथा अपने से हीन मुनि में करना, आज्ञा का पालन करना, तृण आदि का संथारा आर्यिकाओ मे, गृहस्थो मे भी करनी चाहिए। करना, उपकरणों की प्रति लेखना करना इसी प्रकार और विनय का महत्व-विनय मोल का द्वार है। भी जो उपकार यथायोग्य अपने शरीर द्वारा किया जाता विनय से सयम और ज्ञान की प्राप्ति होती है ! उसके है वह कायिक विनय है । कायिक विनय के सात भेद है। द्वारा आचार्य और सर्वसघ आराधित होता है। विनय से ७ भेद इस प्रकार हैं-अभ्युत्थान, सन्नति, आसनदान, ही मनुष्य की सम्पूर्ण शिक्षा सफल है । विनय शिक्षा का अनुप्रवान, प्रतिरूप क्रियाकर्म, आसन, त्याग और अनु- फल है। और विनय का फल सर्वकल्याण है। आचार, प्रजन । अनगार धर्मामृत में कहा है-सिद्धि के इच्छुक जीवो गुणों का प्रकाशन, आत्मशुद्धि, वैमनस्य क साधुओं को गुरुजनों के उपस्थित होने पर सात प्रकार की अभाव, आर्जव, मार्दव, लघुत्व, भक्ति, अपने और दूसरों काय सम्बन्धी औपचारिक विनय करनी चाहिए। उनका को प्रसन्न करना, कीति. मित्रता, मान का नाश, गुरुषों