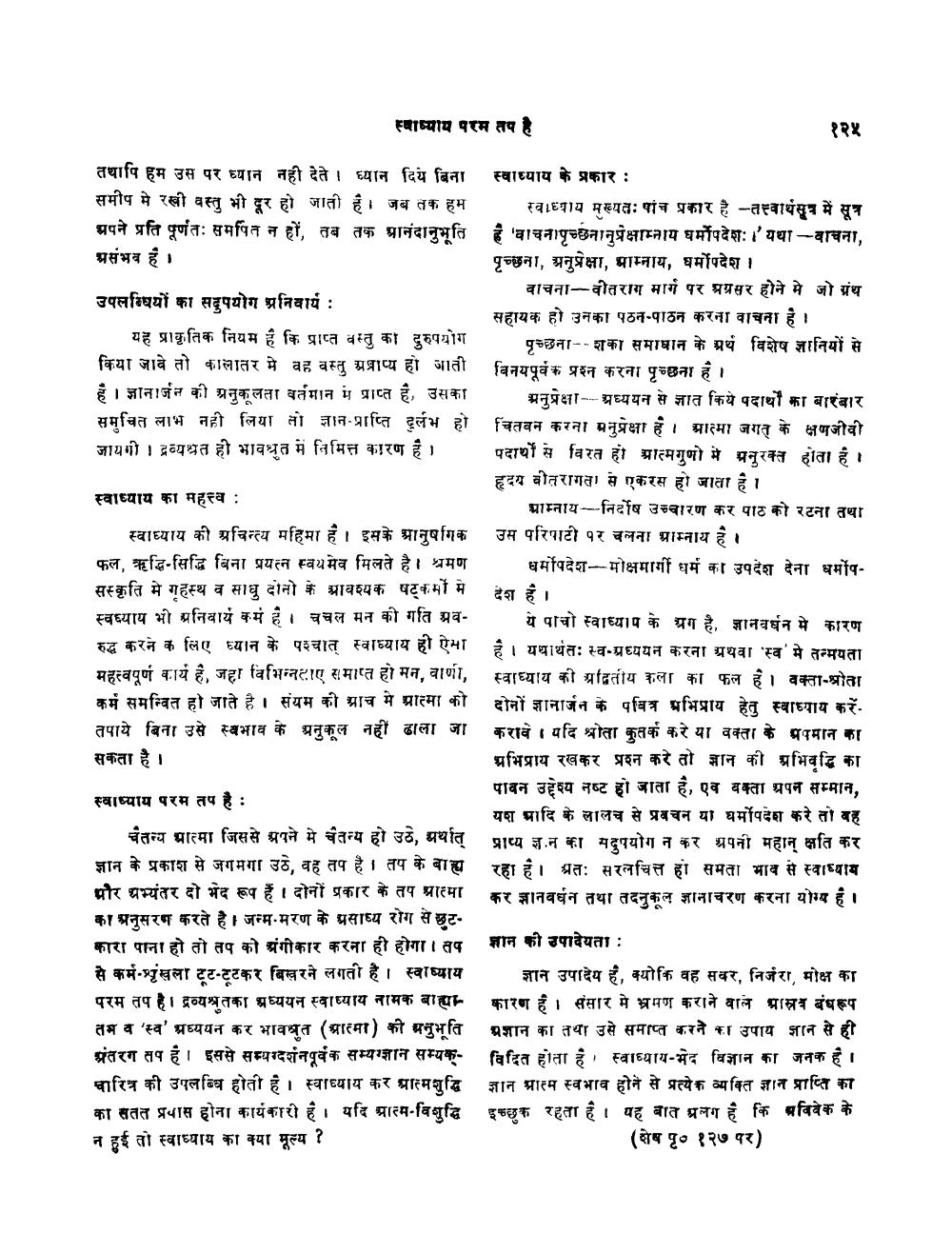________________
स्वाध्याय परम तप है
१२५
तथापि हम उस पर ध्यान नहीं देते। ध्यान दिये बिना स्वाध्याय के प्रकार : समीप मे रखी वस्तु भी दूर हो जाती है। जब तक हम स्वाध्याय मख्यतः पांच प्रकार है -तत्त्वार्थसूत्र में सूत्र अपने प्रति पूर्णतः समर्पित न हों, तब तक प्रानंदानुभूति है वाचनापच्छनानप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशः। यथा-वाचना, असंभव है।
पृच्छना, अनुप्रेक्षा, माम्नाय, धर्मोपदेश।
वाचना-वीतराग मार्ग पर अग्रसर होने मे जो ग्रंथ उपलब्धियों का सदुपयोग अनिवार्य :
सहायक हो उनका पठन-पाठन करना वाचना है। यह प्राकृतिक नियम है कि प्राप्त वस्तु का दुरुपयोग पृच्छना--शका समाधान के अर्थ विशेष ज्ञानियों से किया जावे तो कालातर मे वह वस्तु अप्राप्य हो जाती विनयपूर्वक प्रश्न करना पृच्छना है। है। ज्ञानार्जन की अनुकूलता वर्तमान में प्राप्त है, उसका
अनुप्रेक्षा अध्ययन से ज्ञात किये पदार्थों का बारंबार समचित लाभ नही लिया तो ज्ञान-प्राप्ति दुर्लभ हो चितवन करना मनुप्रेक्षा है। प्रात्मा जगत् के क्षणजीवी जायगी। द्रव्यश्रत ही भावभुत में निमित्त कारण है। पदार्थों से विरत हो प्रात्मगुणो मे अनुरक्त होता है।
हृदय वीतरागता से एकरस हो जाता है। स्वाध्याय का महत्त्व :
माम्नाय ---निर्दोष उच्चारण कर पाठ को रटना तथा स्वाध्याय की अचिन्त्य महिमा है। इसके आनुषंगिक उस परिपाटी पर चलना प्राम्नाय है। फल, ऋद्धि-सिद्धि बिना प्रयत्न स्वयमेव मिलते है। श्रमण धर्मोपदेश-मोक्षमार्गी धर्म का उपदेश देना धर्मोपसस्कृति मे गृहस्थ व साधु दोनो के आवश्यक षट्कमों मे देश है। स्वध्याय भी अनिवार्य कम है। चचल मन को गति अव- ये पाचो स्वाध्याप के अग है, ज्ञानवर्धन मे कारण रुद्ध करने के लिए ध्यान के पश्चात् स्वाध्याय ही ऐमा है। यथार्थतः स्व-प्रध्ययन करना अथवा 'स्व' मे तन्मयता महत्त्वपूर्ण कार्य है, जहा विभिन्नटाए समाप्त हो मन, वाणी, स्वाध्याय की अद्वितीय कला का फल है। वक्ता-श्रोता कर्म समन्वित हो जाते है। संयम की प्राच मे प्रात्मा को दोनों ज्ञानार्जन के पवित्र अभिप्राय हेतु स्वाध्याय करें तपाये बिना उसे स्वभाव के अनुकूल नहीं ढाला जा करावे । यदि श्रोता कुतर्क करे या वक्ता के अपमान का सकता है।
अभिप्राय रखकर प्रश्न करे तो ज्ञान की अभिवृद्धि का
पावन उद्देश्य नष्ट हो जाता है, एव बक्ता अपन सम्मान, स्वाध्याय परम तप है:
यश प्रादि के लालच से प्रवचन या धर्मोपदेश करे तो वह चैतन्य मात्मा जिससे अपने मे चैतन्य हो उठे, अर्थात् प्राप्य ज्ञान का सदुपयोग न कर अपनी महान् क्षति कर ज्ञान के प्रकाश से जगमगा उठे, वह तप है । तप के बाह्य रहा है। प्रतः सरलचित्त हो समता भाव से स्वाध्याय पौर अभ्यंतर दो भेद रूप हैं। दोनों प्रकार के तप प्रात्मा कर ज्ञानवर्धन तथा तदनुकल ज्ञानाचरण करना योग्य है। का अनुसरण करते है। जन्म-मरण के प्रसाध्य रोग से छुटकारा पाना हो तो तप को अंगीकार करना ही होगा। तप ज्ञान की उपादेयता : से कर्म शृंखला टूट-टूटकर बिखरने लगती है। स्वाध्याय ज्ञान उपादेय है, क्योकि वह सवर, निर्जरा, मोक्ष का परम तप है। द्रव्यश्रुतका अध्ययन स्वाध्याय नामक बाह्या कारण है। संसार में भ्रमण कराने वाले प्रास्रव बंधरूप तम व 'स्व' अध्ययन कर भावश्रुत (आत्मा) की अनुभूति प्रज्ञान का तथा उसे समाप्त करने का उपाय ज्ञान से ही अंतरग सप है। इससे सम्यग्दर्शनपूर्वक सम्यग्ज्ञान सम्यक- विदित होता है। स्वाध्याय-भेद विज्ञान का जनक है । चारित्र की उपलब्धि होती है। स्वाध्याय कर प्रात्मशुद्धि ज्ञान प्रात्म स्वभाव होने से प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति का का सतत प्रयास होना कार्यकारी है। यदि प्रात्म-विशुद्धि इच्छुक रहता है। यह बात अलग है कि अविवेक के न हुई तो स्वाध्याय का क्या मूल्य ?
(शेष पृ० १२७ पर)