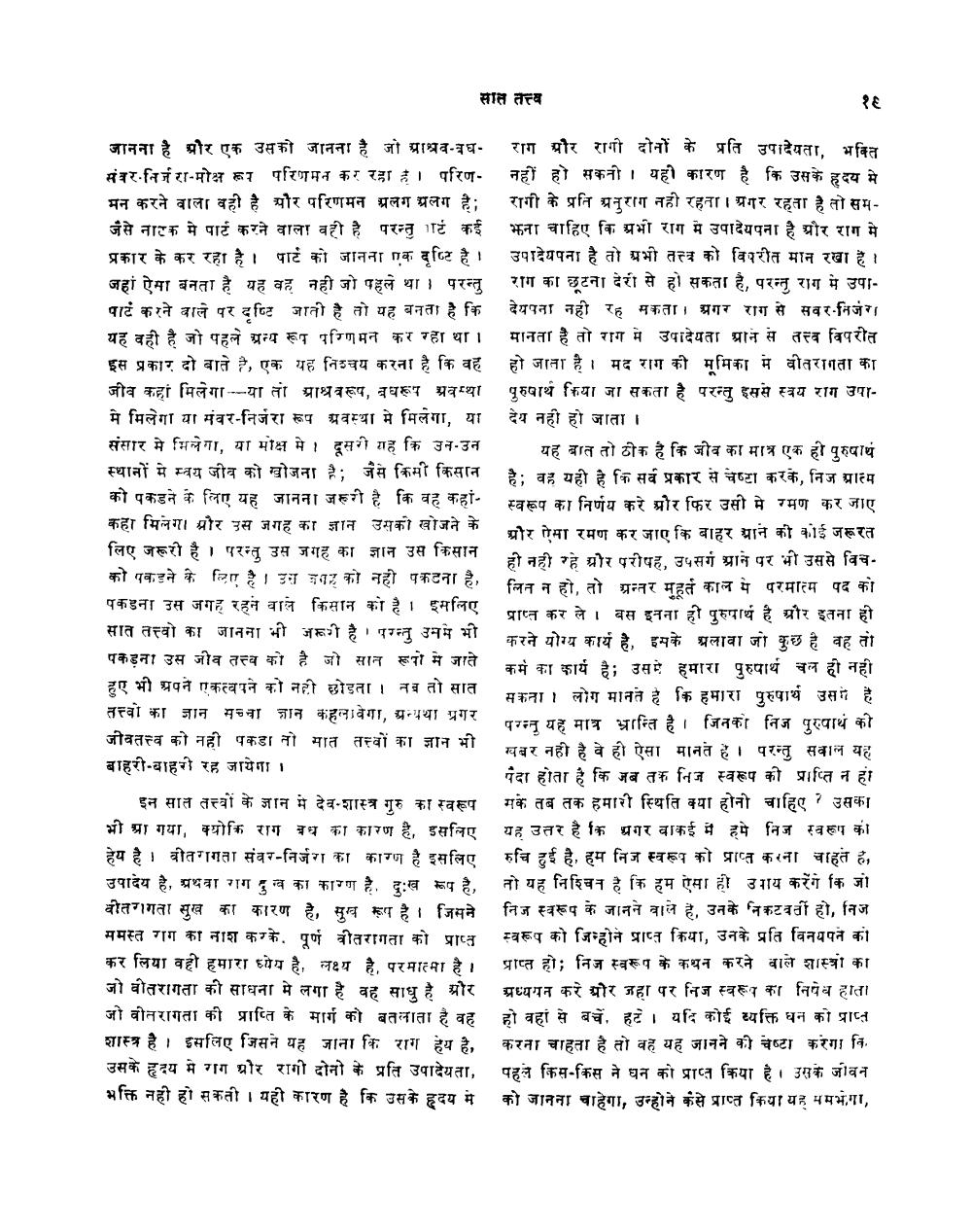________________
सात तत्त्व
जानना है और एक उसको जानना है जो प्राश्रव-वधसंवर. निर्जरा मोक्ष रूप परिणमत कर रहा है। परिणमन करने वाला वही है और परिणमत अलग अलग है; जैसे नाटक मे पार्ट करने वाला वही है परन्तु कई प्रकार के कर रहा है। पार्ट को जानना एक दृष्टि है । जहां ऐसा बनता है यह वह नहीं जो पहले था परन्तु पार्ट करने वाले पर दृष्टि जाती है तो यह बनता है कि यह वही है जो पहले यमन कर रहा था। इस प्रकार दो बाते है, एक यह निश्चय करना है कि वह जीव कहां मिलेगा - या तो आश्रवरूप, बधरूप अवस्था मे मिलेगा या संवर- निर्जरा रूप अवस्था मे मिलेगा, या संसार मे मिलेगा, या मोक्ष मे । दूसरी यह कि उन-उन स्थानों में स्वय जीव को खोजना है; जैसे किसी किसान को पकड़ने के लिए यह जानना जरूरी है कि वह कहांकहा मिलेगा और उस जगह का ज्ञान उसको खोजने के लिए जरूरी है । परन्तु उस जगह का ज्ञान उस किसान को पकड़ने के लिए है। उसको नहीं पकड़ना है, पकड़ना उस जगह रहने वाले किसान को है। इसलिए सात तत्त्वों का जानना भी जरूरी है। परन्तु उनमे भी पकड़ना उस जीव तत्त्व को है जो सान रूपों में जाते हुए भी अपने एकस्वपने को नहीं छोड़ता। नव तो सात तत्त्वों का ज्ञान सच्चा ज्ञान कहलावेगा, अन्यथा प्रगर जीवतत्त्व को नहीं पकड़ा तो सात तत्त्वों का ज्ञान भी बाहरी बाहरी रह जायेगा।
इन सात तत्त्वों के जान मे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप भी आ गया, क्योकि राग वध का कारण है, इसलिए हेय है। वीतरागता संनिग का कारण है इसलिए उपादेय है, अथवा राग दुख का कारण है, दुःख रूप है, वीतरागता सुख का कारण है, सुख रूप है। जिसने समस्त राग का नाश करके. पूर्ण वीतरागता को प्राप्त कर लिया वही हमारा ध्येय है, लक्ष्य है, परमात्मा है । ओ वीतरागता की साधना में लगा है वह साधु है और Satara की प्राप्ति के मार्ग को बतलाता है वह शास्त्र है। इसलिए जिसने यह जाना कि राग हेय है, उसके मे राग और रागी दोनो के प्रति उपादेयता, भक्ति नही हो सकती । यही कारण है कि उसके हृदय में
१६
राग और रानी दोनों के प्रति उपादेयता भवित नहीं हो सकती। यही कारण है कि उसके हृदय मे रागी के प्रति अनुराग नही रहता। अगर रहता है तो समझना चाहिए कि अभी राग में उपादेयपना है और राग मे उपादेयपना है तो अभी तत्व को विपरीत मान रखा है। राग का छूटना देरी से हो सकता है, परन्तु राग में उपादेयपना नहीं रह सकता। अगर राग से सवर-निजंग मानता है तो राग में उपादेयता श्राने से तत्त्व विपरीत हो जाता है। मद राम की भूमिका में वीतरागता का पुरुषार्थ किया जा सकता है परन्तु इससे स्वयं राग उपादेय नहीं हो जाता ।
यह बात तो ठीक है कि जीव का मात्र एक ही पुरुषार्थ है; वह यही है कि सर्व प्रकार से चेष्टा करके, निजाम स्वरूप का निर्णय करे और फिर उसी मे रमण कर जाए और ऐसा रमण कर जाए कि बाहर पाने की कोई जरूरत ही नही रहे और परीषह, उपसर्ग भ्राने पर भी उससे विच लिन न हो, तो ग्रन्तर मुहूर्त काल मे परमात्म पद को प्राप्त कर ले | बस इतना ही पुरुषार्थ है और इतना ही करने योग्य कार्य है, इसके अलावा जो कुछ है वह तो कर्म का कार्य है; उसमे हमारा पुरुषार्थ चल ही नहीं सकता । लोग मानते है कि हमारा पुरुषार्थ उसमें है परन्तु यह मात्र भ्रान्ति है जिनको निज पुरवा की पर नहीं है वे ही ऐसा मानते है परन्तु सवाल यह पैदा होता है कि जब तक निज स्वरूप की प्राप्ति न हो मके तब तक हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए ? उसका यह उत्तर है कि अगर वाकई में हमे निज स्वरूप की रुचि हुई है, हम निज स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह निश्चित है कि हम ऐसा ही आय करेंगे कि जो निज स्वरूप के जानने वाले है, उनके निकटवर्ती हो, निज स्वरूप को जिन्होने प्राप्त किया, उनके प्रति विनय को प्राप्त हो; निज स्वरूप के कथन करने वाले शास्त्रों का अध्ययन करे और जहा पर निज स्वरूप का निषेव हाता हो वहां से बचें, हटे । यदि कोई व्यक्ति धन को प्राप्त करना चाहता है तो वह यह जानने की चेष्टा करेगा कि.. पहले किस-किस ने धन को प्राप्त किया है। उसके जीवन को जानना चाहेगा, उन्होंने कैसे प्राप्त किया यह गा