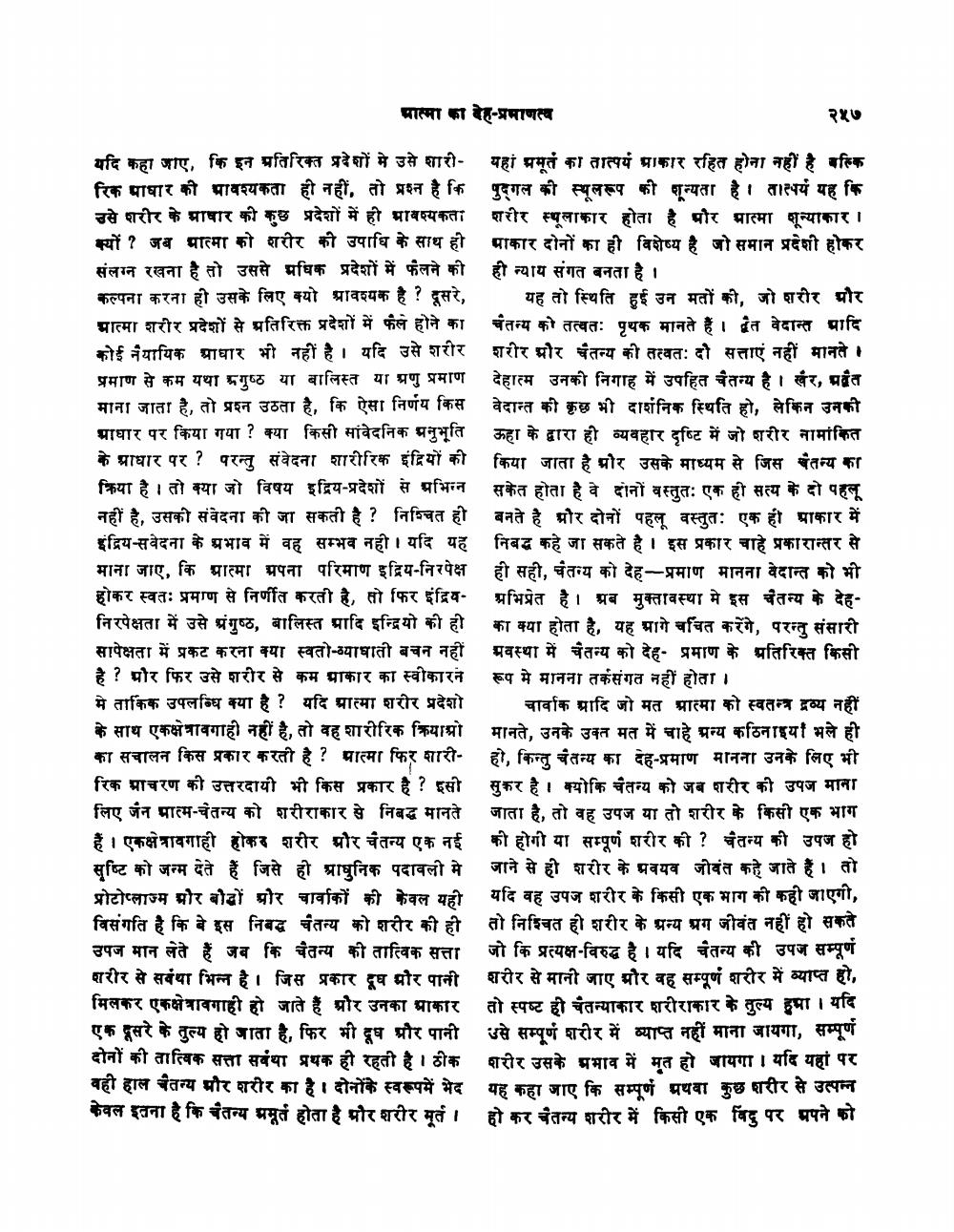________________
मात्मा का देह-प्रमाणत्व
यदि कहा जाए कि इन अतिरिक्त प्रदेशों मे उसे धारीरिक माधार की प्रावश्यकता ही नहीं, तो प्रश्न है कि उसे शरीर के माधार की कुछ प्रदेशों में ही भावश्यकता क्यों ? जब मात्मा को शरीर की उपाधि के साथ ही संलग्न रखना है तो उससे अधिक प्रदेशों में फैलने की कल्पना करना ही उसके लिए क्यो श्रावश्यक है ? दूसरे, आत्मा शरीर प्रदेशों से प्रतिरिक्त प्रदेशों में फैले होने का कोई नैयायिक आधार भी नहीं है । यदि उसे शरीर प्रमाण से कम यथा ऋगुष्ठ या बालिस्त या प्रणु प्रमाण माना जाता है, तो प्रश्न उठता है, कि ऐसा निर्णय किस आधार पर किया गया? क्या किसी सांवेदनिक अनुभूति के आधार पर ? परन्तु संवेदना शारीरिक इंद्रियों की क्रिया है । तो क्या जो विषय इद्रिय प्रदेशों से अभिन्न नहीं है, उसकी संवेदना की जा सकती है ? निश्चित ही इंद्रिय संवेदना के प्रभाव में वह सम्भव नहीं। यदि यह माना जाए कि मात्मा अपना परिमाण इंद्रिय-निरपेक्ष होकर स्वतः प्रमाण से निर्णीत करती है, तो फिर इंद्रिय निरपेक्षता में उसे बंगुष्ठ, बालिस्त भादि इन्द्रियों की ही सापेक्षता में प्रकट करना क्या स्वतो व्याघाती बचन नहीं है ? और फिर उसे शरीर से कम माकार का स्वीकारनं मे तार्किक उपलब्धि क्या है ? यदि श्रात्मा शरीर प्रदेशो के साथ एकक्षेणावगाही नहीं है, तो वह शारीरिक क्रियाओ का सचालन किस प्रकार करती है ? मात्मा फिर शारीरिक घाचरण की उत्तरदायी भी किस प्रकार है ? इसी लिए जंन मात्म- चैतन्य को शरीराकार से निबद्ध मानते हैं । एकक्षेत्रावगाही होकर शरीर और चैतन्य एक नई सृष्टि को जन्म देते हैं जिसे ही प्राधुनिक पदावली मे प्रोटोप्लाज्म मोर बौद्धों मोर चार्वाकों की केवल यही विसंगति है कि वे इस निबद्ध चैतन्य को शरीर की हो उपज मान लेते हैं जब कि चैतन्य की तात्विक सत्ता शरीर से सर्वथा भिन्न है जिस प्रकार दूध और पानी मिलकर एकक्षेत्रावगाही हो जाते हैं और उनका प्राकार एक दूसरे के तुल्य हो जाता है, फिर भी दूध और पानी दोनों की तात्विक सत्ता सर्वथा प्रथक ही रहती है। ठीक वही हाल चैतन्य और शरीर का है। दोनोंके स्वरूपमें भेद केवल इतना है कि चैतन्य अमूर्त होता है और शरीर मूर्त ।
२५७
यहां अमूर्त का तात्पर्य प्राकार रहित होना नहीं है बल्कि पुद्गल की स्थूलरूप की शून्यता है। वास्प यह कि शरीर स्थूलाकार होता है मोर भात्मा शून्याकार । माकार दोनों का ही विशेष्य है जो समान प्रदेशी होकर ही न्याय संगत बनता है। ।
यह तो स्थिति हुई उन मतों की, जो शरीर मौर चैतन्य को तत्वतः पृथक मानते हैं । द्वैत वेदान्त प्रादि शरीर और चैतन्य की तत्वतः दो सत्ताएं नहीं मानते । देहात्म उनकी निगाह में उपहित चैतन्य है। खर वेदान्त की कुछ भी दार्शनिक स्थिति हो, लेकिन उनकी कहा के द्वारा ही व्यवहार दृष्टि में जो शरीर नामांकित किया जाता है और उसके माध्यम से जिस चैतन्य का सकेत होता है वे दोनों वस्तुतः एक ही सत्य के दो पहलू बनते है और दोनों पहलू वस्तुतः एक ही प्राकार में निबद्ध कहे जा सकते है । इस प्रकार चाहे प्रकारान्तर से ही सही, चैतन्य को देह प्रमाण मानना वेदान्त को भी अभिप्रेत है अब मुक्तावस्था मे इस चैतन्य के देहका क्या होता है, यह भागे चर्चित करेंगे, परन्तु संसारी अवस्था में चैतन्य को देह प्रमाण के अतिरिक्त किसी रूप में मानना तर्कसंगत नहीं होता ।
।
चार्वाक प्रादि जो मत श्रात्मा को स्वतन्त्र द्रव्य नहीं मानते, उनके उक्त मत में चाहे अन्य कठिनाइयाँ भले ही हो, किन्तु चैतन्य का देह प्रमाण मानना उनके लिए भी सुकर है । क्योकि चैतन्य को जब शरीर की उपज माना जाता है, तो वह उपज या तो शरीर के किसी एक भाग की होगी या सम्पूर्ण शरीर की ? चैतन्य की उपज हो जाने से ही शरीर के अवयव जीवंत कहे जाते हैं। तो यदि वह उपज शरीर के किसी एक भाग की कही जाएगी, तो निश्चित ही शरीर के अन्य धग जीवंत नहीं हो सकते जो कि प्रत्यक्ष विरुद्ध है। यदि चैतन्य की उपज सम्पूर्ण शरीर से मानी जाए और वह सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त हो, तो स्पष्ट ही चैतन्याकार शरीराकार के तुल्य हुमा यदि उसे सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त नहीं माना जायगा, सम्पूर्ण शरीर उसके प्रभाव में मृत हो जायगा । यदि यहां पर यह कहा जाए कि सम्पूर्ण अथवा कुछ शरीर से उत्पन्न हो कर चैतन्य शरीर में किसी एक बिंदु पर अपने को