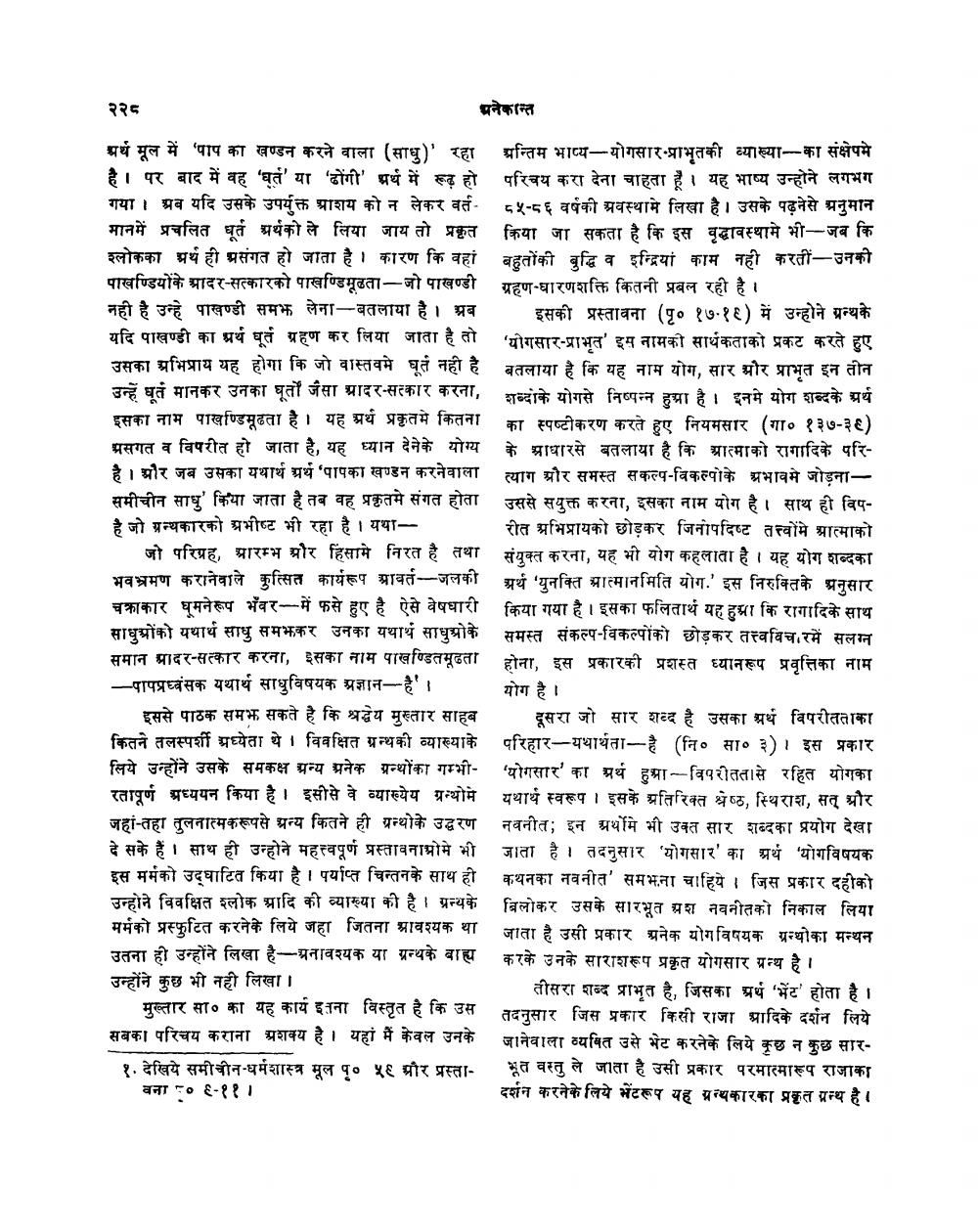________________
२२८
अनेकान्त
अर्थ मूल में 'पाप का खण्डन करने वाला (साधु)' रहा अन्तिम भाप्य-योगसार-प्राभूतकी व्याख्या-का संक्षेपमे है। पर बाद में वह 'धर्त' या 'ढोंगी' अर्थ में रूढ़ हो परिचय करा देना चाहता हूँ। यह भाष्य उन्होने लगभग गया। अब यदि उसके उपर्युक्त प्राशय को न लेकर वर्त- ८५-८६ वर्षकी अवस्थामे लिखा है। उसके पढ़नेसे अनुमान मानमें प्रचलित धूर्त अर्थको ले लिया जाय तो प्रकृत किया जा सकता है कि इस वृद्धावस्थामे भी-जब कि श्लोकका अर्थ ही प्रसंगत हो जाता है। कारण कि वहां बहतोंकी बुद्धि व इन्द्रियां काम नहीं करतीं-उनकी पाखण्डियोंके आदर-सत्कारको पाखण्डिमूढता-जो पाखण्डी ग्रहण-धारणशक्ति कितनी प्रबल रही है। नही है उन्हे पाखण्डी समझ लेना-बतलाया है। अब इसकी प्रस्तावना (पृ० १७.१६) में उन्होंने ग्रन्थके यदि पाखण्डी का अर्थ घूर्त ग्रहण कर लिया जाता है तो 'योगसार-प्राभत' इस नामको सार्थकताको प्रकट करते हुए उसका अभिप्राय यह होगा कि जो वास्तवमे घूर्त नहीं है बतलाया है कि यह नाम योग, सार और प्राभृत इन तीन उन्हें धूत मानकर उनका घूर्तों जैसा प्रादर-सत्कार करना, अनमोनिया
शब्दांके योगसे निष्पन्न हुआ है। इनमे योग शब्दके अर्थ इसका नाम पाखण्डिमूढता है। यह अर्थ प्रकृतमे कितना का स्पष्टीकरण करते हुए नियमसार (गा० १३७-३६) असगत व विपरीत हो जाता है, यह ध्यान देनेके योग्य के प्राधारसे बतलाया है कि आत्माको रागादिके परिहै। और जब उसका यथार्थ अर्थ 'पापका खण्डन करनेवाला त्याग और समस्त सकल्प-विकल्पोके अभावमे जोड़नासमीचीन साधु' किया जाता है तब वह प्रकृतमे संगत होता उससे सयुक्त करना, इसका नाम योग है। साथ ही विपहै जो ग्रन्थकारको अभीष्ट भी रहा है । यथा-
रीत अभिप्रायको छोड़कर जिनोपदिष्ट तत्त्वोंमे आत्माको जो परिग्रह, प्रारम्भ और हिंसामे निरत है तथा संयुक्त करना, यह भी योग कहलाता है । यह योग शब्दका भवभ्रमण करानेवाले कुत्सित कार्यरूप प्रावर्त-जलकी अर्थ 'युनक्ति पात्मानमिति योग.' इस निरुक्तिके अनुसार चक्राकार घूमनेरूप भँवर-में फसे हुए है ऐसे वेषधारी किया गया है । इसका फलितार्थ यह हुमा कि रागादिके साथ साधुओंको यथार्थ साधु समझकर उनका यथार्थ साधुअोके समस्त संकल्प-विकल्पोंको छोड़कर तत्त्वविच रमें सलग्न समान प्रादर-सत्कार करना, इसका नाम पाखण्डितमूढता होना, इस प्रकारकी प्रशस्त ध्यानरूप प्रवृत्तिका नाम —पापप्रध्वंसक यथार्थ साधुविषयक अज्ञान-है।
इससे पाठक समझ सकते है कि श्रद्धेय मुख्तार साहब दूसरा जो सार शब्द है उसका अर्थ विपरीतताका कितने तलस्पर्शी अध्येता थे। विवक्षित ग्रन्थकी व्याख्याके परिहार-यथार्थता-है (नि० सा० ३)। इस प्रकार लिये उन्होंने उसके समकक्ष अन्य अनेक ग्रन्थोंका गम्भी- 'योगसार' का अर्थ हुआ-विपरीततासे रहित योगका रतापूर्ण अध्ययन किया है। इसीसे वे व्याख्येय ग्रन्थोमे ___ यथार्थ स्वरूप । इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ, स्थिराश, सत् और जहां-तहा तुलनात्मकरूपसे अन्य कितने ही ग्रन्थोके उद्धरण नवनीत; इन अर्थोमे भी उक्त सार शब्दका प्रयोग देखा दे सके हैं। साथ ही उन्होने महत्त्वपूर्ण प्रस्तावनामोमे भी जाता है। तदनुसार 'योगसार' का अर्थ 'योगविषयक इस मर्मको उद्घाटित किया है । पर्याप्त चिन्तनके साथ ही कथनका नवनीत' समझना चाहिये। जिस प्रकार दहीको उन्होने विवक्षित श्लोक प्रादि की व्याख्या की है। ग्रन्यके बिलोकर उसके सारभूत प्रश नवनीतको निकाल लिया मर्मको प्रस्फुटित करनेके लिये जहा जितना आवश्यक था जाता है उसी प्रकार अनेक योगविषयक ग्रन्थोका मन्थन उतना ही उन्होंने लिखा है-अनावश्यक या ग्रन्थके बाह्य करके उनके साराशरूप प्रकृत योगसार ग्रन्थ है। उन्होंने कुछ भी नही लिखा।
तीसरा शब्द प्राभूत है, जिसका अर्थ 'भेंट' होता है। मुख्तार सा० का यह कार्य इतना विस्तृत है कि उस तदनुसार जिस प्रकार किसी राजा आदिके दर्शन लिये सबका परिचय कराना अशक्य है। यहां मैं केवल उनके जानेवाला व्यक्ति उसे भेट करनेके लिये कुछ न कुछ सार१. देखिये समीचीन-धर्मशास्त्र मूल १० ५६ और प्रस्ता- भूत वस्तु ले जाता है उसी प्रकार परमात्मारूप राजाका वना ०६-११।
दर्शन करने के लिये भेंटरूप यह ग्रन्थकारका प्रकृत ग्रन्थ है।