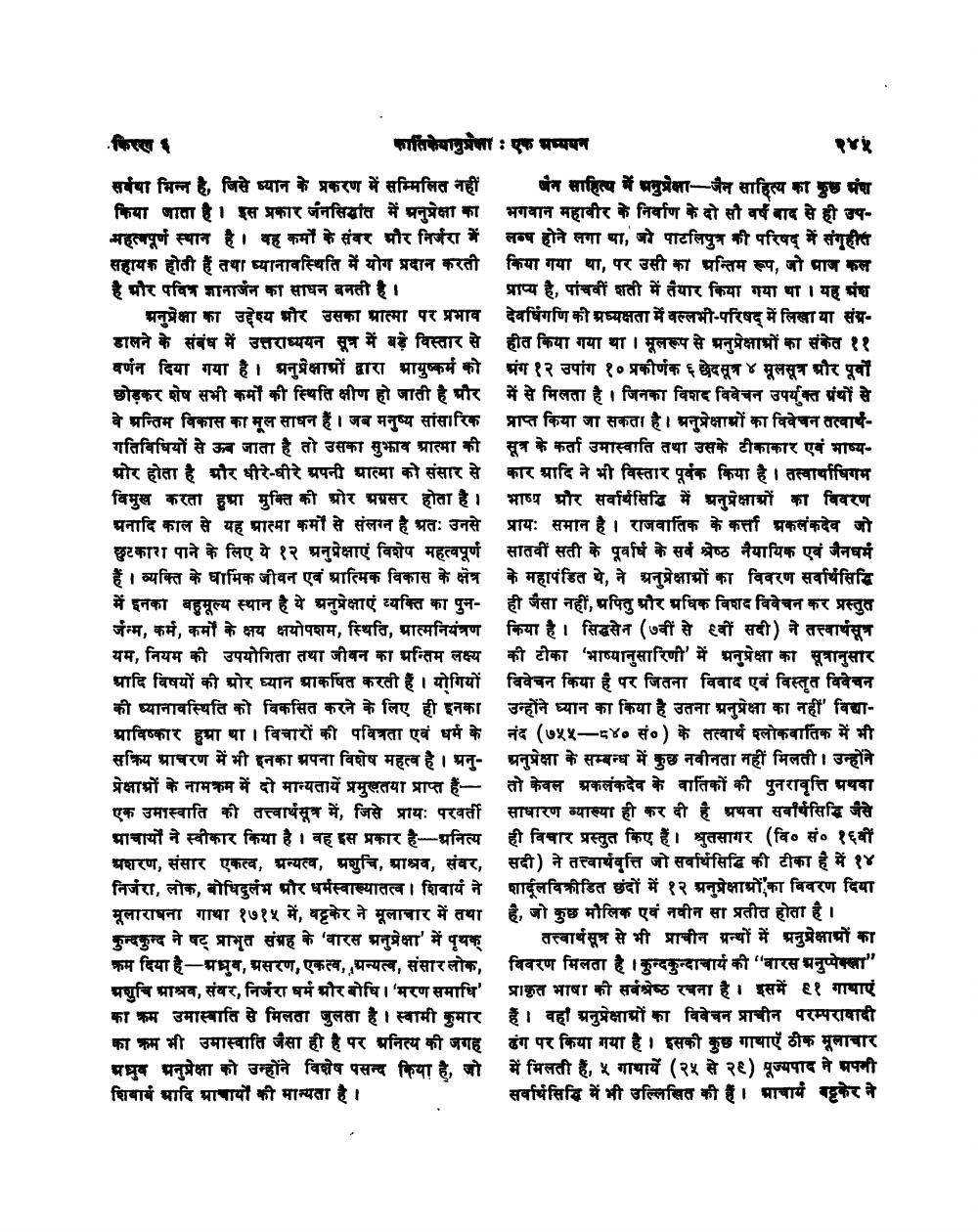________________
कातिकेयानुप्रेणा : एक अध्ययन
२४५ सर्वथा भिन्न है, जिसे ध्यान के प्रकरण में सम्मिलित नहीं जैन साहित्य में अनुप्रेक्षा-जैन साहित्य का कुछ अंश किया जाता है। इस प्रकार जनसिांत में अनुप्रेक्षा का भगवान महावीर के निर्वाण के दो सौ वर्ष बाद से ही उपमहत्वपूर्ण स्थान है। वह कर्मों के संवर मौर निर्जरा में लष होने लगा था, जो पाटलिपुत्र की परिषद् में संग्रहीत सहायक होती हैं तथा ध्यानावस्थिति में योग प्रदान करती किया गया था, पर उसी का अन्तिम रूप, जो पाजकल है और पवित्र ज्ञानार्जन का साधन बनती है।
प्राप्य है, पांचवीं शती में तैयार किया गया था। यह अंश अनुप्रेक्षा का उद्देश्य और उसका प्रात्मा पर प्रभाव देवर्षिगणि की अध्यक्षता में वल्लभी-परिषद् में लिखा या संग्रडालने के संबंध में उत्तराध्ययन सूत्र में बड़े विस्तार से हीत किया गया था। मूलरूप से अनुप्रेक्षानों का संकेत ११ वर्णन दिया गया है। अनुप्रेक्षात्रों द्वारा आयुष्कर्म को भंग १२ उपांग १० प्रकीर्णक ६ छेदसूत्र ४ मूलसूत्र और पूर्वी छोड़कर शेष सभी कर्मों की स्थिति क्षीण हो जाती है और में से मिलता है । जिनका विशद विवेचन उपर्युक्त ग्रंथों से वे अन्तिम विकास का मूल साधन हैं। जब मनुष्य सांसारिक प्राप्त किया जा सकता है। अनुप्रेक्षामों का विवेचन तत्वार्थगतिविधियों से ऊब जाता है तो उसका सुझाव प्रात्मा की सूत्र के कर्ता उमास्वाति तथा उसके टीकाकार एवं भाष्यपोर होता है और धीरे-धीरे अपनी मात्मा को संसार से कार आदि ने भी विस्तार पूर्वक किया है। तत्वार्थाधिगम विमुख करता हुमा मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। भाष्य और सर्वार्थसिद्धि में अनुप्रेक्षाओं का विवरण अनादि काल से यह प्रात्मा कर्मों से संलग्न है अतः उनसे प्रायः समान है। राजवार्तिक के कर्ता प्रकलंकदेव जो छुटकारा पाने के लिए ये १२ अनुप्रेक्षाएं विशेष महत्वपूर्ण सातवीं सती के पूर्वार्ष के सर्व श्रेष्ठ नैयायिक एवं जैनधर्म हैं । व्यक्ति के धार्मिक जीवन एवं प्रात्मिक विकास के क्षेत्र के महापंडित थे, ने अनुप्रेक्षामों का विवरण सर्वार्थसिद्धि में इनका बहुमूल्य स्थान है ये अनुप्रेक्षाएं व्यक्ति का पुन- ही जैसा नहीं, अपितु और अधिक विशद विवेचन कर प्रस्तुत जन्म, कर्म, कर्मों के क्षय क्षयोपशम, स्थिति, प्रात्मनियंत्रण किया है। सिद्धसेन (७वीं से वीं सदी) ने तत्त्वार्थसूत्र यम, नियम की उपयोगिता तथा जीवन का अन्तिम लक्ष्य की टीका 'भाष्यानुसारिणी' में अनुप्रेक्षा का सूत्रानुसार आदि विषयों की ओर ध्यान प्राकर्षित करती हैं । योगियों विवेचन किया है पर जितना विवाद एवं विस्तृत विवेचन की ध्यानावस्थिति को विकसित करने के लिए ही इनका उन्होंने ध्यान का किया है उतना अनुप्रेक्षा का नहीं विद्यामाविष्कार हुआ था। विचारों की पवित्रता एवं धर्म के नंद (७५५-८४० सं०) के तत्वार्थ श्लोकवार्तिक में भी सक्रिय आचरण में भी इनका अपना विशेष महत्व है । अनु- अनुप्रेक्षा के सम्बन्ध में कुछ नवीनता नहीं मिलती। उन्होंने प्रेक्षामों के नामक्रम में दो मान्यतायें प्रमुखतया प्राप्त हैं- तो केवल अकलंकदेव के वार्तिकों की पुनरावृत्ति अथवा एक उमास्वाति की तत्त्वार्थसूत्र में, जिसे प्रायः परवर्ती साधारण ब्याख्या ही कर दी है अथवा सर्वार्थसिद्धि जैसे प्राचार्यों ने स्वीकार किया है। वह इस प्रकार है-अनित्य ही विचार प्रस्तुत किए हैं। श्रुतसागर (वि० सं० १६वीं मशरण, संसार एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, पाश्रव, संवर, सदी) ने तत्त्वार्थवृत्ति जो सर्वार्थसिद्धि की टीका है में १४ निर्जरा, लोक, बोधिदुर्लभ और धर्मस्वाख्यातत्व। शिवायं ने शार्दूलविक्रीडित छंदों में १२ अनुप्रेक्षाओं का विवरण दिया मूलाराधना गाथा १७१५ में, वट्टकेर ने मूलाचार में तथा है, जो कुछ मौलिक एवं नवीन सा प्रतीत होता है। कुन्दकुन्द ने षट् प्राभूत संग्रह के 'वारस अनुप्रेक्षा' में पृथक् तत्त्वार्थ सूत्र से भी प्राचीन ग्रन्थों में अनुप्रेक्षामों का क्रम दिया है-अध्रुव, असरण, एकत्व, अन्यत्व, संसारलोक, विवरण मिलता है ।कुन्दकुन्दाचार्य की "वारस अनुप्पेला" मशुचि पाश्रव, संवर, निर्जरा धर्म और बोधि । 'मरण समाधि' प्राकृत भाषा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसमें ६१ गाथाएं का क्रम उमास्वाति से मिलता जुलता है। स्वामी कुमार हैं। वहां अनुप्रेक्षाओं का विवेचन प्राचीन परम्परावादी का क्रम भी उमास्वाति जैसा ही है पर अनित्य की जगह ढंग पर किया गया है। इसकी कुछ गाथाएं ठीक मूलाचार मध्रुव अनुप्रेक्षा को उन्होंने विशेष पसन्द किया है, जो में मिलती है, ५ गाथायें (२५ से २९) पूज्यपाद ने अपनी शिबाब मादि प्राचार्यों की मान्यता है।
सर्वार्थ सिद्धि में भी उल्लिखित की है। प्राचार्य बट्टकेर ने
१ गाया
विवेचन
किया गया