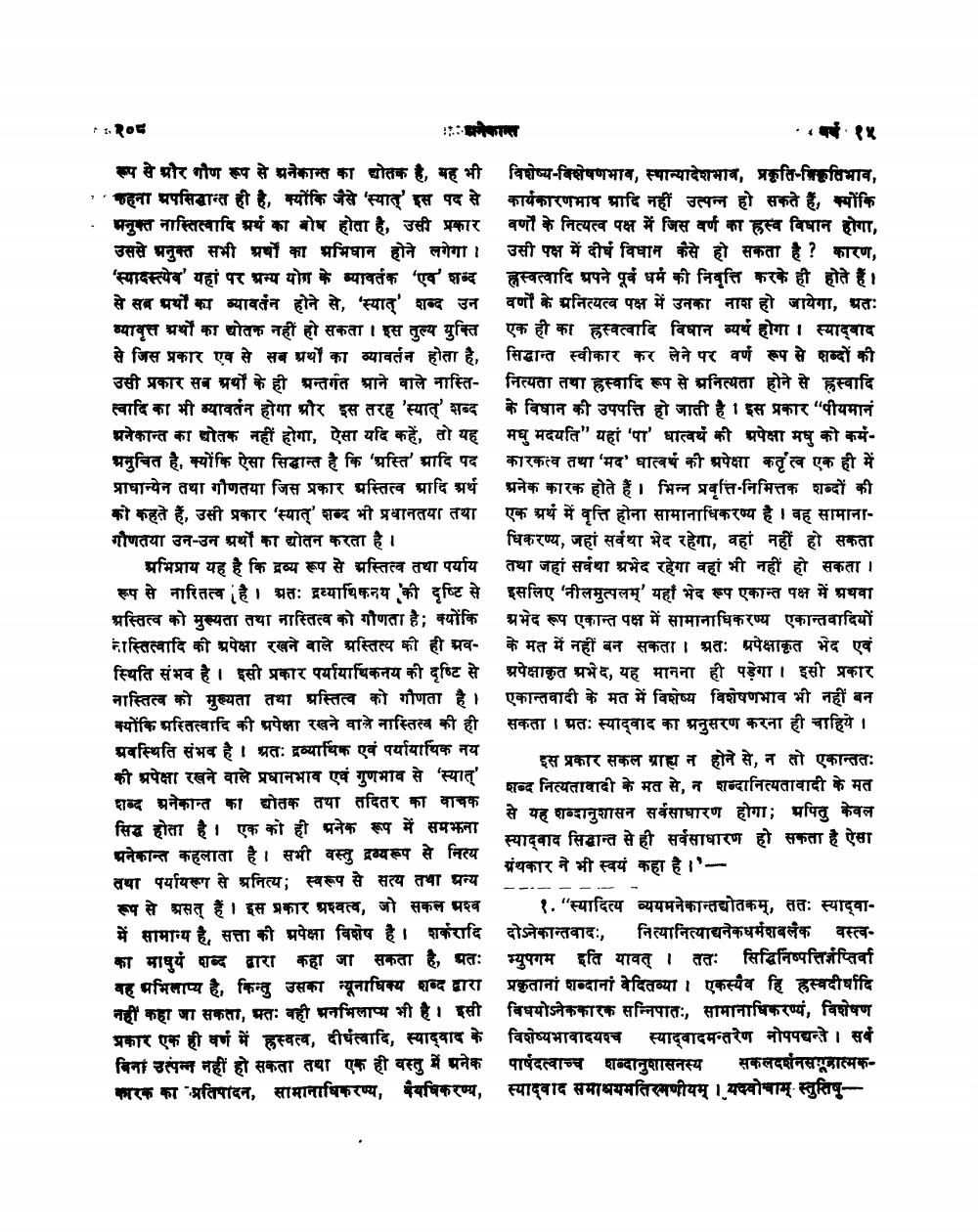________________
२००
रूप से और गौण रूप से अनेकान्त का द्योतक है, यह भी विशेष्य-विशेषणभाव, स्थान्यादेशभाव, प्रकृति-विकृतिभाव, कहना पसिद्धान्त ही है, क्योंकि जैसे 'स्यात्' इस पद से कार्यकारणभाव प्रादि नहीं उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि मनुक्त नास्तित्वादि अर्थ का बोष होता है, उसी प्रकार वर्णों के नित्यत्व पक्ष में जिस वर्ण का ह्रस्व विधान होगा, उससे अनुक्त सभी अर्थों का भभिधान होने लगेगा। उसी पक्ष में दीर्घ विधान कैसे हो सकता है? कारण, 'स्यादस्त्येव' यहां पर अन्य योग के व्यावर्तक 'एवं' शब्द ह्रस्वत्वादि अपने पूर्व धर्म की निवृत्ति करके ही होते हैं। से सब प्रयों का व्यावर्तन होने से, 'स्यात्' शब्द उन वर्गों के प्रनित्यत्व पक्ष में उनका नाश हो जायेगा, अतः व्यावृत्त अर्थों का घोतक नहीं हो सकता । इस तुल्य युक्ति एक ही का ह्रस्वत्वादि विधान व्यर्थ होगा। स्याद्वाद से जिस प्रकार एव से सब अर्थों का व्यावर्तन होता है, सिद्धान्त स्वीकार कर लेने पर वर्ण रूप से शब्दों की उसी प्रकार सब अर्थों के ही अन्तर्गत आने वाले नास्ति- नित्यता तथा ह्रस्वादि रूप से अनित्यता होने से ह्रस्वादि स्वादि का भी व्यावर्तन होगा और इस तरह 'स्यात्' शब्द के विधान की उपपत्ति हो जाती है । इस प्रकार "पीयमानं भनेकान्त का द्योतक नहीं होगा, ऐसा यदि कहें, तो यह मधु मदयति" यहां 'पा' धात्वर्थ की अपेक्षा मधु को कर्मअनुचित है, क्योंकि ऐसा सिद्धान्त है कि 'अस्ति' प्रादि पद कारकत्व तथा 'मद' धात्वर्थ की अपेक्षा कर्तृत्व एक ही में प्राधान्येन तथा गौणतया जिस प्रकार अस्तित्व आदि अर्थ अनेक कारक होते हैं। भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्दों की को कहते हैं, उसी प्रकार 'स्यात्' शब्द भी प्रधानतया तथा एक अर्थ में वृत्ति होना सामानाधिकरण्य है । वह सामानागौणतया उन-उन अर्थों का द्योतन करता है।
धिकरण्य, जहां सर्वथा भेद रहेगा, वहां नहीं हो सकता अभिप्राय यह है कि द्रव्य रूप से अस्तित्व तथा पर्याय तथा जहां सर्वथा अभेद रहेगा वहां भी नहीं हो सकता। रूप से नारितत्व है। अतः द्रव्याथिकनय की दृष्टि से इसलिए 'नीलमुत्पलम्' यहाँ भेद रूप एकान्त पक्ष में अथवा अस्तित्व को मुख्यता तथा नास्तित्व को गौणता है; क्योंकि अभेद रूप एकान्त पक्ष में सामानाधिकरण्य एकान्तवादियों नास्तित्वादि की अपेक्षा रखने वाले अस्तित्य को ही भव- के मत में नहीं बन सकता। अतः अपेक्षाकृत भेद एवं स्थिति संभव है। इसी प्रकार पर्यायाथिकनय की दृष्टि से अपेक्षाकृत प्रभेद, यह मानना ही पड़ेगा। इसी प्रकार नास्तित्व को मुख्यता तथा अस्तित्व को गौणता है। एकान्तवादी के मत में विशेष्य विशेषणभाव भी नहीं बन क्योंकि अस्तित्वादि की अपेक्षा रखने वाले नास्तित्व की ही सकता । प्रतः स्याद्वाद का अनुसरण करना ही चाहिये। अवस्थिति संभव है। अतः द्रव्यार्थिक एवं पर्यायाथिक नय
इस प्रकार सकल ग्राह्य न होने से, न तो एकान्ततः की अपेक्षा रखने वाले प्रधानभाव एवं गुणभाव से 'स्यात्'
शब्द नित्यतावादी के मत से, न शब्दानित्यतावादी के मत शब्द अनेकान्त का द्योतक तथा तदितर का वाचक
से यह शब्दानुशासन सर्वसाधारण होगा; अपितु केवल सिद्ध होता है। एक को ही अनेक रूप में समझना
स्याद्वाद सिद्धान्त से ही सर्वसाधारण हो सकता है ऐसा अनेकान्त कहलाता है। सभी वस्तु द्रव्यरूप से नित्य
ग्रंथकार ने भी स्वयं कहा है।'तथा पर्यायरूप से अनित्य; स्वरूप से सत्य तथा अन्य रूप से असत् हैं । इस प्रकार अश्वत्व, जो सकल प्रश्व १. "स्यादित्य व्ययमनेकान्तद्योतकम्, ततः स्याद्वामें सामान्य है, सत्ता की अपेक्षा विशेष है। शर्करादि दोऽनेकान्तवाद:, नित्यानित्याद्यनेकधर्मशबलक वस्त्वका माषुर्य शब्द द्वारा कहा जा सकता है, अतः भ्युपगम इति यावत् । ततः सिद्धिनिष्पत्तिर्जप्तिर्वा वह मभिलाप्य है, किन्तु उसका न्यूनाधिक्य शब्द द्वारा प्रकृतानां शब्दानां वेदितव्या। एकस्यैव हि ह्रस्वदीर्धादि नहीं कहा जा सकता, मतः वही अनभिलाप्प भी है। इसी विषयोऽनेककारक सन्निपातः, सामानाधिकरण्यं, विशेषण प्रकार एक ही वर्ण में ह्रस्वत्व, दीर्घत्वादि, स्याद्वाद के विशेष्यभावादयश्च स्याद्वादमन्तरेण नोपपद्यन्ते। सर्व बिना उत्पन्न नहीं हो सकता तथा एक ही वस्तु में अनेक पार्षदत्वाच्च शब्दानुशासनस्य सकलदर्शनसएडात्मककारक का प्रतिपादन, सामानाधिकरण्य, वैयधिकरण्य, स्याद्वाद समाधयमतिरमणीयम् । यक्वोचाम् स्तुतिष