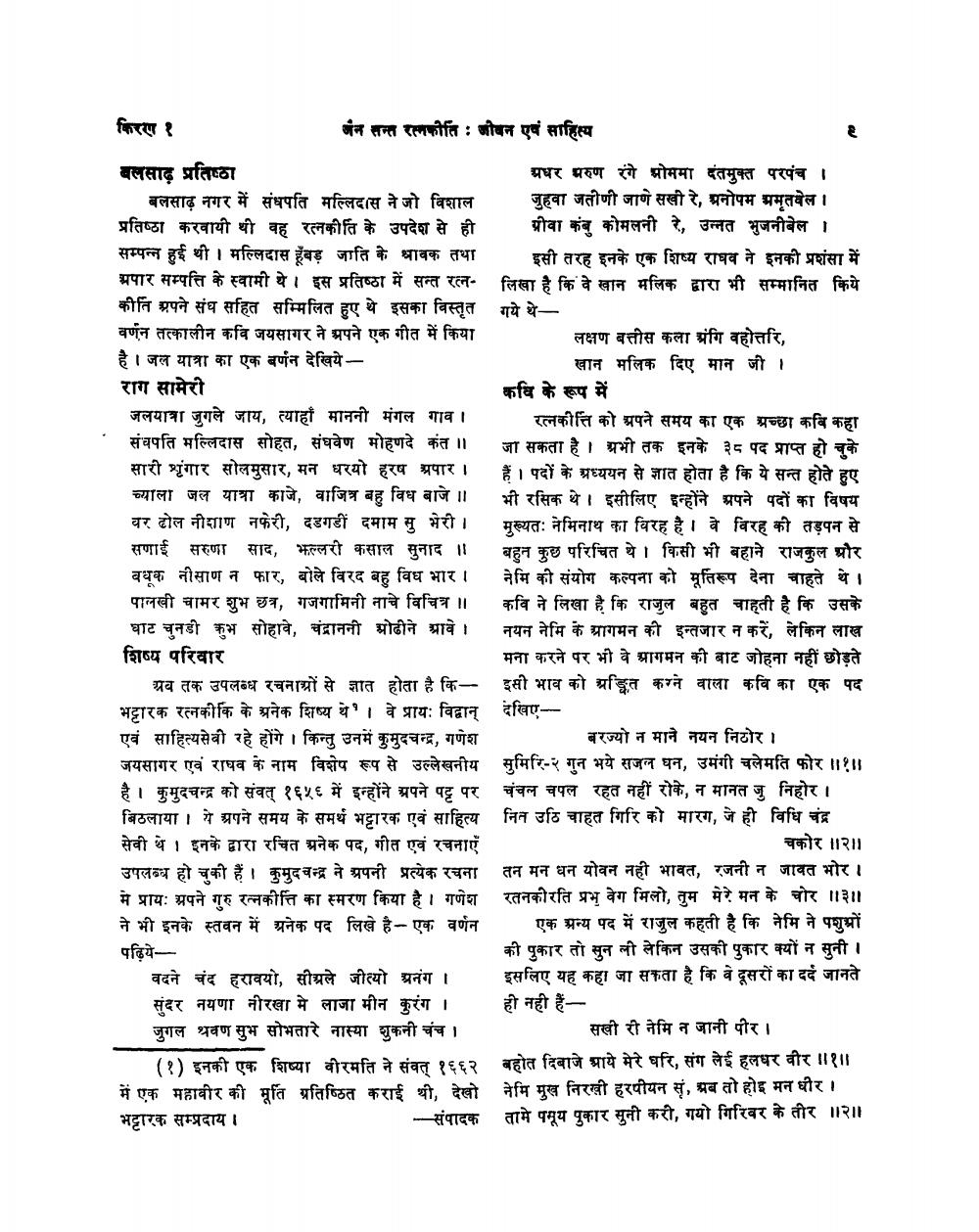________________
किरण १
बलसाढ़ प्रतिष्ठा
बलसाढ़ नगर में संधपति मल्लिदास ने जो विशाल प्रतिष्ठा करवायी थी वह रत्नकीति के उपदेश से ही सम्पन्न हुई थी । मल्लिदास हूँबड़ जाति के धावक तथा अपार सम्पत्ति के स्वामी थे। इस प्रतिष्ठा में सन्त रत्नकीर्ति अपने संघ सहित सम्मिलित हुए थे इसका विस्तृत वर्णन तत्कालीन कवि जयसागर ने अपने एक गीत में किया है । जल यात्रा का एक बर्णन देखिये - राग सामेरी
जंन सन्त रत्नफीति जीवन एवं साहित्य
:
जलयात्रा जुगले जाय, त्याहाँ माननी मंगल गाव । संपति मल्लिदास सोहत संघवेण मोहनदे कंत ॥ सारी श्रृंगार सोलमुसार, मन धरयो हरष अपार । च्याला जल यात्रा काजे, वाजिन बहुविध बाजे ॥ वर ढोल मीशाण नफेरी, दगडी दमाम सु भेरी । सणाई सरुणा साद, भल्लरी कसाल सुनाद ॥ यथूक नीसाण न फार बोले विरद बहुविध भार पालखी चामर शुभ छत्र, गजगामिनी नाचे विचित्र ॥ घाट चुनडी कुभ सोहावे, चंद्राननी ओढीने श्रावे । शिष्य परिवार
अब तक उपलब्ध रचनाओं से ज्ञात होता है कि भट्टारक रत्नकीकि के अनेक शिष्य थे। वे प्रायः विद्वान् एवं साहित्यसेवी रहे होंगे। किन्तु उनमें कुमुदचन्द्र, गणेश जयसागर एवं राघव के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कुमुदचन्द्र को संवत् १६५० में इन्होंने अपने पट्ट पर बिठलाया। ये अपने समय के समर्थ भट्टारक एवं साहित्य सेवी थे । इनके द्वारा रचित अनेक पद, गीत एवं रचनाएँ उपलब्ध हो चुकी हैं। कुमुदवन्द्र ने अपनी प्रत्येक रचना मे प्रायः अपने गुरु रत्नकीत्ति का स्मरण किया है। गणेश ने भी इनके स्तवन में अनेक पद लिखे है- एक वर्णन पड़िये
वदने चंद हरावयो, सीधले जीत्यो घनंग | सुंदर नयणा नीरखा मे लाजा मीन कुरंग । जुगल श्रवण सुभ सोभतारे नास्या शुकनी चंच |
(१) इनकी एक शिष्या वीरमति ने संवत् १६६२ में एक महावीर की मूर्ति प्रतिष्ठित कराई थी, देखो भट्टारक सम्प्रदाय ।
-संपादक
अधर अरुण रंगे श्रममा दंतमुक्त परपंच । जुहवा जतीणी जाणे सखी रे, मनोपम अमृतवेल | प्रीवा कंबु कोमलनी रे, उन्नत भुजनीबेल ।
इसी तरह इनके एक शिष्य राघव ने इनकी प्रशंसा में लिखा है कि वे खान मलिक द्वारा भी सम्मानित किये गये थे
लक्षण बत्तीस कला अंगि वहोत्तरि, खान मलिक दिए मान जी ।
कवि के रूप में
रत्नकीत्ति को अपने समय का एक अच्छा कवि कहा जा सकता है। अभी तक इनके ३८ पद प्राप्त हो चुके हैं। पदों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ये सन्त होते हुए भी रसिक थे । इसीलिए इन्होंने अपने पदों का विषय मुख्यतः नेमिनाथ का विरह है। वे विरह की तड़पन से बहुत कुछ परिचित थे । किसी भी बहाने राजकुल धौर नेमि की संयोग कल्पना को मूर्तिरूप देना चाहते थे। कवि ने लिखा है कि राजुल बहुत चाहती है कि उसके नयन नेमि के आगमन की इन्तजार न करें, लेकिन लाख मना करने पर भी वे आगमन की बाट जोहना नहीं छोड़ते इसी भाव को अङ्कित करने वाला कवि का एक पद देखिए-
बरज्यो न माने नयन निठोर ।
सुमिरि-२ गुन भये सजल घन, उमंगी चलेमति फोर ॥१॥ चंचल चपत रहत नहीं रोके, न मानत जु निहोर । नित उठि चाहत गिरि को मारग, जे ही विधि चंद्र
।
चकोर ||२|| तन मन धन योवन नही भावत, रजनी न जावत भोर । रतनकीरति प्रभु वेग मिलो, तुम मेरे मन के चोर ॥३॥ एक अन्य पद में राजुल कहती है कि नेमि ने पशुभ्रों की पुकार तो सुन मी लेकिन उसकी पुकार क्यों न सुनी। इसलिए यह कहा जा सकता है कि वे दूसरों का दर्द जानते ही नही हैं
सखी री नेमि न जानी पीर ।
बहोत दिबाजे आये मेरे घरि संग लेई हलधर वीर ॥१॥ नेमिमुख निरखी हरपीयन से अब तो होइ मन धीर । तामे पसूय पुकार सुनी करो, गयो गिरिवर के तीर ॥२॥