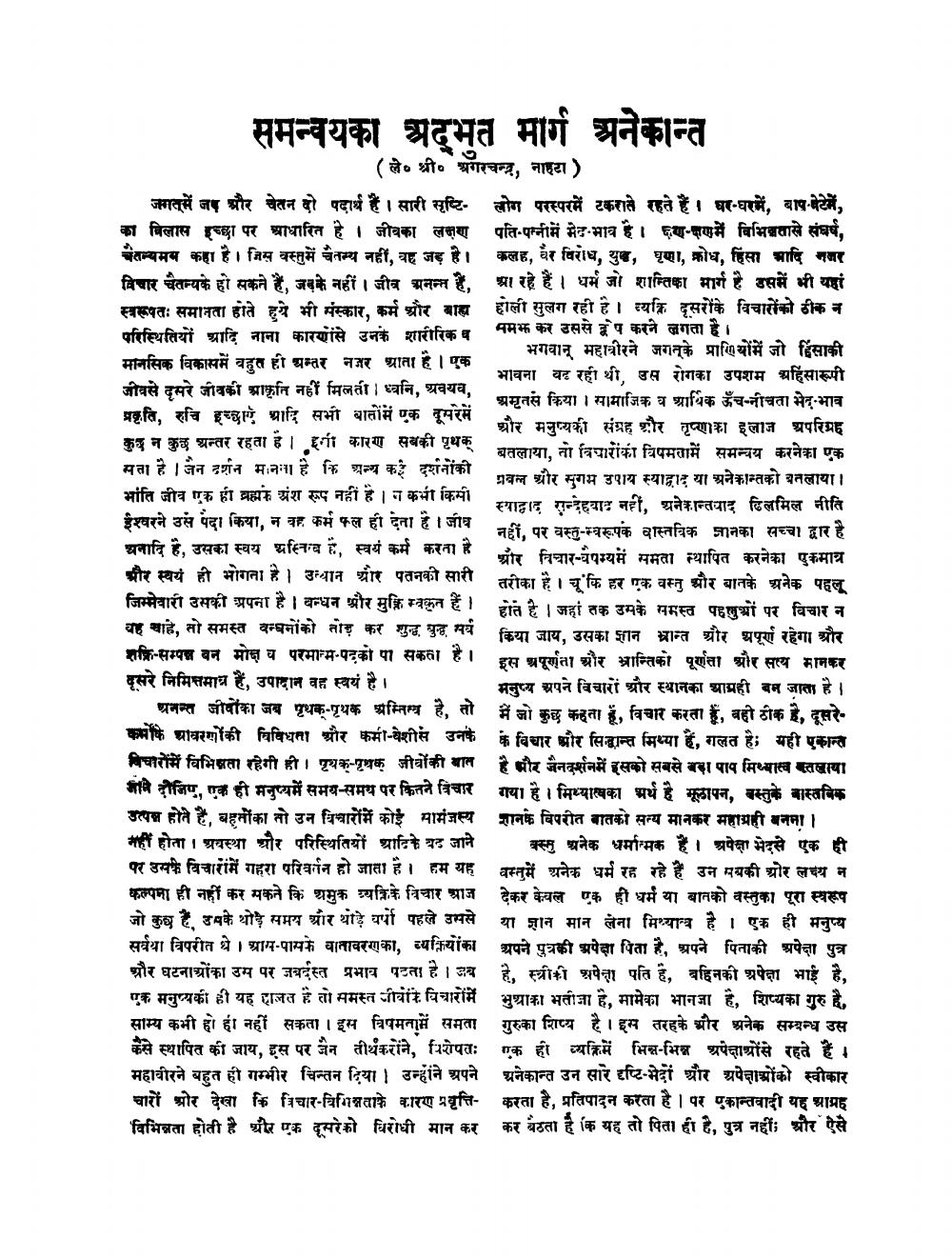________________
समन्वयका अदभत मार्ग अनेकान्त
(ले० श्री. अगरचन्द्र, नाहटा) जगत् में जब और चेतन दो पदार्थ हैं। सारी सृष्टि- लोग परस्परमें टकरासे रहते हैं। घर-घरमें, बाप-बेटेमें, का बिलास इच्छा पर श्राधारित है । जीवका लक्षण पति-पत्नीमें भेद-भाव है। क्षण-क्षण में विभिन्नतासे संघर्ष, चैतन्यमय कहा है। जिस वस्तुमें चैतम्य नहीं, वह जड़ है। कलह, वैर विरोध, युद्ध, घृणा, क्रोध, हिंसा भादि नजर विचार चैतन्यके हो सकते हैं, जनके नहीं । जीव अनन्त है, प्रा रहे हैं। धर्म जो शान्तिका मार्ग है उसमें भी यहां स्वरूपतः समानता होते हये भी संस्कार, कर्म और बाह्य होली सुलग रही है। व्यक्ति दूसरोंके विचारोंको ठीक न परिस्थितियों श्रादि नाना कारणसे उनके शारीरिकव
ममझ कर उससे द्वेष करने लगता है।
____ भगवान् महावीरने जगत्के प्राणियोंमें जो हिंसाकी मानसिक विकासमें बहुत ही अन्तर नजर आता है। एक
भावना वढ रही थी, उस रोगका उपशम अहिंसारूपी जीवसे दूसरे जीवकी प्राकृति नहीं मिलती। ध्वनि, अवयव,
अमृतस किया। सामाजिक व आर्थिक ऊँच-नीचता भेद-भाव प्रकृति, रुचि इच्छारे श्रादि सभी बातों में एक दूसरेमें
और मनुष्यकी संग्रह और तृष्णाका इलाज अपरिग्रह कुछ न कुछ अन्तर रहता है। इसी कारण सबकी पृथक्
बतलाया, तो विचारोंको विषमतामें समन्यय करनेका एक मता है । जैन दर्शन मानना है कि अन्य कई दर्शनोंकी
प्रवल और सुगम उपाय स्यावाद या अनेकान्तको बतलाया। भांति जीव एक ही ब्रह्मक अंश रूप नहीं है । न कभी किसी
स्थाहाद रान्देहवाद नहीं, अनेकान्तवाद ढिलमिल नीति ईश्वरने उस पैदा किया, न कह कर्म फल ही देता है । जीव
नहीं, पर वस्तु-स्वरूपक वास्तविक जानका सच्चा द्वार है अनादि है, उसका स्वय अस्तिाब है, स्वयं कर्म करता है।
और विचार-वैषम्य में समता स्थापित करनेका एकमात्र और स्वयं ही भोगना है। उत्थान और पतनकी सारी
तरीका है। चूंकि हर एक वस्तु और बानके अनेक पहलू जिम्मेवारी उसकी अपना है । बन्धन और मुक्ति म्वकृत है। होत है। जहां तक उसके समस्त पहलुओं पर विचार न यह चाहे, सो समस्त वन्धनोंको तोड़ कर शुद्ध, बुन्द्र मर्य
किया जाय, उसका ज्ञान भ्रान्त और अपूर्ण रहेगा और शक्रि-सम्पन बन मोक्ष व परमात्म-पढ़को पा सकता है।
इस अपूर्णता और भ्रान्तिको पूर्णता और सत्य मानकर दूसरे निमित्तमात्र हैं, उपादान वह स्वयं है।
मनुष्य अपने विचारों और स्थानका प्राग्रही बन जाता है। अनन्त जीवोंका जब पृथक-पृथक अस्तित्व है, तो मैं जो कुछ कहता है, विचार करता हूँ, बही ठीक है, दूसरे कोंक यावरणोंकी विविधता और कमी-येशीसे उनके के विचार और सिद्धान्त मिथ्या है, गलत है। यही एकान्त विचारों में विभिन्नता रहेगी ही। पृथक-पृथक जीवोंकी बात है और जैनदर्शन में इसको सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व बतखाया जाने दीजिए, एक ही मनुष्य में समय-समय पर कितने विचार गया है। मिथ्यात्वका अर्थ है मूळापन, वस्तुके वास्तविक उत्पन्न होते है. बहनोंका तो उन विचारों में कोई सामंजस्य ज्ञानके विपरीत बातको सत्य मानकर महाग्रही बनमा । नहीं होता । अवस्था और परिस्थितियों श्रादिके बढ जाने क्रम अनेक धर्मान्मक है। अपेक्षा भेदसे एक ही पर उसके विचारों में गहरा परिवर्तन हो जाता है। हम यह वस्तु में अनेक धर्म रह रहे है उन सबकी अोर लक्ष्य न कल्पना ही नहीं कर सकते कि अमुक व्यक्रिके विचार अाज देकर केवल एक ही धर्म या बातको वस्तुका पूरा स्वरूप जो कुछ है. उपके थोड़े समय और थोड़े वर्षो पहले उससे या ज्ञान मान लेना मिथ्यात्व है । एक ही मनुष्य सर्वथा विपरीत थे । प्राम-पासके वातावरणका, व्यक्तियोंका अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता है, अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र और घटनाओंका उस पर जबर्दस्त प्रभाव पटता है । जब है, स्त्रीकी अपेना पति है, बहिनकी अपेक्षा भाई है, एक मनुष्यकी ही यह हालत है तो समस्त जीवोंके विचारोंमें भुयाका भतीजा है, मामेका भानजा है, शिप्यका गुरु है, साम्य कभी हो ही नहीं सकता । इस विषमतामें समता गुरुका शिप्य है। इस तरहके और अनेक सम्बन्ध उस कैसे स्थापित की जाय, इस पर जैन तीर्थंकरोंने, विशेषतः एक ही व्यक्किमें भिन्न-भिन्न अपेक्षाओंसे रहते हैं। महावीरने बहुत ही गम्भीर चिन्तन दिया। उन्होंने अपने अनेकान्त उन सारे दृष्टि-भेदों और अपेक्षाओंको स्वीकार चारों ओर देखा कि विचार-विगिनताके कारण प्रवृत्ति- करता है, प्रतिपादन करता है। पर एकान्तवादी यह प्राग्रह विभिन्नता होती है और एक दूसरेको विरोधी मान कर कर बैठता है कि यह तो पिता ही है, पुत्र नहीं और ऐसे