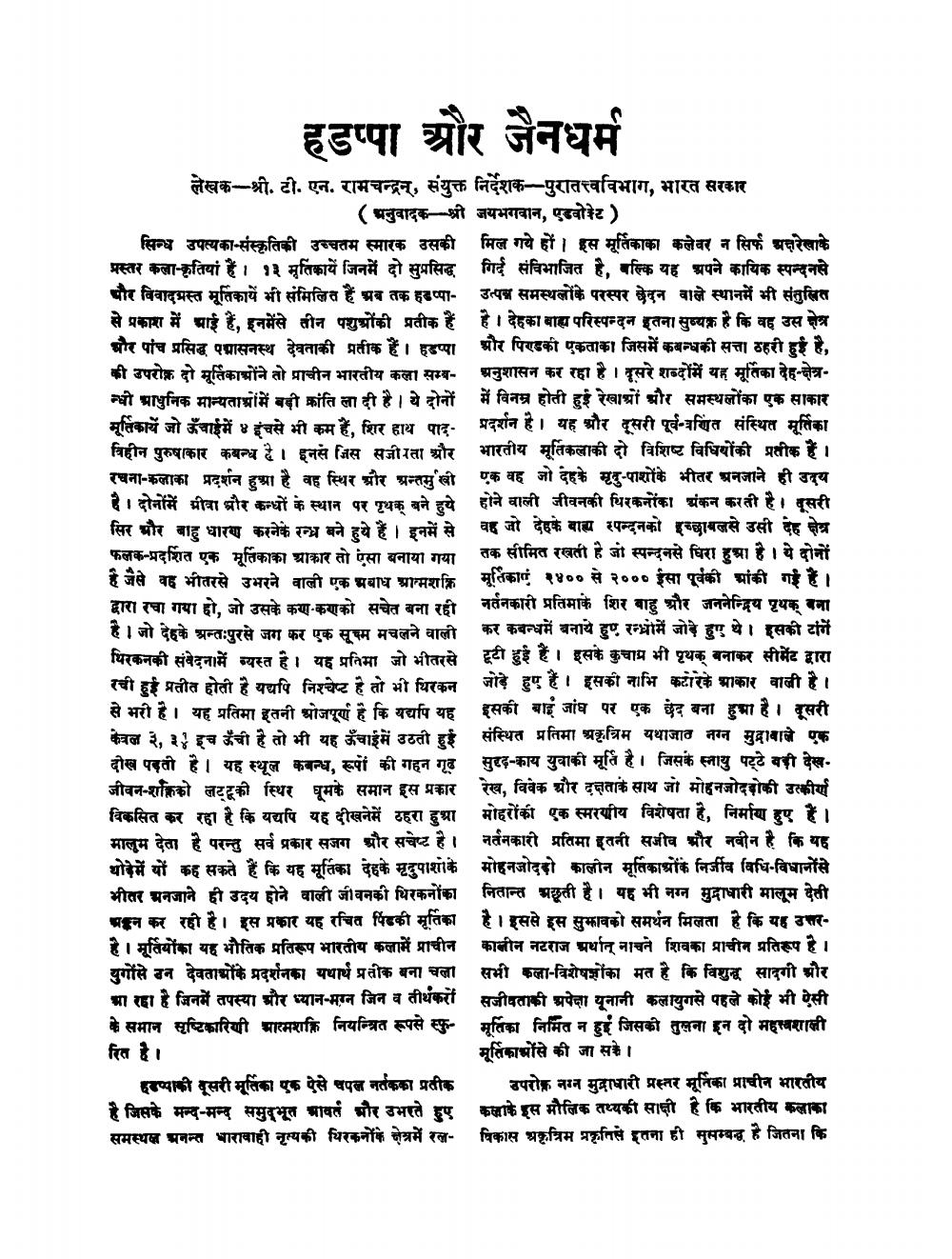________________
हडप्पा और जैनधर्म
लेखक-श्री. टी. एन. रामचन्द्रन, संयुक्त निर्देशक-पुरातत्त्वविभाग, भारत सरकार
(अनुवादक-श्री जयभगवान, एडवोकेट) सिन्ध उपत्यका-संस्कृतिकी उच्चतम स्मारक उसकी मिल गये हों। इस मूर्तिकाका कलेवर न सिर्फ अक्षरेखाके प्रस्तर कला-कृतियां हैं। ३ मृतिकायें जिनमें दो सुप्रसिद्ध गिर्द संविभाजित है, बल्कि यह अपने कायिक स्पन्दनसे पौर विवादग्रस्त मूर्तिकायें भी संमिलित हैं अब तक हडप्पा- उत्पन्न समस्थलोंके परस्पर छेदन वाले स्थानमें भी संतुखित से प्रकाश में पाई है, इनमेंसे तीन पशुओंकी प्रतीक हैं है। देहका बाह्य परिस्पन्दन इतना सुव्यक्त है कि वह उस क्षेत्र और पांच प्रसिद्ध पद्मासनस्थ देवताकी प्रतीक हैं। हडप्पा और पिण्डकी एकताका जिसमें कबन्धकी सत्ता ठहरी हुई है, की उपरोक्त दो मूर्तिकाओंने तो प्राचीन भारतीय कला सम्ब- अनुशासन कर रहा है । दूसरे शब्दों में यह मूर्तिका देह-क्षेत्रन्धी प्राधुनिक मान्यताओं में बढ़ी क्रांति ला दी है। ये दोनों में विनम्र होती हुई रेखाओं और समस्थलोंका एक साकार मूर्तिकायें जो ऊँचाई में ईचसे भी कम हैं, शिर हाथ पाद- प्रदर्शन है। यह और दूसरी पूर्व-वर्णित संस्थित मूर्तिका विहीन पुरुषाकार कबन्ध है। इनसे जिस सजीपता और भारतीय मूर्तिकलाकी दो विशिष्ट विधियोंकी प्रतीक हैं। रचना-कलाका प्रदर्शन हुआ है वह स्थिर और अन्तम खी एक वह जो दहके मृदु-पाशोंके भीतर अनजाने ही उदय है। दोनोंमें ग्रीवा और कन्धों के स्थान पर पृथक बने हुये होने वाली जीवनकी थिरकनोंका अंकन करती है। दूसरी सिर और बाह धारण करनेक रन्ध्र बने हये हैं। इनमें से वह जो देहके बाह्य स्पन्दनको इच्छाबलसे उसी देह क्षेत्र फलक-प्रदर्शित एक मूर्तिकाका श्राकार तो ऐसा बनाया गया तक सीमित रखती है जो स्पन्दनसे घिरा हुआ है। ये दोनों हे जैसे वह भीतरसे उभरने वाली एक भयाध प्रारमशनि मूर्तिकार २४०० से २००० ईसा पूर्वकी पांकी गई है। द्वारा रचा गया हो, जो उसके कण-कणको सचेत बना रही नर्तनकारी प्रतिमाके शिर बाहु और जननेन्द्रिय पृथक बना है। जो देहके अन्तःपुरसे जग कर एक सूक्ष्म मचलने वाली कर कबन्धमें बनाये हुए. रन्ध्रीमें जोड़े हुए थे। इसकी टांगें थिरकनकी संवेदना में व्यस्त है। यह प्रतिमा जो भीतरसे टूटी हुई हैं। इसके कुचाग्र भी पृथक बनाकर सीमेंट द्वारा रची हुई प्रतीत होती है यद्यपि निश्चेष्ट है तो भी थिरकन जोड़े हुए हैं। इसकी नाभि कटोरके प्राकार वाली है। से भरी है। यह प्रतिमा इतनी भोजपूर्ण है कि यद्यपि यह इसकी बाई जांघ पर एक छेद बना हुआ है। दूसरी केवल ३, ३३ इच ऊँची है तो भी यह ऊँचाई में उठती हुई संस्थित प्रतिमा अकृत्रिम यथाजात नग्न मुद्रावाले एक दोख पड़ती है। यह स्थूल कबन्ध, रूपों की गहन गूढ सुदृढ़-काय युवाकी मूर्ति है। जिसके स्नायु पट्टे बड़ी देखजीवन-शक्तिको लटूकी स्थिर घूमके समान इस प्रकार रेख, विवेक और दक्षताके साथ जो मोहनजोदडोकी उत्कीर्ण विकसित कर रहा है कि यद्यपि यह दीखनेमें ठहरा हुआ मोहरोंकी एक स्मरणीय विशेषता है, निर्माण हुए हैं। मालूम देता है परन्तु सर्व प्रकार सजग और सचेष्ट है। नर्तनकारी प्रतिमा इतनी सजीव और नवीन है कि यह थोड़ेमें यों कह सकते हैं कि यह मूर्तिका देहके मृदुपाशोके मोहनजोदड़ो कालीन मूर्तिकाओंके निर्जीव विधि-विधानोंसे भीतर अनजाने ही उदय होने वाली जीवनकी थिरकनोंका नितान्त भछूती है। यह भी नग्न मुद्रापारी मालूम देती मान कर रही है। इस प्रकार यह रचित पिंडकी मूर्तिका है। इससे इस सुझावको समर्थन मिलता है कि यह उत्तरहै। मूर्तियोंका यह भौतिक प्रतिरूप भारतीय कलामें प्राचीन कालीन नटराज अर्थात् नाचने शिवका प्राचीन प्रतिरूप है। युगोंसे उन देवताओंके प्रदर्शनका यथार्थ प्रतीक बना चला सभी कला-विशेषज्ञोंका मत है कि विशुद्ध सादगी और पा रहा है जिनमें तपस्या और ध्यान-मग्न जिन व तीर्थंकरों सजीवताकी अपेक्षा यूनानी कलायुगसे पहले कोई भी ऐसी के समान सृष्टिकारिणी प्रारमशक्ति नियन्त्रित रूपसे स्फु मूर्तिका निर्मित न हुई जिसकी तुलना इन दो महत्त्वशाली
मूर्तिकाओंसे की जा सके। हरप्याकी दूसरी मूर्तिका एक ऐसे चपल नर्तकका प्रतीक उपरोक नग्न मुद्रापारी प्रस्तर मूर्तिका प्राचीन भारतीय है जिसके मन्द-मन्द समुद्भूत बावर्त और उभरते हुए कलाके इस मौलिक तथ्यकी साक्षी है कि भारतीय कलाका समस्थल अनन्त धारावाही नृत्यकी थिरकनोंके क्षेत्रमें रन- विकास प्रकृत्रिम प्रकृतिले इतना ही सुसम्बद्ध है जितना कि