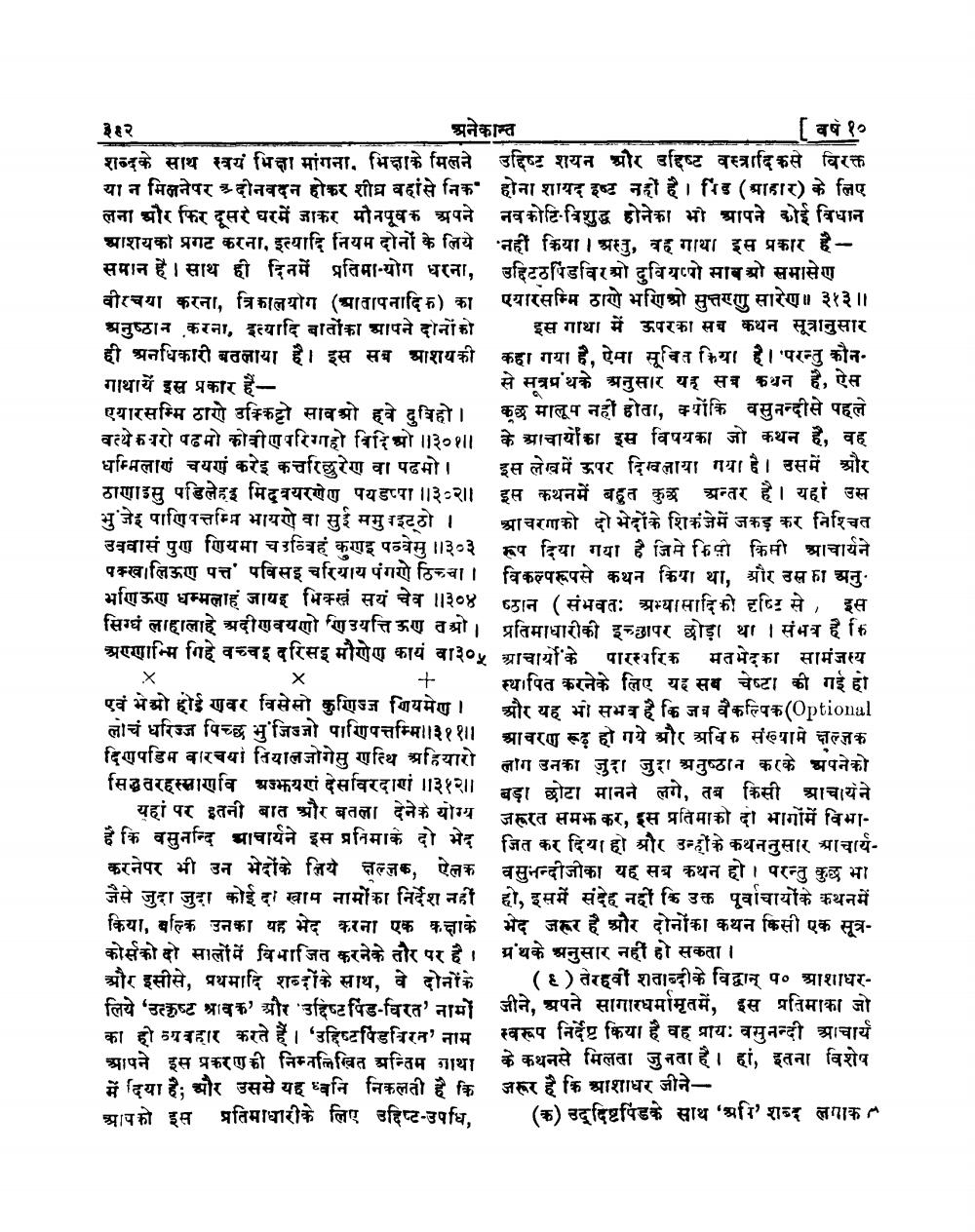________________
३३२
अनेका
शब्द के साथ स्वयं भिक्षा मांगना, भिक्षाके मिलने या न मिलनेपर दोनवदन होकर शीघ्र वहांसे निक ना और फिर दूसरे घर में जाकर मौनपूर्वक अपने आशयको प्रगट करना, इत्यादि नियम दोनों के लिये समान है। साथ ही दिनमें प्रतिमा-योग धरना, वीरचया करना, त्रिकालयोग (आतापनादिक) का अनुष्ठान करना, इत्यादि बातोंका आपने दोनों को ही अनधिकारी बतलाया है। इस सब आशयकी गाथायें इस प्रकार हैं
यारसम्म ठाणे किट्टो सावओ हवे दुविहो । त्येक पढमोकोवीए परिगाहो विदिश्रो ||३०१|| धमिलाणं चयणं करेइ कचरिछुरेण वा पढमो । ठाणासु पडिलेहs मिवयरणेण पयडप्पा ||३०२|| भुजे पाणिपत्तम भायणे वा सुई समुइट्ठो । उवासं पुणणियमा चरन्विहं कुरणइ पव्वेसु || ३०३ पखालिऊण पत्त' पविसइ चरियाय पंगणे ठिच्चा । भणिऊण धम्मलाहं जायद भिक्खं सयं चेव ||३०४ सिग्धं लाहालाहे अदीणवयलो णिउयत्ति ऊण व अण्णामि गिहे वच्च दरिसइ मौणेण कार्य वा३०५ + एवं भेओ होई णवर विसेसो कुणिज्ज नियमेण । लोचं धरिज्ज पिच्छ भुजिज्जो पाणिपत्तम्मि ||३११|| दिएपडिम वारचयां वियालजोगेसु णत्थि अहियारो सिद्धतरहस्याणवि अभय देसविरदा ||३१२||
X
X
[ वर्ष १० उद्दिष्ट शयन और उद्दिष्ट वस्त्रादिकसे विरक्त होना शायद इष्ट नहीं । पिंड (आहार) के लिए नवकोटि-विशुद्ध होने का भी आपने कोई विधान नहीं किया । अस्तु, वह गाथा इस प्रकार हैtfsfar दुवियप्पो साबो समासेण पयारसम्म ठाणे भणिश्रो सुत्तगु सारेण ॥ ३५३ ॥
यहां पर इतनी बात और बतला देनेके योग्य हैं कि वसुनन्दि आचार्यने इस प्रतिमाके दो भेद करनेपर भी उन भेदोंके लिये चल्लक, ऐलक जैसे जुदा जुड़ा कोई दा खाम नामोंका निर्देश नहीं किया, बल्कि उनका यह भेद करना एक कक्षाके कोर्सको दो सालों में विभाजित करनेके तौर पर है। और इसीसे प्रथमादि शब्दों के साथ, वे दोनों के लिये 'उत्कृष्ट श्रावक' और 'उद्दिष्ट पिंड विरत' नामों का हो व्यवहार करते हैं। 'उद्दिष्टपिंडविरत' नाम आपने इस प्रकरण की निम्नलिखित अन्तिम गाथा में दिया है; और उससे यह ध्वनि निकलती है कि आपको इस प्रतिमाधारी के लिए उद्दिष्ट - उपधि,
इस गाथा में ऊपरका सच कथन सूत्रानुसार कहा गया है, ऐमा सूचित किया है । परन्तु कौनसे सूत्र के अनुसार यह सब कथन है, ऐस कुछ मालूम नहीं होता, क्योंकि वसुनन्दीसे पहले के आचार्योंका इस विषयका जो कथन हैं, वह इस लेख में ऊपर दिखलाया गया है। उसमें और इस कथनमें बहुत कुछ अन्तर है । यहां उस आचरणको दो भेदों के शिकंजे में जकड़ कर निश्चित रूप दिया गया है जिसे किसी किसी आचार्यने विकल्परूपसे कथन किया था, और उसका अनु ठान ( संभवत: अभ्यासादिको दृष्टि से, इस प्रतिमाधारीकी इच्छापर छोड़ा था । संभव है कि श्राचार्यों के पारस्परिक मतभेदका सामंजस्य स्थापित करनेके लिए यह सब चेष्टा की गई हो और यह भी संभव है कि जब वैकल्पिक (Optional आचरण रूढ़ हो गये और अधिक संख्यामे चल्लक लोग उनका जुदा जुदा अनुष्ठान करके अपनेको बड़ा छोटा मानने लगे, तब किसी आचार्यने जरूरत समझ कर, इस प्रतिमाको दो भागों में विभा जित कर दिया हो और उन्होंके कथननुसार आचार्यवसुनन्दीजीका यह सब कथन हो । परन्तु कुछ भा हो, इसमें संदेह नहीं कि उक्त पूर्वाचार्यों के कथन में भेद जरूर है और दोनोंका कथन किसी एक सूत्रप्रथके अनुसार नहीं हो सकता ।
(६) तेरहवीं शताब्दी के विद्वान् प० आशाधरजीने, अपने सागारधर्मामृत में, इस प्रतिमाका जो स्वरूप निर्देष्ट किया है वह प्रायः वसुनन्दी आचार्य के कथनसे मिलता जुनता है। हां, इतना विशेष जरूर है कि आशाधर जीने
(क) उद्दिष्टपिंड के साथ 'अनि' शब्द लगाक