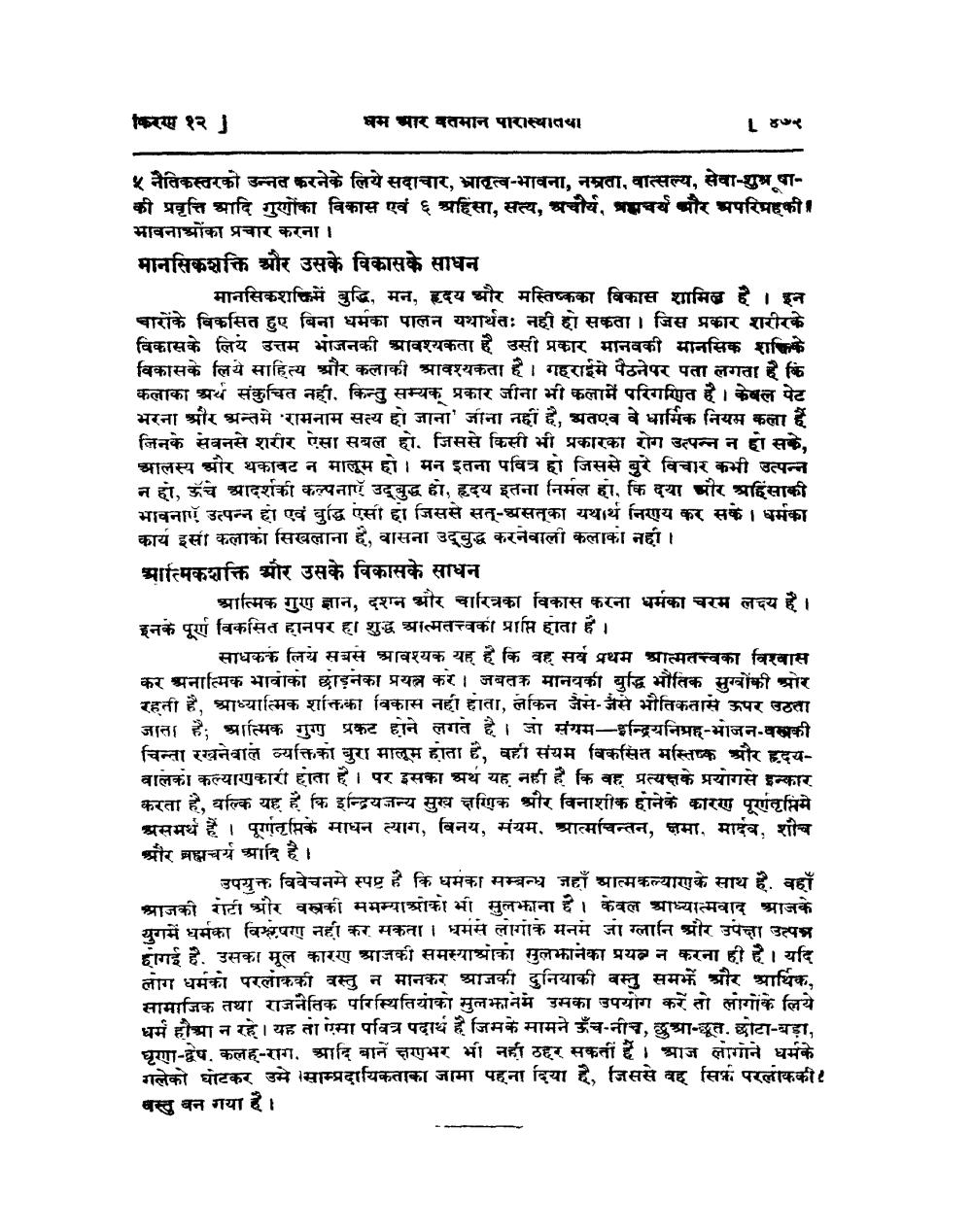________________
किरण १२ ]
५ नैतिकस्तरको उन्नत करनेके लिये सदाचार, भ्रातृत्व-भावना, नम्रता, वात्सल्य, सेवा-शुभ्र पाकी प्रवृत्ति आदि गुणोंका विकास एवं ६ अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहकी । भावनाओंका प्रचार करना ।
मानसिक शक्ति और उसके विकासके साधन
मानसिक शक्ति में बुद्धि, मन, हृदय और मस्तिष्कका विकास शामिल है । इन चारोंके विकसित हुए बिना धर्मका पालन यथार्थतः नही हो सकता। जिस प्रकार शरीरके विकासके लिये उत्तम भोजनकी आवश्यकता है उसी प्रकार मानवकी मानसिक शक्तिके विकासके लिये साहित्य और कलाकी आवश्यकता है। गहराईमे पैठनेपर पता लगता है कि कलाका अर्थ संकुचित नहीं, किन्तु सम्यक् प्रकार जीना भी कलामें परिगणित है । केवल पेट भरना और अन्त मे रामनाम सत्य हो जाना' जीना नहीं है, अतएव वे धार्मिक नियम कला है जिनके सेवन से शरीर ऐसा सबल हो. जिससे किसी भी प्रकारका रोग उत्पन्न न हो सके, आलस्य और थकावट न मालूम हो । मन इतना पवित्र हो जिससे बुरे विचार कभी उत्पन्न न हो, ऊँचे आदर्शकी कल्पनाएँ उद्बुद्ध हो, हृदय इतना निर्मल हो, कि दया और अहिंसाकी भावनाएँ उत्पन्न हो एवं बुद्धि ऐसी हो जिससे सत्-असत्का यथार्थ निरण्य कर सके । धर्मका कार्य इसी कलाको सिखलाना है, वासना उद्बुद्ध करनेवाली कलाको नही ।
आत्मिकशक्ति और उसके विकासके साधन
श्रात्मिक गुण ज्ञान, दर्शन और चारित्रका विकास करना धर्मका चरम लक्ष्य हैं । इनके पूर्ण विकसित हानपर हा शुद्ध आत्मतत्त्वकी प्राप्ति होता है ।
धम आर वतमान पारास्थातथा
[ ४७२
साधकके लिये सबसे आवश्यक यह है कि वह सर्व प्रथम श्रात्मतत्त्वका विश्वास कर अनात्मिक भावांको छोड़नेका प्रयत्न करे। जबतक मानवक बुद्धि भौतिक सुखोंकी ओर रहती हैं, आध्यात्मिक शक्तिका विकास नहीं होता, लेकिन जैसे-जैसे भौतिकतासे ऊपर उठता जाता है; आत्मिक गुग्ण प्रकट होने लगते है। जो संगम - इन्द्रियनिग्रह - भोजन-वस्त्रकी चिन्ता रखनेवाले व्यक्तिको बुरा मालूम होता है, वही संयम विकसित मस्तिष्क और हृदयवालको कल्याणकारी होता है । पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वह प्रत्यक्षके प्रयोगसे इन्कार करता है, बल्कि यह है कि इन्द्रियजन्य सुख क्षणिक और विनाशीक होनेके कारण पूर्णतृप्तिमे असमर्थ हैं । पूर्णतृप्तिके साधन त्याग, विनय, संयम, आत्मचिन्तन, क्षमा, मार्दव, शौच और ब्रह्मचर्य आदि है ।
उपयुक्त विवेचनमे स्पष्ट है कि धर्मका सम्बन्ध जहाँ आत्मकल्याण के साथ है. वहाँ श्रजकी रोटी और वस्त्रकी समस्याओ को भी सुलझाना है । केवल आध्यात्मवाद आजके युगमें धर्मका विश्लेषण नहीं कर सकता । धमंसे लोगोके मनमें जो ग्लानि और उपेक्षा उत्पन्न होगई है. उसका मूल कारण आजकी समस्याओं को सुलझानेका प्रयत्न न करना ही है। यदि लोग धर्मको परलोककी वस्तु न मानकर आजकी दुनियाकी वस्तु समझें और आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक परिस्थितियांको सुलझाने में उसका उपयोग करें तो लोगोंके लिये धर्मं हौआ न रहे। यह तो ऐसा पवित्र पदार्थ है जिसके सामने ऊँच-नीच, छुआ-छूत. छोटा-बड़ा, घृणा द्वेष. कलह-राग, आदि बातें क्षणभर भी नहीं ठहर सकती है। आज लोगोंने धर्मके गलेको घोटकर उसे साम्प्रदायिकताका जामा पहना दिया है, जिससे वह सिर्फ परलोक की बस्तु बन गया है।