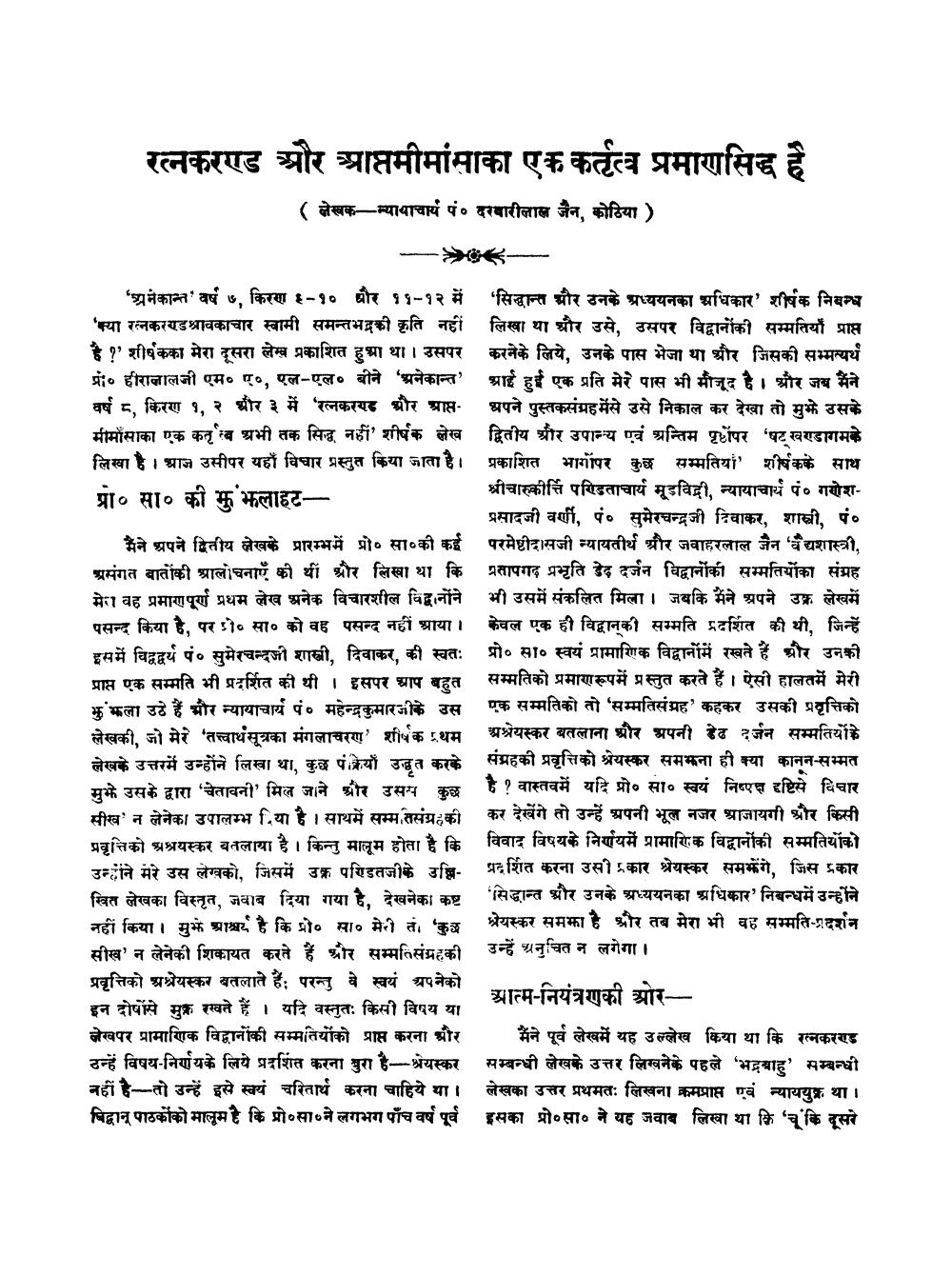________________
रत्नकरण्ड और आप्तमीमांसाका एक कर्तृत्व प्रमाणसिद्ध है
(लेखक म्यायाचार्य पं० दरबारीलाल जैन, कोठिया )
'कात' वर्ष ०, किरण १ १० और ११-१२ में 'क्या रत्नकरण्ड श्रावकाचार स्वामी समन्तभद्रकी कृति नहीं है ?' शीर्षकका मेरा दूसरा लेख प्रकाशित हुआ था उसपर प्रो० हीरालालजी एम० ए०, एल-एल० बीने 'अनेकान्त' वर्ष ८, किरण १, २ र ३ में 'रत्नकरण्ड और श्राप्तमीमांसाका एक कर्तृव अभी तक सिद्ध नहीं' शीर्षक लेख लिखा है । श्राज उसीपर यहाँ विचार प्रस्तुत किया जाता है। प्रो० सा० की मुझलाहट -
मैंने अपने द्वितीय लेखके प्रारम्भ में प्रो० सा०की कई मंगत बातोंकी लोचनाएँ की थीं और लिखा था कि मेरा वह प्रमाण पूर्ण प्रथम लेख अनेक विचारशील विद्वानोंने पसन्द किया है, पर हो० सा० को वह पसन्द नहीं श्राया । इसमें विद्वद्वर्य पं० सुमेरचन्दजी शास्त्री, दिवाकर, की स्वतः प्राप्त एक सम्मति भी प्रदर्शित की थी । इसपर श्राप बहुत ॐ कला उठे हैं और न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारजीके उस लेखकी जो मेरे 'सच्चार्थसूत्रका मंगलाचरण' शीर्षक थम लेखके उत्तरमें उन्होंने लिखा था, कुछ पंक्रियाँ उद्धृत करके मुझे उसके द्वारा 'चेतावनी' मिल जाने और उससे कुछ सीख' न लेनेका उपालम्भ दिया है । साथमें सम्मतिसंग्रह की प्रवृत्तिको श्रश्रयस्कर बतलाया है। किन्तु मालूम होता है कि उन्होंने मेरे उस लेखको, जिसमें उन पनि उि त्रित लेखका विस्तृत जवाब दिया गया है, देखनेका कष्ट नहीं किया। मुझे है कि शे० सा० मेरी तं 'कुछ सीख' न लेनेकी शिकायत करते हैं और सम्मकि प्रवृत्तिको अधेयस्कर बतलाते हैं परन्तु ये स्वयं अपनेको इन दोषोंसे सुक रखते हैं। यदि वस्तुतः किसी विषय या लेखपर प्रामाणिक विद्वानोंकी सम्मतियोंको प्राप्त करना और उन्हें विषय-निर्णय के लिये प्रदर्शित करना बुरा है— श्रेयस्कर नहीं है तो उन्हें इसे स्वयं चरितार्थ करना चाहिये था। बिद्वान् पाठकोंको मालूम है कि प्रो०सा०ने लगभग पाँच वर्ष पूर्व
'सिद्धान्त और उनके अध्ययनका अधिकार' शीर्षक निवन्ध लिखा था और उसे, उसपर विद्वानोंकी सम्मतियाँ प्राप्त करने के लिये, उनके पास भेजा था और जिसकी सम्म श्राई आई हुई एक प्रति मेरे पास भी मौजूद है। और जब मैंने अपने पुस्तकसंग्रह से उसे निकाल कर देखा तो मुझे उसके द्वितीय और उपान्य एवं अन्तिम पृष्ठोंपर 'षट् खण्डागमके प्रकाशित भागोंपर कुछ सम्मतियां' शीर्षकके साथ श्री चारुकीर्त्ति पण्डिताचार्य मूडविद्री, न्यायाचार्य पं० गणेशप्रसादजी वर्णी, पं० सुमेरचन्द्रजी दिवाकर, शास्त्री, पं० परमेष्टीदासजी न्यायतीर्थ और जवाहरलाल जैन 'वैद्यशास्त्री, प्रतापगढ़ प्रभृति डेढ़ दर्जन विद्वानोंकी सम्मतियोंका संग्रह भी उसमें संकलित मिला। जबकि मैंने अपने उम्र लेखमें केवल एक ही विद्वान्की सम्मति प्रदर्शित की थी, जिन्हें प्रो० सा० स्वयं प्रामाणिक विद्वानोंमें रखते हैं और उनकी सम्मतिको प्रमाणरूपमें प्रस्तुत करते हैं। ऐसी हालतमें मेरी एक सम्मतिको तो 'सम्मतिसंग्रह' कहकर उसकी प्रवृत्तिको अश्रेयस्कर बतलाना और अपनी डेढ दर्जन सम्मतियोंके संग्रहकी प्रवृत्तिको श्रेयस्कर समझना ही क्या कानून सम्मत है ? वास्तवमें यदि प्रो० सा० स्वयं निष्पक्ष दृष्टिसे विचार कर देखेंगे तो उन्हें अपनी भूल नजर धाजायगी और किसी विवाद विषयके निर्णयमें प्रामाणिक विद्वानोंकी सम्मतियोंको प्रदर्शित करना उसी कार श्रेयस्कर समझेंगे, जिस प्रकार 'सिद्धान्त और उनके अध्ययनका अधिकार' निबन्धमें उन्होंने श्रेयस्कर समझा है और तब मेरा भी यह सम्मतिदर्शन उन्हें अनुचित न लगेगा।
आत्म-नियंत्रणकी ओर
मैंने पूर्व लेखमें यह उल्लेख किया था कि सनकरण्ड सम्बन्धी लेखके उत्तर लिखनेके पहले 'भद्रबाहु' सम्बन्धी लेखका उत्तर प्रथमतः लिखना क्रमप्राप्त एवं न्याययुक्त था । इसका प्रो०सा० ने यह जवाब लिखा था कि 'चूंकि दूसरे