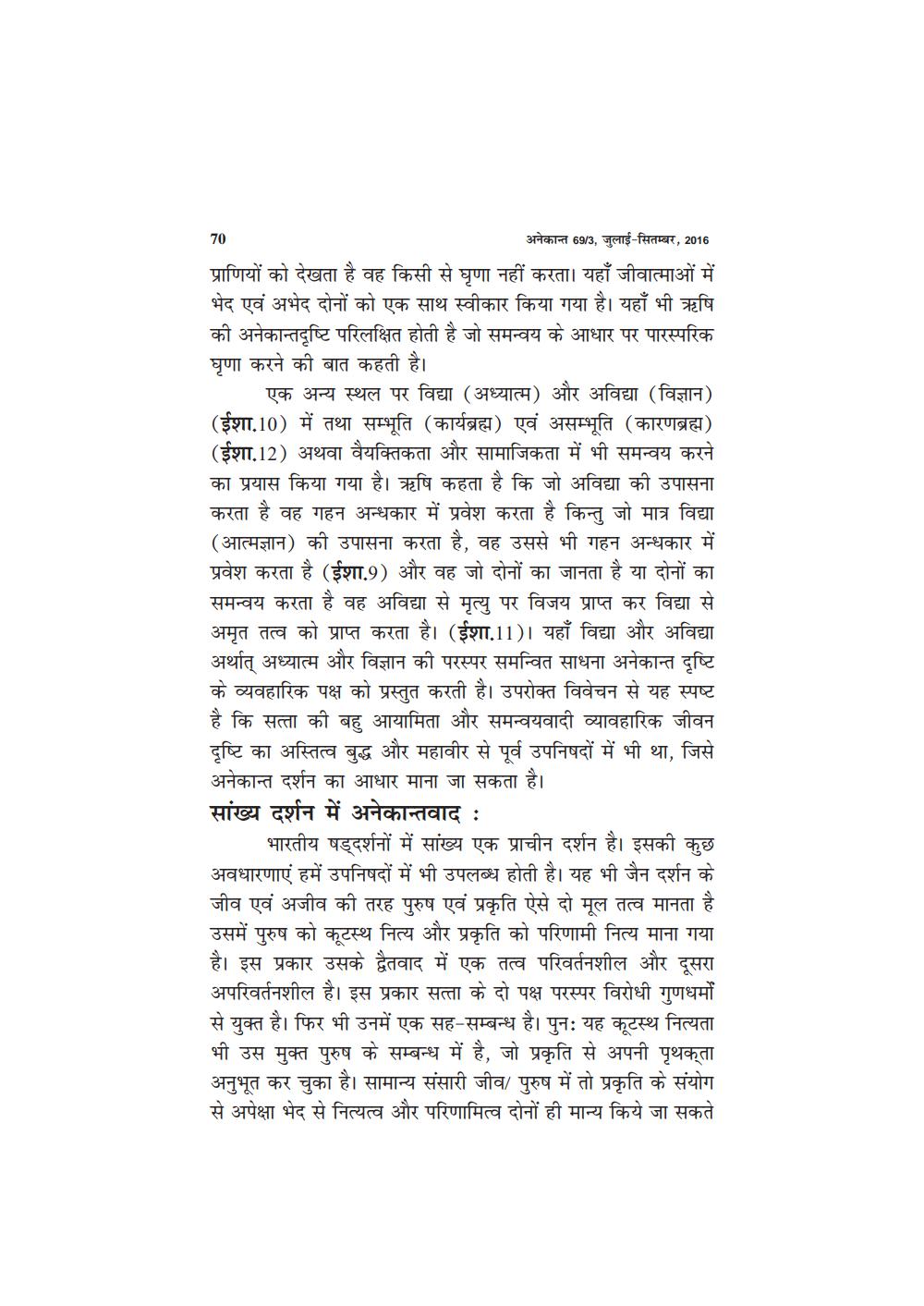________________
अनेकान्त 69/3, जुलाई-सितम्बर, 2016 प्राणियों को देखता है वह किसी से घृणा नहीं करता। यहाँ जीवात्माओं में भेद एवं अभेद दोनों को एक साथ स्वीकार किया गया है। यहाँ भी ऋषि की अनेकान्तदृष्टि परिलक्षित होती है जो समन्वय के आधार पर पारस्परिक घृणा करने की बात कहती है।
70
एक अन्य स्थल पर विद्या (अध्यात्म) और अविद्या (विज्ञान) (ईशा. 10) में तथा सम्भूति ( कार्यब्रह्म) एवं असम्भूति ( कारणब्रह्म ) (ईशा. 12 ) अथवा वैयक्तिकता और सामाजिकता में भी समन्वय करने का प्रयास किया गया है। ऋषि कहता है कि जो अविद्या की उपासना करता है वह गहन अन्धकार में प्रवेश करता है किन्तु जो मात्र विद्या (आत्मज्ञान) की उपासना करता है, वह उससे भी गहन अन्धकार में प्रवेश करता है (ईशा. 9) और वह जो दोनों का जानता है या दोनों का समन्वय करता है वह अविद्या से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर विद्या से अमृत तत्व को प्राप्त करता है। ( ईशा. 11 ) । यहाँ विद्या और अविद्या अर्थात् अध्यात्म और विज्ञान की परस्पर समन्वित साधना अनेकान्त दृष्टि के व्यवहारिक पक्ष को प्रस्तुत करती है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सत्ता की बहु आयामिता और समन्वयवादी व्यावहारिक जीवन दृष्टि का अस्तित्व बुद्ध और महावीर से पूर्व उपनिषदों में भी था, जिसे अनेकान्त दर्शन का आधार माना जा सकता है।
सांख्य दर्शन में अनेकान्तवाद :
भारतीय षड्दर्शनों में सांख्य एक प्राचीन दर्शन है। इसकी कुछ अवधारणाएं हमें उपनिषदों में भी उपलब्ध होती है। यह भी जैन दर्शन के जीव एवं अजीव की तरह पुरुष एवं प्रकृति ऐसे दो मूल तत्व मानता है उसमें पुरुष को कूटस्थ नित्य और प्रकृति को परिणामी नित्य माना गया है। इस प्रकार उसके द्वैतवाद में एक तत्व परिवर्तनशील और दूसरा अपरिवर्तनशील है। इस प्रकार सत्ता के पक्ष परस्पर विरोधी गुणधर्मों से युक्त है। फिर भी उनमें एक सह-सम्बन्ध है । पुनः यह कूटस्थ नित्यता भी उस मुक्त पुरुष के सम्बन्ध में है, जो प्रकृति से अपनी पृथक्ता अनुभूत कर चुका है। सामान्य संसारी जीव/ पुरुष में तो प्रकृति के संयोग से अपेक्षा भेद से नित्यत्व और परिणामित्व दोनों ही मान्य किये जा सकते