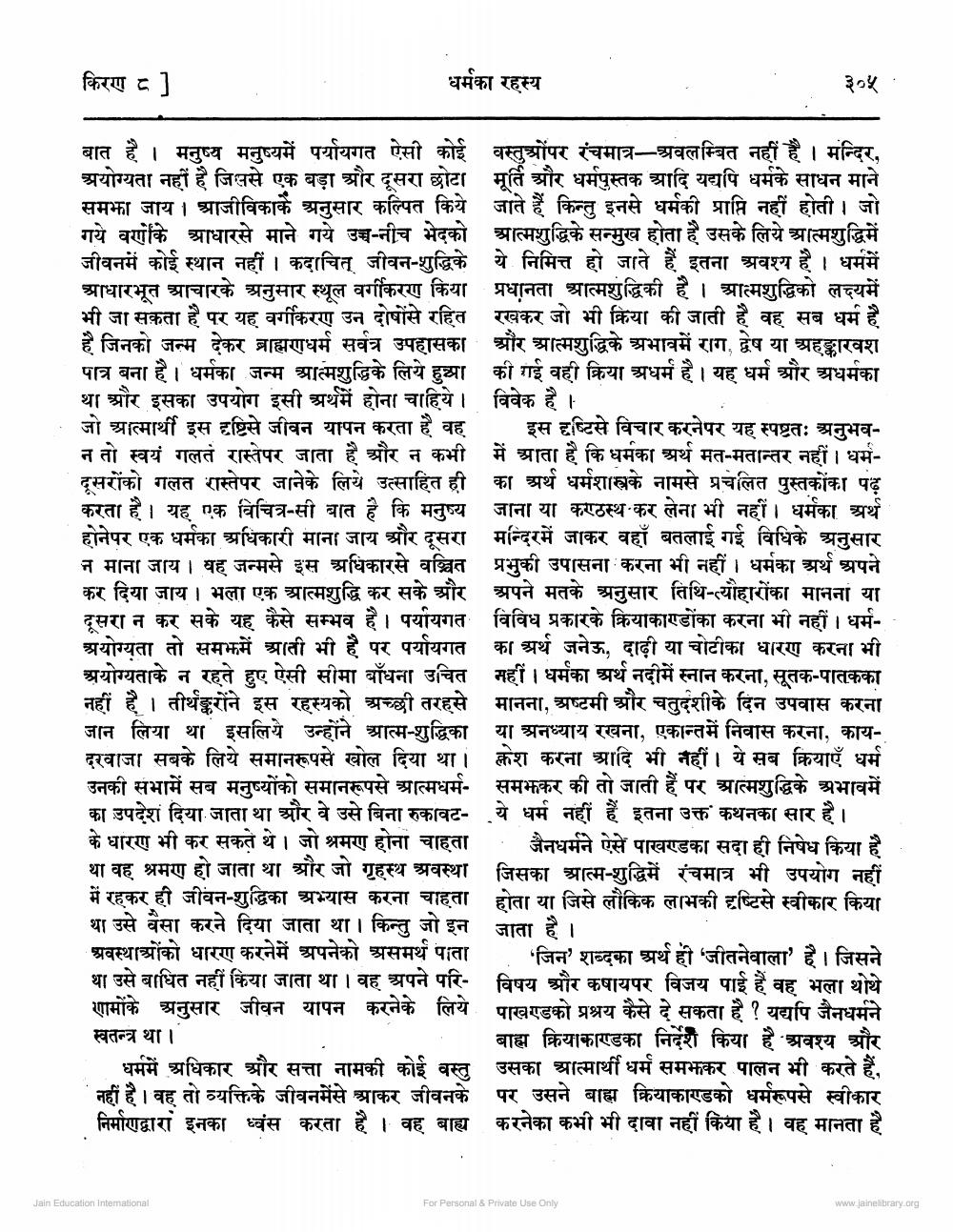________________
किरण ८]
धर्मका रहस्य
बात है। मनुष्य मनुष्यमें पर्यायगत ऐसी कोई वस्तुओंपर रंचमात्र अवलम्बित नहीं है । मन्दिर, अयोग्यता नहीं है जिससे एक बड़ा और दूसरा छोटा मूर्ति और धर्मपुस्तक आदि यद्यपि धर्मके साधन माने समझा जाय । श्राजीविकाके अनुसार कल्पित किये जाते हैं किन्तु इनसे धर्मकी प्राप्ति नहीं होती। जो गये वोंके आधारसे माने गये उच्च-नीच भेदको आत्मशुद्धिके सन्मुख होता है उसके लिये आत्मशुद्धिमें जीवनमें कोई स्थान नहीं । कदाचित् जीवन-शुद्धिके ये निमित्त हो जाते हैं इतना अवश्य है। धर्ममें आधारभूत आचारके अनुसार स्थूल वर्गीकरण किया प्रधानता आत्मशुद्धिकी है । आत्मशुद्धिको लक्ष्यमें भी जा सकता है पर यह वर्गीकरण उन दोषोंसे रहित रखकर जो भी क्रिया की जाती है वह सब धर्म है है जिनको जन्म देकर ब्राह्मणधर्म सर्वत्र उपहासका और आत्मशुद्धिके अभावमें राग, द्वेष या अहङ्कारवश पात्र बना है। धर्मका जन्म आत्मशुद्धिके लिये हुआ की गई वही क्रिया अधर्म है। यह धर्म और अधर्मका था और इसका उपयोग इसी अर्थमें होना चाहिये। विवेक है। जो आत्मार्थी इस दृष्टिसे जीवन यापन करता है वह इस दृष्टिसे विचार करनेपर यह स्पष्टतः अनुभवन तो स्वयं गलत रास्तेपर जाता है और न कभी में आता है कि धर्मका अर्थ मत-मतान्तर नहीं। धर्मदूसरोंको गलत रास्तेपर जानेके लिये उत्साहित ही का अर्थ धर्मशास्त्रके नामसे प्रचलित पुस्तकोंका पढ़ करता है। यह एक विचित्र-सी बात है कि मनुष्य जाना या कण्ठस्थ कर लेना भी नहीं। धर्मका अर्थ होनेपर एक धर्मका अधिकारी माना जाय और दूसरा मन्दिरमें जाकर वहाँ बतलाई गई विधिके अनुसार न माना जाय । वह जन्मसे इस अधिकारसे वञ्चित प्रभुकी उपासना करना भी नहीं। धर्मका अर्थ अपने कर दिया जाय । भला एक आत्मशुद्धि कर सके और अपने मतके अनुसार तिथि-त्यौहारोंका मानना या दूसरा न कर सके यह कैसे सम्भव है। पर्यायगत विविध प्रकारके क्रियाकाण्डोंका करना भी नहीं। धर्मअयोग्यता तो समझमें आती भी है पर पर्यायगत का अर्थ जनेऊ, दाढ़ी या चोटीका धारण करना भी अयोग्यताके न रहते हुए ऐसी सीमा बाँधना उचित महीं । धर्मका अर्थ नदीमें स्नान करना, सूतक-पातकका नहीं है । तीर्थङ्करोंने इस रहस्यको अच्छी तरहसे मानना, अष्टमी और चतुर्दशीके दिन उपवास करना जान लिया था इसलिये उन्होंने आत्म-शुद्धिका या अनध्याय रखना, एकान्तमें निवास करना. कायदरवाजा सबके लिये समानरूपसे खोल दिया था। क्लेश करना आदि भी नहीं। ये सब क्रियाएँ धर्म उनकी सभामें सब मनुष्योंको समानरूपसे आत्मधर्म समझकर की तो जाती है पर आत्मशुद्धिके अभावमें का उपदेशं दिया जाता था और वे उसे बिना रुकावट- ये धर्म नहीं हैं इतना उक्त कथनका सार है। के धारण भी कर सकते थे। जो श्रमण होना चाहता . जैनधर्मने ऐसे पाखण्डका सदा ही निषेध किया है था वह श्रमण हो जाता था और जो गृहस्थ अवस्था जिसका आत्म-शुद्धिमें रंचमात्र भी उपयोग नहीं में रहकर ही जीवन-शुद्धिका अभ्यास करना चाहता होता या जिसे लौकिक लाभकी दृष्टिसे स्वीकार किया था उसे वैसा करने दिया जाता था। किन्तु जो इन जाता है। अवस्थाओंको धारण करने में अपनेको असमर्थ पाता जिन' शब्दका अर्थ ही 'जीतनेवाला' है । जिसने था उसे बाधित नहीं किया जाता था । वह अपने परि- विषय और कषायपर विजय पाई है वह भला थोथे णामोंके अनुसार जीवन यापन करनेके लिये पाखण्डको प्रश्रय कैसे दे सकता है ? यद्यपि जैनधर्मने स्वतन्त्र था।
बाझ क्रियाकाण्डका निर्देश किया है अवश्य और धर्ममें अधिकार और सत्ता नामकी कोई वस्तु उसका आत्मार्थी धर्म समझकर पालन भी करते हैं, नहीं है । वह तो व्यक्तिके जीवनमेंसे आकर जीवनके पर उसने बाह्म क्रियाकाण्डको धर्मरूपसे स्वीकार निर्माणद्वारा इनका ध्वंस करता है । वह बाह्य करनेका कभी भी दावा नहीं किया है। वह मानता है
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org