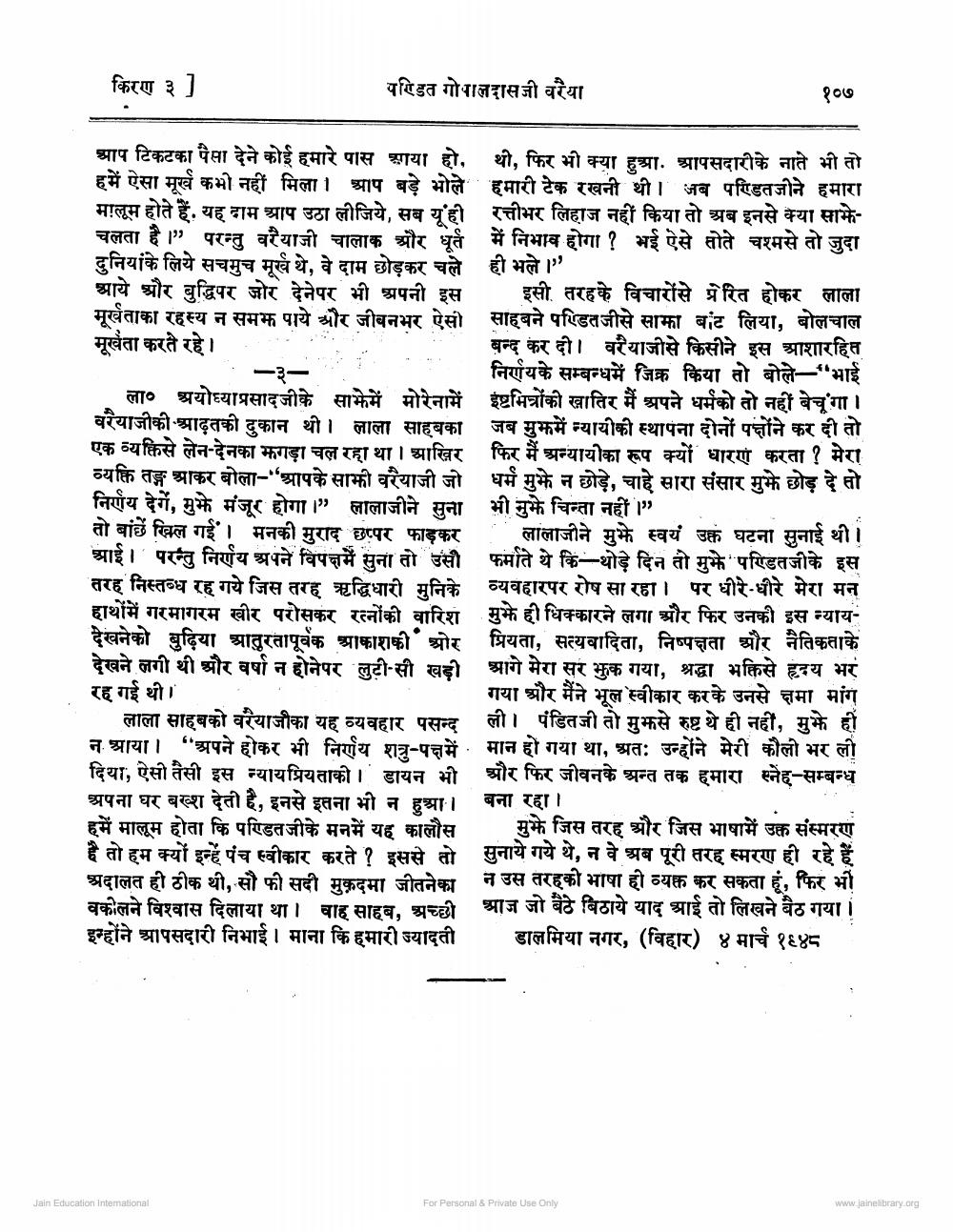________________
किरण ३ ]
आप टिकटका पैसा देने कोई हमारे पास आया हो, हमें ऐसा मूर्ख कभी नहीं मिला । आप बड़े भोले मालूम होते हैं. यह दाम आप उठा लीजिये, सब यूं ही चलता है ।" परन्तु वरैयाजी चालाक और धूर्त दुनियां के लिये सचमुच मूर्ख थे, वे दाम छोड़कर चले आये और बुद्धिपर जोर देनेपर भी अपनी इस मूर्खताका रहस्य न समझ पाये और जीवनभर ऐसी मूर्खता करते रहे।
पण्डित गोपालदासजी वरैया
-३ला० अयोध्याप्रसादजीके साझेमें मोरेनामें वरैयाजीकी आदतकी दुकान थी । लाला साहबका एक व्यक्तिसे लेन-देनका झगड़ा चल रहा था। आखिर व्यक्ति तङ्ग आकर बोला- "आपके साझी वरैयाजी जो निर्णय देगें, मुझे मंजूर होगा ।" लालाजीने सुना तो बांछें खिल गई । मनकी मुराद छप्पर फाड़कर आई । परन्तु निर्णय अपने विपक्ष में सुना तो उसी तरह निस्तब्ध रह गये जिस तरह ऋद्धिधारी मुनिके हाथों में गरमागरम खीर परोसकर रत्नोंकी वारिश देखने को बुढ़िया आतुरतापूर्वक आकाशकी ओर देखने लगी थी और वर्षा न होनेपर लुटी-सी खड़ी रह गई थी।
लाला साहबको वरैयाजीका यह व्यवहार पसन्द न आया । " अपने होकर भी निर्णय शत्रु पक्ष में दिया, ऐसी तैसी इस न्यायप्रियताको । डायन भी अपना घर बख्श देती है, इनसे इतना भी न हुआ । हमें मालूम होता कि पण्डितजीके मन में यह कालौस है तो हम क्यों इन्हें पंच स्वीकार करते ? इससे तो अदालत ही ठीक थी, सौ फीसदी मुक़दमा जीतनेका वकीलने विश्वास दिलाया था। वाह साहब, अच्छी इन्होंने श्रपसदारी निभाई। माना कि हमारी ज्यादती
Jain Education International
१०७
थी, फिर भी क्या हुआ. आपसदारीके नाते भी तो हमारी टेक रखनी थी। जब पण्डितजीने हमारा रत्तीभर लिहाज नहीं किया तो अब इनसे क्या सामें निभाव होगा ? भई ऐसे तोते चश्मसे तो जुदा ही भले ।"
इसी तरह के विचारोंसे प्रेरित होकर लाला साहबने पण्डितजीसे साझा बांट लिया, बोलचाल बन्द कर दी । वरैयाजीसे किसीने इस आशारहित निर्णय के सम्बन्धमें जिक्र किया तो बोले- " भाई इष्टमित्रोंकी खातिर मैं अपने धर्मको तो नहीं बेचूंगा । जब मुझमें न्यायीकी स्थापना दोनों पक्षोंने कर दी तो फिर मैं अन्यायीका रूप क्यों धारण करता ? मेरा धर्मं मुझे न छोड़े, चाहे सारा संसार मुझे छोड़ दे तो भी मुझे चिन्ता नहीं ।"
लालाजीने मुझे स्वयं उक्त घटना सुनाई थी। फर्माते थे कि -थोड़े दिन तो मुझे पण्डितजीके इस व्यवहारपर रोष सा रहा । पर धीरे-धीरे मेरा मन मुझे ही धिक्कारने लगा और फिर उनकी इस न्यायप्रियता, सत्यवादिता, निष्पक्षता और नैतिकता के आगे मेरा सर झुक गया, श्रद्धा भक्तिसे हृदय भर गया और मैंने भूल स्वीकार करके उनसे क्षमा मांग ली । पंडितजी तो मुझसे रुष्ट थे ही नहीं, मुझे ही मान हो गया था, अतः उन्होंने मेरी कौलो भर ली और फिर जीवनके अन्त तक हमारा स्नेह-सम्बन्ध बना रहा ।
मुझे जिस तरह और जिस भाषामें उक्त संस्मरण सुनाये गये थे, न वे अब पूरी तरह स्मरण ही रहे हैं न उस तरह की भाषा ही व्यक्त कर सकता हूं, फिर भी आज जो बैठे बिठाये याद आई तो लिखने बैठ गया । डालमियानगर, (विहार) ४ मार्च १६४८
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org