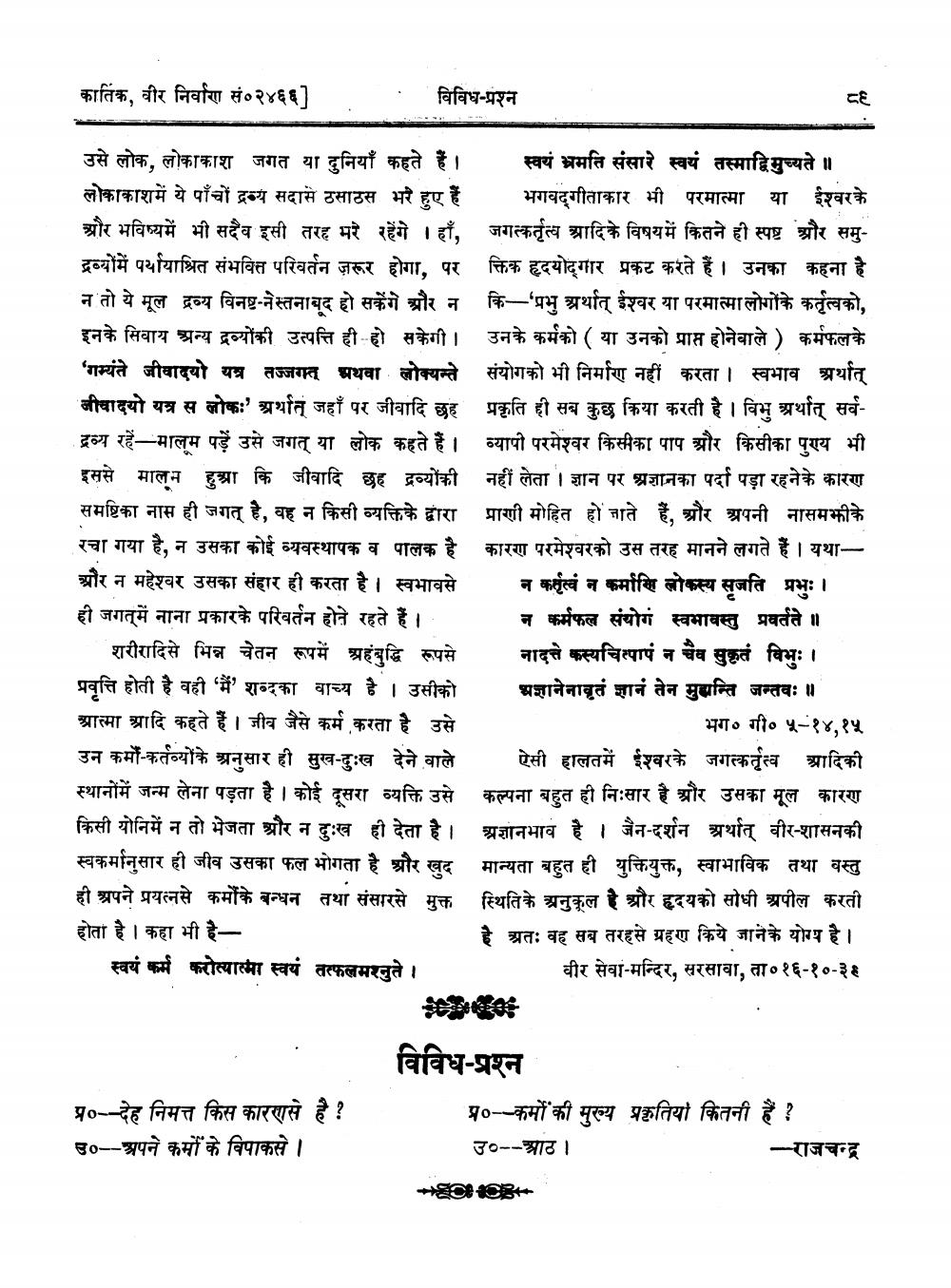________________ कार्तिक, वीर निर्वाण सं०२४६६] विविध प्रश्न दह - उसे लोक, लोकाकाश जगत या दुनियाँ कहते हैं। स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद्विमुच्यते // लोकाकाशमें ये पाँचों द्रन्य सदासे ठसाठस भरे हुए हैं भगवद्गीताकार भी परमात्मा या ईश्वरके और भविष्यमें भी सदैव इसी तरह मरे रहेंगे / हाँ, जगत्कर्तृत्व आदिके विषय में कितने ही स्पष्ट और समुद्रव्यों में पर्यायाश्रित संभवित परिवर्तन जरूर होगा. पर क्तिक हृदयोद्गार प्रकट करते हैं। उनका कहना है न तो ये मूल द्रव्य विनष्ट-नेस्तनाबूद हो सकेंगे और न कि-'प्रभु अर्थात् ईश्वर या परमात्मालोगोंके कर्तृत्वको, इनके सिवाय अन्य द्रव्योंकी उत्पत्ति ही हो सकेगी। उनके कर्मको ( या उनको प्राप्त होनेवाले ) कर्मफलके 'गम्यंते जीवादयो यत्र तज्जगत् अथवा लोक्यन्ते संयोगको भी निर्माण नहीं करता। स्वभाव अर्थात् जीवादयो यत्र स लोका' अर्थात् जहाँ पर जीवादि छह प्रकृति ही सब कुछ किया करती है / विभु अर्थात् सर्वद्रव्य रहे—मालूम पड़ें उसे जगत् या लोक कहते हैं। व्यापी परमेश्वर किसीका पाप और किसीका पुण्य भी इससे मालन हुअा कि जीवादि छह द्रव्योंकी नहीं लेता / ज्ञान पर अज्ञानका पर्दा पड़ा रहनेके कारण समष्टिका नास ही जगत् है, वह न किसी व्यक्तिके द्वारा प्राणी मोहित हो जाते हैं, और अपनी नासमझीके रचा गया है, न उसका कोई व्यवस्थापक व पालक है कारण परमेश्वरको उस तरह मानने लगते हैं / यथा और न महेश्वर उसका संहार ही करता है। स्वभावसे न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः / ही जगत्में नाना प्रकारके परिवर्तन होते रहते हैं। न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते // शरीरादिसे भिन्न चेतन रूपमें अहंबुद्धि रूपसे नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः / प्रवृत्ति होती है वही 'मैं' शब्दका वाच्य है / उसीको अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः // आत्मा आदि कहते हैं / जीव जैसे कर्म करता है उसे भग० गी० 5-14,15 उन कर्मों-कर्तव्योंके अनुसार ही सुख-दुःख देने वाले ऐसी हालतमें ईश्वरके जगत्कर्तृत्व आदिकी स्थानोंमें जन्म लेना पड़ता है / कोई दूसरा व्यक्ति उसे कल्पना बहुत ही निःसार है और उसका मूल कारण किसी योनिमें न तो भेजता और न दुःख ही देता है। अज्ञानभाव है / जैन-दर्शन अर्थात् वीर-शासनकी स्वकर्मानुसार ही जीव उसका फल भोगता है और खुद मान्यता बहुत ही युक्तियुक्त, स्वाभाविक तथा वस्तु ही अपने प्रयत्नसे कोंके बन्धन तथा संसारसे मुक्त स्थिति के अनुकूल है और हृदयको सोधी अपील करती होता है / कहा भी है है अतः वह सब तरहसे ग्रहण किये जानेके योग्य है। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमरनुते / वीर सेवा-मन्दिर, सरसावा, ता०१६-१०-३६ प्रo--देह निमत्त किस कारणसे है ? उ०--अपने कर्मों के विपाकसे / विविध-प्रश्न प्र०--कर्मों की मुख्य प्रकृतियो कितनी हैं ? उ०--आठ। -राजचन्द्र