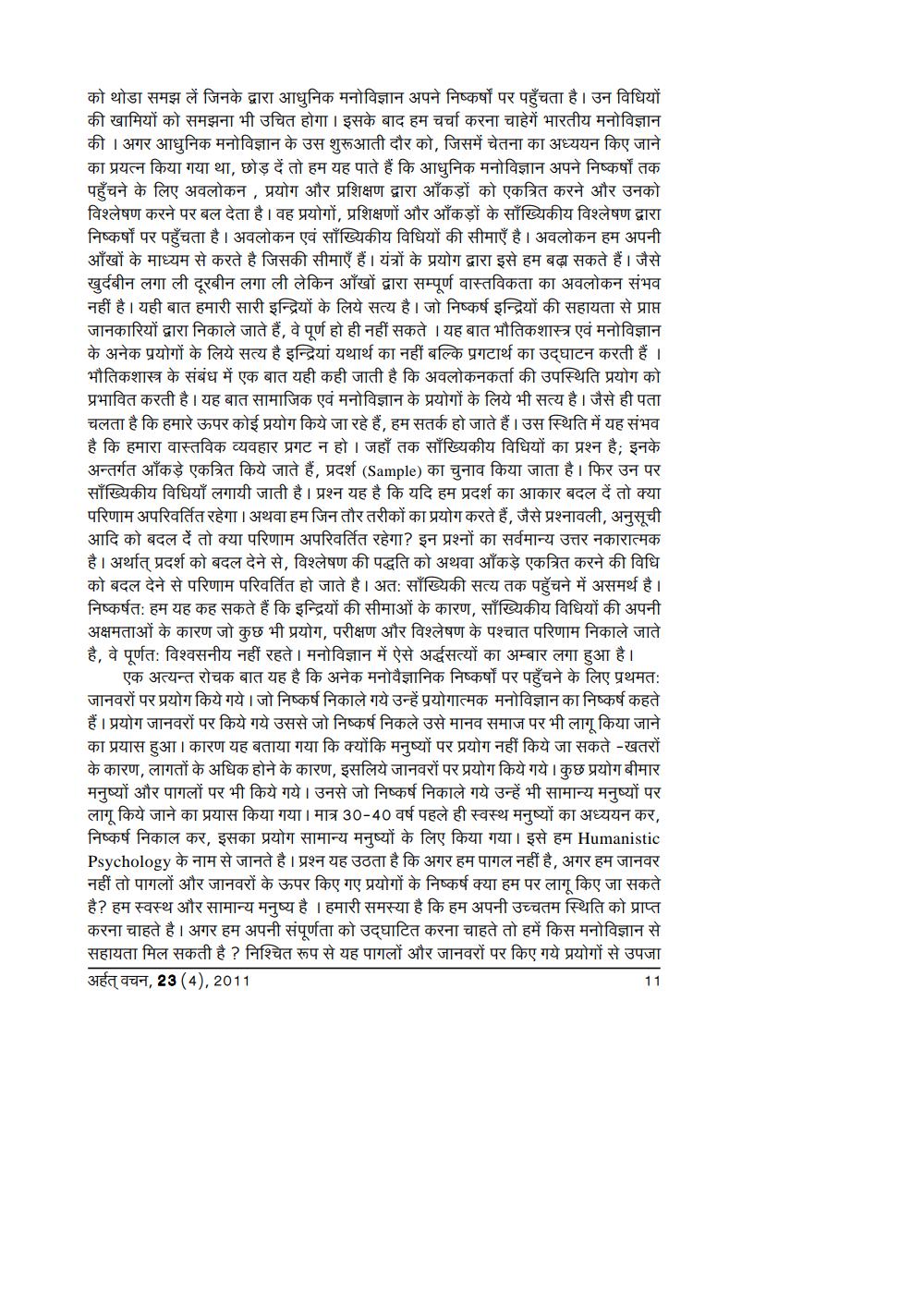________________
को थोडा समझ लें जिनके द्वारा आधुनिक मनोविज्ञान अपने निष्कर्षों पर पहुँचता है। उन विधियों की खामियों को समझना भी उचित होगा। इसके बाद हम चर्चा करना चाहेगें भारतीय मनोविज्ञान की । अगर आधुनिक मनोविज्ञान के उस शुरूआती दौर को, जिसमें चेतना का अध्ययन किए जाने का प्रयत्न किया गया था, छोड़ दें तो हम यह पाते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान अपने निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए अवलोकन , प्रयोग और प्रशिक्षण द्वारा आँकड़ों को एकत्रित करने और उनको विश्लेषण करने पर बल देता है। वह प्रयोगों, प्रशिक्षणों और आँकड़ों के साँख्यिकीय विश्लेषण द्वारा निष्कर्षों पर पहुँचता है। अवलोकन एवं सांख्यिकीय विधियों की सीमाएँ है। अवलोकन हम अपनी आँखों के माध्यम से करते है जिसकी सीमाएँ हैं। यंत्रों के प्रयोग द्वारा इसे हम बढ़ा सकते हैं। जैसे खुर्दबीन लगा ली दूरबीन लगा ली लेकिन आँखों द्वारा सम्पूर्ण वास्तविकता का अवलोकन संभव नहीं है। यही बात हमारी सारी इन्द्रियों के लिये सत्य है। जो निष्कर्ष इन्द्रियों की सहायता से प्राप्त जानकारियों द्वारा निकाले जाते हैं, वे पूर्ण हो ही नहीं सकते । यह बात भौतिकशास्त्र एवं मनोविज्ञान के अनेक प्रयोगों के लिये सत्य है इन्द्रियां यथार्थ का नहीं बल्कि प्रगटार्थ का उद्घाटन करती हैं । भौतिकशास्त्र के संबंध में एक बात यही कही जाती है कि अवलोकनकर्ता की उपस्थिति प्रयोग को प्रभावित करती है। यह बात सामाजिक एवं मनोविज्ञान के प्रयोगों के लिये भी सत्य है। जैसे ही पता चलता है कि हमारे ऊपर कोई प्रयोग किये जा रहे हैं, हम सतर्क हो जाते हैं। उस स्थिति में यह संभव है कि हमारा वास्तविक व्यवहार प्रगट न हो । जहाँ तक साँख्यिकीय विधियों का प्रश्न है; इनके अन्तर्गत आँकड़े एकत्रित किये जाते हैं, प्रदर्श (Sample) का चुनाव किया जाता है। फिर उन पर साँख्यिकीय विधियाँ लगायी जाती है। प्रश्न यह है कि यदि हम प्रदर्श का आकार बदल दें तो क्या परिणाम अपरिवर्तित रहेगा। अथवा हम जिन तौर तरीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रश्नावली, अनुसूची आदि को बदल दें तो क्या परिणाम अपरिवर्तित रहेगा? इन प्रश्नों का सर्वमान्य उत्तर नकारात्मक है। अर्थात् प्रदर्श को बदल देने से, विश्लेषण की पद्धति को अथवा आँकड़े एकत्रित करने की विधि को बदल देने से परिणाम परिवर्तित हो जाते है। अत: साँख्यिकी सत्य तक पहुँचने में असमर्थ है। निष्कर्षत: हम यह कह सकते हैं कि इन्द्रियों की सीमाओं के कारण, साँख्यिकीय विधियों की अपनी अक्षमताओं के कारण जो कुछ भी प्रयोग, परीक्षण और विश्लेषण के पश्चात परिणाम निकाले जाते है, वे पूर्णत: विश्वसनीय नहीं रहते। मनोविज्ञान में ऐसे अर्द्धसत्यों का अम्बार लगा हुआ है।
एक अत्यन्त रोचक बात यह है कि अनेक मनोवैज्ञानिक निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए प्रथमत: जानवरों पर प्रयोग किये गये। जो निष्कर्ष निकाले गये उन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का निष्कर्ष कहते हैं। प्रयोग जानवरों पर किये गये उससे जो निष्कर्ष निकले उसे मानव समाज पर भी लागू किया जाने का प्रयास हुआ। कारण यह बताया गया कि क्योंकि मनुष्यों पर प्रयोग नहीं किये जा सकते -खतरों के कारण, लागतों के अधिक होने के कारण, इसलिये जानवरों पर प्रयोग किये गये। कुछ प्रयोग बीमार मनुष्यों और पागलों पर भी किये गये। उनसे जो निष्कर्ष निकाले गये उन्हें भी सामान्य मनुष्यों पर लागू किये जाने का प्रयास किया गया। मात्र 30-40 वर्ष पहले ही स्वस्थ मनुष्यों का अध्ययन कर, निष्कर्ष निकाल कर, इसका प्रयोग सामान्य मनुष्यों के लिए किया गया। इसे हम Humanistic Psychology के नाम से जानते है । प्रश्न यह उठता है कि अगर हम पागल नहीं है, अगर हम जानवर नहीं तो पागलों और जानवरों के ऊपर किए गए प्रयोगों के निष्कर्ष क्या हम पर लागू किए जा सकते है? हम स्वस्थ और सामान्य मनुष्य है । हमारी समस्या है कि हम अपनी उच्चतम स्थिति को प्राप्त करना चाहते है। अगर हम अपनी संपूर्णता को उद्घाटित करना चाहते तो हमें किस मनोविज्ञान से सहायता मिल सकती है ? निश्चित रूप से यह पागलों और जानवरों पर किए गये प्रयोगों से उपजा अर्हत् वचन, 23 (4), 2011